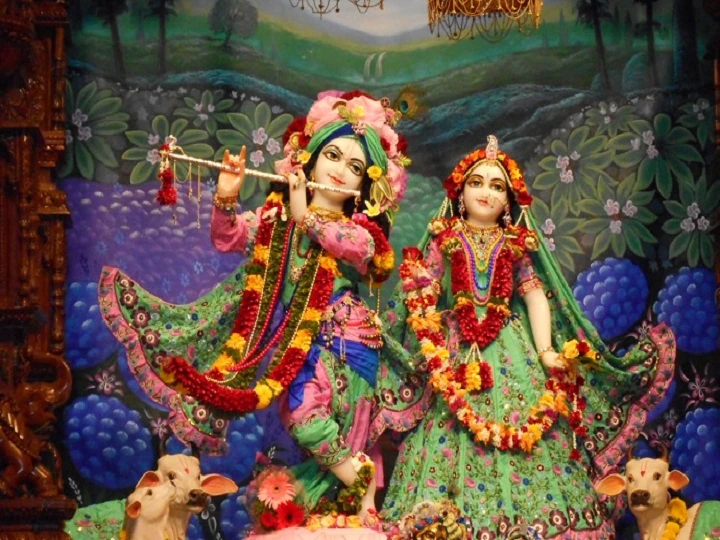।। Shrimadbhagwad Geeta ।। A Practical Approach ।।
।। श्रीमद्भगवत गीता ।। एक व्यवहारिक सोच ।।
।। Chapter 18.67 II
।। अध्याय 18.67 II
॥ श्रीमद्भगवद्गीता ॥ 18.67॥
इदं ते नातपस्काय नाभक्ताय कदाचन ।
न चाशुश्रूषवे वाच्यं न च मां योऽभ्यसूयति॥
“idaḿ te nātapaskāya,
nābhaktāya kadācana..।
na cāśuśrūṣave vācyaḿ,
na ca māḿ yo ‘bhyasūyati”..।।
भावार्थ:
तुझे यह गीत रूप रहस्यमय उपदेश किसी भी काल में न तो तपरहित मनुष्य से कहना चाहिए, न भक्ति-(वेद, शास्त्र और परमेश्वर तथा महात्मा और गुरुजनों में श्रद्धा, प्रेम और पूज्य भाव का नाम ‘भक्ति’ है।)-रहित से और न बिना सुनने की इच्छा वाले से ही कहना चाहिए तथा जो मुझमें दोषदृष्टि रखता है, उससे तो कभी भी नहीं कहना चाहिए ॥६७॥
Meaning:
This what has been taught to you, should never be taught to one without penance, one who is not a devotee, one without service, and to one who has an objection to me.
Explanation:
In India, scriptural knowledge has always been handed down from the teacher to the student. There are rules with regards to how a teacher should be selected, how a student should be selected, what the teaching method should look like. We cannot read a serious text like we read a magazine or a newspaper, nor can we expect an undergraduate student of arts to solve a PhD level differential equation. Therefore, a serious study of the Gita should also follow certain guidelines and rules. Here, Shri Krishna enumerates these rules.
The vast majority of people may be eligible for karm yog, and it would be a great folly for them to prematurely take karm sanyās. It is better to instruct them to fulfil their bodily dharma and practice devotion alongside. That is why, in this verse Shree Krishna says that this confidential teaching given by him is not for everyone. Before sharing it with others, we should check their eligibility for this teaching. By giving transcendental instructions to those who are faithless and averse to God, we cause them to become offenders.
The Gita should not be taught to one who has not undergone a certain degree of penance or austerity. He should be willing to bear some physical discomfort while attending a discourse, for instance. It is clear that one who wants to visit the bar every night and follow it with a visit to the club will not gain any benefit from the Gita. A certain level of detachment from the material world is required. Secondly, the Gita should not be taught to someone who is not a devotee. If the student does not harbour respect for the guru, the teacher, he does not have the requisite level of humility to undertake spiritual inquiry.
The word shushrushaa has two meanings. It refers to one who has an attitude of service towards the world, instead of a highly selfish outlook. It also refers to one who is fond of listening to discourses. The Gita should not be taught to one who is highly selfish, nor to one who is not interested in listening to any kind of discourse. Finally, the Gita should not be taught to anyone who has objection to the notion that there is Ishvara, there is something beyond the material world. The Gita is not meant for purely materialistic individuals who are content with their existence.
।। हिंदी समीक्षा ।।
प्राय अध्यात्मशास्त्र के समस्त ग्रन्थों के अन्तिम भाग में शास्त्र संप्रदाय की विधि अर्थात् ज्ञान के अधिकारी का वर्णन किया जाता है। इसी महान् परम्परा का अनुसरण करते हुए, इस श्लोक में, भगवान् श्रीकृष्ण बताते हैं कि यह ज्ञान किसे नहीं देना चाहिए। इसी के द्वारा यहाँ इसका भी बोध कराया गया है कि ज्ञान के योग्य अधिकारी में कौन से गुण होने चाहिए। यहाँ उल्लिखित गुणों के अध्ययन से ज्ञात होगा कि साधक के आन्तरिक व्यक्तित्व के सुगठन के लिए इन गुणों का होना आवश्यक है। साधन सम्पन्न साधक ही इस ज्ञान का ग्रहण, धारण एवं स्मरण करने में समर्थ होता है। वही इस ज्ञानानन्द का अनुभव एवं अर्जन करके उसे अपने जीवन में प्रकट कर सकता है।
अधिकांश लोग कर्म योग के लिए पात्र हो सकते हैं और उनके लिए समय से पहले कर्म संन्यास लेना एक बड़ी मूर्खता होगी। उन्हें अपने शारीरिक धर्म को पूरा करने और साथ ही भक्ति का अभ्यास करने का निर्देश देना बेहतर है। इसीलिए, इस श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं कि उनके द्वारा दी गई यह गोपनीय शिक्षा सभी के लिए नहीं है। इसे दूसरों के साथ साझा करने से पहले, हमें इस शिक्षा के लिए उनकी पात्रता की जांच करनी चाहिए। जो लोग श्रद्धाहीन और ईश्वर से विमुख हैं, उन्हें दिव्य शिक्षा देकर हम उन्हें अपराधी बना देते हैं।
यह ज्ञान ऐसे पुरुष को नहीं देना चाहिए जो
(1) तपरहित है शरीर, वाणी और मन का संयम ही तप है जिसके द्वारा हम समस्त शक्तियों का संचय कर सकते हैं। संयमरूपी तप से रहित पुरुष में इस ज्ञान को ग्रहण करने की मानसिक और बौद्धिक क्षमता ही नहीं होती। इसलिए, तप रहित व्यक्ति से ज्ञान नहीं कहना चाहिए, क्योंकि इससे उस व्यक्ति को कोई लाभ नहीं होगा। इस कथन में रंचमात्र भी पूर्वाग्रह और दुराग्रह नहीं है। यह कथन इसी प्रकार का है कि, कृपया चट्टानों पर बीजारोपण मत करो। कारण यह है कि कृषक को इससे कोई फसल प्राप्त नहीं होगी।
(2) जो अभक्त है तपयुक्त हो किन्तु भक्त न हो, तो उस पुरुष से भी यह ज्ञान नहीं कहना चाहिए। जो साधक अपने लक्ष्य के साथ तादात्म्य नहीं कर सकते, उससे प्रेम नहीं कर सकते, वे इस ज्ञान के अधिकारी नहीं हैं। प्रेम के अभाव में त्याग और उत्साह संभव नहीं है। प्रेमालिंगन में अपने आदर्श को बांध लेना ही भक्ति है।
(3) जो अशुश्रुषु (सेवा में अतत्पर) है यदि कोई पुरुष तपस्वी और भक्त है, परन्तु गुरुसेवा और जनसेवा करने में संकोच करता है, तो वह भी योग्य विद्यार्थी नहीं कहा जा सकता। भगवान् श्रीकृष्ण ने सम्पूर्ण गीता में निस्वार्थ सेवा पर विशेष बल दिया है, क्योंकि चित्तशुद्धि का वही सर्वश्रेष्ठ साधन है। स्वार्थी लोग कभी भी इस ज्ञान को ग्रहण नहीं कर पाते हैं और न ही उसके आनन्द का अनुभव कर सकते हैं।
(4) जो मुझे से असूया अर्थात् मुझ में दोष देखता है गुणों में दोष देखना असूया है, जो लोग ईश्वर, गुरु और शास्त्रप्रमाण में भी दोष देखते हैं, वे किस प्रकार आत्मज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं मुझसे असूया का अर्थ परमात्मा से असूया है। उसी प्रकार, तत्त्वज्ञान का अनादर करने वाले लोग भी अभ्यसूयक कहलाते हैं। बल प्रयोग के द्वारा कराये गये धर्म परिवर्तन से उस मत के अनुयायियों का संख्याबल तो बढ़ाया जा सकता है। परन्तु, ऐसे प्रयोग से आत्मविकास नहीं कराया जा सकता। किसी के भी ऊपर धर्म को नहीं थोपना चाहिए। यदि तत्त्वज्ञान के प्रति मन में तिरस्कार का भाव है, तो बुद्धि से उसे समझने पर भी हम उसे अपने जीवन में कार्यान्वित नहीं कर सकते हैं। इसलिए, असूया युक्त पुरुष इस ज्ञान का अधिकारी नहीं है। इस प्रकार के श्लोकों का प्रयोजन साधकों को साधन मार्ग दर्शाना होता है।
अथपित्ति से यह निश्चय होता है कि यह शास्त्र भगवान् में भक्ति रखनेवाले, तपस्वी, शुश्रूषायुक्त और दोषदृष्टिरहित पुरुष को ही सुनाना चाहिये। अन्य स्मृतियों में मेधावीको या तपस्वी को, इस प्रकार इन दोनों का विकल्प देखा जाता है।
गीता के अध्ययन से तत्काल ही किसी लाभ की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। रातोरात व्यक्तित्व का सुगठन नहीं किया जा सकता। गीता इस प्रकार के चमत्कार का आश्वासन नहीं देती। इस श्लोक का अभिप्राय यह हुआ कि तप, भक्ति, सेवाभाव और आदर से युक्त पुरुष ही आत्मज्ञान का उत्तम अधिकारी है। यदि हम शास्त्र के अध्ययन से अधिक लाभान्वित नहीं होते हैं, तो, निश्चय ही हममें किसी आवश्यक गुण का अभाव होना चाहिए। उस स्थिति में आत्मनिरीक्षण के द्वारा हम आत्मशोधन करें। जैसे, दर्पण पर जमी धूल को स्वच्छ कर देने से प्रतिबिम्ब स्पष्ट दिखाई देता है, उसी प्रकार अन्तकरण के शुद्ध और स्थिर होने पर आत्मानुभव स्पष्ट होता है।
गीता के अध्ययन के स्मरण एवम समर्पण की आवश्यकता है। मुख्य बात यही है कि आज के युग मे व्यक्ति अपने दैनिक क्रिया कलापो में इतना व्यस्त एवम अहंकार युक्त है कि उसे यही लगता है जो वह करता है एवम जानता है वही सर्वश्रेष्ठ है। उस के पास गीता जैसे महान ग्रंथ का अध्ययन तक करने का समय नही, तो उस का चिंतन एवम मनन का प्रश्न ही नही है। कुरुक्षेत्र में अर्जुन को छोड़ कर किसी को गीता का ज्ञान नही दिया गया। गीता ही विश्व का एक मात्र ग्रन्थ है जिस का संसार की हर भाषा मे अनुवाद हुआ है। इसे समझने के लिये ही आज के युग मे हमारे जैसे अल्प ज्ञानी लोगो को कम से कम तीन-चार बार पढ़ना पड़ता है, जब कि हर बार इस का नया अर्थ समझ मे आता है।
बल प्रयोग के द्वारा कराये गये धर्म परिवर्तन से उस मत के अनुयायियों का संख्याबल तो बढ़ाया जा सकता है, परन्तु, ऐसे प्रयोग से आत्मविकास नहीं कराया जा सकता। किसी के भी ऊपर धर्म को नहीं थोपना चाहिए। यदि तत्त्वज्ञान के प्रति मन में तिरस्कार का भाव है, तो बुद्धि से उसे समझने पर भी हम उसे अपने जीवन में कार्यान्वित नहीं कर सकते हैं।
श्रीमद्भगवद् गीता का यह प्रभाव है कि जो प्रचार करेगा, उससे बढ़कर मेरा प्यारा कोई नहीं होगा, यह बात भगवान् आगे को दो श्लोकों में बताते हैं।
।। हरि ॐ तत सत ।। गीता – 18.67 ।।
Complied by: CA R K Ganeriwala (+91 9422310075)