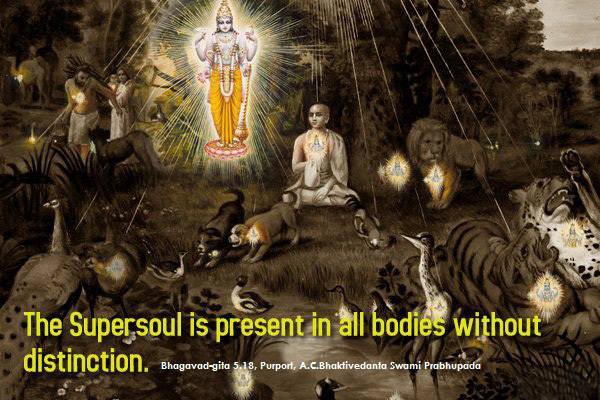।। Shrimadbhagwad Geeta ।। A Practical Approach ।।
।। श्रीमद्भगवत गीता ।। एक व्यवहारिक सोच ।।
।। Chapter 18.57 II
।। अध्याय 18.57 II
॥ श्रीमद्भगवद्गीता ॥ 18.57॥
चेतसा सर्वकर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः।
बुद्धियोगमुपाश्रित्य मच्चित्तः सततं भव॥
“cetasā sarva- karmāṇi,
mayi sannyasya mat- paraḥ..।
buddhi- yogam upāśritya,
mac- cittaḥ satataḿ bhava”..।।
भावार्थ:
सब कर्मों को मन से मुझ में अर्पण कर के (गीता अध्याय 9 श्लोक 27 में जिस की विधि कही है) तथा समबुद्धि रूप योग को अवलंबन कर के मेरे परायण और निरंतर मुझ में चित्तवाला हो ॥५७॥
Meaning:
Mentally surrender all actions to me, designate me as the supreme goal, fix your mind on me by depending upon the yoga of intellect.
Explanation:
Shri Krishna summarizes karma yoga and bhakti yoga in this shloka. As we saw in the previous shloka, we need to continue performing our duty, and not to worry too much if we inadvertently perform a prohibited action, and to consider Ishvara as the one and only one aashraya, the ultimate refuge.
Yog means “union,” and buddhi yog means “having the intellect united with God.” This union of the intellect occurs when it is firmly convinced that everything in existence has emanated from God, is connected to him, and is meant for his satisfaction.
Within our body is the subtle antaḥ karaṇ, which we also refer to colloquially as the heart, or the etheric heart. It has four aspects to it. When it creates thoughts, we call it mana, or mind. When it analyses and decides, we call it buddhi, or intellect. When it gets attached to an object or person, we call it chitta. When it identifies with the attributes of the body and becomes proud, we call it ahankār, or ego.
In this internal machinery, the position of the intellect is dominant. It makes decision, while the mind desires in accordance with those decisions, and the chitta gets attached to the objects of affection.
Throughout the day, we humans control our mind with the intellect. Thus, we must cultivate the intellect with proper knowledge and use it to guide the mind in the proper direction. This is what Shree Krishna means by buddhi yog—developing a resolute decision of the intellect that all work and all things are meant for the pleasure of God. For such a person of resolute intellect, the chitta easily gets attached to God.
How does this actually work in practice? A step-by-step approach towards karma yoga and bhakti yoga is enumerated in this shloka for the convenience of the seeker.
First, the seeker should fix Ishvara as his ultimate goal. This is mat paraha, one who is completely oriented towards Ishvara. Next, such a seeker should surrender all his actions to Ishvara. In the ninth chapter, Shri Krishna had said – whatever you do, whatever you consume, whatever you offer or donate, and whatever penance you perform, submit it to me. This is sarvakarmaani sanyasya. Nothing is done for selfish ends such as wealth, power, position, vanity and so on. All is done for Ishvara only.
Now, when the seeker faces challenges in life, he needs to have a method to deal with them. Equanimity is the answer. All actions are performed with full awareness and knowledge, as an offering to Ishvara. No action is performed haphazardly. Once the action is complete, the seeker should neither be attached to success, nor to failure. Such an attitude will only develop as a result of accepting every object, person or situation encountered in life as a gift or a praasada from Ishvara. This is buddhi yoga, as described in the second chapter.
।। हिंदी समीक्षा ।।
अपने उपदेश के उपसंहार में भगवान श्री कृष्ण निर्देश देते हुए अर्जुन को अंत मे कुछ वचन कहते है, जिन्हें हम आगे कुछ श्लोक में पढ़ते है।
भगवान श्री कृष्ण कहते है कि तू दृष्ट और अदृष्ट फलवाले समस्त कर्मों को विवेक बुद्धि से अर्थात् बतलाये हुए भाव से, मुझ ईश्वर में समर्पण कर के तथा मेरे परायण होकर अर्थात् मैं वासुदेव ही जिस का पर,( परमगति ) हूँ ऐसा होकर, मुझ में बुद्धि को स्थिर करते हुए बुद्धियोग का आश्रय लेकर, बुद्धियोग के अनन्यशरण होकर, निरन्तर मुझ में चित्तवाला हो अर्थात् जिस का निरन्तर मुझ में ही चित्त रहे, ऐसा हो। यही नित्य कर्म सन्यास होगा। अपना चित्त सदा आत्मविवेक में रखने से तुम मेरे स्वरूप और प्रकृति के भेद को समझ पाओगे। प्रकृति भी आत्मतत्व से शरीर और छाया की भांति जुड़ी है, इसलिए आत्मतत्व से जुड़ने से प्रकृति का अवसान हो जाता है और जो शेष रहता है, वह आत्मतत्व वासुदेव परमात्मा ही रहता है।
मन से अर्थात् ज्ञानपूर्वक समस्त कर्मों का संन्यास मुझ में करो। इस वाक्य का अर्थ है कर्मों में कर्तृत्वाभिमान और फलासक्ति का त्याग कर के केवल ईश्वरार्पण की भावना से कर्म करो। चित्त से कर्मों को अर्पित करने का तात्पर्य है कि मनुष्य चित्त से यह दृढ़ता से मान ले कि मन, बुद्धि, इन्द्रियाँ, शरीर आदि और संसार के व्यक्ति, पदार्थ, घटना, परिस्थिति आदि सब भगवान् के ही हैं। भगवान् ही इन सब के मालिक हैं। इन में से कोई भी चीज किसी की व्यक्तिगत नहीं है। केवल इन वस्तुओंका सदुपयोग करनेके लिये ही भगवान् ने व्यक्तिगत अधिकार दिया है। हर कार्य का कर्ता भगवान ही है और वह केवल कठपुतली की भांति भगवान के द्वारा निर्देशित कार्य कर रहा है। कर्म सन्यास का अर्थ कर्म त्याग नही है, अपितु कर्म के फलों को त्याग कर परमात्मा को समर्पित एवम अकर्ता भाव से कर्म करना ही कर्म सन्यास है।
योग का अर्थ है “मिलन”, और बुद्धि योग का अर्थ है “बुद्धि का ईश्वर के साथ एकाकार होना।” बुद्धि का यह मिलन तब होता है जब यह दृढ़ विश्वास हो जाता है कि अस्तित्व में मौजूद हर चीज़ ईश्वर से निकली है, उससे जुड़ी हुई है और उसकी संतुष्टि के लिए है। हमारे शरीर के भीतर सूक्ष्म अन्तः कारण है, जिसे हम बोलचाल की भाषा में हृदय या ईथरिक हृदय भी कहते हैं। इसके चार पहलू हैं। जब यह विचार बनाता है, तो हम इसे मन कहते हैं। जब यह विश्लेषण करता है और निर्णय लेता है, तो हम इसे बुद्धि कहते हैं। जब यह किसी वस्तु या व्यक्ति से जुड़ जाता है, तो हम इसे चित्त कहते हैं। जब यह शरीर के गुणों से तादात्म्य स्थापित कर लेता है और गर्वित हो जाता है, तो हम इसे अहंकार कहते हैं।
इस आंतरिक तंत्र में बुद्धि की स्थिति प्रमुख है। यह निर्णय लेती है, जबकि मन उन निर्णयों के अनुसार इच्छा करता है, और चित्त स्नेह की वस्तुओं से जुड़ जाता है।
दिन भर हम मनुष्य अपनी बुद्धि से अपने मन को नियंत्रित करते हैं। इसलिए हमें बुद्धि को उचित ज्ञान से विकसित करना चाहिए और इसका उपयोग मन को उचित दिशा में ले जाने के लिए करना चाहिए। श्री कृष्ण बुद्धि योग से यही अभिप्राय रखते हैं – बुद्धि का दृढ़ निश्चय विकसित करना कि सभी कार्य और सभी चीजें भगवान की प्रसन्नता के लिए हैं। दृढ़ बुद्धि वाले ऐसे व्यक्ति का चित्त आसानी से भगवान से जुड़ जाता है।
मत्पर भव जिस पुरुष के लिए मैं अर्थात् परमात्मा ही परम लक्ष्य है, वह पुरुष मत्पर कहा जाता है। ईश्वर को ही जीवन का लक्ष्य समझे बिना हम में ईश्वरार्पण की भावना नहीं आ सकती। इसलिए, भगवान् श्रीकृष्ण अर्जुन को ईश्वर परायण होने का उपदेश देते हैं।
इंद्रियों और मन पर बुद्धि का नियंत्रण है, इसलिए कर्म मन द्वारा बुद्धि से किए जाते है। अहंकार बुद्धि का लक्षण है। इसलिए कहा गया है कि समस्त कार्यो को करते हुए इंद्रियाओ एवम मन पर बुद्धि का नियंत्रण रहे एवम सिद्धि-असिद्धि में, सुख-दुख में, लाभ-हानि में, संसार के हर प्राणी, वस्तु एवम परिस्थितियो में समबुद्धि भाव से स्थितप्रज्ञ हो कर कर्म करना ही बुद्धियोग है। इसलिये ईश्वर के प्रति समर्पित भाव बुद्धियोग हो, भगवान को ही अपना परम हितेषी, प्राप्य, परमगति, परमाधार मानते हुए उस है हर विधान में संतुष्ट रहना ही मत्पर हो कर ईश्वर की शरणागति है।
मानसिक जीवन का यह नियम है कि जैसा हम चिन्तन करते हैं, वैसे ही हम बनते हैं। इस नियमानुसार जो भक्त सतत कृष्ण तत्त्व का चिन्तन करता है वह स्वयं श्रीकृष्ण परमात्मा स्वरूप बन जाता है। यही अव्यय आत्मस्वरूप है।
व्यवहार में हम सामाजिक मनुष्य होने के नाते समाज में पढ़ाई लिखाई करते हुए, नौकरी या व्यवसाय करते है और शादी करते हुए परिवार का पालन करते है। नौकरी या व्यवसाय में उच्च पद की आकांक्षा और स्वास्थ्य, सुंदर और समझदार जीवन साथी, ऐश्वर्य और धन की लालसा में जीवन व्यतीत हो जाता है। इस का कारण हमारी मन और बुद्धि पर राग – द्वेष का अधिकरण हो जाता है और हमारी भावना स्वार्थ के साथ कार्य करती है। इसलिए जो मन के अनुकूल हो वह सही और जो मन के विपरीत हो तो दुख लगता है। कर्मयोग में बुद्धि के शुद्ध होने पर यदि हम परमात्मा में चित्त लगा दे, हमारा प्रत्येक कार्य उस को समर्पित हो एवं जो भी फल की प्राप्ति हो तो, वह उस का प्रसाद माने तो हमारी भावना, राग – द्वेष, लोभ, स्वार्थ और कामनाएं परमात्मा के परायण हो जाती है। यही बुद्धि योग है। एक सेवक ही भांति अपने स्वामी के कार्य को करना ही बुद्धि युक्त कर्म योग है। जिस में फल पर ध्यान नहीं रखते हुए, कार्य को कुशलता पूर्वक करने पर ध्यान रहे, जिस से स्वामी प्रसन्न हो। यही परमात्मा के प्रति निस्वार्थ समर्पण होगा और हमारे कार्य भी परमात्मा के कार्य होंगे। मनुष्य को दुख और सुख का अनुभव तभी होता है जब वह स्वयं को कर्ता और भोक्ता मानता है। जब वह कर्ता और भोक्ता भाव से मुक्त हो कर परमात्मा की पराभक्ति में समस्त कर्म करता है तो वह कर्म फलों के बंधन से भी मुक्त हो कर परमात्मा के लीन भी होने लगता है।
यदि कोई मनुष्य भगवान् के इस उपदेश को अस्वीकार करता है, तो उस की क्या गति होगी, पढ़ते है।
।। हरि ॐ तत सत ।। गीता – 18.57 ।।
Complied by: CA R K Ganeriwala (+91 9422310075)