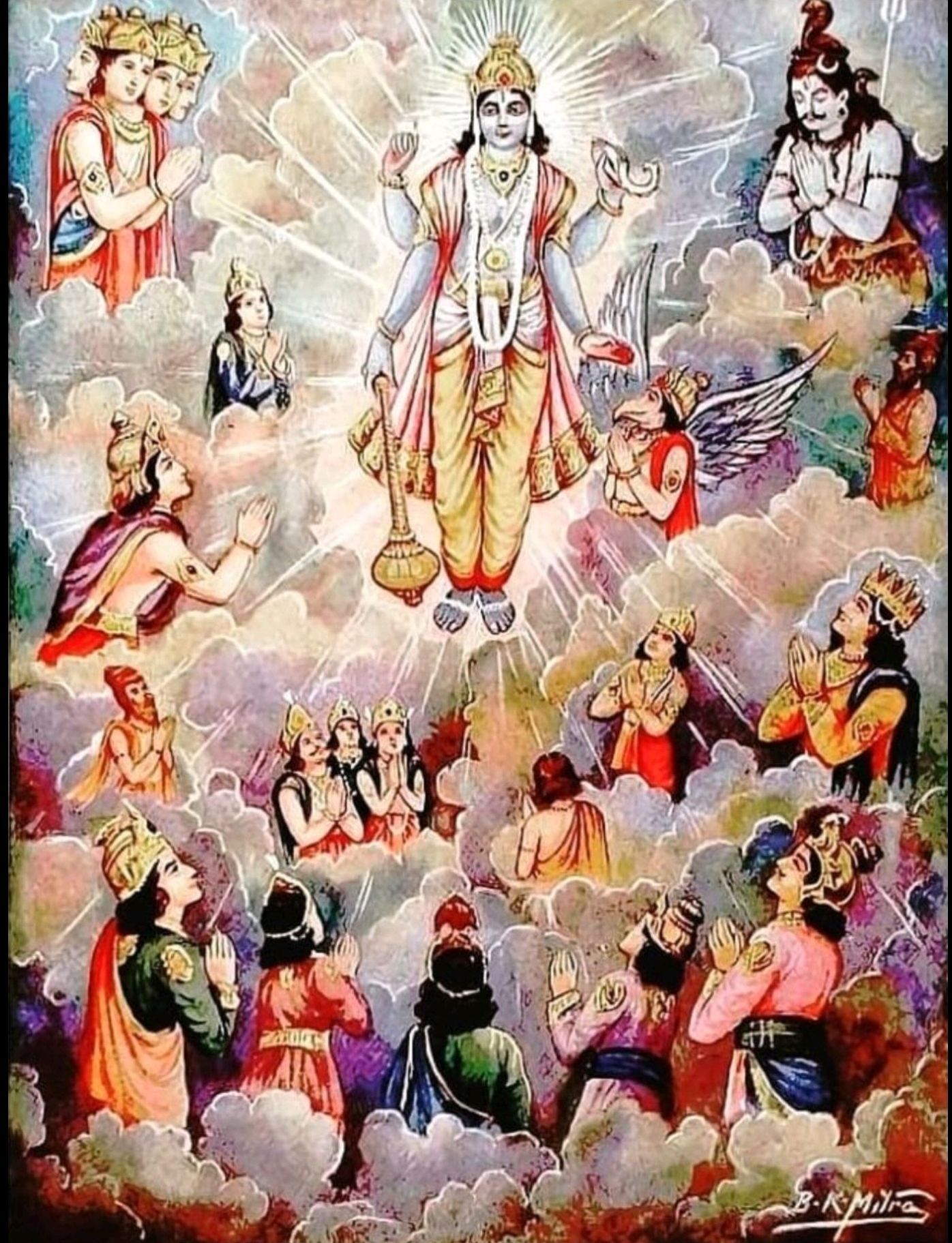।। Shrimadbhagwad Geeta ।। A Practical Approach ।।
।। श्रीमद्भगवत गीता ।। एक व्यवहारिक सोच ।।
।। Chapter 18.48 II
।। अध्याय 18.48 II
॥ श्रीमद्भगवद्गीता ॥ 18.48॥
सहजं कर्म कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत्।
*सर्वारम्भा हि दोषेण धूमेनाग्निरिवावृताः॥”
“saha-jaḿ karma kaunteya,
sa-doṣam api na tyajet..।
sarvārambhā hi doṣeṇa,
dhūmenāgnir ivāvṛtāḥ”..।।
भावार्थ:
अतएव हे कुन्तीपुत्र! दोषयुक्त होने पर भी सहज कर्म (प्रकृति के अनुसार शास्त्र विधि से नियत किए हुए वर्णाश्रम के धर्म और सामान्य धर्मरूप स्वाभाविक कर्म हैं उनको ही यहाँ स्वधर्म, सहज कर्म, स्वकर्म, नियत कर्म, स्वभावज कर्म, स्वभावनियत कर्म इत्यादि नामों से कहा है) को नहीं त्यागना चाहिए, क्योंकि धूएँ से अग्नि की भाँति सभी कर्म किसी-न-किसी दोष से युक्त हैं। ॥४८॥
Meaning:
Natural duty, even though fraught with defect, should not be abandoned. For, all undertakings are covered with defect, like fire by smoke.
Explanation:
Some people in this world are perfectionists. Either we know such people as friends or co-workers, or we may be one ourselves. Perfectionism is a recipe for constant sorrow, because no matter who performs the actions, they will never be perfect. As we have seen earlier, an action is based on several factors, including the mental state of the performer, the instruments used, the state of the outside world and so on. It is next to impossible to expect all these factors to line up in such a manner that the action and its result will be perfect.
Shri Krishna says, the profession can be chosen based on our own svabhāva or inclination, aptitude or it can be based on the heredity also. And Lord Krishna points out that whatever profession you choose, learn to enjoy that; have commitment, never compare your profession with another’s, because ultimately any type of profession has got its own plus points and minus points. We have an expression: occupational hazard. Occupational hazard means whatever occupation you take, you will have problems.
There is no perfect profession at all; it is your attitude which makes any profession enjoyable; there is no enjoyable profession. It is a mind which makes the mind enjoyable; and if the mind does not have the skill of enjoying; any profession will become dull; and therefore, change your attitude. This is the uniqueness of vedic tradition. They never ask you to change the set up.
And the minimum points every profession has is boredom. boredom is a natural consequence one has to find out one’s own method of fighting boredom and the only method is innovation of one’s own profession; whether it is mechanical or skilled profession, we have to find out our own method of creativity and innovation.
But the benefits of the swa-dharma far outweigh its defects. And the foremost benefit is that it provides a comfortable and natural path for one’s purification and elevation.
So, materialism talks about successful change of the surrounding; vēda talks about the successful change of the attitude, so that you can be contended with any set up that you are in.
Shri Krishna says that any undertaking, any project, any action will always have some imperfection built into it, just like any fire will have some smoke covering it. So there is no point giving up our actions and our duties because they contain some imperfection or the other. Even the human body, the most intricate organism on this earth, has some minor defect in one form or the other, in the form of ill health or deformity and so on. Therefore, we have to accept this fact and continue to perform our best actions, not focus too much on the result.
With this shloka, the topic of karma yoga is concluded. If we recall, this topic was prompted by Arjuna in the beginning of this chapter, when he wanted to know the difference between sanyaasa and tyaaga. Tyaaga was redefined by Shri Krishna to mean karma yoga, and was analysed in great detail. Tyaaga or karma yoga, combined with bhakti, is a process, is a means to get us to a destination. When practised properly, it lifts us from our materialistic life and places us on the path towards liberation. So then, if tyaaga is the means, what is the goal? This is taken up next.
।। हिंदी समीक्षा ।।
ज्ञान, कर्म, कर्ता, बुद्धि, धृति के साथ प्रकृति सत-रज-तम गुणों के अनुसार प्रत्येक जीव के नियत कर्म को निर्धारित करती है। यही सहज कर्म कहे गए है। कर्म प्रकृति की ही क्रिया है क्योंकि जीव साक्षी एवम अकर्ता ही है। अतः कोई भी कर्म निर्दोष नही हो सकता। भगवान श्री कृष्ण कहते है कि अपने वर्ण धर्म के अनुसार जो भी कर्म है उसे ही करना चाहिए चाहे वह दोषयुक्त भी क्यों न हो।
श्री कृष्ण कहते हैं, पेशे का चुनाव हमारे अपने स्वभाव या झुकाव, योग्यता के आधार पर किया जा सकता है या यह आनुवंशिकता के आधार पर भी हो सकता है। और भगवान कृष्ण बताते हैं कि आप जो भी पेशा चुनें, उसका आनंद लेना सीखें; प्रतिबद्धता रखें, अपने पेशे की तुलना कभी दूसरे के पेशे से न करें, क्योंकि आखिरकार हर तरह के पेशे के अपने प्लस पॉइंट और माइनस पॉइंट होते हैं। हमारे पास एक मुहावरा है: व्यावसायिक खतरा। व्यावसायिक खतरा का मतलब है कि आप जो भी पेशा चुनें, आपको समस्याएँ होंगी।
और हर पेशे में न्यूनतम बिंदु बोरियत है। बोरियत एक स्वाभाविक परिणाम है, किसी को बोरियत से लड़ने का अपना तरीका खोजना होगा और एकमात्र तरीका अपने पेशे का नवाचार है; चाहे वह यांत्रिक या कुशल पेशा हो, हमें रचनात्मकता और नवाचार की अपनी विधि ढूंढनी होगी।
लेकिन स्वधर्म के लाभ इसके दोषों से कहीं अधिक हैं। और सबसे बड़ा लाभ यह है कि यह व्यक्ति की शुद्धि और उन्नति के लिए एक सहज और स्वाभाविक मार्ग प्रदान करता है।
व्यवहार में हम यह मान ले कि परिस्थितियों और वातावरण के अनुसार हम जिस भी कर्म क्षेत्र को धारण कर लेते है, वह हमारी प्रकृति के अनुरूप होता है, इसलिए कोई व्यापारी, सैनिक, राजनेता, Dr., CA, वकील या संवाददाता आदि बनता है। उस के कर्मक्षेत्र के अनुरूप उस के समक्ष कार्य भी आते है, जैसे कोई मांस विक्रेता हो तो उस का कार्य दिन भर मांस तो तैयार करने और बेचने में रहेगा। जैसे अग्नि में धुएं का समावेश है, वैसे ही प्रत्येक कार्य में कष्ट और असुविधाएं भी और कठोर निर्णय का समय भी आता है। ऐसे समय व्यक्ति अपना कर्म क्षेत्र छोड़ कर दूसरे कर्म क्षेत्र को सरल या अधिक लाभदायक समझ कर करे तो वह असफल और असहज होगा। जैसे सैनिक युद्ध के समय दूसरी नौकरी की बात करे। Dr. इलाज करते हुए, असफल होने पर व्यवसाय की सोचे। भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी, कालाबजारी आदि के वातावरण में अपने क्लाइंट के हित के बारे में कार्य करना, कष्टदायक या अरुचिकर भले ही हो, किंतु सहज कर्म होने से सरल होता है। वकील को झूठ भी बोलना पड़ता है, यह उस का कार्य ही है। किंतु इस के लिए यदि कार्य क्षेत्र ही बदलते रहे तो कर्मफलों से मुक्ति भी नही मिलेगी। किसी भी व्यक्ति का कर्मक्षेत्र और कार्य प्रकृति उस के कर्मफलों के अनुसार होती है, इसलिए रुचिकर या अरुचिकर कार्य भी उसी के अनुसार होते है।
इसलिए स्वाभाविक कर्म सदोष होने के बावजूद जब निष्काम भाव से किया जाता है तो वह वासनाओं का क्षय करता ही है। इस को अग्नि में धूम्र की उपस्थिति से तुलना की गई है कि कोई भी अग्नि धूम्र रहित नही होती, किन्तु प्रज्वलित होने के बाद धूम्र से मुक्त हो जाती है, वैसे ही कर्म सदोष हो किन्तु निष्काम भाव से करने से दोषमुक्त ही करता है।
प्रत्येक व्यक्ति का जन्म अपनी पूर्वार्जित वासनाओं के साथ ही होता है। अत सहज कर्म से तात्पर्य उन वासनाओं से है जिन के साथ मनुष्य का जन्म होता है। भगवान् श्रीकृष्ण का यह कथन है कि उन कर्मों को नहीं त्यागना चाहिए, जो मनुष्य की सहज अर्थात् स्वाभाविक वासनाओं से प्रेरित होते हैं, परन्तु उन्होंने यह नहीं कहा कि जिस दूषित वातावरण में मनुष्य का जन्म होता है उस वातावरण के दोषयुक्त कर्मो को उसे करना चाहिए।
दो प्रकार की शक्तियां हमारे कर्मों को प्रेरित और नियमित, सीमित और निश्चित करती हैं (1) आन्तरिक मानसिक स्वभाविक से उत्पन्न होने वाली प्रवृत्तियाँ तथा (2) बाह्य वातावरण तथा विषयों से उत्पन्न होने वाली नये नये प्रलोभन। मनुष्य को अपनी स्वाभाविक वासनाओं के सदोष होने पर भी उनका अनुसरण करना चाहिए, परन्तु उसी समय, उस में बाह्य प्रलोभनों का त्याग करने का साहस और क्षमता होनी चाहिए।
जिन संस्कारों के साथ हमारा जन्म हुआ है, उसके अनुसार हम को कर्म करने चाहिए। परन्तु स्मरण रहे कि ये कर्म निरहंकार और निस्वार्थ भाव से ही किये जाने चाहिए। बाह्य जगत् के प्रलोभन हमारे प्रलोभन को दूषित नहीं कर सकें, इस की हमें सावधानी रखनी चाहिए। इस तथ्य पर भगवान् श्रीकृष्ण विशेष बल देते हैं। गीता के अनुसार, मनुष्य परिस्थितियों का स्वामी है, दास नहीं। जिस मात्रा में मनुष्य अपने स्वामित्व को दृढ़तापूर्वक व्यक्त कर पायेगा, उसी मात्रा में उसका विकास संभव होगा।क्या सभी कर्म दोष से आवृत नहीं हैं भगवान् श्रीकृष्ण का युक्तिवाद यह है कि जब सभी कर्म दोषयुक्त हैं, तो स्वकर्म का त्याग कर परधर्म का आचरण क्यों करना चाहिए यह सर्वथा अनुपयुक्त है। दूसरी बात यह है कि अहंकार पूर्वक कर्म करने पर ही वे बन्धन कारक होते हैं अन्यथा नहीं। अत साधक को निरहंकार भाव से सहज कर्म का पालन करना चाहिए। इस तथ्य को यहाँ आरम्भ शब्द से इंगित किया गया है।
कोई भी पेशा पूर्ण रूप से सामान्य नहीं होता; ये होता है आपका नजरिया जो किसी को भी आनंद देता है; कोई भी पेशा आनंददायक नहीं होता। ऐसा होता है जो मन को आनंद देता है; और अगर मन में आनंद लेने का कौशल नहीं है, तो कोई भी पेशा नीरस हो जाएगा; और इसलिए अपना दृष्टिकोण छोटा। यह वैदिक परंपरा की विशेषता है। वे कभी-कभी आपसे व्यवस्था के लिए कुछ नहीं कहते हैं।
कोई भी पेशा पूर्ण रूप से परिपूर्ण नहीं होता; यह आपका दृष्टिकोण होता है जो किसी भी पेशे को आनंददायक बनाता है; कोई भी पेशा आनंददायक नहीं होता। यह मन होता है जो मन को आनंददायक बनाता है; और अगर मन में आनंद लेने का कौशल नहीं है, तो कोई भी पेशा नीरस हो जाएगा; और इसलिए अपना दृष्टिकोण बदलें। यह वैदिक परंपरा की विशिष्टता है। वे कभी भी आपको व्यवस्था बदलने के लिए नहीं कहते हैं
इस के पूर्व, हम आरम्भ शब्द का वास्तविक अर्थ देख चुके हैं कि कर्तृत्वाभिमान रहित कर्म। कर्तृत्व का अभिमान ही वासनाओं को उत्पन्न कर के कर्म को दोषयुक्त बना देता है।अज्ञान अवस्था में यह दोष अपरिहार्य है, जैसे अग्नि के साथ धूम्र। परन्तु यदि चूल्हे को बाहर खुले वातावरण में रखा जाये, तो धुंआ नष्ट हो जाता है और अग्नि प्रज्वलित हो उठती है। इसी प्रकार, ईश्वर का स्मरण करके निरहंकार भाव से जगत् कर्म करने पर अहंकार के अभाव में वासनाओं का आवरण नष्ट होकर स्वयं का शुद्ध चैतन्य स्वरूप स्पष्ट अनुभव होता है।
सामाजिक दृष्टिकोण से लोकसंग्रह एवम सृष्टि को चलायमान रखने के कोई भी कार्य छोटा या बड़ा नही होता। समाज के धारण एवम पोषण के लिये ब्राह्मण से ले कर शुद्र तक सभी समान रूप से ज्ञान-विज्ञान युक्त पुरुष अर्थात शूरवीर, किसान, वैश्य, रोजगार, लुहार, बढई, कुम्हार एवम मांस विक्रेता व्याध सभी आवश्यक है। सभी अपनी योग्यता के अनुसार समाज मे योगदान देते है। ब्राह्मण युद्ध नहीं कर सकता और क्षत्रिय व्यापार। वैश्य लुहार का कार्य नही कर सकता। सभी सन्यासी हो जाये तो भला देश, समाज, सृष्टि किस प्रकार कार्य कर सकती है। लोकसंग्रह ही कर्मयोग का धैय है, जिस से समाज एवम व्यक्ति उन्नत हो।
मोक्ष सन्यास मार्ग में ही है यह सत्य नहीं है। मनुष्य की लघुता-महता उस के व्यवसाय पर निर्भर नहीं है, किन्तु जिस बुद्धि से वह अपना व्यवसाय या कर्म करता है, उसी बुद्धि पर उस की योग्यता अध्यात्म दृष्टि से अवलंबित रहती है। जिस का मन शांत है, और जिस ने सब प्राणियों के अंतर्गत एकता को पहचान लिया है, वह मनुष्य जाति या व्यवसाय से व्यापारी हो, चाहे कसाई; निष्काम बुद्धि से उक्त व्यवसाय करने वाला वह मनुष्य स्नान संध्याशील ब्राह्मण अथवा शूरवीर क्षत्रिय के बराबर ही माननीय एवम मोक्ष का अधिकारी है।
किसी भी कार्य में सफलता की बात करे तो भौतिकवाद अपने आस-पास के वातावरण में सफल परिवर्तन की बात करता है। वेद आप के अपने दृष्टिकोण में सफल परिवर्तन की बात करता है, ताकि आप जिस भी स्थिति में हों, उससे संतुष्ट रह सकें।
अतः “सहजम” विश्लेषण का अर्थ है वर्ण, आश्रम, स्वभाव और परिस्थितियों के अनुसार जो स्वधर्म, स्वकर्म, नियत कर्म, स्वाभाविक कर्म प्रकृति किसी जीव के लिए नियत करती है, उसे कर्तव्य भाव से सात्विक स्वरूप मे अपनी पूर्ण दक्षता के साथ निष्काम होकर करना । फिर उस में कोई दोष भी हो, तो उस का पाप या दोष करने वाले को नही लगता।
अर्जुन के प्रथम अध्याय में मोह से उत्पन्न सन्यास भाव में भगवान द्वारा स्पष्टता पूर्वक उसे युद्ध करने के यह उत्तर, तर्क की दृष्टि से दिया गया है। अर्जुन सहित पाड़व योद्धा बने किंतु अपनो से युद्ध करने की कोई इच्छा नहीं रखते थे। प्रकृति ने उन्हें युद्ध भूमि में खड़ा कर दिया, क्योंकि युद्ध का परित्याग वे पहले भी कर सकते थे, किंतु वह नही हुआ। इस युद्ध में जो भी जन – धन की हानि होगी, अपनो और परायो की हत्या भी होती है, तो भी उस का पाप नही लगता। इसलिए युद्ध भूमि से क्षत्रिय यदि युद्ध नही करता है, तो उस का कर्म का वेग असहज भाव से उस मन, बुद्धि और सांसारिक जीवन में अशांति ही पैदा करेगा। जिस के कारण उस का अंतिम धैर्य मोक्ष की ओर बढ़ना संभव नही होगा।
त्याग का विस्तृत विवरण के बाद सांख्य योग में सन्यास का वर्णन आगे पढ़ते है।
।। हरि ॐ तत सत।। गीता – 18.48 ।।
Complied by: CA R K Ganeriwala (+91 9422310075)