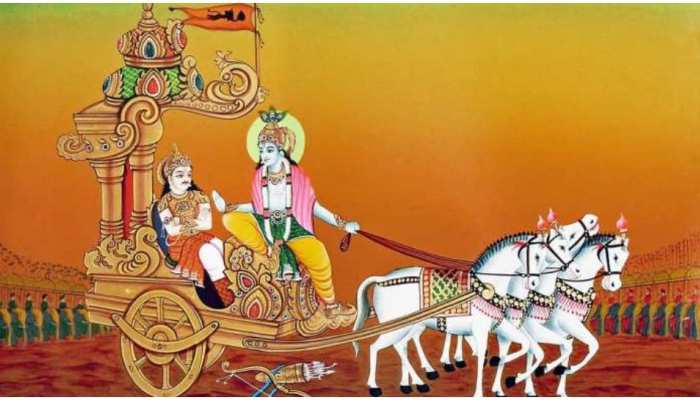।। Shrimadbhagwad Geeta ।। A Practical Approach ।।
।। श्रीमद्भगवत गीता ।। एक व्यवहारिक सोच ।।
।। Chapter 18.36-37 II
।। अध्याय 18.36-37 II
॥ श्रीमद्भगवद्गीता ॥ 18.36-37॥
सुखं त्विदानीं त्रिविधं श्रृणु मे भरतर्षभ।
अभ्यासाद्रमते यत्र दुःखान्तं च निगच्छति॥36।।
यत्तदग्रे विषमिव परिणामेऽमृतोपमम्।
तत्सुखं सात्त्विकं प्रोक्तमात्मबुद्धिप्रसादजम्॥37।।
“sukhaḿ tv idānīḿ tri-vidhaḿ,
śṛṇu me bharatarṣabha..।
abhyāsād ramate yatra,
duḥkhāntaḿ ca nigacchati”..।।36।।
“yat tad agre viṣam iva,
pariṇāme ‘mṛtopamam..।
tat sukhaḿ sāttvikaḿ proktam,
ātma- buddhi- prasāda- jam”..।।37।।
भावार्थ:
हे भरतश्रेष्ठ! अब तीन प्रकार के सुख को भी तू मुझसे सुन। जिस सुख में साधक मनुष्य भजन, ध्यान और सेवादि के अभ्यास से रमण करता है और जिससे दुःखों के अंत को प्राप्त हो जाता है, जो ऐसा सुख है, वह आरंभकाल में यद्यपि विष के तुल्य प्रतीत (जैसे खेल में आसक्ति वाले बालक को विद्या का अभ्यास मूढ़ता के कारण प्रथम विष के तुल्य भासता है वैसे ही विषयों में आसक्ति वाले पुरुष को भगवद्भजन, ध्यान, सेवा आदि साधनाओं का अभ्यास मर्म न जानने के कारण प्रथम ‘विष के तुल्य प्रतीत होता’ है) होता है, परन्तु परिणाम में अमृत के तुल्य है, इसलिए वह परमात्मविषयक बुद्धि के प्रसाद से उत्पन्न होने वाला सुख सात्त्विक कहा गया है ॥३६-३७॥
Meaning:
Now, listen also to the three types of joy from me, O foremost among Bharatas, in which one enjoys its practice and attains the end of sorrow. That which is like poison initially, but is like nectar in its result, that joy is said to be saattvic, born of one’s mental purity.
Explanation:
we all know every human instinctively craves for happiness. Our craving for happiness is not a learned desire, it is an instinctive desire. Everybody wants happiness; but there is a choice with regard to the type of happiness, an intelligent person chooses the right brand of happiness. Happiness is relative terms, a thing which is boring for you is given happiness to other. A thing which you avoid in beginning as useless, by age and circumstance may convert into a great thing for your happiness. Happiness also has three classifications i.e. Satvik, Rajsic and Tamasi.
At the end of the day, the end goal of any endeavour or action is to eliminate some type of sorrow, whether it is in the short term to remove hunger, or it is in the long term to prevent financial instability in our family. The lifecycle of an action begins with Vaasanaas.
These Vaasanaas or deep-rooted impressions create thoughts, some of these thoughts become desires, and consequently, desires become actions. When the action is complete and the target of the action is attained, the desire subsides, and the mind is free of desires for a split second. This stillness of the mind results in joy.
Shri Krishna says that even this joy obtained as the result of an action is in the realm of Prakrirti. Any by-product of an action is in the realm of Prakriti since actions themselves are in Prakriti. So therefore, this joy can also be classified into three types, which are saattvic, raajasic and taamasic. This also mean that the type of joy obtained is closely related to the knowledge, doer and action behind obtaining that joy. A taamasic action will not result in saattvic joy.
But Krishna gives a warning, it is a great ānadā. But you have to work hard to gain it. It is not easily attainable; you have to go through a long winding spiritual sādhanā, start with karma yōga; which is nothing but reduction of sakāma karma and increase of niṣkāma karma.This spiritual joy or the spiritual path appears to be poison in the beginning, poison means painful in the beginning, because it involves discipline and any person who has succeeded in any field; it is because of hard work done by him. But at the end of it; it is like amrutham or nectar, once you have started seeing the benefit which is born out of sādanā catuṣṭaya sampathi – first stage, sādanā catuṣṭaya sampathi will itself give an ānandā; later the atmānandā, that ānandā is called sātvic pleasure. Therefore, An intelligent person chooses sātvic ānandā.
When sādhanā catuṣṭaya sampathi is developed, there is an ānandā. And the beauty is that ānanda comes from inside; he does not seem to derive ānandā from external sources. This person only knows what is the unique inner ānandā; and the height of this ānandā is ātma-jñāna-janya-ānandā; which is called vidya ānandā; ānandā born out of sheer knowledge of my nature; the sheer knowledge of the nature of the world. And the glory of that ānandā is, knowledge is never subject to loss.
The Indian gooseberry (āmlā) is one of those super-foods that are very beneficial for health. It has the Vitamin C of more than 10 oranges. But children dislike it, since it has a bitter taste. Parents in North India encourage children to eat it, saying: āmle kā khāyā aur baḍoṅ kā kahā, bād meṅ patā chalatā hai [v20.1] “The benefits of both these—eating of āmlā and the advice of the elders—are experienced in the future.” Interestingly, after eating the āmlā, in just a couple of minutes, the bitter taste disappears, and sweetness is experienced. And the long-term benefits of consuming the natural Vitamin C are undoubtedly numerous. In the above verse, Shree Krishna says that happiness in the mode of goodness is of the same nature; it seems bitter in the short run, but it tastes like nectar in the end.
Shri Krishna also adds that the complete end of sorrow is only obtained through saattvic joy. This is because the other two types of joy, raajasic and taamasic, are mixed and impure respectively. They either have a tinge of sattva, or none at all. Furthermore, saattvic joy is such that having tasted it even a little bit, one becomes so attracted to it that one delights in performing actions that result in sattvic joy. That is why, saattvic joy is described in detail in the next shloka.
Most of us dread going to the doctor’s office for a vaccination. Some of us will try to postpone, or even cancel, an upcoming vaccination. What causes such fear? It is just a little bit of a pinch, that too for a few seconds, caused by the needle of the syringe. Fear is also caused by the anticipation of this pain. But we all know that any vaccination is given to us for our own long-term benefit. It will prevent us from catching all kinds of diseases that can cripple us or even kill us.
So therefore, the reward for bearing pain is extremely beneficial to us. Shri Krishna says that sattvic joy is similar, in that when we first begin to experience it, it is quite unpleasant, but in the end, it is as pleasant as nectar. No spiritual path is easy to take up in the beginning. In karma yoga, one has to work selflessly, chipping away at the ego. The leap of faith needed for bhakti is difficult for people who have grown up doubting everything. Jnyaana yoga requires a high degree of awareness, whereas most of us lead automated robotic lives where someone else has done out thinking for us.
All of these practices have their goal as the purification of the mind, and of removing its three main doshas or faults: mala or selfish desire, vikshepa or lack of focus, and avarana or ignorance. Unless these three faults are diminished to a great extent, we will be unable to comprehend the nature of sattvic joy. This is unlike any joy we know so far, because it does not depend on any external factors such as objects, people or situations. It comes from inside, from the intellect that has turned inward towards the self.
।। हिंदी समीक्षा ।।
इस अध्याय में प्रतिपादित विचारों के विकास क्रम में सर्वप्रथम कार्य सम्पादन के तीन तत्त्वों ज्ञान, कर्ता और कर्म का वर्णन किया गया है। तत्पश्चात् कर्म के प्रेरक, नियामक और मार्गनिर्देशक दो तत्त्वों, बुद्धि और धृति का विस्तृत विवेचन किया गया है। भगवान् श्रीकृष्ण ने इन सब के त्रिविध भेदों को पृथक्पृथक् रूप से दर्शाया है। प्रत्येक कर्ता अपने कर्मक्षेत्र में, अपने ज्ञान से निर्देशित बुद्धि से शासित और धृति से लक्ष्य को धारण करके कर्म करता है। इस प्रकार कार्य की शारीरिक एवं प्राणिक संरचना का विश्लेषण एवं निरीक्षण पूर्ण होता है।
अब विचार्य विषय है कार्य का मनोविज्ञान। मनुष्य किस लिए कर्म करता है प्राणियों की प्रवृत्तियों का अवलोकन करने से यह ज्ञात होता है कि प्रत्येक प्राणी केवल सुख प्राप्ति के लिए ही कर्म में प्रवृत होता है। गर्भ से लेकर शवागर्त तक प्राणियों के समस्त प्रयत्न सतत सुख प्राप्त करने के लिए ही होते हैं। इस प्रकार, यद्यपि सब का एक लक्ष्य सुख ही है, तथापि ज्ञान, कर्ता, कर्म बुद्धि और धृति में भेद होने से विभिन्न लोगों के द्वारा अपनाये गये सुख प्राप्ति के मार्ग भी भिन्नभिन्न होते हैं। “आत्मनिष्ठ बुद्धि” अर्थात जो सुख की अनुभूति इंद्रियों से न हो कर आत्म अर्थात अपनी बुद्धि से ग्राह्य हो, वह सुख ही अतिंद्रिय अर्थात टिकने वाला होता है। इसलिए योग में सर्व प्रथम इंद्रियों और मन का निग्रह किया जाता है। यही पतंजलि योग में अधिक विस्तार से वर्णित किया गया है। क्योंकि बुद्धि ऐसी इंद्री है जो एक ओर प्रकृति के त्रिगुणात्मक विस्तार को देखती है और दूसरी ओर आत्मस्वरूपी परब्रह्म का बोध भी करती है।
सुख को समझने से पूर्व यह भी जानना आवश्यक है कि सुख क्या है। सुख इन्द्रिय भोग या मन के क्षणिक आनन्द की अनुभूति नही है। क्योंकि यदि यह सत्य है तो सुख के जाने से दुख या पीड़ा का अनुभव होगा। यह मन एवम बुद्धि से गाह्य अनुभूति है जो निरंतर हमे परमानन्द की ओर ले जाती है। इसलिये इस को बताने से पूर्व बुद्धि एवम धृति को भगवान श्री कृष्ण ने बताया।
हम सभी जानते हैं कि हर इंसान सहज रूप से खुशी की चाहत रखता है। खुशी की हमारी चाहत कोई सीखी हुई इच्छा नहीं है, यह एक सहज इच्छा है। हर कोई खुशी चाहता है; लेकिन खुशी के प्रकार के संबंध में एक विकल्प होता है, एक बुद्धिमान व्यक्ति खुशी का सही ब्रांड चुनता है। खुशी सापेक्ष शब्दों में होती है, जो चीज आपको उबाऊ लगती है, वह दूसरों को खुशी देती है। एक चीज जिसे आप शुरू में बेकार समझकर टालते हैं, उम्र और परिस्थिति के कारण आपकी खुशी के लिए एक बड़ी चीज बन सकती है। खुशी के भी तीन वर्गीकरण हैं यानी सात्विक, राजसिक और तामसी।
जब साधना चतुष्टय सम्पत्ती विकसित होती है, तब आनन्द होता है और सुन्दरता यह है कि आनन्द अन्दर से आता है। ऐसा नहीं होता है कि उसे आनन्द बाहरी स्रोतों से मिलता है। यह व्यक्ति केवल यह जानता है कि अद्वितीय आन्तरिक आनन्द क्या है; और इस आनन्द की पराकाष्ठा आत्म-ज्ञानजन्य-आनन्द है; जिसे विद्या आनन्द कहते हैं; आनन्द जो मेरे स्वरूप के विशुद्ध ज्ञान से उत्पन्न होता है; जगत् के स्वरूप के विशुद्ध ज्ञान से और उस आनन्द की महिमा यह है कि ज्ञान कभी नष्ट नहीं होता।
लेकिन कृष्ण चेतावनी देते हैं, यह एक महान आनंद है। लेकिन आपको इसे प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी। यह आसानी से प्राप्त होने योग्य नहीं है; आपको एक लंबी घुमावदार आध्यात्मिक साधना से गुजरना होगा, कर्म योग से शुरू करना होगा; जो कि सकाम कर्म को कम करने और निष्काम कर्म को बढ़ाने के अलावा और कुछ नहीं है। यह आध्यात्मिक आनंद या आध्यात्मिक मार्ग शुरुआत में जहर लगता है, जहर का मतलब है शुरुआत में दर्दनाक, क्योंकि इसमें अनुशासन शामिल है और कोई भी व्यक्ति जिसने किसी भी क्षेत्र में सफलता हासिल की है; यह उसके द्वारा की गई कड़ी मेहनत के कारण है। लेकिन इसके अंत में; यह अमृत की तरह है, एक बार जब आप ना चतुष्टय सम्पति से पैदा हुए लाभ को देखना शुरू कर देते हैं – पहला चरण, साधना चतुष्टय सम्पति अपने आप में आनंद देगा। बाद में आत्मानंद, उस आनंद को सात्विक आनंद कहा जाता है। इसलिए, एक बुद्धिमान व्यक्ति सात्विक आनंद चुनता है।
भारतीय फल आंवला उत्तम आहारों में से एक है जो स्वास्थ्य के लिए अत्यंत लाभकारी है। इसमें दस संतरों से भी अधिक विटामिन-सी होता है। लेकिन बच्चे इसे नापसंद करते हैं क्योंकि इसका स्वाद कड़वा होता है। उत्तर भारत में माता-पिता बच्चों को इसका सेवन करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं और एक ऐसी कहावत भी है-“आंवले का खाया और बड़ों का कहा, बाद में पता चलता है।” अर्थात “आंवले का सेवन और बड़ों का परामर्श” इन दोनों का लाभ भविष्य में ज्ञात होता है। वास्तव में आंवला खाने के कुछ क्षणों के पश्चात उसका कड़वापन समाप्त हो जाता है और मिठास का अनुभव होता है। प्राकृतिक रूप से विटामिन-सी का सेवन करने से निःसंदेह दीर्घ काल तक लाभ प्राप्त होता है। श्रीकृष्ण कहते हैं कि सात्विक सुख भी इसी प्रकृति का होता है जो अल्पकाल के लिए दुःख के रूप में कड़वा लगता है और अंत में सुख के रूप में इसका स्वाद अमृत बन जाता है।
सात्त्विक, राजसिक और तामसिक लोग विविध कर्मों के द्वारा अपने अपने सुख की खोज करते हैं। कर्म के संघटकों में भेद होने के कारण उन विभिन्न प्रकार के कर्मों से प्राप्त सुखों में भेद होना अनिवार्य है। प्रस्तुत प्रकरण में सुख के तीन प्रकारों का वर्गीकरण किया गया है। जिस सुख में रमण करने वाला मनुष्य आध्यात्मिक, आधिदैविक और आतिभौतिक सभी प्रकार के दुखो से मुक्त हो कर सच्चिदानंदघन आनंद की प्राप्ति को प्राप्त करता है, वही सात्विक और वास्तविक सुख है। अभ्यासात् इस अध्याय में वर्णित वर्गीकरण को समझकर एक सच्चे साधक को आत्म निरीक्षण की सार्मथ्य प्राप्त हो जाती है। इस प्रकार, अपने दुखों के कारण को समझने से उनका परित्याग कर वह अपने जीवन को पुर्नव्यवस्थित कर सकता है। ऐसे अभ्यास से उसके दुखों का सर्वथा अन्त हो जाना संभव है।
जो ऐसा सुख है, वह पहले पहल सुख की महिमा सुन कर “अग्रे” हो कर उस को प्राप्त करने की इच्छा से ज्ञान, वैराग्य, शम, दम, तितिक्षा, ध्यान और समाधि के कार्य में लगता है, उसे वह सब आरम्भ काल में, अत्यन्त श्रम साध्य होने के कारण, विष के सदृश दुःखात्मक होता है। परंतु परिणाम में वह ज्ञान वैराग्यादि के परिपाक से उत्पन्न हुआ सुख, अमृत के समान है। वह आत्मबुद्धि के प्रसाद से उत्पन्न हुआ सुख, विद्वानों द्वारा सात्त्विक बतलाया गया है। अपनी बुद्धि का नाम आत्मबुद्धि है, उस का जो जल की भाँति स्वच्छ निर्मल हो जाना है, वह आत्मबुद्धिप्रसाद है, उस से उत्पन्न हुआ सुख आत्मबुद्धि प्रसादजन्य सुख है। अथवा आत्मविषयक या आत्मा को अवलम्बन करनेवाली बुद्धि का नाम आत्मबुद्धि है, उसके प्रसाद की अधिकता से उत्पन्न सुख आत्मबुद्धि प्रसाद से उत्पन्न है, इसीलिये वह सात्त्विक है।
जो प्रथम विष के समान है यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि वास्तव में सात्त्विक सुख कभी विष के समान नहीं होता है, परन्तु मनुष्य की स्वाभाविक प्रवृत्ति बहिर्मुखी होने के कारण उसे ज्ञान, वैराग्य, ध्यान आदि सात्त्विक सुख के साधनों का अभ्यास करने में कठिनाई अनुभव होती है। इसलिए ऐसे दुर्बल व्यक्ति को यह सात्त्विक सुख प्रारम्भ में विष के समान दुखदायी प्रतीत होता है, किन्तु यह वास्तविकता नहीं है। उदाहरणार्थ बालकों को खेलकूद में आसक्ति होने के कारण पाठशाला का अध्ययन दुखदायी प्रतीत होता है। इसी प्रकार किसी भी कार्य को सफलता पूर्वक करने के मन, बुद्धि, शरीर, अनुशासन एवम एकाग्रता की आवश्यकता होती है जिस से हम सांसारिक सुख को छोड़ कर करते है, यही अंत मे परिणाम में अमृत के समान है । परिणाम में अर्थात् जब ज्ञान, वैराग्य आदि साधनाभ्यास में परिपक्वता आने पर वास्तविक मनशान्ति का अनुभव होता है तब वह अमृत के समान आनन्दायक होता है। यह सुख सात्त्विक कहा गया है।
किसी भी लक्ष्य की पूर्ति के लिए दृढ़ संकल्प, अनुशासन, त्याग, परिश्रम, धैर्य और परिश्रम की आवश्यकता होती है। यह सब कार्य मन के विपरीत होने से इंद्रियों एवम मन को कठोरता एवम ज्ञान से साधना पड़ता है, इसलिए यह प्रारंभ में दुखदाई लगता है, किंतु लक्ष्य प्राप्ति के साथ आनंदमय हो जाता है। संसार में जितने भी उच्च पद और शिक्षा और प्रतियोगिता में प्रथम आने के लिए निरंतर अभ्यास, अनुशासन और ज्ञान की आवश्यकता होती है।
आत्म बुद्धि के प्रसाद से उत्पन्न प्राय लोग प्रसाद का अर्थ कर्मकाण्डीय पूजा की सम्पन्नता होने पर वितरित किया जाने वाला भोज्य प्रसाद ही समझते हैं। परन्तु यहाँ प्रसाद का अर्थ व्यापक और गम्भीर है। बुद्धि एक ऐसी इंद्री को कह सकते है जो एक ओर से त्रिगुणात्मक प्रकृति के विस्तार की ओर देखती है, और दूसरी ओर से उस को आत्म स्वरूपी परब्रह का भी बोध हो सकता है, कि जो इस प्रकृति के विस्तार के मूल में अर्थात प्राणी मात्र में समानता से व्याप्त है।
मन एवम इंद्रियाओ से गाह्य सुख प्राकृतिक एवम अस्थायी होगा एवम बुद्धि द्वारा वही सुख एक के लिये सुख दूसरे के दुख भी हो सकता है। मीठा खाना स्वाद के अनुसार सुख है और बुद्धि कर अनुसार दुख भी हो सकता है।
इन्द्रियनिग्रह के द्वारा बुद्धि को त्रिगुणात्मक प्रकृति के विस्तार से हटा कर अंतर्मुख एवम आत्मनिष्ठ क्रिया एवम पातंजल योग से साधना में लगाया जाए तो इस आत्मानुसंधान के द्वारा आत्मस्वरूप में समाहित बुद्धि आत्म बुद्धि कहलाती है। उस बुद्धि के प्रसाद का अर्थ है, प्रसन्नता, निर्मलता। बुद्धि के शान्त, शुद्ध और स्थिर होने पर, जो सुख की अनुभूति होती है, वही आत्मबुद्धि प्रसादज सात्त्विक सुख है। ऐसा सर्वश्रेष्ठ सुख केवल सुशिक्षित, सुसंस्कृत और सात्त्विक पुरुषों को ही प्राप्त होता है।
वेदों में सात्विक सुखों का ‘श्रेय’ के रूप में उल्लेख किया गया है जोकि वर्तमान में दुखद और अंततः लाभकारी होता है। इस के विपरीत ‘प्रेय’ है जो आरम्भ में सुखद लेकिन अंततः हानिकारक होता है। ‘श्रेय’ और ‘प्रेय’ के संबंध में कठोपनिषद् में वर्णन है
अन्यच्छ्रेयोऽन्यदुतैव प्रेयस्ते उभे नानार्थे पुरुषम् सिनीतः। तयोः श्रेय आददानस्य साधु भवति हीयतेऽर्थाद्य उ प्रेयो वृणीते ।।
श्रेयश्च प्रेयश्च मनुष्यमेतस्तौ सम्परीत्य विविनक्ति धीरः। श्रेयो हि धीरोऽभि प्रेयसो वृणीते प्रेयो मन्दो योगक्षेमाद् वृणीते ।। (कठोपनिषद्-1.2.1-2)
“दो प्रकार के मार्ग होते हैं-एक लाभप्रद और दूसरा सुखद। ये दोनों मनुष्य को विभिन्न दिशा की ओर ले जाते हैं। सुखद प्रारम्भ में आनन्द प्रदान करता है लेकिन इसका अंत पीड़ादायक होता है। अज्ञानी लोग सुख और विनाश के पाश में बंधते हैं लेकिन बुद्धिमान आकर्षण के धोखे में नहीं आते और लाभप्रद का चयन करते हैं और अंततः सुख प्राप्त करते हैं।
यह स्पष्ट है कि सुख बुद्धि गाह्य ही है अतः सात्विक बुद्धि द्वारा गाह्य सुख सात्विक होगा। आगे हम राजसी सुख को पढ़ते है।
।। हरि ॐ तत सत ।। गीता – 18.36-37।।
Complied by: CA R K Ganeriwala (+91 9422310075)