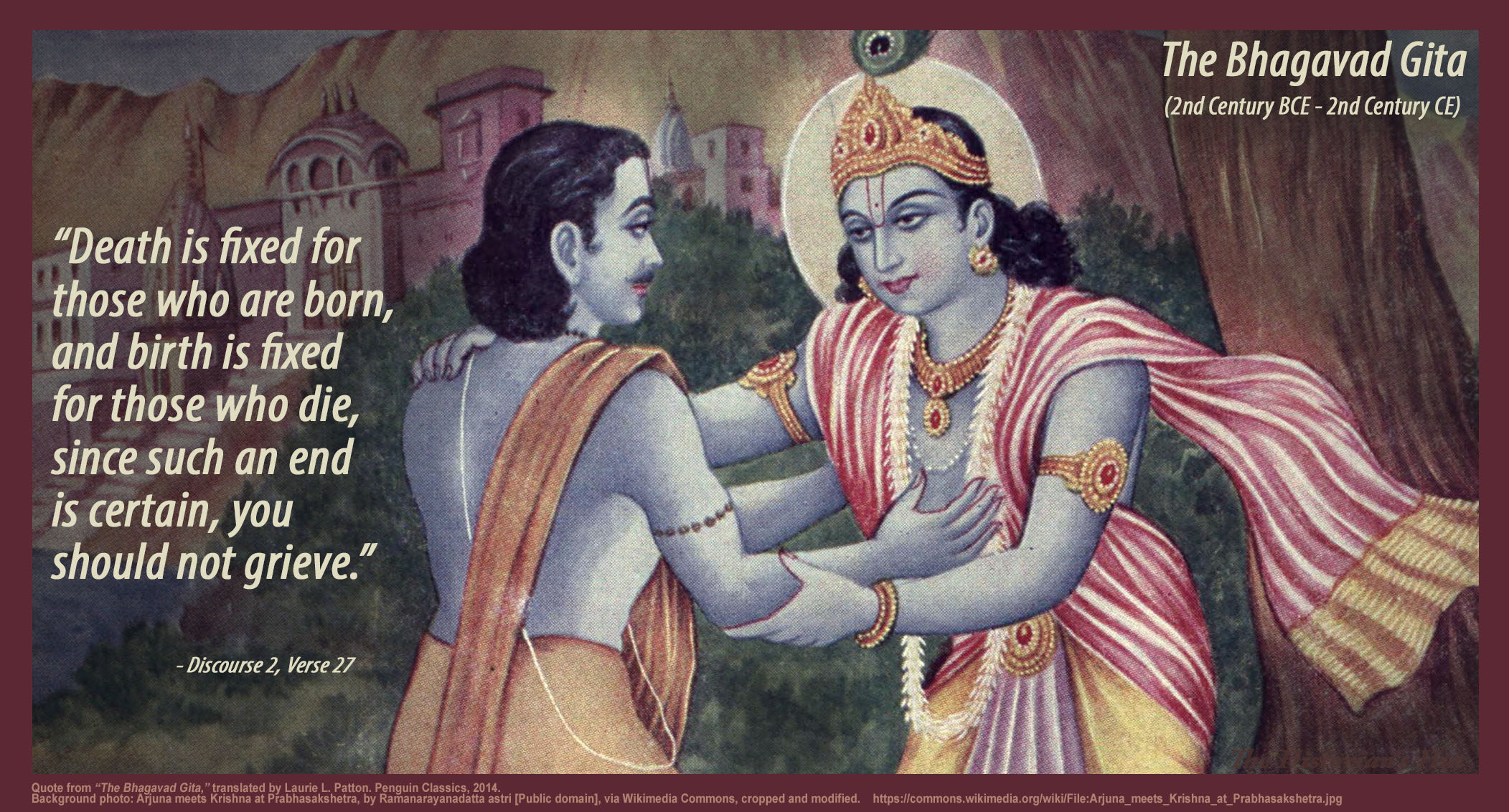।। Shrimadbhagwad Geeta ।। A Practical Approach ।।
।। श्रीमद्भगवत गीता ।। एक व्यवहारिक सोच ।।
।। Chapter 18.16 II
।। अध्याय 18.16 II
॥ श्रीमद्भगवद्गीता ॥ 18.16॥
तत्रैवं सति कर्तारमात्मानं केवलं तु यः ।
पश्यत्यकृतबुद्धित्वान्न स पश्यति दुर्मतिः॥
“tatraivaḿ sati kartāram,
ātmānaḿ kevalaḿ tu yaḥ..।
paśyaty akṛta- buddhitvān,
na sa paśyati durmatiḥ”..।।
भावार्थ:
परन्तु ऐसा होने पर भी जो मनुष्य अशुद्ध बुद्धि (सत्संग और शास्त्र के अभ्यास से तथा भगवदर्थ कर्म और उपासना के करने से मनुष्य की बुद्धि शुद्ध होती है, इसलिए जो उपर्युक्त साधनों से रहित है, उसकी बुद्धि अशुद्ध है, ऐसा समझना चाहिए।) होने के कारण उस विषय में यानी कर्मों के होने में केवल शुद्ध स्वरूप आत्मा को कर्ता समझता है, वह मलीन बुद्धि वाला अज्ञानी यथार्थ नहीं समझता॥१६॥
Meaning:
This being the case, the one who has an untrained intellect, sees the pure self as the doer. Indeed, that person of perverted understanding sees not.
Explanation:
We look at the clouds moving in the sky, and we imagine that the moon is moving, though it is stationary. We see other vehicles moving and think that our vehicle, which is stationary, to be moving. The actions of one object can be superimposed on another object due to optical illusion. Shri Shankaraachaarya provides these examples in this commentary of this shloka to drive home the point that what we see, or experience may not really be the truth.
So, every one of us is a mixture of acētana aṁśa and cētana aṁśa; a jñāni is also a mixture of both of them; an ajñāni also is a mixture of both of them; the difference is only in the perspective. Means how he looks at himself and ultimately the way you interpret the world, depends upon the way you look at yourselves.
That is why somebody said; ultimately, the world is a mirror; what you see in front is only your own personality; if you are a strong physically oriented personality; all the time bothered about the height, weight and figure and the complexion, if you are a physical personality, whenever you look out; you look for the physical personality of others; that alone registers. On the other hand, if I am a thinker or a scientist, or a philosopher, I look for that personality in others. If I am too much dress-conscious, I look at what are the different dresses a person has put; so, as I look at myself, so I look at the world. And ajñāni’s unfortunate perspective is given an ignorant person whose mind is polluted by ignorance of wrong notion of me. He prospects himself as doer and user of world, even forgetting that he is mortal. He behaves in ego.
Self-correction brings about the correction in the way you look at the world. And if there is a change, in the way you look at the world, there is a change in your response to life’s situation. In fact, saṁsāra is wrong response to life’s situations. Response is calling the situations problems. If you study shastra or vedantanta for passing of time or just educated yourself for satisfaction your ego in society. you will not understand the real knowledge of your identity as soul, it becomes as per your prospective just for time pass.
Shri Krishna says that our entire life is steeped in the incorrect notion that we perform actions. With regards to the analogies taken up, the self is stationary, and Prakriti is moving. But we do not see this because our intellect is untrained. It is akrita buddhi. We have not imbibed the knowledge that action is performed by the five factors mentioned in the prior shlokas. The scriptures, and Shri Krishna, are repeatedly informing us that ultimately Ishvara’s Prakriti is performing all the actions, not our self, not the aatmaa, not the eternal essence. But we fail to see this. We are durmati, we have a perverted understanding.
This does not mean that the soul has no role in performing karmas. It is like the driver in the car, who controls the steering wheel of the car and decides where to turn it and at what speed to drive. Similarly, the soul too governs the actions of the body, mind, and intellect, but it should not claim credit for any action(s) for itself. If we see ourselves to be the sole cause of action, then we want to be the enjoyers of our actions as well. But when we free ourselves from the pride of doership and ascribe the credit of our efforts to the grace of God and the tools provided by him, then we also realize that we are not the enjoyers of our actions, and all actions are meant for his pleasure.
Unless someone hears this statement from a teacher well versed in the scriptures, this ancient misunderstanding never comes up for questioning. The most common understanding is that the body is the self, the aatmaa. Some other people think that the jeeva, the individualized soul, is the aatmaa. But both these schools of thought attribute action to the aatmaa, which is incorrect. Furthermore, even the results of the actions go to the Prakriti. They do not go to the self, the aatmaa. The aatmaa is kevala, it is untainted, pure, and incapable of any change, modification or action. So then, what is the correct understanding? This is taken up next.
।। हिंदी समीक्षा ।।
पूर्व श्लोक में कर्म के पांच कारण अधिष्ठान, कर्ता, करण, विविधाश्च पृथकचेष्टा, दैव बताए गए एवम उस के करने के तीन करण मन, वाणी और शरीर भी पढ़े। इस में जीव को वर्ण, आश्रम, प्रकृति और परिस्थितियों के अनुसार कर्म करने पड़ते है। इस से यह स्पष्ट है कि वास्तव में आत्मा नित्य, शुद्ध, बुद्ध, निर्विकार और सर्वथा असंग है; प्रकृति से, प्रकृतिजनित पदार्थो से या कर्मो से उस का कुछ भी सम्बन्ध नहीं है। किंतु अनादि सिद्ध अविद्या के कारण असंग आत्मा का ही इस प्रकृति के साथ सम्बन्ध से हो रहा है अतः वह प्रकृति द्वारा संपादित क्रियाओ में मिथ्या अभिमान कर के स्वयं उन कर्मो का कर्ता बन जाता है। इस प्रकार कर्त्ता बने हुए पुरुष का नाम ही प्रकृतिस्थ पुरुष है। वह उन प्रकृति द्वारा सम्पन्न हुई क्रियाओ का कर्ता बनता है, तभी उन की कर्म संज्ञा होती है और वे कर्म फल देनेवाले बन जाते है। इसलिये उस प्रकृतिस्थ पुरुष को अच्छी बुरी योनियों में जन्म धारण कर के उन कर्मो का फल भोगना पड़ता है।
तो हम में से हर एक अचेतन अंश और चेतना अंश का मिश्रण है; ज्ञानी भी उन दोनों का मिश्रण है; अज्ञानी भी उन दोनों का मिश्रण है; अंतर केवल दृष्टिकोण में है। यानी वह खुद को कैसे देखता है और अंततः आप दुनिया की व्याख्या कैसे करते हैं, यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप खुद को कैसे देखते हैं। इसीलिए किसी ने कहा है; अंततः, दुनिया एक दर्पण है; जो आप सामने देखते हैं वह केवल आपका अपना व्यक्तित्व है; यदि आप एक मजबूत शारीरिक रूप से उन्मुख व्यक्तित्व हैं; हर समय ऊंचाई, वजन और फिगर और रंग-रूप के बारे में चिंतित रहते हैं, यदि आप एक भौतिक व्यक्तित्व हैं, तो जब भी आप बाहर देखते हैं; आप दूसरों के भौतिक व्यक्तित्व को देखते हैं; वही दर्ज होता है। दूसरी ओर, यदि मैं एक विचारक या वैज्ञानिक या दार्शनिक हूं, तो मैं दूसरों में उस व्यक्तित्व को देखता हूं। यदि मैं बहुत अधिक पोशाक के प्रति सचेत हूं, तो मैं देखता हूं कि किसी व्यक्ति ने क्या-क्या अलग-अलग पोशाकें पहन रखी हैं; अतः जैसे मैं अपने आप को देखता हूँ, वैसे ही मैं दुनिया को भी देखता हूँ।
और अज्ञानी का दुर्भाग्यपूर्ण दृष्टिकोण एक अज्ञानी व्यक्ति को दिया जाता है जिसका मन ‘मैं’ की गलत धारणा की अज्ञानता से प्रदूषित है। वह खुद को दुनिया का कर्ता और उपयोगकर्ता मानता है, यहाँ तक कि यह भी भूल जाता है कि वह नश्वर है। वह अहंकार में व्यवहार करता है। आत्म-सुधार से दुनिया को देखने के आपके नज़रिए में सुधार आता है। और अगर दुनिया को देखने के आपके नज़रिए में कोई बदलाव होता है, तो जीवन की परिस्थितियों के प्रति आपकी प्रतिक्रिया में भी बदलाव आता है। वास्तव में, संसार जीवन की परिस्थितियों के प्रति गलत प्रतिक्रिया है। प्रतिक्रिया का मतलब है परिस्थितियों को समस्या कहना। अगर आप समय बिताने के लिए शास्त्र या वेदांत या गीता का अध्ययन करते हैं या समाज में अपने अहंकार को संतुष्ट करने के लिए खुद को शिक्षित करते हैं, तो आप आत्मा के रूप में अपनी पहचान के वास्तविक ज्ञान को नहीं समझ पाएंगे, गीता का यह समय गुजरने का ही माध्यम बन कर रह जाएगा।
इसे हम यूं समझे की कंप्यूटर के विभिन्न हिस्से होते है, उस में उस का mother board में कंप्यूटर के specification रहते है। उस के अनुसार उस में एक ऑपरेटिंग एप्लीकेशन लोड कर दिया जाता है, इस ऑपरेटिग सिस्टम के अनुसार कमर्शियल एप्लीकेशन लोड होता है, जिस में ऑपरेटर अपने ज्ञान के अनुसार काम करता है। इस लिए किसी कंप्यूटर का कार्य उस के मदर बोर्ड, ऑपरेटिंग सिस्टम, कमर्शियल सिस्टम, ऑपरेटर और। पावर सप्लाई एवम उस के पार्ट्स पर निर्भर है। यदि कंप्यूटर ऑपरेटर यह सोचे की वह कर्ता है, तो यह उस की अविकसित बुद्धि होगी। क्योंकि बिना सभी के संयोग के काम नही हो सकता।
जितने भी कर्म होते हैं, वे सब अधिष्ठान, कर्ता, करण, चेष्टा और दैव – इन पाँच हेतुओं से ही होते हैं, अपने स्वरूप से नहीं। परन्तु ऐसा होने पर भी जो पुरुष अपने स्वरूप को कर्ता मान लेता है, उस की बुद्धि शुद्ध नहीं है – अकृतबुद्धित्वात् अर्थात् उसने विवेकविचार को महत्त्व नहीं दिया है। जड और चेतन का, प्रकृति और पुरुष का जो वास्तविक विवेक है, अलगाव है, उस की तरफ उस ने ध्यान नहीं दिया है। इसलिये उस की बुद्धि में दोष आ गया है। उस दोष के कारण वह अपने को कर्ता मान लेता है। यहाँ आये अकृतबुद्धित्वात् और दुर्मतिःपदों का समान अर्थ दीखते हुए भी इन में थोड़ा फरक है
अकृतबुद्धित्वात् पद हेतु के रूप में आया है और दुर्मतिः पद कर्ता के विशेषण के रूपमें आया है अर्थात् कर्ता के दुर्मति होने में अकृतबुद्धि ही हेतु है। तात्पर्य है कि बुद्धि को शुद्ध न करने से अर्थात् बुद्धि में विवेक जाग्रत् न करने से ही वह दुर्मति है। अगर वह विवेक को जाग्रत् करता, तो वह दुर्मति नहीं रहता।
पहले बतलाये हुए पाँच कारणों द्वारा ही समस्त कर्म सिद्ध होते हैं, इसलिये, जो अज्ञानी पुरुष, वेदान्त और आचार्य के उपदेश द्वारा तथा तर्कद्वारा संस्कृतबुद्धि न होनेके कारण, उन अधिष्ठानादि पाँचों कारणों के साथ अविद्या से आत्मा की एकता मानकर, उनके द्वारा किये हुए कर्मों का मैं ही कर्ता हूं इस प्रकार केवल शुद्ध आत्मा को ( उन कर्मोंका ) कर्ता समझता है, ( वह वास्तव में कुछ भी नहीं समझता ) तथा आत्मा को शरीरादि से अलग माननेवाला भी, जो शरीरादि से अलग केवल आत्मा को ही कर्ता समझता है, वह भी अकृतबुद्धि ही है। अतः असंस्कृतबुद्धि होने के कारण वह भी वास्तव में आत्मा का या कर्म का तत्त्व नहीं समझता, यह अभिप्राय है। इसलिये वह दुर्बुद्धि है। जिसकी बुद्धि कुत्सित, विपरीत, दुष्ट और बारम्बार जन्ममरण देने में कारणरूप हो उसे दुर्बुद्धि कहते हैं ऐसा मनुष्य देखता हुआ भी वास्तव में नहीं देखता। जैसे तिमिररोगवाला अनेक चन्द्र देखता है या जैसे बालक दौड़ते हुए बादलों में चन्द्रमा को दौड़ता हुआ देखता है अथवा जैसे ( पालकी आदि ) किसी सवारी पर चढ़ा हुआ मनुष्य दूसरों के चलने में अपना चलना समझता है।
परमात्मा द्वारा कठोर शब्दो का प्रयोग हम सब के लिये है, क्योंकि गीता किताबी ज्ञान नही है, इसे पढ़ने, सुनने या प्रचवन देने से कोई फर्क नही पड़ता। ऐसा व्यक्ति सुसंस्कृत तो है किंतु दुर्बुद्धि ही है क्योंकि उस ने गीता पढ़ने के बाद चिंतन, मनन एवम आचरण में धारण नही किया और तत्वज्ञान को समझ कर भी वह मूढ़ अपने को कर्त्ता ही मानता है या फिर जीव एवम प्रकृति के संयोग में आत्मा को कर्ता मानते हुए कर्म करता है।
किसी रेलगाड़ी में सफर करते हुए यदि हम समझते है कि हम चल रहे है तो गलत है क्योंकि चल गाड़ी रही है। फिर यदि कोई स्थान आ गया समझते है तो भी गलत है क्योंकि हम स्थान पर पहुचते है, न कि स्थान पहुचता है। प्रकृति की क्रियाएं स्वतः होती है और हम उस के कर्ता बन जाते है।
वर्षाकाल में वायु द्वारा लाये गये मेघ के समान; यह महाशक्तिमान अहंकार जड़-मूल से नष्ट किये जाने पर भी, यदि चित्त द्वारा क्षणभर के लिए भी पुनः संकल्पित हो जाय , तो वह पुनः प्रकट होकर सैकड़ों उत्पात खड़े कर देता है।
हमे यह भी ज्ञात होना चाहिये कि भगवान और प्रकृति के बीच एक आकर्षण रेखा है। जब तक साधक प्रकृति की सीमा में रहता है और स्वयं को कर्त्ता समझता है, तब तक परमात्मा मात्र दृष्टा बन कर सब कुछ देखता रहता है। जब साधक का कर्त्ता भाव लुप्त हो जाता है और वह परमात्मा को समर्पित हो जाता है तो परमात्मा जाग्रत हो कर उस के नियत कर्म के खड़ा हो जाता है। अर्जुन ने कर्ता के रूप में परमात्मा को चुना किन्तु उस का अहंकार नही छूटा था। परंतु जैसे ही वह अपना अहंकार छोड़कर युद्ध के समर्पित भाव से तैयार हो जाता है तो परमात्मा ही वह युद्ध उस की रक्षा करते हुए करता है।
अब इस में एक बात विशेष ध्यान देने की है कि कर्मयोग में केवल शब्द शरीर, मन आदि के साथ रहने से शरीर, मन, बुद्धि आदि के साथ अहम् भी संसार की सेवा में लग जायगा तथा स्वरूप ज्यों का त्यों रह जायगा और सांख्ययोग में स्वरूप के साथ केवल रहने से मैं निर्लेप हूँ, मैं शुद्धबुद्धमुक्त हूँ इस प्रकार सूक्ष्मरीति से अहम् की गंध रह जायगी। मैं निर्लेप रहूँ मेरे में कर्तृत्व नहीं है – ऐसी स्थिति बहुत काल तक रहने से यह अहम् भी अपने आप गल जायगा अर्थात् अपने कारण प्रकृति में लीन हो जायगा।
व्यवहार में गीता को हम धर्म ग्रंथ समझ कर पढ़ते है और सोचते है कि इस के पाठ से हमारा उद्धार हो जाएगा। गीता मनन और चिंतन का ग्रंथ है, जो इस बात को समझ लेता है, उस का अहम भाव की मैं कर्ता हूं, जाता रहता है। किंतु चिंतन से इस बात को समझने के बाद भी वह लोभ, आसक्ति और कामना रखता है और अहम में जीवन व्यतीत करता है, तो वह दुर्मति पुरुष है। और यदि केवल अहम भाव रखता है तो वह कुबुद्धि पुरुष है।
इसका मतलब यह नहीं है कि कर्म करने में आत्मा की कोई भूमिका नहीं है। यह कार के ड्राइवर की तरह है, जो कार के स्टीयरिंग व्हील को नियंत्रित करता है और तय करता है कि उसे कहाँ मोड़ना है और किस गति से चलाना है। इसी तरह, आत्मा भी शरीर, मन और बुद्धि के कार्यों को नियंत्रित करती है, लेकिन उसे किसी भी कार्य का श्रेय खुद नहीं लेना चाहिए। अगर हम खुद को कर्म का एकमात्र कारण मानते हैं, तो हम अपने कर्मों के भोक्ता भी बनना चाहते हैं। लेकिन जब हम खुद को कर्तापन के अभिमान से मुक्त करते हैं और अपने प्रयासों का श्रेय भगवान की कृपा और उनके द्वारा दिए गए साधनों को देते हैं, तो हमें यह भी पता चलता है कि हम अपने कर्मों के भोक्ता नहीं हैं और सभी कर्म उनके सुख के लिए हैं।
प्रस्तुत श्लोक से किसी भी ज्ञानी पुरुष द्वारा ज्ञान होने पर भी यदि अहम है और कर्तृत्व भाव है तो उस की संज्ञा हम धृष्टराष्ट्र या संजय से कर सकते है, दोनों ने गीता को दोहराया या सुना किन्तु एक का अहम अर्थात कर्ता भाव नही छुट्टा और दूसरे का आसक्ति भाव। गीता पढ़ने से नही, चिंतन, मनन एवम धारण करने से ही तत्वज्ञान आता है। एक तत्वदर्शी जीव जो कर्ता भाव से मुक्त है, उस के लिये गीता के सार स्वरूप में परमात्मा अगले श्लोक में क्या बताते है, पढ़ते है।
।। हरि ॐ तत सत ।। गीता – 18. 16 ।।
Complied by: CA R K Ganeriwala (+91 9422310075)