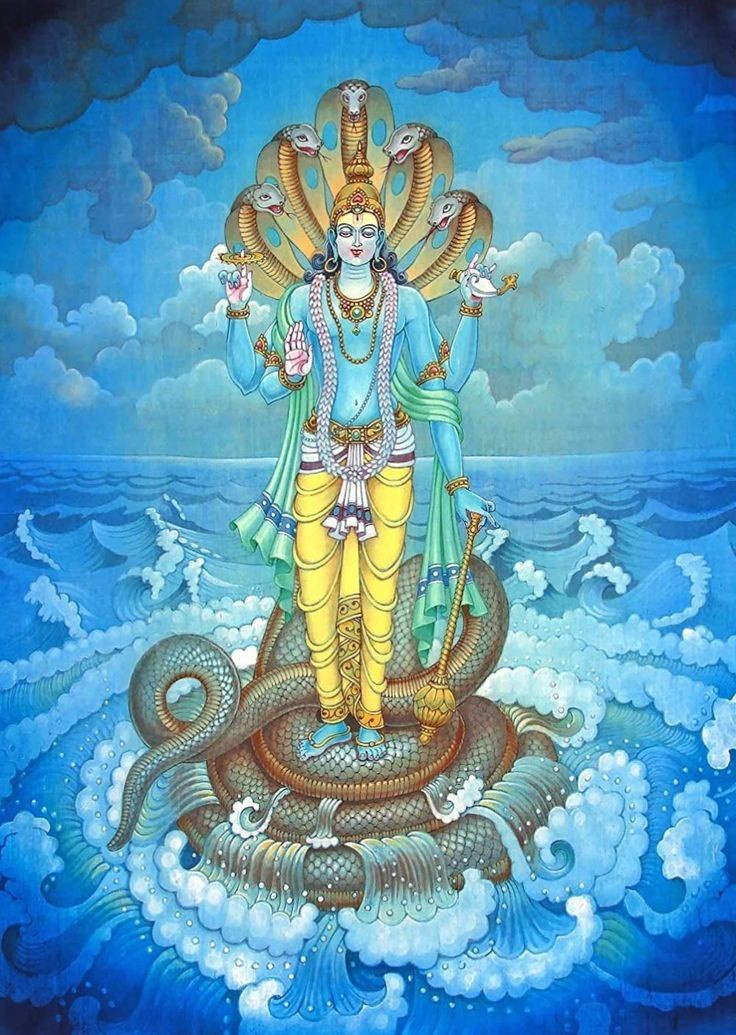।। Shrimadbhagwad Geeta ।। A Practical Approach ।।
।। श्रीमद्भगवत गीता ।। एक व्यवहारिक सोच ।।
।। Chapter 18.06 II
।। अध्याय 18.06 II
॥ श्रीमद्भगवद्गीता ॥ 18.6॥
एतान्यपि तु कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा फलानि च ।
कर्तव्यानीति में पार्थ निश्चितं मतमुत्तमम्॥
“etāny api tu karmāṇi,
sańgaḿ tyaktvā phalāni ca..।
kartavyānīti me pārtha,
niścitaḿ matam uttamam”..।।
भावार्थ:
इसलिए हे पार्थ! इन यज्ञ, दान और तपरूप कर्मों को तथा और भी सम्पूर्ण कर्तव्यकर्मों को आसक्ति और फलों का त्याग करके अवश्य करना चाहिए, यह मेरा निश्चय किया हुआ उत्तम मत है॥६॥
Meaning:
But even those actions should be performed, giving up attachment and rewards. This, O Paartha, is my definite and foremost conclusion.
Explanation:
Acts of sacrifice, charity, and penance should be done in the mood of devotion to the Supreme Lord. If that consciousness has not been attained, then they should verily be performed as a matter of duty, without desire for reward.
One has to perform sacrifice, charity and penance as his duty to purify himself. But he does not get attached to even the religious karma. Because later after purification, he has to renounce them; that is important, he should get attached and follow them initially, but after
sometimes he must renounce, there are people attached to rituals, they would not come to vēdānta. Two extremes. One group never enter yajña dāna tapaḥ, the other group which enters, but they never come out of them. What is intelligence? Enter, purify and get out; and after getting out what should you do? Vēdānta śravaṇa, manana, nidhidhyāsana. Therefore, religious activities are important; but do not get attached even to them. Treat them as a sadhana; not an end in itself. Therefore, saṅgam tvakta; without attachment; and phalani cha. According to the scriptures, yajña dānam and tapaḥ, these three religious disciplines can produce two types of puṇyaṁ; One puṇyaṁ is called spiritual puṇyaṁ, another puṇyaṁ is called material puṇyaṁ.
Shri Krishna says that the only way to convert selfish actions into selfless actions is to give up attachment to the action and to the rewards of the action. Consider an architect who spends months creating the plans for a building. If the architect designs the building keeping the bonus payment in mind, he is performing the action with an attitude of selfishness. If the architect designs the building with the sole motive of creating the best possible living space for people, he is performing the action with an attitude of selflessness.
Let us be clear about one thing. There is nothing wrong in the architect expecting a fair payment for the rendering of his services. But he does not keep a monetary expectation every second of his time while designing his buildings. He does it out of a sense of duty. His svadharma, which means his aptitude, his training and his passion, is to be an architect. Regardless of how his day goes, he derives joy in the performance of his svadharma, his duty to the world, as an architect.
In addition to giving up attachment to the reward of action, Shri Krishna also advises us to give up attachment to the action itself. Here, we have to keep two things in mind. First, it is not guaranteed that every action of ours will be successful, since there are external factors that may intervene. Second, even if we insist that an action should be performed in a certain way, there could be other ways that could sometimes work better. Insisting that every action ends successfully, and that every action has to be done our way, are the two ways in which we get attached to action. Giving up these attachments, along with the attachment to reward, is the only way that we bring the purifying effect of karma yoga into every action we perform. This is Shri Krishna’s foremost conclusion on karma yoga.
So then, if this is the case, how should one treat actions performed for one’s career? If we love our career, and it gives us a personal reward in the form of salary, should we give up that as well? We need to resolve this issue by converting our reward-oriented actions into selfless actions. Only then will we be able to weaken the samskaaraas or mental impressions that impel us to perform our career-oriented actions every day. What is the technique by which we can convert our selfish actions into selfless actions? This is taken up next.
।। हिंदी समीक्षा ।।
कर्म का दोष अर्थात बंधकर्ता कर्म में नही, उस की फल की आशा में है, इसलिये जब भी गीता में कर्मयोग के तत्व को बताया गया तो प्रत्येक बार सभी कर्म ममता- आसक्ति एवम फलाशा त्याग कर बिना कर्तृत्त्व अभिमान के निष्काम बुद्धि से कर्तव्य धर्म के अनुसार कर्म करने को कहा गया। यही गीता के कर्म योग का उपसंहार भी कह सकते है।
यज्ञ, दान तथा तप के कर्म भगवान की भक्ति की भावना से करने चाहिए। यदि वह चेतना प्राप्त नहीं हुई है, तो उन्हें फल की इच्छा किए बिना कर्तव्य समझकर करना चाहिए। व्यक्ति को अपने आपको शुद्ध करने के लिए यज्ञ, दान और तपस्या करना अपना कर्तव्य समझना चाहिए। लेकिन वह धार्मिक कर्मों से भी आसक्त नहीं होता। क्योंकि बाद में शुद्धि के बाद उसे उनका त्याग करना पड़ता है; यह महत्वपूर्ण है, उसे आसक्त होना चाहिए और शुरू में उनका पालन करना चाहिए, लेकिन कुछ समय बाद उसे त्याग करना होगा, ऐसे लोग हैं जो कर्मकांडों से आसक्त हैं, वे वेदान्त तक नहीं आएंगे। दो अतियाँ। एक समूह कभी यज्ञ दान तपः में प्रवेश नहीं करता, दूसरा समूह जो प्रवेश करता है, लेकिन वे कभी उनसे बाहर नहीं आते। बुद्धि क्या है? प्रवेश करो, शुद्ध हो जाओ और बाहर निकल जाओ; और बाहर निकलने के बाद तुम्हें क्या करना चाहिए? वेदान्त श्रवण, मनन, निधिध्यासन। इसलिए धार्मिक गतिविधियाँ महत्वपूर्ण हैं; लेकिन उनमें भी आसक्त मत होओ। उन्हें एक साधना के रूप में मानो; अपने आप में एक अंत नहीं। इसलिए संगं त्वक्ता; आसक्ति रहित; और फलानि च। शास्त्रों के अनुसार, यज्ञ दान और तप, इन तीन धार्मिक अनुशासनों से दो प्रकार के पुण्य उत्पन्न होते हैं; एक पुण्य को आध्यात्मिक पुण्य कहा जाता है, दूसरे पुण्य को भौतिक पुण्य कहा जाता है।
सन्यास मार्ग की मान्यता की समस्त कर्म दोष युक्त है, त्याज्य है, गीता को मान्य नही है। गीता केवल काम्य कर्मो का सन्यास लेने की बात कहती है। धर्मशास्त्र में जिन कर्मो का प्रतिपादन है, वे सभी काम्य ही है, इसलिये अब यह कहना ही पड़ता है कि यदि सभी काम्य कर्मो का सन्यास करना पड़े तो यज्ञ चक्र ही बन्द हो जाएगा और सृष्टि भी उद्ध्वस्त हो सकती है। इसलिये गीता में सभी कर्म निष्काम भाव से, लोकसंग्रह हेतु करने का मत प्रकट किया गया है। लोकसंग्रह हेतु निष्काम भाव से किया प्रत्येक कर्म बंधनमुक्त सात्विक कर्म है, जिसे स्वयम परमात्मा ने भी मानव रूप में जन्म लेकर उदाहरण के द्वारा कर के भी बताया है।
उदाहरणार्थ, नव विवाहित दम्पत्ति को पुत्र की इच्छा होती है। यह सामान्य इच्छा है। परन्तु, यदि वे कहें, हमें पुत्र ही चाहिए, पुत्री नहीं, तो उनका यह आग्रह संग या आसक्ति है। ऐसा आग्रह रखना अविवेक का ही लक्षण है।
अन्य उदाहरण में हम अपने जीवन मे किसी लक्ष्य को निर्धारित कर के उस को प्राप्त करने के अपनी क्षमता, कार्य कुशलता एवम बुद्धिमत्ता का पूर्ण उपयोग करते है, किन्तु यदि परिणाम विपरीत हो तो भी लक्ष्य से प्राप्त होने वाले फल की आशा त्याग करने से कर्तृत्त्व भाव का अभाव रहता है और व्यक्ति को उस कर्म का कोई बंधन नही रहता। लक्ष्य अपने, समाज और देश को उन्नत करना हमे किसी भी काम को करने की प्रेरणा देता है, किन्तु लक्ष्य लोकसंग्रह एवम निष्काम होना चाहिए। परमात्मा के समस्त अवतार किसी न किसी लक्ष्य हेतु ही थे, इसलिये लक्ष्य मोह, कामना या आसक्ति एवम कर्तृत्त्व भाव नहीं है।
अर्जुन को कर्तव्य धर्म से युद्ध करने की आज्ञा दी गई थी किन्तु उस को जीत या हार के लिये कुछ नही कहा गया। इसलिये कर्तव्य धर्म कर्म को लक्ष्य के साथ पूर्ण क्षमता और कुशलता के निर्देश है, जिसे कुछ लोग कहते है कि बिना फल की आशा के काम करने की प्रेरणा जाग्रत नही होती। किंतु उन्हें यह समझना होगा कि फल उन द्वारा किये कर्म पर निर्भर नहीं है अपितु उस के अन्य तत्व समय, स्थान, प्रतिद्वन्दी एवम साधन आदि भी अन्य तत्व है, इसलिये फल की आशा रखने से, परिणाम विपरीत होने पर निराशा होगी और सार्थक होने से कर्तृत्त्व अभिमान से अहंकार उत्पन्न होगा।
आसक्ति से अभिभूत पुरुष अपने इष्टफल को प्राप्त करने में अविवेकपूर्ण या आत्मघातक चिन्ताओं से ग्रस्त हो जाता है। फल प्राप्ति के पूर्व ही उसके विषय में चिन्ता और व्याकुलता होने से मनुष्य की कार्यकुशलता समाप्तप्राय हो जाती है। इसलिए भगवान् का उपदेश है कि यज्ञादिक कर्म भी फलासक्ति के बिना करने चाहिए। यह भगवान् श्रीकृष्ण का अपना मत है। इसका अर्थ यह नहीं हुआ कि उनका यह सर्वथा मौलिक मत है। वेदों में भी निष्काम कर्म के सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया है।कर्मयोग के जीवन को अपनाने से अन्तकरण की शुद्धि के द्वारा मनुष्य अपने नित्य शुद्धबुद्ध मुक्त स्वरूप का साक्षात्कार कर सकता है।
इस श्लोक में एतान्यपि शब्द के साथ यज्ञ, दान और तप को अन्य सभी नित्य, नैमित्तिक और काम्य कर्मो के साथ जोड़ा है अर्थात यह भी काम अन्य कामो के समान करना चाहिये। यह परमात्मा का निश्चय किया हुआ मत सन्यास एवम त्याग कर्म के संदर्भ में दिया मत है।
वास्तव में आसक्ति हमारे स्वरूप में है नहीं, केवल मानी हुई है।दूसरी बात, जो अपना स्वरूप होता है, उसका त्याग नहीं होता जैसे – प्रज्वलित अग्नि उष्णता और प्रकाश का त्याग नहीं कर सकती। जो चीज अपनी नहीं होती, उस का भी त्याग नहीं होता जैसे – संसार में अनेक वस्तुएँ पड़ी हैं परन्तु उनका हम त्याग करें – ऐसा कहना भी नहीं बनता क्योंकि वे वस्तुएँ हमारी हैं ही नहीं। इसलिये त्याग उसी का होता है, जो वास्तवमें अपना नहीं है, पर जिस को अपना मान लिया है। ऐसे ही प्रकृति और प्रकृति के कार्य शरीर आदि हमारे नहीं हैं, फिर भी उन को हम अपना मानते हैं, तो इस अपनेपन की मान्यता का ही त्याग करना है। मनुष्य के सामने कर्तव्य रूप से जो कर्म आ जाय, उस को फल और आसक्ति का त्याग कर के सावधानी के साथ तत्परतापूर्वक करना चाहिये – कर्तव्यानि। कर्मयोग में विधि निषेध को लेकर अमुक काम करना है और अमुक काम नहीं करना है – ऐसा विचार तो करना ही है परन्तु अमुक काम ब़ड़ा है और अमुक काम छोटा है – ऐसा विचार नहीं करना है। कारण कि जहाँ कर्म और उस के फल से अपना कोई सम्बन्ध ही नहीं है, वहाँ यह कर्म बड़ा है, यह कर्म छोटा है इस कर्म का फल बड़ा है, इस कर्म का फल छोटा है – ऐसा विचार हो ही नहीं सकता। कर्म का बड़ा या छोटा होना फल की इच्छा के कारण ही दीखता है, जब कि कर्मयोग में फलेच्छा का त्याग होता है। कर्म करना रागपूर्ति के लिये भी होता है और रागनिवृत्ति के लिये भी। कर्मयोगी रागनिवृत्ति के लिये अर्थात् करने का राग मिटाने के लिये ही सम्पूर्ण कर्तव्यकर्म करता है
कर्तव्य शब्दका अर्थ होता है — जिस को हम कर सकते हैं तथा जिस को जरूर करना चाहिये और जिस को करने से उद्देश्य की सिद्धि जरूर होती है। उद्देश्य वही कहलाता है, जो नित्यसिद्ध और अनुत्पन्न है अर्थात् जो अनादि है और जिस का कभी विनाश नहीं होता। उस उद्देश्य की सिद्धि मनुष्य जन्म में ही होती है और उस की सिद्धि के लिये ही मनुष्य शरीर मिला है, न कि कर्म जन्य परिस्थिति रूप सुखदुःख भोगने के लिये। कर्मजन्य परिस्थिति वह होती है, जो उत्पन्न और नष्ट होती हो। वह परिस्थिति तो मनुष्य के अलावा पशुपक्षी, कीटपतङ्ग, वृक्षलता, नारकीय स्वर्गीय आदि योनियों के प्राणियों को भी मिलती है, जहाँ कर्तव्य का कोई प्रश्न ही नहीं है और जहाँ उद्देश्य की पूर्ति का अधिकार भी नहीं है।
एक छोटा बालक अपना हो तो ममता और आसक्ति से हम उस के समस्त कार्य करते है, किंतु पराया हो तो उस की आवश्यकता की बेपरवाह नही हो सकते और जहां तक हो सकता है, उस का कार्य बिना मोह, ममता और आसक्ति के कर्तव्य समझ कर कर देते है। संन्यासी यदि कर्म में आसक्ति, कामना और मोह सोच कर त्याग करता है तो वह काम्य कर्म तो नही करता किंतु उस की आसक्ति, कामना और मोह बने ही रहते है।
मतों में अपना मत उत्तम कहते हुए, अन्य मतों का प्रतिकार नही किया, क्योंकि यह मत अर्जुन को कहा जा रहा है, जो युद्ध भूमि में। इस से पूर्व युद्ध न करने की बात कहते हुए, समझौते के प्रयास निम्न स्तर तक झुक कर लिए गए थे। इसलिए कर्तव्य कर्म नम्र, स्वार्थ रहित हो कर करने का होता है। कर्तव्य कर्म वही कर सकता है जो सात्विक वृति का हो, अपने वर्ण धर्म का पालन करता हो, कर्म का उद्देश्य व्यक्तिगत न हो कर लोकसंग्रह का हो, जिस कर्म को करने से उस को कीर्ति, धन, पद, या अन्य किसी प्रकार की कामना या आसक्ति भी न हो। इसलिए भगवान का कर्तव्य कर्म आसक्ति में करने वाला राजसी या तामसी वृति का गुणधर्म नही है।
अतिभौतिकवादी भी कहते है कि मनुष्य को अपने स्वार्थ और परार्थ के लिए जीना चाहिए। स्वार्थ यानि वह समस्त कार्य जिस से आप जीवन के सुख का आनंद ले सके और परार्थ का अर्थ वह समस्त कार्य जिस को करने से आप को आत्मिक सुख और आनंद मिले। अर्थात यज्ञ, तप और दान कर्म को करने का उद्देश्य अपने शारीरिक, मानसिक और आत्मिक सुख में वृद्धि करना। जैसे खुद आराम से रहना और साथ वालों को भी आराम से रहने देना और फिर समाज में भी पद, सम्मान और प्रभाव जमा करने के उन्हें भी आराम देना। आध्यात्म कहता है कि जिस को सुख और आराम अर्थात अपनी आत्मा के लिए इतना कुछ करते हो तो अपनी आत्मा को भी जानो। यज्ञ, तप और दान से सात्विक भाव की उत्पत्ति इसी आत्मज्ञान के लिए है। जब तक काम, लालसा, स्वार्थ, राग – द्वेष नहीं मिल जाता तब तक स्वार्थ और परार्थ से यज्ञ, तप और दान करते रहना चाहिए। इस को करने से ही निष्काम कर्म योग की प्राप्ति होगी, यदि हम आसक्ति से ग्रस्त नहीं हुए तो।
अतः किसी भी काम्य कर्म में त्याग का अर्थ कर्म का त्याग न हो कर उस मे ममता, आसक्ति, फलाशा, कर्तृत्त्व भाव का त्याग है। गीता में यह मत संसार का उत्तम मत इसलिए भी है, यदि स्वार्थ और लोभ को त्याग का सभी लोकसंग्रह हेतु कार्य करे तो परिवार, व्यापार, समाज और विश्व में प्रेम, शांति, सहिष्णुता, भाईचारा भी बना रहेगा। संसार में युद्ध स्वार्थ, लोभ, मतांधंता आदि के कारण ही होते है।
।। हरि ॐ तत सत ।। गीता – 18.06।।
Complied by: CA R K Ganeriwala (+91 9422310075)