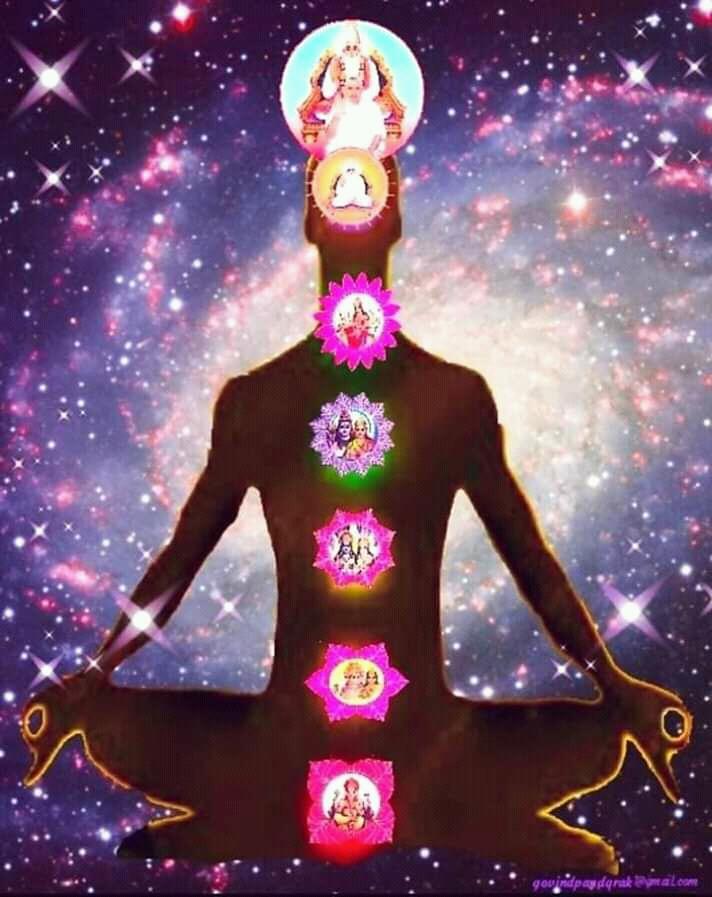।। Shrimadbhagwad Geeta ।। A Practical Approach ।।
।। श्रीमद्भगवत गीता ।। एक व्यवहारिक सोच ।।
।। Chapter 18.05 II
।। अध्याय 18.05 II
॥ श्रीमद्भगवद्गीता ॥ 18.5॥
यज्ञदानतपःकर्म न त्याज्यं कार्यमेव तत् ।
यज्ञो दानं तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम्॥
“yajña- dāna- tapaḥ- karma,
na tyājyaḿ kāryam eva tat..।
yajño dānaḿ tapaś caiva,
pāvanāni manīṣiṇām”..।।
भावार्थ:
यज्ञ, दान और तपरूप कर्म त्याग करने के योग्य नहीं है, बल्कि वह तो अवश्य कर्तव्य है, क्योंकि यज्ञ, दान और तप -ये तीनों ही कर्म बुद्धिमान पुरुषों को (वह मनुष्य बुद्धिमान है, जो फल और आसक्ति को त्याग कर केवल भगवदर्थ कर्म करता है।) पवित्र करने वाले हैं॥५॥
Meaning:
Actions of sacrifice, charity and penance should not be given up, they should certainly be performed. Sacrifice, charity and penance are purifiers of wise people.
Explanation:
Shri Krishna begins to describe his criteria for actions that should be performed for karma yoga. Instead of creating the criteria from scratch, he uses a viewpoint mentioned earlier as the basis. He says that nitya karmas, the obligatory duties towards society, Ishvara and oneself should be performed. They should never be given up. Only nishiddha karmas or prohibited actions, and kaamya karmas or selfish actions should be given up.
The scriptures divide the entire humanity into two types, broadly: one type is those people who have got jñāna yōgyatha means learned and wise people. You may call it a mature mind; a purified mind; a prepared mind, which can take to a life without any relationship. A human mind is an emotional mind generally looks for relationship. And the health of the emotional mind is heavily dependent on the relationship. If certain healthy relationships are absent, then the human mind can go crazy. It wants companionship. It wants to claim some people as mine; you belong to me; and it wants some people to claim that I belong to you. So, it wants relationship, companionship. Without that the mind feels lonely and it will get into several type of psychiatric problem. In fact, generally the psychiatric people will say that several psychiatric problems. Talk to a psychiatric privately and he would say that all Sanyāsis would have psychological problems, because human mind requires companionship, relationship. A mind which does not have a strong bonding with someone or the other; that mind will face lot of problems; And therefore, the scriptures say you should talk about sanyāsa only to those people whose minds are ready with complete knowledge and exercise.
This criterion is to be followed by those who are maneeshi, who are wise, who have understood that blind pursuit of material gain is not for them. Such people are interested in liberation only. When these wise people perform their obligatory duties, the performance of those actions acts as a cleanser, a purifier. All traces of raaga and dvesha, likes and dislikes, are slowly cleared out by the performance of obligatory duties. Their actions are propelled out of an attitude of seva or service, not out of personal and selfish likes and dislikes.
But if the person is not ready and majority of humanity is not ready then the definition will change. And Krishna is addressing the majority. Therefore, the following definition of sanyāsa is in keeping with the majority of humanity, which is not mature in mind. And therefore, Krishna addresses the people who are not yet ready due to their eternal short fall.
Therefore, Krishna says yajñō dānaṁ tapaścaiva; means action of sacrifice, charity and penance these three fundamental religious practices are pāvanāni. Pāvanāni means purifiers of the mind and purification, removal of all the emotional obstacles to vēdāntic study.
So then, if this is the case, how should one treat actions performed for one’s career? If we love our career, and it gives us a personal reward in the form of salary, should we give up that as well? We need to resolve this issue by converting our reward-oriented actions into selfless actions. Only then will we be able to weaken the samskaaraas or mental impressions that impel us to perform our career-oriented actions every day. What is the technique by which we can convert our selfish actions into selfless actions? This is taken up next.
।। हिंदी समीक्षा ।।
किसी भी मत को व्यक्त करने से पूर्व सभी मतों का व्याख्यान करना एवम उस मे श्रेष्ठ मत को अपने मत की सहमति देना, प्रबंधन एवम ज्ञान देने वाले गुरु की सर्वोत्तम अभिव्यक्ति होती है, जिस से उस कार्य को क्रियावन्तित करने वाले शिष्य या अधीनस्थ कर्मचारी को कार्य करते वक्त कोई संशय न रहे। पूर्व के श्लोक में सन्यास एवम त्याग को लेकर विभिन्न मतों का उल्लेख करने का उद्देश्य भी यही है कि जिस समय गीता की रचना की गई थी तब भी विभिन्न मतांतर थे जिस के कारण अर्जुन संशय एवम मोह में पढ़ कर युद्ध न करते हुए, त्याग का आश्रय ले कर सन्यास लेने की बात भी कर रहा था एवम शास्त्रो द्वारा उसे उचित भी सिद्ध कर रहा था।
भगवान श्री कृष्ण अपना मत व्यक्त करते हुए कहते है यज्ञ, दान एवम तप त्यागने योग्य कर्म नहीं है, क्योंकि यह योगी पुरुष का कर्तव्य ही है। यज्ञ, दान और तप तीनो ही बुद्धिमान पुरुषों को पवित्र करने वाले है। मनीषियों द्वारा यज्ञ, दान और तप शास्त्र विहित कर्तव्य कर्म बताए गए है। इसलिए अर्जुन एक क्षत्रिय योद्धा एवम सात्विक पुरुष है तो युद्ध भूमि में युद्ध करना उस का कर्तव्य कर्म है, इस का त्याग करना समाज, देश, संसार के उपयुक्त नहीं होगा। मनीषी के कर्म स्वयं के लिए नही होते क्योंकि वह फलाशा त्याग कर लोकसंग्रह के लिए किए जाते है। मनीषियों द्वारा किए कर्तव्य कर्म समाज का पथ प्रदर्शन भी करते है।
विशेष बात यही है कि यज्ञ, तप और दान का मनीषियों द्वारा करने का समर्थन करते हुए भी भगवान अन्य किसी मत का खण्डन नही करते। उन का यही कहना है कि कर्तव्य कर्म मनीषियों को अधिक पवित्र करता है क्योंकि मनीषी ही लोकसंग्रह के लिए कर्म करते है। अर्जुन को युद्ध के उकसाने की बजाय युद्ध करना क्यो चाहिए, क्योंकि यह अर्जुन का कर्तव्य कर्म है।
शास्त्र पूरी मानवता को मोटे तौर पर दो प्रकारों में विभाजित करते हैं: एक प्रकार वे लोग हैं जिन्हें ज्ञान योग्यता प्राप्त है। आप इसे परिपक्व मन कह सकते हैं। एक शुद्ध मन, एक तैयार मन, जो बिना किसी संबंध के जीवन जी सकता है। एक मानव मन; एक भावुक मन आम तौर पर संबंध खोजता है और भावुक मन का स्वास्थ्य काफी हद तक संबंधों पर निर्भर करता है। अगर कुछ स्वस्थ संबंध न हों, तो मानव मन पागल हो सकता है। उसे संगति चाहिए। वह चाहता है कि कुछ लोग मेरे हों; तुम मेरे हो; और वह चाहता है कि कुछ लोग दावा करें कि मैं तुम्हारा हूं। इसलिए उसे संबंध चाहिए, संगति चाहिए। इसके बिना मन अकेला महसूस करता है और वह कई तरह की मानसिक समस्याओं में फंस जाता है। वास्तव में, आम तौर पर मनोरोग विशेषज्ञ कई तरह की मानसिक समस्याओं की बात कहते हैं। किसी मनोरोग विशेषज्ञ से निजी तौर पर बात करें और वह कहेगा कि सभी संन्यासियों को मनोवैज्ञानिक समस्याएं होती और इसीलिए शास्त्र कहते हैं कि संन्यास के बारे में केवल उन्हीं लोगों से बात करनी चाहिए जिनका मन इसके लिए तैयार हो।
लेकिन अगर व्यक्ति तैयार नहीं है और मानवता का बहुमत तैयार नहीं है तो परिभाषा बदल जाएगी। और कृष्ण बहुमत को संबोधित कर रहे हैं। इसलिए संन्यास की निम्नलिखित परिभाषा मानवता के बहुमत के अनुरूप है, जो मन में परिपक्व नहीं है। और इसलिए कृष्ण उन लोगों को संबोधित करते हैं जो अपनी शाश्वत कमियों के कारण अभी तक तैयार नहीं हैं।
इसलिए कृष्ण कहते हैं यज्ञो दानं तपश्चैव; अर्थात त्याग, दान और तपस्या ये तीन मूलभूत धार्मिक क्रियाएँ पावनानि हैं। पावनानि का अर्थ है मन को शुद्ध करने वाली और शुद्ध करने वाली, वेदान्तिक अध्ययन में आने वाली सभी भावनात्मक बाधाओं को दूर करने वाली।
व्यवहार में जब राजसी या तामसी प्रवृति के लोग कोई गलत काम करते है, जिन्हे हम सामाजिक या पारिवारिक बुराई भी कह सकते है तो अक्सर सात्विक लोग “हमे कुछ लेना देना नही कह कर पल्ला झाड़ लेते है”। आसुरी या तामसी वृति का विरोध करना सात्विक अर्थात मनीषियों का कर्तव्य कर्म है। अधिकांश व्यापार संसार में धार्मिक या व्यवसायिक राजसी या तामसी होता है। कुछ की लोग सात्विक वृति के होते है, किंतु उन के उदासीन भाव से राजसी और तामसी वृत्तियों को बढ़ावा मिलता है। अतः जब सात्विक अर्थात सज्जन पुरुष अपने कर्तव्य धर्म का पालन नहीं करते तो समाज में फैलती हुई अव्यवस्था के वो लोग भी परोक्ष रूप से जिम्मेदार होते है।
नित्य, नैमित्तिक, जीविका सम्बन्धी, शरीर सम्बन्धी आदि जितने भी कर्तव्यकर्म हैं, उन को भी जरूर करना चाहिये क्योंकि वे भी मनीषियों को पवित्र करनेवाले हैं। जो मनुष्य समत्व बुद्धि से युक्त होकर कर्मजन्य फल का त्याग कर देते हैं, वे मनीषी हैं। ऐसे मनीषियों को वे यज्ञादि कर्म पवित्र करते हैं। परन्तु जो वास्तव में मनीषी नहीं हैं, जिन की इन्द्रियाँ वश में नहीं हैं अर्थात् अपने सुख भोग के लिये ही जो यज्ञ, दानादि कर्म करते हैं, उन को वे कर्म पवित्र नहीं करते, प्रत्युत वे कर्म बन्धनकारक हो जाते हैं।
संत ज्ञानेश्वर ने कहते है, जब जीवन रूपी नौका में सवार हो कर नदी को पार कर रहे है, तो नौका का त्याग तट पर पहुचने से पहले नही हो सकता। जब दीपक जला कर किसी वस्तु को खोज रहे है, तो बिना वस्तु खोजे दीपक नही बुझाना चाहिए। स्वर्ण में जब एक के बाद एक इस प्रकार क्षारो के अनेक पुट दिए जाते है, तब उस में मिश्रित अशुद्ध अंश निरंतर जलता जाता है और स्वर्ण शुद्ध हो जाता है, इसी प्रकार सात्विक भाव से यज्ञ, तप और दान निरंतर करते रहने से रज और तम के दूषित गुण भी समाप्त होते है।
पश्चिम देशों में अतिभौतिकवाद के विस्तार में अतिदैविक और अध्यात्मवाद को नकार दिया है। उन का कहना है जो प्रत्यक्ष है या जिसे सिद्ध किया जा सके वहीं सत्य है। जीवन से पहले और बाद के जीवन का कोई अर्थ नहीं। किंतु भय और स्वार्थ में यह भी विश्वास करता है कि यदि जीवन सुख और शांति से व्यतीत हो तो व्यक्ति को दान, दया, कर्म और व्यवसायिक शिक्षा और ज्ञान प्राप्त करते रहना चाहिए। बिना कर्म के भौगोलिक जीवन में भी सुख और ऐश्वर्य प्राप्त नहीं होते। अतः यज्ञ, तप और दान अतिभौतिकवाद में भी स्वार्थ और भय से स्वीकृत किया जाता है। फिर अतिदैविक और अध्यात्म में इस को कर्मयोगी के लिए इसलिए अनिवार्य कहा गया है कि जब तक वह पूर्णतः निष्काम, निस्वार्थ और कामना, आसक्ति, राग – द्वेष से मुक्त नहीं हो जाता, उस के लिए यज्ञ, तप और दान उस को पवित्र और शुद्ध करने के लिए अनिवार्य है। अर्जुन क्षत्रिय योद्धा था, उस के अंदर संन्यासी होने का विचार मोह के कारण आया था, इसलिए यदि वह कर्म का त्याग भी कर दे, वह संन्यासी नहीं हो सकता है। वह आज के युग के घूमते अनेक साधु, संत और महंत जैसा ही होता जिन्हे अपना मठ, आश्रम, शिष्य और आम नागरिक से सम्मान तथा सुख सुविधाएं चाहिए।
इन कर्मों का सम्यक् आचरण करने पर वे अन्तकरण को शुद्धि प्रदान करते हैं, जो आत्मोन्नति और आत्मसाक्षात्कार के लिए आवश्यक है। अविद्याजनित बन्धनों से मुक्ति पाने के इच्छुक साधकों को श्रद्धा भक्ति पूर्वक यज्ञ, दान और तप का आचरण करना चाहिए। इसके द्वारा वे आन्तरिक शान्ति और संतुलन को प्राप्त कर सकते हैं।
।। हरि ॐ तत सत ।। गीता – 18.05।।
Complied by: CA R K Ganeriwala (+91 9422310075)