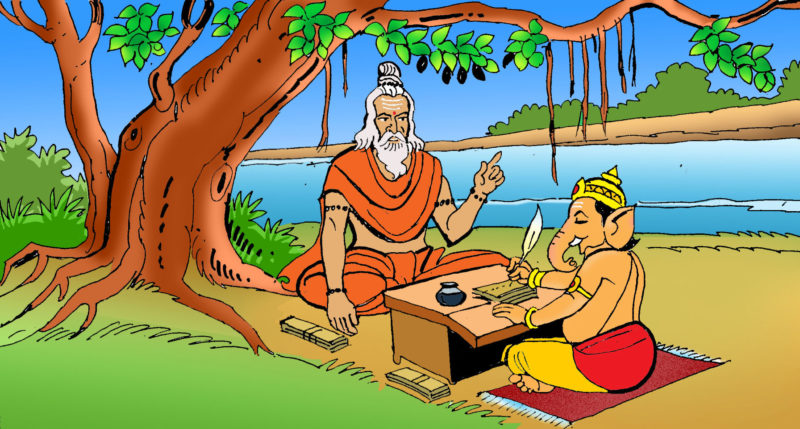।। Shrimadbhagwad Geeta ।। A Practical Approach ।।
।। श्रीमद्भगवत गीता ।। एक व्यवहारिक सोच ।।
।। Chapter 18.02 II
।। अध्याय 18.02 II
॥ श्रीमद्भगवद्गीता ॥ 18.2॥
श्रीभगवानुवाच
काम्यानां कर्मणा न्यासं सन्न्यासं कवयो विदुः ।
सर्वकर्मफलत्यागं प्राहुस्त्यागं विचक्षणाः॥
“śrī-bhagavān uvāca,
kāmyānāḿ karmaṇāḿ nyāsaḿ,
sannyāsaḿ kavayo viduḥ..।
sarva- karma- phala- tyāgaḿ,
prāhus tyāgaḿ vicakṣaṇāḥ”..।।
भावार्थ:
श्री भगवान बोले- कितने ही पण्डितजन तो काम्य कर्मों के (स्त्री, पुत्र और धन आदि प्रिय वस्तुओं की प्राप्ति के लिए तथा रोग-संकटादि की निवृत्ति के लिए जो यज्ञ, दान, तप और उपासना आदि कर्म किए जाते हैं, उनका नाम काम्यकर्म है।) त्याग को संन्यास समझते हैं तथा दूसरे विचारकुशल पुरुष सब कर्मों के फल के त्याग को (ईश्वर की भक्ति, देवताओं का पूजन, माता-पितादि गुरुजनों की सेवा, यज्ञ, दान और तप तथा वर्णाश्रम के अनुसार आजीविका द्वारा गृहस्थ का निर्वाह एवं शरीर संबंधी खान-पान इत्यादि जितने कर्तव्यकर्म हैं, उन सबमें इस लोक और परलोक की सम्पूर्ण कामनाओं के त्याग का नाम सब कर्मों के फल का त्याग है, कहते हैं॥२॥
Meaning:
Shree Bhagavaan said:
Sages understand sannyasa to be the giving up of desire prompted actions. Giving up the rewards of all actions is tyaāg, the learned ones declare.
Explanation:
Arjuna wanted to know the difference between sanyaasa and tyaaga. Shri Krishna did not answer this question directly. He wanted to answer the question in such a way that Arjuna would be able to put the answer into practical use, and not get caught in complicated semantics, something that has only academic value. It was almost as though he said – Arjuna, you don’t worry about the difference in meaning of sanyaasa and tyaaga for now. You are a warrior, a kshatriya. I will tell you what is appropriate for you such that you can advance spiritually.
Renunciation is primarily associated with karma or action. Even though renunciation is associated with all things, including possessions and relationship, generally renunciation is associated with karma or activity. In fact, that is the toughest job also, because not to do anything is the toughest thing. An idle mind is a devil’s worship.
Renunciation is associated with karma and in the śāstra, karmas are divided into five types; which I have talked about before, but you can briefly note here: No.1 is called vihita karma, compulsory duties; No.2, kamya karma or sakāma karma, optional activities, to be taken to, if you want to; optional activities; No.3 Niṣidha (prohibited) karma, prohibited activity. No.4 is prāyaschitta karma, prāyaschitta karma, i.e. remedial activities; an action done to remedy a Niṣidha karmaḥ, karma when Niṣidha karma is done; and No.5. finally, naimithika karma; occasional duties when the situation arises.
Vihita karma, compulsory duties; keeping that only and giving up of all other karmas, what are they, kāmya karma, prāyaschitta karma, Niṣidha karma. So, giving up of kāmya karma, and the other etc. is understood, is called sanyāsaḥ according to some scholars. That means what? One should retain the nitya karma and even naimithika karma is considered to be compulsory. So, two has to be kept. one and five are compulsory, 2,3,4 can be given up. Giving up of 2,3 and 4, is called sanyāsa, retaining one and 5. Vihita and naimithika; Vihitha is sometime called nithya also; nithya and naimithika karmas are returned; Kāmya, Niṣidhaḥ and prāyaschitta karmas are given up. This karma renunciation is called sanyāsa.
When a person does nithya, naimithika karma, without expecting even acknowledgement or compensation, that renunciation of materialistic result, karma phala Tyāgaḥ. Karma phalam of what? One and five; one and five karmas should do and the result of that karma, one should not expect; that is Tyāgaḥ, according to some.
So, karma tyāga is sanyāsa and karma phala Tyāgaḥ is Tyāgaḥ. Sarva karma; here sarva means, sarva 1 and 5 karmas are done, without expecting any award or reward; that is called Tyāgaḥ.
Shree Krishna states that wise people lay emphasis on tyāg, meaning “internal renunciation.” This implies not relinquishing the prescribed Vedic duties, rather renouncing the desires for enjoying their fruits. Therefore, the attitude of giving up attachment to the rewards of actions is tyāg, while the attitude of giving up works is sanyas. Both sanyās and tyāg seem plausible and reasonable options to pursue for enlightenment. Of these two courses of action, which one does Shree Krishna recommend? He provides more clarity on this topic in the subsequent verses.
According to kavayaḥ vicakṣaṇāḥ. kavayaḥ means learned people, vicakṣaṇāḥ means enlightened people or śāstra kuśalā, experts in the śāstras. the view presented here is learned and enlighten people for sannyasa and tyaāg, it is not shri krishna view. He expressed his view in coming chapters.
।। हिन्दी समीक्षा ।।
कर्म के विषय में शास्त्र, धर्म, सन्यास में विभिन्न मत है, सांख्य मत यही कहता है कि कर्म करने से उस के फल से बचा नही जा सकता, अतः संन्यासी को कर्म का ही त्याग करना चाहिए। शास्त्र कहते है, पुण्य कमाने और स्वर्ग लोक आदि का सुख भोगने के लिए यज्ञ, तप और दान करना चाहिए। किंतु गीता में कर्म की बजाए उस के फल की आशा का त्याग करने की बात कही गई है।
पहले अध्यायों में जिन का जगह जगह निर्देश किया गया है, वे संन्यास और त्याग – दोनों शब्द स्पष्टार्थयुक्त नहीं हैं, इसलिये ( उनका स्पष्ट अर्थ जानने की इच्छासे ) पूछने वाले अर्जुन को उन का निर्णय सुनाने के लिये श्रीभगवान् बिना अपना मत प्रकट किए, ऋषि मुनि द्वारा व्यक्त किये कथन को कहते है, कितने ही बुद्धिमान पण्डित लोग अश्वमेधादि सकाम कर्मों के त्याग को संन्यास समझते हैं अर्थात् कर्तव्यरूप से प्राप्त ( शास्त्रविहित ) सकाम कर्मों के न करने को संन्यास शब्द का अर्थ समझते हैं। कुछ विचक्षण पण्डितजन अनुष्ठान किये जानेवाले नित्य नैमित्तिक सम्पूर्ण कर्मों के, अपने से सम्बन्ध रखनेवाले फल का परित्याग करना रूप जो सर्वकर्मफल त्याग है, उसे ही त्याग कहते हैं। अर्थात् त्याग शब्द का वे ऐसा अभिप्राय बतलाते हैं। कहने का अभिप्राय, चाहे काम्य कर्मों का ( स्वरूप से ) त्याग करना हो और चाहे समस्त कर्मों का फल छोड़ना ही हो, सभी प्रकार से संन्यास और त्याग इन दोनों शब्दों का अर्थ तो, एकमात्र त्याग ही है।
कर्म को तीन विभाग में बांट सकते है ।
1. नित्य कर्म
2. नैमित्तिक कर्म
3. काम्य कर्म
इस के अतिरिक्त निषिद्ध कर्म भी होते है, क्योंकि ये आसुरी वृति के कर्म करने योग्य ही नही है, इन को चर्चा में भी नही लिया गया है। निषिद्ध कर्म के अतिरिक्त उपरोक्त तीन कर्मों में विहित कर्म (प्रथम) जो नित्य कर्म का ही भाग है और प्रायश्चित में किया कर्म भी कुछ लोग पांचवा कर्म कहते है, किंतु यह काम्य कर्म का ही भाग है।
जब कोई व्यक्ति नित्य, नैमित्तिक कर्म करता है, बिना किसी स्वीकृति या प्रतिफल की आशा किए, तो वह भौतिकवादी परिणाम का त्याग करता है, कर्म फल त्याग: करता है, अर्थात एक और पाँच कर्म करने चाहिए और उस कर्म के परिणाम की आशा नहीं करनी चाहिए; कुछ लोगों के अनुसार वह त्याग: है। अतः कर्म त्याग ही संन्यास है और कर्म फल त्याग ही त्याग है। सर्व कर्म; यहाँ सर्व का अर्थ है, सर्व १ और ५ कर्म बिना किसी पुरस्कार या इनाम की अपेक्षा के किए जाते हैं; उसे त्याग कहते हैं।
भगवान कहते है कि वामदेव, सनत्कुमार, विश्वामित्र वशिष्ठ आदि ज्ञानी जन कहते है कि नित्य, नैमित्तिक एवम काम्य इन सभी कर्मो को करना, परंतु उन के फलों के त्याग को ही मुख्य शास्त्र में त्याग कहते है, न कि कर्म के त्याग को। जबकि अतिक्रांति कवि लोग कामना ले कर किये गए कर्मो के त्याग को सन्यास समझते है और ज्ञानी पंडित जन नित्य, नैमित्तिक और काम्य कर्मो के फल के त्याग को त्याग कहते है। कवि शब्द उन महामुनियो और संतो के लिए जिन्होंने तप से उच्च स्थान प्राप्त किया। यहां कविता लिखने वाले को कवि नही कहा है।
ब्रह्मा, बाल्मीकि शुक्राचार्य आदि अति क्रांतिदर्शी कवि लोगो का सिंद्धान्त है कि काम्य कर्म अर्थात कामना ले कर कर्म को नही करना ही सन्यास है।
काम्य कर्मों का त्याग संन्यास कहलाता है और समस्त कर्मों का फलत्याग त्याग कहा जाता हा। शास्त्रीय सिद्धांतों से अनभिज्ञ लोगों को इन दोनों में कोई अन्तर नहीं ज्ञात होता क्योंकि कामना सदैव फलप्राप्ति की ही होती है। अतः कामना प्रेरित कर्मों का त्याग और कर्मफल की आसक्ति का त्याग ये दोनों ही समान प्रतीत होते हैं। इस का कारण शास्त्रों से अनभिज्ञता अथवा उनका सतही अध्ययन ही हो सकता है। इसमें कोई सन्देह नहीं कि दोनों का अर्थ कामना का त्याग ही है, परन्तु त्याग और संन्यास में कुछ अन्तर है।
फिर भी त्याग, संन्यास का अविभाज्य अंग है। मनुष्य वर्तमान में कर्म करता है और आशा करता है कि उसे इष्टफल भविष्य में प्राप्त होगा। वर्तमान के कर्म का परिणाम ही भावी फल है। इसलिए, निष्काम कर्म वर्तमान में ही हो सकते हैं, जब कि फलभोग की चिन्ता से उत्पन्न होने वाली मन की व्याकुलता का संबंध भविष्य काल से होता है। वर्तमान के कर्म की परिसमाप्ति भावी फल में होती है। कामना और विक्षेप मन में अशान्ति उत्पन्न करते हैं। कामना जितनी अधिक तीव्र होगी, उतनी ही अधिक मात्रा में हमारी आन्तरिक शक्तियों का ह्रास होगा और ऐसा शक्तिहीन पुरुष किसी भी कर्म को कुशलता एवं उत्साह के साथ सम्पादित नहीं कर सकता।
यह भी ध्यान देने योग्य बात है कि अहंकार या जीव ही इच्छा करता है। अतः अहंकार की निवृत्ति का अर्थ है, व्यष्टि जीव की विरति और उस साधक की अपने सर्वोच्च स्वरूप में दृढ़ स्थिति। कर्म वर्तमान में होते हैं और उनके फल भविष्य में प्राप्त होने की सम्भावना रहती है। जो व्यक्ति फल की चिन्ता करता है वह वर्तमान में कार्य करने की अपनी क्षमता खो देता है। स्वाभाविक ही है कि उस व्यक्ति को इष्ट फल मिलने की सम्भावना कम हो जाती है, क्योंकि कर्म का फल कर्ता के प्रयत्न तथा प्रकृति के नियमादि अन्य कई कारणों पर निर्भर करता है। अत हमें फलासक्ति का त्याग करने का उपदेश दिया जाता है।संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि त्याग साधन है और संन्यास साध्य है। त्याग और संन्यास की साधना का संबंध हमारे कर्मों से है। भगवान् श्रीकृष्ण कर्म के महत्त्व पर बल देते हुए कभी नहीं थकते। इन दोनों शब्दों में से कोई भी यह नहीं दर्शाता है कि हमको कर्म की उपेक्षा करनी चाहिए। इसके विपरीत, दोनों का आग्रह कर्म के पालन पर ही है। हम को कर्म करने ही चाहिए। तथापि, ये कर्म अहंकार और स्वार्थ या फलासक्ति से रहित होने चाहिए। फलासक्ति ही हमारी कार्यकुशलता में बाधक बनती है। फलासक्ति के अभाव में हमारे कर्म हमें अपना पूर्ण पुरस्कार प्रदान कर सकते हैं।
हम कह सकते हैं कि वेदों में प्रयुक्त इन दो शब्दों के अर्थों की अपेक्षा गीता में दी गई इनकी परिभाषाएं अधिक उदार एवं सहिष्णु हैं।
अनुभवी (कवय:) और शास्त्र को जानने वाले ( विचक्षणा:) दार्शनिक विद्वानों के मत बताने के बाद अब भगवान् द्वारा त्याग के विषय में कहा गया ज्ञान पढ़ते है। परन्तु यह भी समझना चाहिए कि कृष्ण ने यह मत क्यों रखा। प्रवृति और निवृति यह दो मोक्ष के मार्ग है, जिस को शास्त्र और अनुभव के आधार पर लोग आपस में चर्चा का विषय बना कर रखते है। अर्जुन को विषाद के समय भी इन दोनों मार्ग का ज्ञान अनुभव और शास्त्र जन्य ही था, इसलिए वह युद्ध भूमि में युद्ध को नहीं करते हुए, उसे युद्ध का त्याग करना, सन्यास लेने जैसा लग रहा था। किंतु वह संन्यासी प्रवृति का नहीं हो कर एक क्षत्रिय योद्धा था। इसलिए वनवास के 12 साल भटकने पर भी उसे सन्यास लेने का कोई विचार नहीं आया। जब परिस्थिति विपरीत हो या अवसाद हो तो भय और मोह से व्यक्ति स्थिति का सामना नहीं करते हुए अन्य मार्ग को खोजता है तो वह उस का विवेकपूर्ण निर्णय नहीं हो कर, कायरता का निर्णय कहलाता है। अतः अंतिम अध्याय में अर्जुन को सन्यास और उस शास्त्र ज्ञान के विषय में स्पष्ट करना आवश्यक था।
।। हरि ॐ तत सत ।। गीता – 18.02।।
Complied by: CA R K Ganeriwala (+91 9422310075)