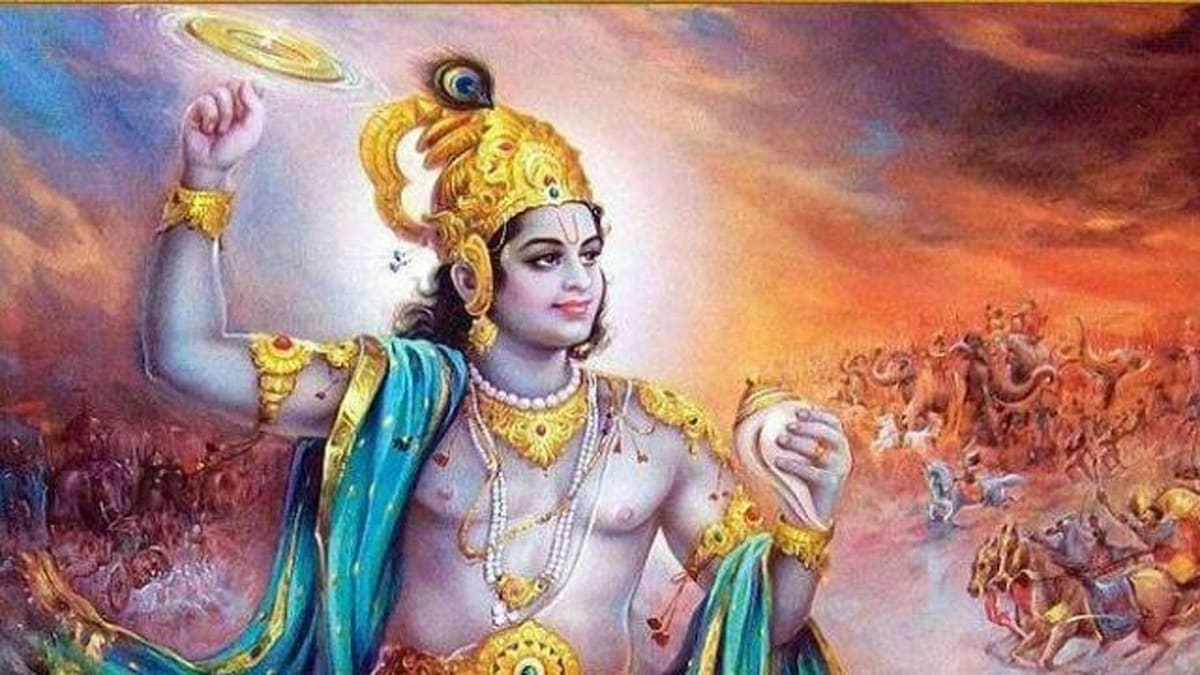।। Shrimadbhagwad Geeta ।। A Practical Approach ।।
।। श्रीमद्भगवत गीता ।। एक व्यवहारिक सोच ।।
।। Chapter 17.26 II
।। अध्याय 17.26 II
॥ श्रीमद्भगवद्गीता ॥ 17.26॥
सद्भावे साधुभावे च सदित्यतत्प्रयुज्यते ।
प्रशस्ते कर्मणि तथा सच्छब्दः पार्थ युज्यते॥
“sad- bhāve sādhu-bhāve ca,
sad ity etat prayujyate..।
praśaste karmaṇi tathā,
sac- chabdaḥ pārtha yujyate”..।।
भावार्थ:
हे पृथापुत्र अर्जुन! इस प्रकार साधु स्वभाव वाले मनुष्यों द्वारा परमात्मा के लिये “सत्” शब्द का प्रयोग किया जाता है तथा परमात्मा प्राप्ति के लिये जो कर्म किये जाते हैं उनमें भी “सत्” शब्द का प्रयोग किया जाता है। (२६)
Meaning:
The word Sat is used in the sense of existence and goodness, and also, O Paartha, the word Sat is added in the sense of an auspicious act.
Explanation:
The utterance of Om is used to focus our attention on the action, and the utterance of Tat is used to dedicate the actions and their reward to Ishvara. Even if we do all this, there could be a defect in the way the action is performed. We may have not followed some guidelines, or some external entity may have caused some problem which we may be unaware of. For most of us who are not well versed in the scriptures, is there an easy solution to this problem?
Shri Krishna says that the chanting of the word Sat during the performance of a saattvic action has the effect of removing all the errors and defects of that action. This is why words such as satkarma (good actions) and sadaachaar (good conduct) use sat as a synonym for good. But just purifying an action is not enough. The emotions, the feelings behind the action are equally important. Chanting of the word Sat has the effect of purifying our emotions as well. Words such as sadbhaava (good emotion) and sadguna (good values) illustrate this point.
In addition, auspicious performance of sacrifice, austerity, and charity is also described as Sat. Sat also means that which always exists i.e., it is an eternal truth. The Śhrīmad Bhāgavatam states: “O Lord, your vow is true, for not only are you the Supreme Truth, but you are also the truth in the three phases of the cosmic manifestation—creation, maintenance, and dissolution. You are the origin of all that is true, and you are also its end. You are the essence of all truth, and you are also the eyes by which the truth is seen. Therefore, we surrender unto you, the Sat i.e., Supreme Absolute Truth. Kindly give us protection.”
Lord Krishna has given meaning of sat, this is apart from om and tat as the same were not defined. He defined meaning in two shloks 26 and 27.
1. The word Sat is employed, is used, sat bhāve, in the meaning of Nobility; goodness; good conduct, good behaviour, is called sat bhavaḥ, that is why noble people are called sat purusha or santaḥ.Therefore one meaning is good conduct.
2. The second meaning is the word Sat bhāvaḥ means existence. In the philosophical context, the word Sat means eternal existence.
3. Then the third meaning is any good karma is also called Sat. Any great noble action is also called Sat. Then two more given in shlok 27.
4. The fourth meaning of the word Sat means perseverance, or commitment or will power with regard to Action (yajñē), Sacrifice (tapasi) and charity (danēcha) with regard to the practice of these three spiritual disciplines and commintment.
5. The fifth meaning is any other activity, any other secondary activity; satellite activity, which will promote sacrifice, austerity and charity i.e.yajñāh, dānam, and tapas. So previously we said yajñāh, dānah, tapas, the primary activities are called sat; now all the other activities also, even mundane activity also, which is meant to promote, yajñāh, dāna, tapa. Suppose I do a business, and I earn lot of money, it is a pucca commercial activity. But suppose earn money, and use the money for any noble purpose, yajñāh, dānam or tapas, then that business activity will become sat.
The real meaning of the word Sat, however,is existence. It is a pointer to brahman, the eternal essence, the one reality. “Naabhaavo vidyate sataha” found in the second chapter of the Gita denotes that Sat, the eternal essence, always exists. It is always complete, without any duality. Therefore, the ultimate goal of uttering Sat is to mentally remove any notions of duality, mentally remove all the upaadhis or limitations, and merge oneself into the one reality, the one eternal essence.
।। हिंदी समीक्षा ।।
शंकराचार्य जी अद्वेतवाद में ब्रह्म सत्य – जीव एवम जगत मिथ्या कहा गया है। जीव को ब्रह्म में विलय होना ही मोक्ष है।
वल्लभाचार्य अपने शुद्धाद्वैत दर्शन में ब्रह्म, जीव और जगत, तीनों को सत्य मानते हैं, जिसे वेदों, उपनिषदों, ब्रह्मसूत्र, गीता तथा श्रीमद्भागवत द्वारा उन्होंने सिद्ध किया है। अद्वैत सिद्धांत चराचर सृष्टि में भी व्याप्त है। जब पैर में काँटा चुभता है तब आखोँ से पानी आता है और हाथ काँटा निकालने के लिए जाता है। ये अद्वैत का एक उत्तम उदाहरण है।
संसार सत्य है और इस में होने वाले भेद भी सत्य हैं। वस्तु का स्वरूप ही भेदमय है। ज्ञान में हम वस्तु को अन्य वस्तुओें से अलग कर के एक विलक्षण रूप में जानते हैं। चूँकि ज्ञेय विषय भिन्न हैं अत: हमारा ज्ञान भी ज्ञेय के अनुसार भिन्न भिन्न होता है। रामानुज की तरह द्वैतवाद में भी ईश्वर, चित् और अचित् इन तीन नित्य, परस्पर भिन्न तत्वों को सत्य माना गया है। इन में से चित् और अचित् ईश्वराश्रित हैं। केवल ईश्वर अनाश्रित तत्व है। वह अनंत सद्गुणों से युक्त है। वही विश्व का स्रष्टा, पालक और संहारक है। वह दिव्य शरीरधारी विश्वातीत और विश्वांतर्यामी दोनों माना गया है। ईश्वर पूर्ण है- कर्मों का अधिष्ठाता ईश्वर केवल भक्ति से प्रसन्न होता है।
सत् का प्रयोग शाश्वत भगवान और धर्माचरण के प्रयोजनार्थ किया जाता है। ‘सत्’ का यह भी अर्थ है कि जो सदैव विद्यमान रहता है अर्थात् यह शाश्वत सत्य है। श्रीमद्भागवतम् में कहा गया है
सत्यव्रतं सत्यपरं त्रिसत्यं सत्यस्य योनिं निहितं च सत्य। सत्यस्य सत्यमृतसत्यनेत्रं सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्नाः।।(श्रीमद्भागवतम्-10.2.26)
“हे भगवान! आप सत्य संकल्प हो क्योंकि तुम केवल परम सत्य ही नहीं बल्कि तुम ब्रह्माण्डीय अभिव्यक्ति के तीन चरणों- सृजन, स्थिति और लय में भी सत्य स्वरूप हो। तुम सबके मूल हो,यह सब भी सत्य है और इसका अंत भी हो। तुम सभी सत्यों का सार हो और तुम वे नेत्र भी हो जिससे सत्य को देखा जा सकता है। इसलिए हम तुम्हारे ‘सत्‘ अर्थात् परम सत्य के शरण गत हैं, कृपया हमारी रक्षा करें।”
भगवान कृष्ण ने सत् का अर्थ बताया है, यह ॐ और तत् का एक भाग है क्योंकि इनकी परिभाषा नहीं थी। उन्होंने दो श्लोक 26 और 27 में इसका अर्थ बताया है।
1. सत् शब्द का प्रयोग, सत् भावे, कुलीनता; अच्छा आचरण, अच्छे व्यवहार के अर्थ में किया जाता है, इसे सत् भावः कहते हैं, इसीलिए श्रेष्ठ लोगों को सत् पुरुष या सन्तः कहा जाता है। इसलिए एक अर्थ अच्छा आचरण है।
2. दूसरा अर्थ है सत् भावः शब्द का अर्थ है अस्तित्व। दार्शनिक संदर्भ में, सत् शब्द का अर्थ है शाश्वत अस्तित्व।
3. फिर तीसरा अर्थ है कोई भी अच्छा कर्म भी सत् कहलाता है। कोई भी महान नेक कार्य भी सत् कहलाता है। फिर श्लोक २७ में दो और दिए गए हैं।
४. सत् शब्द का चौथा अर्थ है दृढ़ता, या प्रतिबद्धता या कर्म (यज्ञ), त्याग (तपसी) और दान (दानेच) के संबंध में इच्छा शक्ति, इन तीन आध्यात्मिक अनुशासनों और प्रतिबद्धता के अभ्यास के संबंध में।
५. पाँचवाँ अर्थ है कोई अन्य गतिविधि, कोई अन्य माध्यमिक गतिविधि; उपग्रह गतिविधि, जो त्याग, तपस्या और दान को बढ़ावा देगी यानी यज्ञ, दानम और तपस। तो पहले हमने कहा यज्ञ, दान, तपस, प्राथमिक गतिविधियों को सत् कहा जाता है; अब अन्य सभी गतिविधियाँ भी, यहाँ तक कि सांसारिक गतिविधि भी, जो बढ़ावा देने के लिए हैं, यज्ञ, दान, तप। मान लीजिए मैं एक व्यवसाय करता हूँ, और मैं बहुत पैसा कमाता हूँ, यह एक पक्का वाणिज्यिक गतिविधि है। लेकिन मान लीजिए कि आप धन कमाते हैं और उस धन का उपयोग किसी महान उद्देश्य, यज्ञ, दान या तप के लिए करते हैं, तो वह व्यवसायिक गतिविधि सत् हो जाएगी।
सत का वर्णन करते हुए परमात्मा कहते है, वह समस्त भाव जो हमे परमात्मा के सतत होने अनुभव कराते है, सद्भाव कहलाते है। इसलिये सुबह शाम राम राम बोलना या राधे राधे बोलना या किसी भी स्वरूप में परमात्मा को पूजना सद्भाव ही है।
इसी प्रकार जिन का अन्तःकरण शुद्ध, सरल एवम निर्मल है जो प्राणी मात्र के लिये श्रेष्ठ भाव रखते है, यह साधुभावे है। हृदय के दया, क्षमा आदि श्रेष्ठ उत्तम भाव सब के सब साधुभाव के अन्तर्गत हैं।
जो शुभ कर्म परमात्मा की प्राप्ति, लोककल्याण के लिये शास्त्र विहित निष्काम किये जाते है, जिस से प्राणी अर्थात जीव मात्र का हित होता है, उन्हें प्रशस्त कर्म कहते है। शास्त्र विधि के अनुसार यज्ञोपवीत, विवाह आदि संस्कार अन्नदान, भूमिदान, गोदान आदि दान और कुआँबावड़ी खुदवाना, धर्मशाला बनवाना, मन्दिर बनवाना, बगीचा लगवाना आदि श्रेष्ठ कर्म भी प्रशस्ते कर्मणि के अन्तर्गत आते हैं। इन सब श्रेष्ठ आचरणों में, श्रेष्ठ कर्मों में सत् शब्द का प्रयोग किया जाता है जैसे – सदाचार, सत्कर्म, सत्सेवा, सद्व्यवहार आदि।
जो हम आंखों से देखते है या कानो से सुनते है आदि मिथ्या या भ्रम नही कह सकते। युद्ध के मैदान में अर्जुन अपने सगे संबंधियों को देख रहा था, वह असत्य है, ऐसा समझना गलत होगा। प्रकृति शाश्वत है, जीव और प्रकृति का सम्बंध ही शाश्वत है। किंतु जो दिख रहा है वह ही हमेशा रहेगा यह समझना ही भ्रम या असत्य है। हम अपने शरीर को यदि सत्य समझ रहे है तो असत्य है क्योंकि यह परिवर्तनशील है। किन्तु शरीर, पत्नी, पुत्र या भूख प्यास, चोट, इन्द्रीयजनित क्षणिक सुख इन को असत्य भी नही कह सकते। अनित्य में नित्य तत्व के सत जानते हुए, नाशवान सत को स्वीकार करना ही सत है।इसलिये सत में श्रद्धा का भाव या यज्ञ उस के प्रति होना चाहिए जो नित्य है और अपने कर्तव्य धर्म केअनुसार श्रद्धा भाव से कर्म करते रहना ही सत को ब्रह्म के जोड़ने का गीता का यह संदेश सत्वगुण युक्त राजसी कर्म को भी स्वीकार करता है।
सत को वही समझ सकता है जो जगत के प्रत्येक कार्य, वस्तु और प्राणी को प्रकृति के अनुसार स्वीकार करते हुए भी, एक ही परम सत्य परमात्मा की देन या स्वरूप समझता है। क्योंकि सत सर्वव्याप्त और नित्य है, इसलिए जो प्रत्यक्ष हम देखते, समझते, सुनते, अनुभव करते हुए व्यवहार करते है, वह उस नित्य और सर्वव्याप्त सत्य का स्वरूप है। भूखे को भोजन कराना, मंदिर में पूजा करना, भजन करना, व्यापार या समाज में काम करना, प्रकृति के आनंद को सद्भाव में भोगना, सभी उसी सत स्वरूप परमात्मा के कर्म है।
सत्यता और साधुता तथा कर्म की प्रशस्तता को सत् शब्द के द्वारा लक्षित किया जाता है। हम सब आपेक्षिक सत्यत्व वाले जगत् में रहते हैं। हमारे लिए यह स्वाभाविक है कि अपने शरीर, मन और बुद्धि के द्वारा अनुभूयमान इस जगत् को ही हम पारमार्थिक सत्य समझ लें। अत सत् शब्द के द्वारा हमें यह स्मरण कराया जाता है कि पारमार्थिक सत्य इस आपेक्षिक सत्य रूप जगत् का भी अधिष्ठान है।
जगत में जितने भी मंगल कार्य होते है, जैसे व्यापार, विवाह, घर बनाना, देश रक्षा, दान, धर्म और पुण्य आदि, उन सब मे परमात्मा का सहयोग जीव की आस्था एवम श्रद्धा के साथ सद्भावपूर्ण बना रहे। इसलिये सत शब्द द्वारा उन समस्त सात्विक कार्यो को परमात्मा से जोड़ कर मंगलाचार किया जाता है। कुछ लोग पद या प्रसिद्धि के लिये ही सही, लोकसंग्रह हेतु दान- धर्म मे श्रद्धा भाव रखते है यह सत उन के लिये गीता द्वारा स्वीकार किया गया है।
जीव का लक्ष्य मोक्ष को प्राप्त करना है। राजसी सत्वगुण के कर्म करते करते ही जीव निष्काम सात्विक गुण को प्राप्त करता है, फिर निष्काम कर्म करते हुए ही ज्ञानविद होता है और परब्रह को प्राप्त होता है।
संक्षेप में हम यह कह सकते है, वह समस्त कर्म, दैवी – देवता, मांगलिक कार्य और धर्म – संप्रदाय, विचार दान धर्म, क्षमा, अहिंसा, दया आदि सत का स्वरूप है जो हमे परमात्मा से जोड़े रखता है।
बीमार पड़ने पर कार्य नही होता या पंचर होने से गाड़ी नहीं चलती, वैसे सात्विक भाव न होने से ॐ तत् सत् के कार्य ओंकार स्वरूप परमात्मा के बंधन रहित कर्म नहीं हो सकते। यह हम अगले श्लोक में पढ़ते है।
।। हरि ॐ तत सत ।। गीता – 17.26 ।।
Complied by: CA R K Ganeriwala (+91 9422310075)