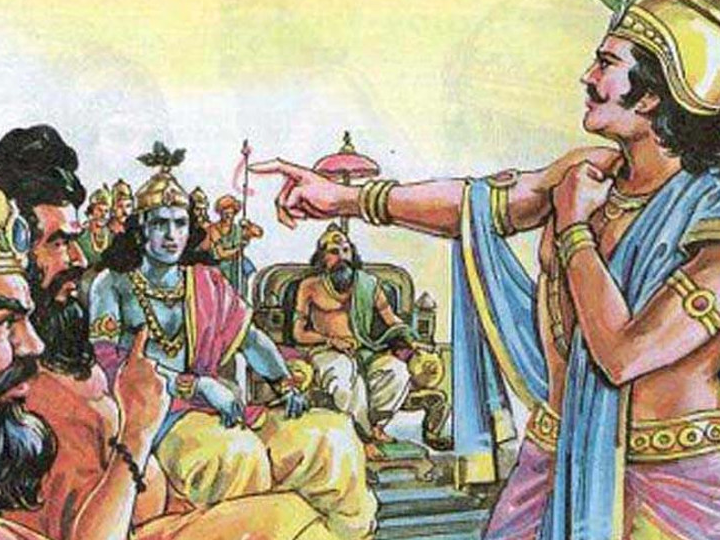।। Shrimadbhagwad Geeta ।। A Practical Approach ।।
।। श्रीमद्भगवत गीता ।। एक व्यवहारिक सोच ।।
।। Chapter 17.20 II
।। अध्याय 17.20 II
॥ श्रीमद्भगवद्गीता ॥ 17.20॥
दातव्यमिति यद्दानं दीयतेऽनुपकारिणे।
देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्त्विकं स्मृतम्॥
“dātavyam iti yad dānaḿ,
dīyate ‘nupakāriṇe..।
deśe kāle ca pātre ca,
tad dānaḿ sāttvikaḿ smṛtam”..।।
भावार्थ:
दान देना ही कर्तव्य है- ऐसे भाव से जो दान देश तथा काल (जिस देश-काल में जिस वस्तु का अभाव हो, वही देश-काल, उस वस्तु द्वारा प्राणियों की सेवा करने के लिए योग्य समझा जाता है।) और पात्र के (भूखे, अनाथ, दुःखी, रोगी और असमर्थ तथा भिक्षुक आदि तो अन्न, वस्त्र और ओषधि एवं जिस वस्तु का जिसके पास अभाव हो, उस वस्तु द्वारा सेवा करने के लिए योग्य पात्र समझे जाते हैं और श्रेष्ठ आचरणों वाले विद्वान् ब्राह्मणजन धनादि सब प्रकार के पदार्थों द्वारा सेवा करने के लिए योग्य पात्र समझे जाते हैं।) प्राप्त होने पर उपकार न करने वाले के प्रति दिया जाता है, वह दान सात्त्विक कहा गया है॥२०॥
Meaning:
That which is donated knowing that charity is duty, to whom one is not obliged, in the right place and time, to a worthy person, that charity is called saattvic.
Explanation:
Every living being in this world knows and understands about the mortal body but does not accept it. He keeps a feeling of insecurity within himself. The child clings to the mother, meaning insecurity is there from birth. The reason for insecurity is considering the mortal body as one’s own, instead of recognising one’s own self. The reason for this is attachment. He searches for this insecurity in worldly things and because of this he starts collecting worldly things. This collection makes him greedy. Greed means collecting more and more for security. By collecting, he does not use his things with everyone and does not even want to share them, due to which his habit becomes miserly. Then the fear of something getting destroyed also haunts him. Therefore, charity is necessary for the cure of attachment, greed, miserliness and fear. It is possible to know one’s own self and live without fear only when we are free from attachment, greed, miserliness and fear. Therefore, charity is of the utmost importance for liberation and salvation. Only a donor can become a sanyasi. But how can the donor and the recipient of donation be in a Satvik spirit, we will read about this later after understanding the importance of donation.
It is an act of duty to give according to one’s capacity. The Bhaviṣhya Purāṇ states: “In the age of Kali, giving in charity is the means for purification.” The Ramayan states this too: “Dharma has four basic tenets, one amongst which is the most important in the age of Kali—give in charity by whatever means possible.” The act of charity bestows many benefits. It reduces the attachment of the giver toward material objects; it develops the attitude of service; it expands the heart and fosters the sentiment of compassion for others. Hence, most religious traditions follow the injunction of giving away one-tenth of one’s earnings in charity. The Skandh Purāṇ states: “From the wealth you have earned by rightful means, take out one-tenth, and as a matter of duty, give it away in charity. Dedicate your charity for the pleasure of God.”
So far, Shri Krishna described the three types of food, sacrifice and penance. Food gives us energy to serve the world, to perform sacrifice. Penance enables us to conserve and channel that energy towards sacrifice. Sacrifice results in a result that is received by the recipient of the sacrifice as well as to us, the performers of the sacrifice. Accumulating results beyond what we need to support ourselves and our family can result in greed. To check this greed, we need to perform daanam or charity.
Now, even the attitude towards charity can reveal a lot about the texture of our faith. Shri Krishna described the characteristics or conditions of charity performed with a saattvic attitude. Conducting charity out of a sense of duty is the first condition. It should come naturally to us, and not because someone has asked us to do it. Charity should never be treated as a business deal. For instance, if someone has done us a favour, we should not give him something in the guise of charity. Furthermore, we should not donate something expecting something in return.
Charity is a sacred act, therefore it has to be performed thoughtfully. Tossing a coin to a beggar on the street may be a noble act, but it does not quality as an act of saattvic charity. It has to be done at the right place and during an auspicious occasion. It also has to be directed towards a worthy person. Shri Shankaraachaarya in his commentary gives the example of the occasion of Sankraanti, the beginning of the month, as an auspicious occasion. He also gives the example of a learned teacher as one who is worthy of receiving a charitable donation.
।। हिंदी समीक्षा ।।
इस संसार में प्रत्येक प्राणी नश्वर शरीर को जानता और समझता है किंतु मानता नहीं है। वह अपने अंदर एक असुरक्षा की भावना रखता है, बच्चा मां से लिपटा रहता है अर्थात असुरक्षा जन्म से ही होती है। असुरक्षा का कारण अपने आत्म स्वरूप को न पहचान कर, नश्वर शरीर को अपना मानना। इस का कारण है मोह। इस असुरक्षा को संसारी चीजों में खोजता है और इस कारण वह संसारी चीजों का संग्रह करने लगता है। यह संग्रह उसे लोभ में डाल देता है। लोभ यानि सुरक्षा के लिए अधिक से अधिक संग्रह। संग्रह से वह सभी के साथ अपनी वस्तुओ को उपयोग में नहीं लाता और बाटना भी नहीं चाहता जिस से उस की आदत कंजूस हो जाती है। फिर कुछ नष्ट न हो जाए, इस का भय भी उसे सताता रहता है। अतः मोह, लोभ, कृपणता और भय, इन सब से निदान के लिए दान आवश्यक है। अपने आत्म स्वरूप को जानना और निर्भय हो कर रहना तभी संभव है जब हम मोह, लोभ, कृपणता और भय से मुक्त हो। इसलिए दान का महत्व मुक्ति और मोक्ष के लिए सर्वाधिक है। दानी ही संन्यासी हो सकता है। किंतु दान दाता और दान लेने वाला सात्विक भाव में कैसे हो, यह हम आगे दान का महत्व समझ कर पढ़ते है।
दान के तीन विभाग है। सामर्थ्यानुसार दान देना मानवीय कर्त्तव्य माना गया है। भविष्य पुराण में कहा गया है “दानमेकम् कलौ युगे” अर्थात् कलि के युग में दान देने का अर्थ शुद्धिकरण है। रामचरितमानस में भी ऐसा कहा गया है: प्रगतचारी पद धर्म के कली महुन्न इक प्रधान । जेन केन बिधि दीन्हें दान कराई कल्याण ।। “धर्म के चार मूलभूत सिद्धांत हैं। कलियुग में इनमें से एक बहुत ही महत्वपूर्ण है, वह है यथासंभव जो भी हो वह दान में दें।” दान करने से कई प्रकार के लाभ होते हैं। दान देने से दानदाता का भौतिक वस्तुओं से मोह कम होता है। इससे सेवाभाव में वृद्धि होती है। इससे हृदय विशाल होता है तथा अन्य लोगों के प्रति करुणा की भावना को बढ़ावा मिलता है। अतः अधिकांश धार्मिक परम्पराएँ अपनी आय का 10वां भाग दान में दिए जाने वाली आज्ञाओं का अनुसरण करती हैं। स्कंदपुराण में उल्लेख किया गया है
न्यायोपार्जित वित्तस्य दश्मानशेन धीमतः। कर्त्तव्या विनियोगश्च ईश्वरप्रीत्यर्थमेव च ।। “उचित साधनों द्वारा और श्रेष्ट बौद्धिक बल द्वारा अर्जित की गई पूंजी में से 10वां भाग निकालकर इसे कर्त्तव्य मानकर दान में दे देना चाहिए। अपने दान को भगवान की प्रसन्नता के लिए अर्पित करो।”
तप के पश्चात दान के स्वरूप की श्रद्धा को भगवान श्री कृष्ण बतलाते है। दान भी तीन गुणों से युक्त सात्विक, राजसी और तामसी होता है। दान के यह गुण दान देनेवाले के भाव और कामना, लेनेवाले की आवश्यकता और दान में दी जानेवाली वस्तु के अनुसार तय होता है। भाव से अभिप्राय हम दान करने वाले की श्रद्धा, प्रेम और विश्वास से ले सकते है कि वह दान करते समय दान ग्रहण करने वाले व्यक्ति के प्रति किसी प्रकार की श्रद्धा, प्रेम और विश्वास के साथ दान कर रहा है।
यदि हम किसी भी व्यक्ति, समाज, देश या विश्व मे ऐसी वस्तु या सेवा को प्रदान करते है जिसे हम भौतिक रूप से अपनी मान रहे है तो वह बिना मूल्य के, ऐच्छिक एवम बिना किसी प्रत्युकार के बदले में, देश एवम स्थान के अनुसार योग्य पात्र को निष्काम भाव से दी जानी चाहिये। निष्काम भाव की प्रधानता का प्रतिपादन करते हुए, यह बताया गया है वर्ण, आश्रम, अवस्था और परिस्थिति के अनुसार शास्त्रविहित दान करना और अपने स्वत्व को यथा शक्ति दूसरो के हित में लगाना ही मनुष्य जीवन का कर्तव्य है।
दान के अर्थववेद का सूक्त है – सौ हाथों के उत्साह एवं प्रयत्न द्वारा हे मानव! धन धान्य आदि का संपादन कर और हजारों हाथों की उदारता द्वारा तू उस का कर, योग्य अधिकारियो में वितरण कर। ऋग्वेद में भी बताया है कि अतिथि, बंधु वर्ग, दरिद्र आदि को न दे कर, केवल आप अकेला ही अन्नादि को खाता है वह अन्न नही अपितु पाप ही खाता है।
यदि किसी सेवा या प्रत्युकार के बदले में कोई दान दिया जाए तो वह कर्तव्य निर्वाह एवम आदान-प्रदान का व्यापार ही माना जाता है क्योंकि ऐसा करते समय मन मे किसी की सेवा या वस्तु के ऋण से उऋण होने की भावना रहती है। जिस वस्तु पर न्यायोचित अधिकार नही है अर्थात चोरी, लूट या अनैतिक तरीके से कमाए धन का दान करना, आध्यात्मिक और सात्विक भाव का दान नही है। इस के अतिरिक्त जो वस्तु अपने लिए अनुपयोगी न हो, उस को नष्ट करने या निकालने के उद्देश्य से किसी को दे देना भी दान नही है।
इसी दान देते वक्त मन मे कुछ पाने की कामना रहती है जिस से यह लोक या परलोक सुधर जाए या नाम, मान या सम्मान चाहिये तो भी यह व्यापार है। भगवान के मंदिर में चढ़ावा, विद्यालय, गौशाला, धर्मशाला या अस्तपताल में दान करते हुए तख्ती लगवाना, इसी श्रेणी में आता है।
किसी ऐसी वस्तु या सेवा को करना जो जिस के प्रति अनुपयोगी हो, तो भी वह दान नही है। जैसे ग्रीष्म ऋतु में कंबल बाटना, भूख से पीडित व्यक्ति को उपदेश देना या किसी रोग से पीड़ित व्यक्ति को वर्जित भोजन देना।
दान के उपयुक्त पात्र दो प्रकार के बताए गए है। प्रथम जो परिस्थितियो से आर्त है, गरीब है और विवश है। जैसे भूकम्प, बाढ़ या दंगो से पीड़ित आदि। इन की निष्काम सेवा एवम सहायता करने में पात्रता नही देखी जाती की वह किस धर्म, जाति या वर्ग से है।
द्वितीय उन पात्रों को लेते है जो ब्राह्मण, वानप्रस्थ-सन्यासी या विद्वान है एवम जिन्होंने ने विद्या दान या ब्रह्म व्रत धारण कर के भिक्षुक वृति को मात्र शरीर को पालन करने स्वीकार किया है, यह लोग संग्रह भी नही करते। प्रथम पात्र के अतिरिक्त दान श्रेष्ठ आचरण वाले विद्वान, उत्तम ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ, संन्यासी और सेवाव्रती लोगो को दिया दान श्रेष्ठ है।
समय और स्थान के लिये भी दान की उपयोगिता बात बताई है कि तीर्थ स्थान, मंदिर, अनाथाश्रम, वृद्धाश्रम, सेवालय आदि स्थान दान के उत्तम स्थान है एवम उत्तम काल भी कालगणना के अनुसार संक्रांति, एकादशी, त्योहार आदि भी है।
आज के युग में बीमार, असहाय, असमर्थ व्यक्ति के लिए रक्तदान, नेत्रदान या अंगदान भी कर के मनुष्य अपने भौतिक शरीर का जीवन मृत्यु के उपरांत भी उपयोग कर सकता है।
भगवान श्री कृष्ण कहते है वही दान सात्विक है जो उपयुक्त पात्र को निष्काम भाव से देश एवम काल के अनुसार बिना किसी प्रत्युकार के दिया जाए। जब अनेक लोगों को उपर्युक्त मत में विश्वास रखकर तदनुसार दान करने में कठिनाई अनुभव होती हो। तो गीता का यह कथन उचित ही है कि मनुष्य को निष्काम हो कर बस इसी बात का विचार करना चाहिए कि उसका दान समाज के योग्य पुरुषों को प्राप्त हो रहा है अथवा नहीं। दान को कर्तव्य समझकर दिये जाने पर वह सात्त्विक दान ही कहलाता है।
इस प्रकार दानवीरों में अनेक नाम है जिन में कर्ण, राजा बलि आदि की कीर्ति की कथाएँ आज भी जन जन से सुनी जा सकती है। आगे हम राजसी दान को पढ़ते है।
।। हरि ॐ तत सत ।। गीता – 17.20 ।।
Complied by: CA R K Ganeriwala (+91 9422310075)