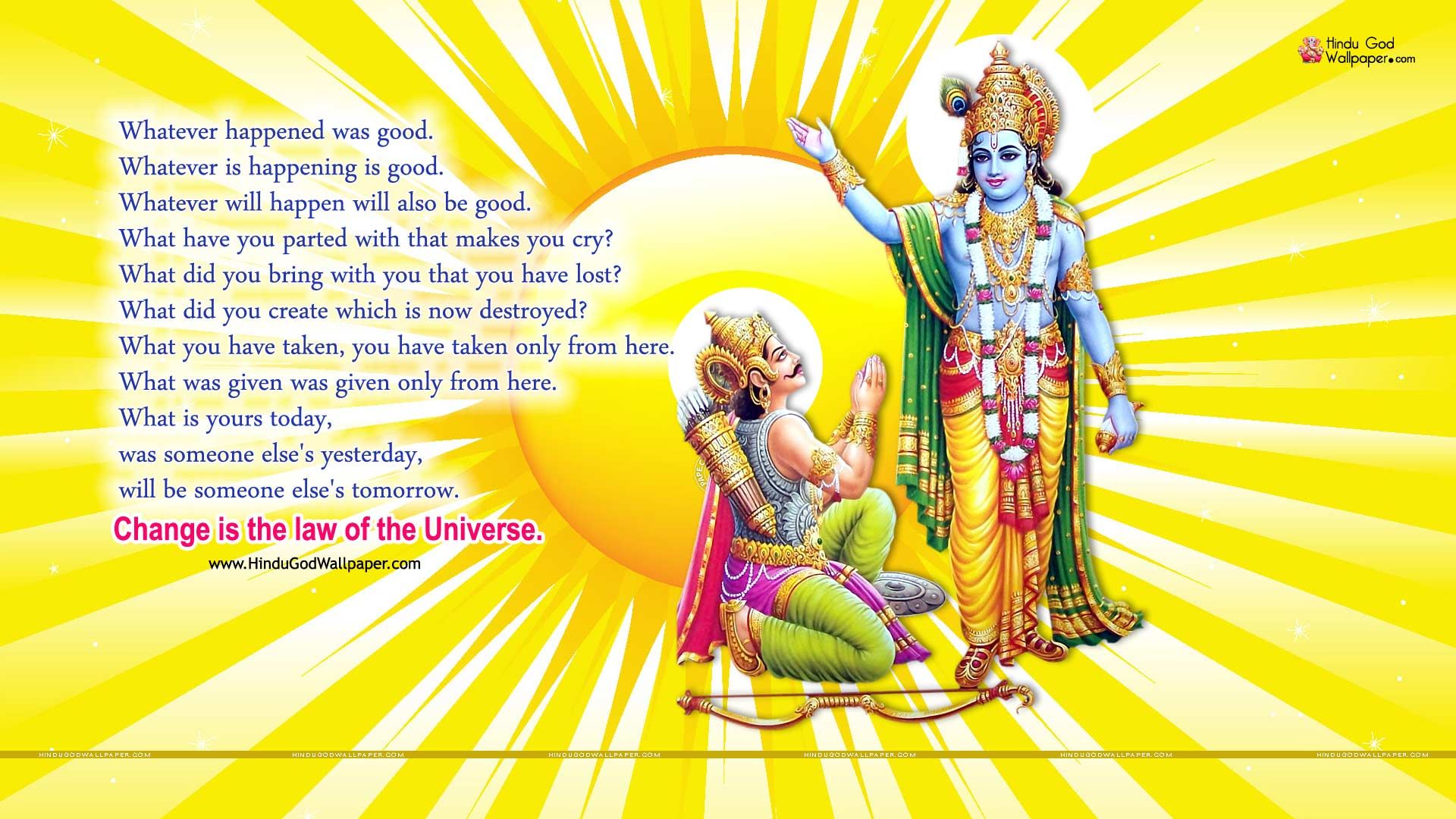।। Shrimadbhagwad Geeta ।। A Practical Approach ।।
।। श्रीमद्भगवत गीता ।। एक व्यवहारिक सोच ।।
।। Chapter 16.S II Summary II
।। अध्याय 16.S II सारांश II
॥ श्रीमद्भगवद्गीता ॥ अध्याय: १६ सारांश॥
ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्नीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन दैवासुरसम्पद्विभागयोगो नाम षोडशोऽध्यायः॥
||ōṃ tatsaditi śrīmadbhagavadgītāsūpaniṣatsu brahmavidyāyāṃ yōgaśāstrē śrīkṛṣṇārjunasaṃvādē daivāsurasampadvibhāgayōgō nāma ṣōḍaśō’dhyāyaḥ||
भावार्थ:
इस प्रकार उपनिषद, ब्रह्मविद्या तथा योगशास्त्र रूप श्रीमद् भगवद् गीता के श्रीकृष्ण-अर्जुन संवाद में दैवासुर संपद्विभाग-योग नाम का सोलहवाँ अध्याय संपूर्ण हुआ ॥
Meaning:
Thus, in the Upaniṣad sung by the Lord, the science of Brahma, The scriptures Yoga, the dialogue between Sri Krishna And Arjuna, ends the sixteenth chapter entitled “The Yoga of division between the Divine And the demonical properties”
॥ हरि: ॐ तत् सत् ॥
Summary of Bhagvad Gita Chapter 16:
The theme of the sixteenth chapter is the analysis of divine and devilish qualities that are present in every human being. Shri Krishna beings by listing all of the divine qualities such as fearlessness and purity of mind. He then provides a similar but brief list of devilish qualities such as ostentation and arrogance. He underscores the point that the divine qualities are a stepping stone towards self-realization and liberation, but the devilish qualities are a slippery slope towards never-ending bondage and sorrow
Next, the philosophy of materialists is analyzed in great detail, because extreme materialism is considered no different than devilish nature. At its core, materialists do not believe in any overarching humanitarian laws or values, since they see the world as nothing but a combination of elements. Material gain is the sole aim of their lives. Anyone or anything that comes in their aim is a target for annihilation.
Shri Krishna says that such people are steeped in delusion and ignorance. Instead of bringing happiness, their infinite desires only bring them infinite worries. These infinite desires bind them and prod them to illegal and unethical means of accumulating wealth. What should I acquire next, whom should I harm next, this becomes their thinking. They develop extreme arrogance and pride towards their family, their wealth and their actions. They totally sever any association with whatever little values and conscience in them.
Such people never realize that by hating everyone they hate Ishvara who dwells in everyone and everything, who is the support of this creation. Although such people think that they are above all laws, they are not above the law of karma. They get the results of their actions in this life and several others to come. Caring only for themselves, they have begun behaving like animals even when they are human. Therefore, they are cast into an endless cycle of births and deaths as animals, insects and other creatures.
Shri Krishna ends this chapter with an extremely practical message. He gives us a simple formula that will give us peace and happiness in this world, and also put us on a fast track to liberation. All we need to do is to avoid the three gates of hell which are desire, anger and greed. We do so by making scripture become the motivator and the prompter of our actions and not selfish desire.
।। सारांश ।। षोडशोSध्याय ।।
गीता में पँचदशोSध्याय में श्री पुरुषोत्तम योग के द्वारा भगवान श्री कृष्ण ने परम ज्ञान से अवगत कराया। किन्तु कोई भी ज्ञान व्यवहारिक होने के लिये उसे के प्रयुक्त मुख्य तत्वों एवम वाक्यों को सही स्वरूप के साथ समझना भी आवश्यक है। अतः आगे के अध्याय में यही बहुत ही सुंदर ढंग से वर्णित है।
सोलहवाँ अध्याय में योगेश्वर श्री कृष्ण ने देवीसम्पद एवम आसुरी सम्पद का विस्तार पूर्वक वर्णन किया है। जिस में ध्यान में स्थिति, सर्वस्व का समर्पण, अन्तःकरण की शुद्धि, इंद्रियाओ का दमन, मन का शमन, स्वरूप को स्मरण दिलानेवाला अध्ययन, यज्ञ के लिये प्रयत्न, मनसहित इंद्रियाओ को तपाना, अक्रोध, चित्त का शांत प्रवाहित रहना आदि 26 लक्षण बताए गए है। जो योग साधना में लगे योगी में सभी मिलते है किंतु कुछ न कुछ मात्रा में सभी मे रहते ही है।
अध्याय में देवीसम्पद एवम आसुरी सम्पद का विस्तार से वर्णन है, जिस का अंत अत्यंत गंभीर और सुंदर ढंग से किया है। प्रथम 3 श्लोकों में देवीसम्पद फिर आसुरी सम्पद गुण है।
जीव एक मक्खन के समान समझे तो यदि मख्खन को एक अच्छे चिकने साफ सुधरे पात्र में रखे तो उस का आनंद भी लंबे समय तक खाने में व अन्य उपयोग में किया जा सकता है किंतु यही मख्खन यदि गंदे, बदबूदार या केरोसिन के पात्र में रख दे तो इस का कोई उपयोग नहीं रहेगा या फिर जो भी उपयोग होगा वह इस के गुण के हिसाब से दुरुपयोग ही होगा।
इसी प्रकार जीव रूपी मख्खन को कामना, भय, क्रोध, हिंसा, पैशुन्य, लोलुपता, चपलता, राग, द्वेष, मान, मोह एवम द्रोह आदि मलयुक्त पात्र के बजाय शम, दम, दान, स्वाध्याय, आर्जव, सत्य, दया, कोमलता, तेज, क्षमा, धैर्य एवं शौच आदि के निर्मल एवम चिकने पात्र में रखे तो इस का सही आनन्द चीर कालीन होगा।
प्रकृति के त्रियामी गुण सत-रज-तम हम ने पढ़े। यह तीनों गुण अस्थायी रहते है एवम जब जिस गुण की प्रधानता हो तो जीव वैसा व्यवहार करता है। किंतु जब सत्व गुण की प्रधानता रज गुण के साथ स्थायी हो तो उसे देवीसम्पद एवम जब तम गुण की प्रधानता रज गुण के साथ स्थायी हो तो आसुरी सम्पद कहेंगे। यह प्रकृति के दो नए गुण भी कहे जा सकते है।
देवीसम्पद गुणों के बाद आसुरी सम्पद लोग काम, अशौच, कठोरता एवम असत्य के वातावरण में जीते है, बताया गया है। जिस के कारण अहंकार जन्म लेता है और अपने सांसारिक सुखों के नीति नियमो को ताक में रख कर यह लोग अपने सुख के लिए किसी को भी धोखा, हत्या या कोई भी कष्ट देने से नही परहेज करते है। यह लोग स्वयं को ईश्वर तक घोषित कर देते है।
इस प्रकार आसुरी सम्पद लोगो की प्रकृति एवम स्वभाव का वर्णन करने के बाद, भगवान श्री कृष्ण बतलाते है कि उन्हें अपने कर्मो के कारण घोर कष्टों का सामना करना पड़ता है एवम जन्म मरण के चक्कर मे निम्नतर योनि में जन्म लेना पड़ता है। अर्थात नरक के समस्त दुख इन के हिस्से में आते है।
इस के बाद काम, क्रोध एवम लोभ तीन मुख्य नरक के द्वार बताया गया। जीव को इन तीन गुणों को त्याग करके अपने को आसुरी सम्पद गुण से अपने को बचा कर रखना चाहिए।
मनुष्य जीवन इतना सरल नहीं है जिसे हम जैसा चाहे वैसा जी सके। कर्मयोग जीवन मे अनेक बार ऐसे प्रसंग या घटनाक्रम आते है जो मनुष्य को निर्णय लेने के लिये किंकर्तव्यविमूढ़ स्थिति में खड़ा कर देते। यह अक्सर परस्पर विरुद्ध दो धर्मो के कर्तव्य-अकर्तव्य की स्थिति में आता ही है। युद्ध भूमि में अपने सामने खड़े स्वजनों को देख कर अर्जुन के मन मे मोह उत्पन्न हुआ एवम मोह से युक्त हो कर उस ने शास्त्रों से युक्त बाते करते हुए अकर्तव्य का मार्ग चुनने की बाते करने लगा। किन्तु यहां उस को बचाने एवम सही मार्ग दिखाने के लिये कृष्ण थे, जिन्होंने पूरी गीता का ज्ञान दिया। कहते है ऐसी ही स्थिति युधिष्ठर की भी युद्ध के उपरांत स्वजनों का श्राद्ध करते समय हुई थी, जिस में उस ज्ञान की प्राप्ति कैसे हुई, यह महाभारत के शांतिपर्व में बताया गया है।
कर्तव्य-अकर्तव्य के बीच मे संशय कोई अनोखी बात नही है। प्रसिद्ध अंग्रेजी के नाटककार शेक्सपियर के हैमलेट नामक नाटक में राजपुत्र की मनःस्थिति का वर्णन किया है, जिस में उस के पिता के हत्यारे चाचा, जिस ने न केवल उस के पिता को मारा, उन की पत्नी से विवाह कर के राजा भी बन गया। इस राजपुत्र को समझ नही आ रहा कि वह चाचा से पिता की हत्या का बदला ले या दया कर के अपनी माँ के जीवन को शांति से रहने दे। भगवान श्री कृष्ण सरीखा मार्गदर्शक न होने से बेचारा कर्तव्य-अकर्तव्य में अनिर्णीत हो कर पागल सा हो गया।
ऐसा ही प्रसंग शेक्सपियर के अन्य नाटक कोरियोलेन्स में कोरियोलेन्स नामक शूरवीर का है जिसे देश निकाला मिला और वह दुश्मनों से जा मिला। वहाँ उस मे प्रतिज्ञा की वह उन लोगो का साथ कभी भी नही छोड़ेगा। किन्तु अपने ही देश पर हमला करते वक्त जब उस की मां एवम पत्नी से उस को उस के कर्तव्य की याद दिलाते हुए, देश का साथ देने की प्रार्थना की, तो उस ने निर्णय लेते हुए अपनी प्रतिज्ञा का त्याग कर के देश के लिये लड़ने का निर्णय लिया।
धर्म, सत्य, नैतिकता एवम नीति यह निर्णय लेने के चार स्तम्भ माने गए है किंतु समय एवम स्थान के अनुसार इन मे परिवर्तन होता गया। इन के बारे में यदि विस्तार से कही वर्णन है तो वह हमारे धर्म ग्रंथ है जिन्हें सत्वगुण के युक्त ब्रह्मसन्ध ऋषि-मुनि एवम ज्ञानी लोगो ने वेद, उपनिषद, श्रुतियां, स्मृतियां, पुराण आदि संजो कर रखा है। यही हमारे लिए मार्गदर्शक भी है। भगवान श्री कृष्ण कहते है कि जब भी अनिर्णय की स्थिति तो हमे शास्त्र के अनुसार ही कार्य करना चाहिए।
जब व्यक्ति काम, क्रोध एवम लोभ से ग्रसित होता है तो वह शास्त्रों के अर्थ का अनर्थ करता है। अक्सर हम ने देखा है कोई भी कार्य करने के लिये हम पंडित को कहते है तो वह भी जजमान की इच्छा एवम अपनी दक्षिणा के लालच में शास्त्र में से ही कोई उपाय निकालता है, यदि वह ऐसा न करे तो उस कर्म के फल के मोह में यजमान पंडित बदलना पसंद करता है। अतः शास्त्र के अनुसार भी कार्य करने के लिये हमें काम, क्रोध एवम मोह से मुक्त निष्काम कर्मयोगी होना ही पड़ेगा। अतः यह भी निश्चित है धर्म एवम सत्य के आचरण को तय करते समय यदि मन काम, क्रोध या लोभ से ग्रस्त है तो धर्म एवम सत्य को अपने अनुकूल बनाने की चेष्टा करता है। इसे शास्त्रों का मन माना निरादर ही मानना चाहिए।
जब अनिर्णय के क्षण आते है तो अक्सर यह कहा जाता है जो तेरा मन कहे वह कर। मन जीव का सब से महत्वपूर्ण प्रकृति स्वरूप है क्योंकि दस इंद्रियाओ का वो ही ज्ञाता है, यह इंद्रियाए मन के बिना शून्य है। मन न हो तो आँखे नही देखती, कान नही सुनते यहाँ तक बुद्धि भी काम नही करती। यही मन काम, क्रोध एवम मोह से ग्रसित हो कर गलत -सही करता रहता है किंतु यदि यही मन जब काम-क्रोध-लोभ से मुक्त हो तो सदचिदानन्द स्वरूप होता है। इस मन से जो निर्णय लिया जाता है वो गलत नहीं हो सकता। शुद्ध मन परमात्मा की ही आवाज होता है। ऐसा कौन व्यक्ति हो सकता है जिसे मन ने गलत काम करते वक्त न टोका हो। उस को सुना वही करता है जो काम, क्रोध या लोभ से ग्रसित है।
कुछ लोगो का कथन है गीता में भगवान स्वजनों से लड़ने एवम हत्या के लिये प्रेरित करते है, ऐसे व्यक्ति मोह ग्रस्त होते है। कृष्ण भगवान ने युद्ध को टालने के अंतिम प्रयास पांच गांव तक लेने तक किया किन्तु परिस्थितियो को कुछ और मंजूर था। आसुरी प्रवृति ही दुर्योधन एवम उस से वचन, कर्तव्य एवम अपने मोह से ग्रसित लोगो को युद्ध भूमि तक लाये। अतः जब सब रास्ते बंद हो जाये और आप युद्ध भूमि में खड़े हो तो भी भगवान कर्तव्य धर्म का पालन बिना काम, क्रोध एवम मोह के निष्काम करने को कहते है क्योंकि इस के अतिरिक्त अर्जुन जैसे क्षत्रिय के कोई मार्ग है नहीं।
मनुष्य चाहे या न चाहे, परिस्थितियां उसे उस स्थान पर खड़ा कर ही देती है जहां उसे कुछ न कुछ निर्णय लेना आवश्यक हो जाता है। अर्जुन अपनी इच्छा से युद्ध नही चुनता किन्तु यदि परिस्थिति ने उसे युद्ध भूमि में खड़ा कर दिया तो भगवान उसे उपदेश देते है कि नियतं कुरु कर्म त्वम यज्ञ की प्रक्रिया में जो तुम्हारा नियति ने कर्म तय कर दिया है उसे बिना काम, क्रोध एवम लोभ के साथ पूरा करो। यही तुम्हारा कर्तव्य धर्म है अब किस से युद्ध करना है, हार होगी या जीत, सब त्याग कर अपने कर्म को निष्काम भाव से करो और अपने धर्म का शास्त्रों से युक्त पालन करो। परमात्मा दया का सागर है वो जो भी निर्णय लेता है उस के अन्तर्हित में कल्याण की भावना रहती है क्योंकि वह प्रकृति एवम जीव दोनों का ही स्वामी है।
प्रकृति की कार्य विधि में कुछ कार्य अपने अपने स्वभाव से होते है। शरीर कसरत करने से बलिष्ठ होता ही है, अग्नि का स्वभाव तेज का है, वह जिस के संपर्क में आएगी, उसे जला देगी। इसी प्रकार व्यवसाय, व्यापार, रण कुशलता, शिक्षा प्रकृति के स्वाभाविक गुण है, जो इस दिशा में मेहनत करेगा, वह कुशल और योग्य होगा। किंतु दैवीय तत्व और आसुरी तत्व मनुष्य के अधिकार क्षेत्र के तत्व है। मनुष्य दैवीय तत्व से परमात्मा की ओर अधिक निकटम होता है, वह मानसिक शांति एवम आनंद का अनुभव करता है और आसुरी तत्व काम, क्रोध और लोभ में मनुष्य निम्न स्तर पर गिरता जाता है और मानसिक बैचेनी, तनाव, खिन्नता एवम अधोगति को प्राप्त होता है। पढ़ा लिखा होना, ज्ञानी होना, अध्ययन शील, पूजा पाठी होना किसी को उच्च कोटि का व्यक्ति या श्रेष्ठ नही बनाती, यह गुण रावण, कंस, हिटलर, ओसामा बिन लादेन या आतंकवादियों में भी हो सकते है, किंतु यह संसार दैवीय गुणों से युक्त मनुष्य को ही चिरकाल तक सम्मानित करता है।
इस अध्याय में कर्तव्य धर्म के पालन एवम स्वयं को आसुरी सम्पद से मुक्त रहने का अत्यंत सुंदर वर्णन है। हमे ध्यान रखना चाहिए कि पाप-पुण्य के तत्व को इस मे कोई स्थान नहीं दिया गया है। जब कर्तव्य धर्म का पालन किया जाता है और यदि काम, क्रोध एवम मोह से मुक्त है तो उस के किये कार्य निष्काम कर्मयोग है , निष्काम कर्मयोग ही गीता का प्रमुख ज्ञान भी है अतः शास्त्र को मध्य रखते हुए कर्तव्य पालन पर अधिक जोर दिया है। जब कर्म निष्काम है तो जीव उस कर्म फल से लिप्त भी नही रहता, इसलिये पाप-पुण्य को गौण मानते हुए, उसे शास्त्रों पर छोड़ दिया गया है। यही इस अध्याय का सार है।
।। हरि ॐ तत सत।। सारांश – अध्याय 16 ।।
===================================================================
Complied by: CA R K Ganeriwala (+91 9422310075)