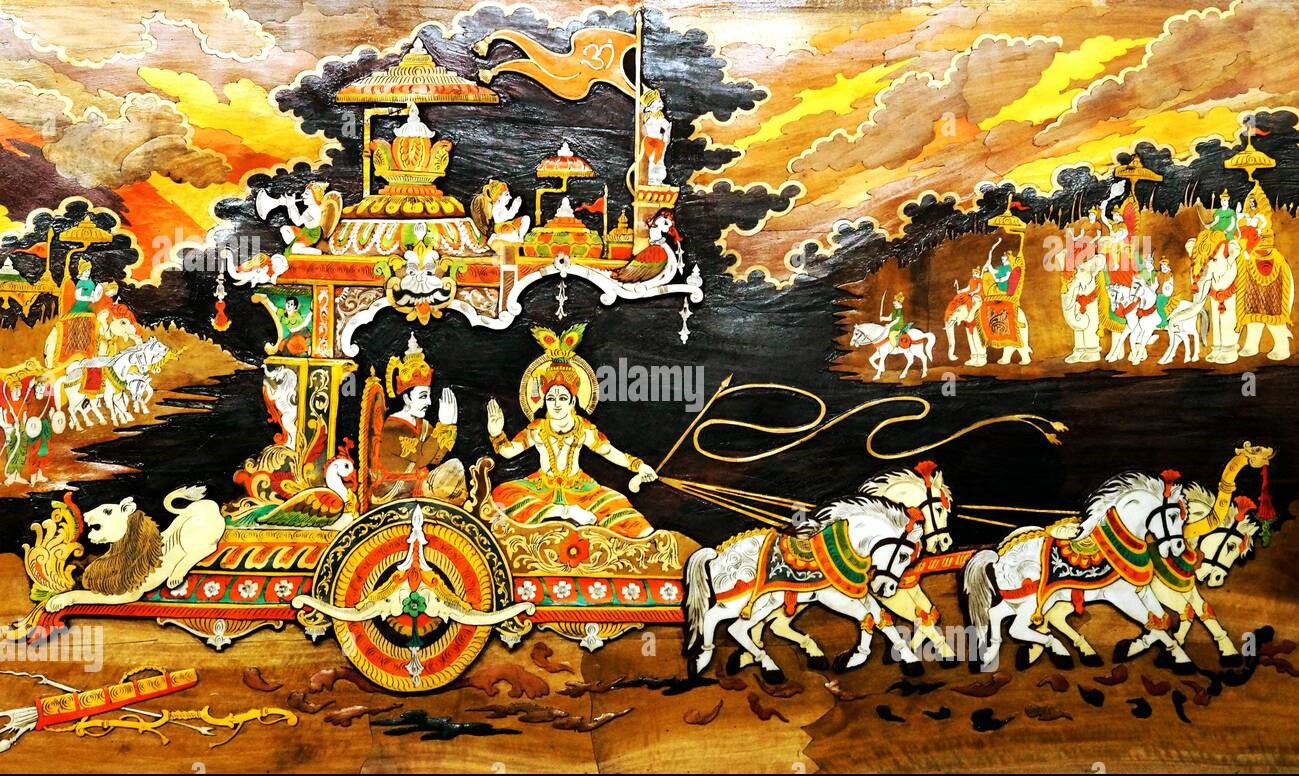।। Shrimadbhagwad Geeta ।। A Practical Approach ।।
।। श्रीमद्भगवत गीता ।। एक व्यवहारिक सोच ।।
।। Chapter 16.14 II Additional II
।। अध्याय 16.14 II विशेष II
।। दर्शनशास्त्र – भारतीय वैदिक (आस्तिक) दर्शन – मीमांसा 2।। विशेष भाग 7, गीता 16.14 ।।
विधि
प्रत्यक्ष, अनुमान आदि से अनवगत (अज्ञात) अर्थ के बोधक वाक्य को विधि कहते हैं अर्थात् अज्ञातज्ञापक अप्रवृत्तप्रवर्तक जो वाक्य हैं उस का नाम “विधि” है। विध्यर्थ के संबंध में मीमांसकों के दो पक्ष हैं – एक प्रवर्तना को विध्यर्थ मानता है। इस में प्रायशः सभी मीमांसक आ जाते हैं। दूसरा कार्य को विध्यर्थ मानता है। यह प्रभाकर का सिद्धांत है। इस पक्ष में इस प्रकार का उत्पादन होता है।
लोक में प्रवर्तक पुरुष, आचार्य अथवा राजा अपने शिष्य अथवा भृत्य को प्रवृत्त कराने के लिए “गामानय” इत्यादि वाक्य का प्रयोग करते है। शिष्य या भृत्य उक्त वाक्य को सुनकर उस के अर्थ का अनुसंधान करता है। पश्चात् “गवानयन” (गाय लाने) आदि कार्य में प्रवृत्त होता है। इसलिए प्रवर्तक पुरुष का जो अभिप्राय विशेष है, उसे लोक में विध्यर्थ कहते हैं। वह पुरुष की क्रिया है जो पुरुष में रहती है। अतएव इसे पुरुषाभिप्राय भी कहते हैं। वेद अपौरुषेय होने के कारण वैदिक लिंगादि का अर्थ पुरुषाभिप्राय नहीं कहा जा सकता। अतः पुरुष के स्थान पर लिंगादि (लिंग लुंग आदि लकार) शब्द का प्रयोग होता है।
उस का व्यापार विशेष ही विध्यर्थ है। शब्दनिष्ठ होने के कारण इसे शाब्दी भावना भी कहते हैं। इस का लक्षण इस प्रकार किया गया है “पुरुषप्रवृत्यनुकूलः प्रवर्तक लिंगादिनिष्ठो व्यापारविशेषः शाब्दी भावना”। शास्त्र में इसे ही प्रवर्तना, प्रेरणा आदि कहा गया हैं। लोक में प्रवृत्ति दो प्रकार की होती है – प्रथम अपनी इच्छा से (इष्ट साधन समझकर) पुरुष प्रवृत्त होता है। द्वितीय प्रवर्तक पुरुष, अथवा शब्द के द्वारा व्यक्ति प्रवृत्त होता है, जिसे “प्रेरणा जन्य” कहते हैं। जहाँ प्रेरणा के पश्चात् प्रवृत्ति होती है, वहाँ प्रवर्तन ज्ञान ही प्रवर्तक माना जाता है, जिसे मंडन मिश्र, पार्थसारथि प्रभृति विद्वानों ने “इष्टसाधन” माना है। न्याय सुधाकर ने इसे अलौकिक धर्म विशेष माना है। प्रभाकर मिश्र ने प्रवृत्ति के प्रति कार्यताज्ञान को कारण माना है, जिससे इष्ट साधनत्व आदि आक्षिप्त हो जाता है। अतः “चोदना लक्षणो धर्मः” सूत्र में लिखा है – “आचार्य चोदित” करोमि” इस भाष्य की व्याख्या करते हुए शालिकनाथ ने कहा है – चोदितः प्रवर्तितः, कार्यमवबोधितः इत्यर्थः, कार्यताज्ञान विना प्रवृत्तेरसंभवादिति” (तदभूतादि प्र0 पं0) अतएव प्रभाकर मत में कहा गया है – “कार्य विध्यर्थः, तच्च कार्य धात्वर्थातिरिक्तम्, अपूर्व शब्द वाच्यम् तदेव विध्यर्थ इति”
विधि का भेद
वेद वाक्यार्थ निर्णय के लिए प्रवृत्त मीमांसा दर्शन में चार प्रकार की विधि का प्रतिपादन किया गया है।
(1) उत्त्पत्तिविधि: जिस वाक्य से कर्म स्वरूप की कृत्रव्यता प्रथमतः विदित होती हो उसे उत्पत्ति विधि कहते हैं। उदाहरणार्थ “अग्निहोत्रं जुहोति” इस वाक्य से अग्निहोत्र नामक होम से इष्ट को प्राप्त करना अर्थ होता है।
(2) विनियोग विधि: अंगप्रधान का संबंध जिस विधिवाक्य से ज्ञात होता है, उसे विनियोगविधि कहते हैं। उदाहरणार्थ “दध्ना जुहोति” इस वाक्य से दही से हवन करने का अर्थ बोधित होता है। इस में दधि साधन है और होम साध्य है। यहाँ विनियोग विधि में विनियोग शब्द से संबंध को समझना चाहिए। वह संबंध साध्य-साधन-भाव, अंगांगि भाव अथवा शेषशेषी भाव में समाप्त होता है।
(3) प्रयोगविधि: जो प्रधान और अंग के अनुष्ठान में क्रम का बोध कराता है उसे प्रयोगविधि कहते हैं। उदाहरणार्थ प्रयाजादि अंग से उपकृत प्रधान दर्शपूर्णमास याग से स्वर्ग की प्राप्ति होती है। इसी अभिप्राय से लक्षण किया गया है “अंगानां क्रमबोधको विधि; प्रयोगविधिः”
(4) अधिकारविधि: जिस विधि से कर्मजन्य फल का भोक्ता कर्ता को माना जाता हो उसे अधिकार विधि कहते हैं। उदाहरणार्थ “यजेत स्वर्ग कामः” यहाँ जो यागकर्ता है वही स्वर्गफल का भोक्ता है।
इसी प्रकार से अपूर्व विधि, नियम विधि और परिसंख्या विधि के भेद से तीन प्रकार की विधियाँ प्रसिद्ध हैं –
(क) जो अत्यन्त अप्राप्य विषय का विधान करता हो उसे अपूर्व विधि कहते हैं। उदाहरणार्थ “ब्रीहीन् प्रोक्षति, दर्शपूर्ण मासाभ्यां स्वर्गकामो यजेत” यहाँ ब्रीही में प्रोक्षण क्रिया का विधान है और दर्शपूर्णमास में स्वर्ग के साधन का विधान है। यह बात उपर्युक्त वाक्यों के अतिरिक्त अन्य प्रमाणों से सर्वदा और सर्वथा अप्राप्त है। अतः यह अपूर्वविधि है।
(ख) जो पक्ष प्राप्त अर्थ को नियमित (अप्राप्तांश पूरक) करता है उसे नियमविधि कहते हैं। उदाहरणार्थ “ब्रीहीन् अवहंति”। यहाँ वैतुष्य के प्रति अवधात साधन है। ऐसे ही अश्म कुट्टनादि साधन है। जो पुरुष शास्त्रीय उपाय अवधात को त्यागकर अश्म कुट्टनादि या नखविदलनादि से वैतुष्य करता हो उसे शास्त्रीय विधि के अनुसार अवधात से ही वैतुष्य करना चाहिए – “ब्रीहीनवहन्यादेव” यहाँ अवधात के प्रत्यक्ष होने पर भी अवधात नियम अप्रत्यक्ष है।
(ग) जहाँ एक काल में दो समुच्चय से प्राप्त हों और उनमें एक की व्यावृत्ति (निवृत्ति) करना ही जिसका फल हो उसे परिसंख्या विधि कहते हैं। उदाहरणार्थ – ‘पंच पंचनखा भक्ष्याः’ यह पंचनख भक्षण राग प्राप्त होने के कारण इसका विधान नहीं करता। पंचनखेतर पंचनख भक्षण भी प्राप्त है अर्थात् राग से पंचनखवाले पाँच का भक्षण जैसे प्राप्त होता है वैसे ही पंचनख से भिन्न पंचनखवालों का भी भक्षण रागतः प्राप्त है।
इसलिए यहाँ अपूर्व विधि या नियम विधि नहीं। पंचेतर पंचनख भक्षण निवृत्ति है। इसलिए यह परिसंख्याविधि का उदाहरण है। नियम विधि में इतर निवृत्ति का वाचक शब्द नहीं किंतु अर्थात् होती है। परिसंख्या विधि में इतर निवृत्ति का बोधक शब्द रहता है। एवकार का दोनों में प्रयोग होता है। लेकिन नियमविधि में एवकार अयोग व्यावृत्ति का बोधक है और परिसंख्याविधि में एवकार अन्य योग व्यावृत्ति का बोधक है।
ऊपर विधियों के दो प्रकार बताए गए हैं, उसे इस प्रकार समझना चाहिए कि अपूर्वविधि में उत्पत्ति, विनियोग प्रयोग और अधिकार विधि चारों अंतर्गत होते हैं। नियम तथा परिसंख्या विधि, विनियोग विधि में ही अंतर्गत है। इस विषय का विशेष ज्ञान भाट्ट चिन्तामणि में द्रष्टव्य है।
पूर्वमीमांसा में वर्णित अर्थीकरण के सिद्धान्त
मीमांसा दर्शन में वाक्यार्थ करने की प्रक्रिया भी समझाई गई है, विशेषकर वैदिक वाक्यों के अर्थ करने की प्रक्रिया। सबसे पहले कुछ ऐसे सिद्धान्त बताए गए हैं, जिनके आधार पर अर्थनिर्धारण करना चाहिए।
(१) सार्थक्यता – प्रत्येक शब्द व वाक्य को सार्थक समझना चाहिए, व उसकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। कारिका में इस सिद्धान्त की व्याख्या की गयी है।
शब्दाधिक्यात् अर्थाधिक्यम् ( अर्थ – जितने ही अधिक शब्द प्रयुक्त होते हैं, उतने ही अधिक अर्थ निकलते हैं।)
(२) लाघव – जहां एक नियम पर्याप्त हो, वहाँ अन्यों का ग्रहण नहीं करना चाहिए। वेदों में यह चर्चा बहुत काल से रही है कि मन्त्रों के दोबारा, तिबारा पढ़े जाने से वहां पुनरुक्ति दोष है।
(३) अर्थैकत्व – एक स्थान पर एक पद अथवा वाक्य का एक ही अर्थ ग्रहण करना चाहिए, अनेक नहीं। (यह निर्देश तो वेदों पर कहीं नहीं घटता। वेदों के पदों अथवा मन्त्रों के तीन अर्थ – आधिदैविक, आधिभौतिक और आध्यात्मिक – तो लगभग सर्वत्र ही घटते हैं, और इन से अधिक अर्थ भी यत्र- तत्र सम्भव हैं। प्रतीत होता है कि यह सिद्धान्त ब्राह्मण, स्मृति आदियों के लिए ही निर्दिष्ट है । इससे यहां कुछ सन्देह भी हो जाता है कि पूर्वमीमांसा के सिद्धान्त वेदों के लिए हैं भी या केवल इतर ग्रन्थों के लिए।)
(४) गुणप्रधान – यदि कोई पद वा वाक्य उत्सर्ग वाक्य के विपरीत हो, तो उत्सर्ग वाक्य को या तो अपवाद वाक्य के अनुसार कुछ परिवर्तित कर देना चाहिए, या फिर पूर्णतया त्याग देना चाहिए। (गुणमुख्यव्यतिक्रमे तदर्थत्वान्मुख्येन वेदसंयोगः) धर्म- विषय में इस को ऐसे समझना चाहिए – प्राणी हिंसा वर्जित है, परन्तु राजा और क्षत्रियों के लिए यह किन्हीं स्थितियों में निर्दिष्ट है, जैसे दण्ड देने अथवा राष्ट्र-रक्षा में। पाणिनि की अष्टाध्यायी तो सम्पूर्णतया इसी आधार पर लिखी गई है। प्रतीत होता है यह पद्धति हमारे ग्रन्थों में आरम्भ से चली आ रही है।
(५) सामञ्जस्य – जहां भी वैपरीत्य प्रतीत हो रहा हो, वहां पहले पदों वा वाक्यों में सामंजस्य बैठाने का प्रयत्न करना चाहिए।
(६) विकल्प – जहां अपरिहार्य वैपरीत्य है, वहां दोनों पदों वा वाक्यों में से किसी का भी ग्रहण किया जा सकता है । यह निर्देश प्रक्रियाओं, विशेषकर याज्ञिक प्रक्रियाओं से अधिक सम्बद्ध है । जैसे – किसी अनुष्ठान में एक स्थल पर दूध के प्रयोग का निर्देश हो, अन्यत्र जल का, तो दोनों में से किसी का भी प्रयोग किया जा सकता है।
अर्थनिर्धारण के विधान
नीचे पूर्वमीमांसा में कुछ विशेष विधान दिए गए हैं जिनसे अर्थ ग्रहण किया जाए –
श्रुति- लिङ्ग- वाक्य- प्रकरण- स्थान- समाख्यानां समवाये परदौर्ब ल्यमर्थविप्रकर्षात्
(१) श्रुति – जब क्रियापद व उससे सम्बद्ध संज्ञापद स्पष्ट अर्थ व्यक्त करते हैं, वाक्यार्थ सुनने से ही ज्ञात हो जाता है, तो उस अर्थ को वैसे ही ग्रहण कर लेना चाहिए, उसमें और तोड़-मरोड़ नहीं करनी चाहिए।
(२) लिङ्ग – जिस में शब्द अथवा वाक्य किसी अन्य वस्तु व तथ्य के संकेत होते हैं, और वाक्य को समझने के लिए उस संकेत को समझना आवश्यक होता है । इसको लोक में लक्ष्यार्थ कहा जाता है, जैसे जब हम कहते है, “रिक्शा, इधर आओ!”, तब हम रिक्शा को नहीं, अपितु रिक्शा-चालक को सम्बोधित कर रहे होते हैं – ‘रिक्शा’ चालक का लिङ्ग है।
(३) वाक्य – जब पढ़ा गया वाक्य लगता तो पूर्ण है, परन्तु उस का अर्थ वास्तव में सही नही बैठता, तब उसके अर्थ को पूर्ण करने के लिए कहीं और से किसी अन्य पद व वाक्यांश का अध्याहार करना होता है।
मीमांसादर्शन के कुछ मौलिक सिद्धान्त
(१) वेद नित्य स्वयंभू एवं अपौरुषेय और अमोघ है।
(२) शब्द और अर्थ का सम्बन्ध नित्य है, वह किसी व्यक्ति के द्वारा उत्पन्न नही है।
(३) आत्माएँ अनेक नित्य एवं शरीर से भिन्न हैं। वे ज्ञान एवं मन से भी भिन्न हैं। आत्मा का निवास शरीर में होता है।
(४) यज्ञ में हवि प्रधान है और देवता गौण।
(५) फल की प्राप्ति यज्ञ से ही होती है, ईश्वर या देवताओं से नहीं।
(६) सीमित बुद्धि वाले लोग वेदवचनों को भली भांति न जानने के कारण भ्रामक बातें करते हैं।
(७) अखिल विश्व की न तो वास्तविक सृष्टि होती है और न ही विनाश।
(८) यज्ञसम्पादन सम्बन्धी कर्म एवं फल के बीच दोनों को जोड़ने वाली “अपूर्व” नामक शक्ति होती है। यज्ञ का प्रत्येक कृत्य एक “अपूर्व” की उत्पत्ति करता है, जो सम्पूर्ण कृत्य के अपूर्व का छोटा रूप होता है।
(९) प्रत्येक अनुभव सप्रमाण होता है, अतः वह भ्रामक या मिथ्या नहीं कहा जा सकता।
(१०) महाभारत एवं पुराण मनुष्यकृत हैं, अतः उनकी स्वर्गविषयक धारणा अविचारणीय है। स्वर्गसम्बन्धी वैदिक निरूपण केवल अर्थवाद (प्रशंसा पर वचन) है।
(११) निरातिशय सुख ही स्वर्ग है और उसे सभी खोजते हैं।
(१२) अभिलषित वस्तुओं की प्राप्ति के लिए वेद में जो उपाय घोषित है वह इह या परलोक में अवश्य फलदायक होगा।
(१३) निरतिशय सुख (स्वर्ग) व्यक्ति के पास तब तक नही आता जब तक वह जीवित रहता है। अतः स्वर्ग का उपभोग दूसरे जीवन में ही होता है।
(१४) आत्मज्ञान के विषय में उपनिषदों की उक्तियां केवल अर्थवाद है क्योंकि वे कर्ता को यही ज्ञान देती हैं कि वह आत्मवान् है और आत्मा कि कुछ विशेषताएं हैं।
(१५) निषिद्ध और काम्य कर्मों को सर्वथा छोड़ कर नित्य एवं नैमित्तिक कर्म निष्काम बुद्धि से करना ही मोक्ष (अर्थात् जन्म मरण से छुटकारा) पाने का साधन है।
(१६) कर्मों के फल उन्ही को प्राप्त होते हैं जो उन्हे चाहते हैं।
(१७) प्रत्यक्ष ज्ञान के दो भेद होते है: – (१) निर्विकल्प (२) सविकल्पक।
(१८) वेदों के दो प्रकार के वाक्य होते हैं:– सिद्धार्थक (जैसे– ‘सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म)’ और विधायक। वेद का तात्पर्य विधायक वाक्यों में ही है।
सिद्धार्थक वाक्य अन्ततो गत्वा विधि वाक्यों से संबंधित होने के कारण ही चरितार्थ होते हैं।
(१९) वेदमन्त्रों में जिन ऋषियों के नाम पाये जाते हैं वे उन मन्त्रों के “द्रष्टा” होते हैं, कर्ता नहीं।
(२०) स्वतः प्रामाण्यवाद: – ज्ञान की प्रामाणिकता या यथार्थता कही बाहर से नही आती अपितु वह ज्ञान की उत्पादक सामग्री के संग में अपने आप उत्पन्न होती है।
(२१) ज्ञान उत्पन्न होते ही उस के प्रामाण्य का ज्ञान भी उस समय होता है। उस की सिद्धि के लिए अन्य प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती।
(२२) ज्ञान का प्रामाण्य स्वतः होता है किन्तु उसका अप्रामाण्य “परतः” होता है।
(२३) यह संसार भोगायतन (शरीर), भोगसाधन (इन्द्रियां) और भोगविषय (शब्दादि) इन तीन वस्तुओं से युक्त तथा अनादि और अनन्त है।
(२४) कर्मों के फलोन्मुख होने पर अणुसंयोग से व्यक्ति उत्पन्न होते हैं और कर्म फल की समाप्ति होने पर उनका नाश होता है।
(२५) कार्य की उत्पत्ति के लिए उत्पादन कारण के अतिरिक्त “शक्ति” की भी आवश्यकता होती है। शक्तिहीन उत्पादन कारण से कार्योत्पत्ति नहीं होती।
(२६) आत्मा – कर्ता, भोक्ता, व्यापक और प्रतिशरीर में भिन्न होता है। वह परिणामशील होने पर भी नित्य पदार्थ है।
(२७) आत्मा में चित् तथा अचित् दो अंश होते हैं। चिदंश से वह ज्ञान का अनुभव पाता है और अचित् अंश से वह परिणाम को प्राप्त करता है।
(२८) आत्मा चैतन्यस्वरूप नहीं अपि तु चैतन्यविशिष्ट है।
(२९) अनुकुल परिस्थिति में आत्मा में चैतन्य का उदय होता है, स्वप्नावस्था में शरीर का विषय से सम्बंध न होने से आत्मा मे चैतन्य नही रहता।
(३०) कुमारिल भट्ट आत्मा को ज्ञान का कर्ता तथा ज्ञान का विषय दोनों मानते हैं, परन्तु प्रभाकर आत्मा को प्रत्येक ज्ञान का केवल कर्ता मानते है क्योंकि एक ही वस्तु एकसाथ कर्ता तथा कर्म नहीं हो सकती।
(३१) भूत, भविष्य, वर्तमान, सूक्ष्म, व्यवहित और विप्रकृष्ट पदार्थों को बतलाने में जितना सामर्थ्य “चोदना” में (अर्थात् विधि प्रतिपादक वेदवाक्यों में) है उतना इन्द्रियों या अन्य प्रमाणों में नहीं है।
(३२) नित्य कर्मों के अनुष्ठान से दुरितक्षय (पापों का नाश) होता है। उनके न करने से प्रत्यवाय दोष उत्पन्न होता है।
(३३) देवता शब्दमय या मन्त्रात्मक होते हैं। मन्त्रों के अतिरिक्त देवताओं का अस्तित्व नहीं होता।
(३४) प्राचीन मीमांसा ग्रन्थों के आधार पर ईश्वर की सत्ता सिद्ध नहीं मानी जाती। उत्तरकालीन मीमांसकों ने ईश्वर को कर्मफल के दाता के रूप में स्वीकार किया है।
(३५) जब लौकिक या दृष्ट प्रयोजन मिलता है तब अलौकिक या अदृष्ट की कल्पना नहीं करनी चाहिए।
(३६) वेदमन्त्रों के अर्थज्ञान के सहित किये हुए कर्म ही फलदायक हो सकते हैं, अन्य नहीं।
(३७) किसी भी ग्रन्थ के तत्त्वज्ञान या तात्पयार्य का निर्णय- उपक्रम, उपसंहार, अभ्यास, अपूर्वता, फल, अर्थवाद और उपपत्ति इन सात प्रमाणों के आधार पर करना चाहिए ।
(३८) किसी भी सिद्धान्त का प्रतिपादन विषय, संशय, पूर्वपक्ष, उत्तरपक्ष और प्रयोजन (या निर्णय) इन पांचो अंगों के द्वारा होना चाहिए ।
मीमांसासूत्र , भारतीय दर्शन के सबसे महत्वपूर्ण ग्रन्थों में से एक है। इसके रचयिता महर्षि जैमिनि हैं। इसे पूर्वमीमांसासूत्र भी कहते हैं। इसका रचनाकाल ३०० ईसापूर्व से २०० ईसापूर्व माना जाता है। मीमांसासूत्र, मीमांसा दर्शन का आधारभूत ग्रन्थ है। परम्परानुसार ऋषि जैमिनि को महर्षि वेद व्यास का शिष्य माना जाता है।
धर्म और वेद-विषयक विचार को मीमांसा कहते हैं। इस दर्शन का जिज्ञास्य विषय धर्म है। इस दर्शन में वेदार्थ का विचार होने से इसे मीमांसा दर्शन कहते हैं। इस दर्शन में यज्ञों की दार्शनिक दृष्टि से व्याख्या की गई है। इसके मुख्य तीन भाग हैं। प्रथम भाग में ज्ञानोपलब्धि के मुख्य साधनों पर विचार है। दूसरे भाग में अध्यात्म -विवेचन है और तीसरे भाग में कर्तव्य- अकर्तव्य की समीक्षा है। मीमांसा दर्शन में ज्ञानोपलब्धि के साधन-भूत छह प्रमाण माने गये हैं –१. प्रत्यक्ष, २. अनुमान, ३. उपमान, ४. शब्द, ५. अर्थोपत्ति और ६. अनुपलब्धि। इस दर्शन के अनुसार वेद अपौरुषेय, नित्य एवं सर्वोपरि है। वेद में किसी प्रकार की अपूर्णता नहीं है, अतः हमारा कर्तव्य वही है, जिसका प्रतिपादन वेद ने किया है। हमारा कर्तव्य वेदाज्ञा का पालन करना है। यह मीमांसा का कर्त्तव्याकर्त्तव्यविषयक निर्णय है। मीमांसा का ध्येय मनुष्यों को सुःख प्राप्ति कराना है। मीमांसा में सुःख प्राप्ति के दो साधन बताए गये हैं – निष्काम कर्म और आत्मिक ज्ञान। मीमांसा दुःखों के अत्यन्ताभाव को मोक्ष मानता है।
मीमांसासूत्र को ‘पूर्वमीमांसा‘ तथा वेदान्त को ‘उत्तरमीमांसा‘ भी कहा जाता है। पूर्ममीमांसा में धर्म का विचार है और उत्तरमीमांसा में ब्रह्म का। अतः पूर्वमीमांसा को ‘धर्ममीमांसा‘ तथा उत्तरमीमांसा को ‘ब्रह्ममीमांसा‘ भी कहा जाता है। जैमिनि मुनि द्वारा रचित सूत्र हाेने से मीमांसा को ‘जैमिनीय धर्ममीमांसा’ कहा जाता है। पूर्वमीमांसा में वेद के यज्ञपरक वचनों की व्याख्या बड़े विचार के साथ की गयी है। मीमांसा शास्त्र में यज्ञों का विस्तृत विवेचन है, इससे इसे ‘यज्ञविद्या’ भी कहते हैं । बारह अध्यायों में विभक्त होने के कारण यह मीमांसा ‘द्वादशलक्षणी’ भी कहलाती है।
इस शास्त्र का ‘पूर्वमीमांसा’ नाम इस अभिप्राय से नहीं रखा गया है कि यह उत्तरमीमांसा से पहले बना। ‘पूर्व’ कहने का तात्पर्य यह है कि कर्मकाण्ड मनुष्य का प्रथम धर्म है, ज्ञानकाण्ड का अधिकार उसके उपरान्त आता है । ‘मीमांसा’ शब्द का अर्थ (पाणिनि के अनुसार) ‘जिज्ञासा’ है। जिज्ञासा, अर्थात् जानने की लालसा। मनुष्य जब इस संसार में अवतरित हुआ उसकी प्रथम जिज्ञासा यही रही थी कि वह क्या करे? ग्रन्थ का आरम्भ ही महिर्ष जैमिनि इस प्रकार करते हैं-
अथातो धर्मजिज्ञासा॥
(अब धर्म (करने योग्य कर्म) के जानने की लालसा है।)
अतएव इस दर्शनशास्त्र का प्रथम सूत्र मनुष्य की इस इच्छा का प्रतीक है।
इस ग्रन्थ में ज्ञान-उपलब्धि के जिन छह साधनों की चर्चा की गई है, वे हैं-प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, अर्थापत्ति और अनुपलब्धि। मीमांसा दर्शन के अनुसार वेद अपौरूषेय, नित्य एवं सर्वोपरि है और वेद- प्रतिपादित अर्थ को ही धर्म कहा गया है। इस के दूसरे सूत्र में कहा गया है-
चोदनालक्षणार्थो धर्मः
(वेद में जिसकी प्रेरणा की गयी है, वह पदार्थ धर्म है। अर्थात् वेद में लिखे अनुसार कर्म करना धर्म है और उसमें निषेध किये हुए कर्म का न करना भी धर्म है।)
मीमांसा का तत्वसिद्धान्त
विलक्षण है। कई लोग इसकी गणना अनीश्वरवादी दर्शनों में करते हैं। आत्मा, ब्रह्म, जगत् आदि का विवेचन इसमें नहीं है। यह केवल वेद वा उसके शब्द की नित्यता का ही प्रतिपादन करता है। इसके अनुसार मन्त्र ही सब कुछ हैं। वे ही देवता हैं; देवताओं की अलग कोई सत्ता नहीं।
‘भट्टदीपिका‘ में स्पष्ट कहा है ‘शब्द मात्रं देवता‘ । परन्तु मूल मीमांसासूत्र इसके विपरीत ईश्वरवाद के प्रमाण देता है। मीमांसा में में शंका की गई कि–
लोके कर्माणि वेदवत् ततोऽधिपुरुषज्ञानम् -६,२.१६
‘लोक में भी वेद की भाँति कर्म किये जाते हैं, उनसे ही परमात्मा का ज्ञान हो जायेगा, फिर वेद के मानने की क्या आवश्यकता है)
इसी बात की पुष्टि आगे है–
अपराधेऽपि च तैः शास्त्रम् -६,२.१७
(अपराध करने पर लौकिक पुरुष भी अपराधी के लिये दंड बता देते हैं, फिर वेद के मानने की कोई आवश्यकता नहीं।)
समाधान– अशास्त्रात् तूपसम्प्राप्तिः शास्त्रं स्यान् न प्रकल्पकं तस्माद् अर्थेन गम्येताप्राप्ते शास्त्रम् अर्थवत् -६,२.१८
(यदि वेद को न माना जाये, तो परमात्मा का प्राप्ति अशास्त्रीय हो जायेगी, इसलिये शास्त्र को मानना चाहिये। इंद्रियगोचर परमेश्वर के बतलाने से शास्त्र सार्थक है, निरर्थक नहीं।)
मीमांसकों का तर्क यह है कि सब कर्म, फल के उद्देश्य से होते हैं। फल की प्राप्ति कर्म द्वारा ही होती हैं अतः वे कहते हैं कि कर्म और उसके प्रतिपादक वचनों के अतिरिक्त ऊपर से और किसी देवता या ईश्वर को मानने की क्या आवश्यकता है। परन्तु ये बातें बाद के मीमांसकों की हैं महर्षि जैमिनि इसके विपरीत ईश्वरवादी थे। वे वेदव्यास के शिष्य थे, जो कि परमास्तिक थे, और ब्रह्मसूत्रों के रचयिता थे। भला, वे कैसे नास्तिक हो सकते हैं।
मीमांसादर्शन में कहीं पर भी ईश्वर के अस्तित्व का खण्डन नहीं मिलता है।
मीमांसकों और नैयायिकों में बड़ा भारी भेद यह है कि मीमांसक शब्द को नित्य मानते हैं और नैयायिक अनित्य । यह एक भ्राँति है कि सांख्य और मीमांसा दोनों अनीश्वरवादी माने जाते हैं, पर वेद की प्रामाणिकता दोनों मानते हैं । परन्तु मीमांसदर्शन में इसके विपरीत ईश्वर को मानने के कई प्रमाण मिलते हैं। ऊपर कई सूत्र दिये जा चुके हैं, उसी तरह एक सूत्र वेदांतदर्शन में भी है–
ब्राह्मणे जैमिनिरुपन्यासादिभ्यः॥ ( वेदान्त ४/४/५)
(जैमिनि आचार्य का मत है कि मुक्ति में जीव ब्रह्म के आनंद आदि गुणों को धारण करता है।)
इस से सिद्ध है कि जैमिनि जी आत्मा, परमात्मा, मुक्ति आदि मानते थे भले मीमांसदर्शन में यज्ञादि कर्म मूल विषय होने से इन का अधिक उल्लेख न हुआ हो।
भेद इतना ही है कि सांख्य प्रत्येक कल्प में वेद का नवीन प्रकाशन मानता है, और मीमांसक उसे नित्य अर्थात् कल्पान्त में भी नष्ट न होने वाला कहते हैं। परन्तु ये भी कोई परस्परविरोध नहीं है। मीमांसा के अनुसार शब्द नित्य है क्योंकि ईश्वर का ज्ञान नित्य है, और सांख्य के अनुसार हर कल्प के आरंभ में परमात्मा ऋषियों को वेदों का उपदेश करता है, जिसे वेदोत्पत्ति कहा जाता है।
उत्तरमीमांसा
उत्तरमीमांसा छः भारतीय दर्शनों में से एक। उत्तरमीमांसा को ‘शारीरिक मीमांसा‘ और ‘वेदान्त दर्शन‘ भी कहते हैं। ये नाम बादरायण के बनाए हुए ब्रह्मसूत्र नामक ग्रन्थ के हैं।
‘मीमांसा‘ शब्द का अर्थ है अनुसन्धान, गंभीर विचार, खोज। प्राचीन भारत में वेदों को परम प्रमाण माना जाता था। वेद वाङ्मय बहुत विस्तृत है और उसमें यज्ञ, उपासना और ज्ञान सम्बन्धी मंत्र पाए जाते हैं। वे मंत्र (संहिता), ब्राह्मण और आरण्यक, उपनिषद् नामक भागों में विभाजित किए गए हैं। बहुत प्राचीन (भारतीय विचारपद्धति के अनुसार अपौरुषेय) होने के कारण वेदवाक्यों के अर्थ, प्रयोग और परस्पर संबंध समन्वय का ज्ञान लुप्त हो जाने से उनके संबंध में अनुसंधान करने की आवश्यकता पड़ी। मंत्र और ब्राह्मण भागों के अंतर्गत वाक्यों का समन्वय जैमिनि ने अपने ग्रंथ मीमांसासूत्र (पूर्वमीमांसा दर्शन) में किया। मंत्र और ब्रह्मण वेद के पूर्वभाग होने के कारण उनके अर्थ और उपयोग की मीमांसा का नाम पूर्वमीमांसा पड़ा। वेद के उत्तर भाग आरण्यक और उपनिषद् के वाक्यों का समन्वय बादरायण ने ब्रह्मसूत्र नामक ग्रंथों में किया, अतएव उसका नाम ‘उत्तरमीमांसा‘ पड़ा। उत्तरमीमांसा, ‘शारीरिक मीमांसा‘ भी इस कारण कहलाता है कि इसमें शरीरधारी आत्मा के लिए उन साधनों और उपासनाओं का संकेत है जिनके द्वारा वह अपने ब्रह्मत्व का अनुभव कर सकता है। इसका नाम ‘वेदान्त दर्शन‘ इस कारण पड़ा कि इसमें वेद के अन्तिम भाग के वाक्यों के विषयों का समन्वय किया गया है। इसका नाम ‘ब्रह्ममीमांसा‘ अथवा ‘ब्रह्मसूत्र‘ इस कारण पड़ा कि इसमें विशेष विषय ब्रह्म और उसके स्वरूप की मीमांसा है, जबकि पूर्वमीमांसा का विषय यज्ञ और धार्मिक कृत्य हैं।
उत्तरमीमांसा में केवल वेद (आरण्यकों और उपनिषदों के) वाक्यों के अर्थ का निरूपण और समन्वय ही नहीं है, उसमें जीव, जगत् और ब्रह्म संबंधी दार्शनिक समस्याओं पर भी विचार किया गया है। एक सर्वांगीण दर्शन का निर्माण करके उसका युक्तियों द्वारा प्रतिपादन और उससे भिन्न मतवाले दर्शनों का खण्डन भी किया गया है। दार्शनिक दृष्टि से यह भाग बहुत महत्वूपर्ण समझा जाता है।
समस्त ब्रह्मसूत्र में चार अध्याय हैं और प्रत्येक अध्याय में चार पाद हैं। प्रथम अध्याय में प्रथम पाद के प्रथम चार सूत्र और दूसरे अध्याय के प्रथम और द्वितीय पादों में वेदान्त दर्शन संबंधी प्रायः सभी बातें आ जाती हैं। इनमें ही वेदान्तदर्शन के ऊपर जो आक्षेप किए जा सकते हैं वे और वेदान्त को दूसरे दर्शनों में-पूर्वमीमांसा, बौद्ध, जैन, वैशेषिक, पाशुपत दर्शनों में, जो उस समय प्रचलित थे-जो त्रुटियाँ दिखाई देती हैं वे आ जाती हैं।
समस्त ग्रंथ सूक्ष्म और दुरूह सूत्रों के रूप में होने के कारण इतना सरल नहीं है कि सब कोई उसका अर्थ और संगति समझ सकें। गुरु लोग इन सूत्रों के द्वारा अपने शिष्यों को उपनिषदों के विचार समझाया करते थे। कालांतर में उनका पूरा ज्ञान लुप्त हो गया और उनके ऊपर भाष्य लिखने की आवश्यकता पड़ी। सबसे प्राचीन भाष्य, जो इस समय प्रचलित और प्राप्य है, श्री शंकराचार्य का है। शंकर के पश्चात् और आचार्यों ने भी अपने-अपने संप्रदाय के मतों की पुष्टि करने के लिए और अपने मतों के अनुरूप ब्रह्मसूत्र पर भाष्य लिखे। श्री रामानुजाचार्य, श्री मध्वाचार्य, श्री निम्बार्काचार्य और श्री वल्लभाचार्य के भाष्य प्रख्यात हैं। इन सब आचार्यों के मत, कुछ अंशों में समान होते हुए भी, बहुत कुछ भिन्न हैं।
स्वयं बादरायण के विचार क्या हैं, यह निश्चित करना और किस आचार्य का भाष्य बादरायण के विचारों का समर्थन करता है और उनके अनुकूल है, यह कहना बहुत कठिन है क्योंकि सूत्र बहुत दुरूह हैं। इस समस्या के साथ यह समस्या भी सम्बद्ध है कि जिन उपनिषद्वाक्यों का ब्रह्मसूत्र में समन्वय करने का प्रयत्न किया गया है उनके दार्शनिक विचार क्या हैं। बादरायण ने उनको क्या समझा और भाष्यकारों ने उनको क्या समझा है? वही भाष्य अधिकतर ठीक समझा जाना चाहिए जो उपनिषदों और ब्रह्मसूत्र दोनों के अनुरूप हो। इस दृष्टि से श्री शंकराचार्य का मत अधिक समीचीन जान पड़ता है। कुछ विद्वान् रामानुजाचार्य के मत को अधिक सूत्रानुकूल बतलाते हैं।
उत्तरमीमांसा का सबसे विशेष दार्शनिक सिद्धान्त यह है कि जड़ जगत का उपादान और निमित्त कारण चेतन ब्रह्म है। जैसे मकड़ी अपने भीतर से ही जाल तानती है, वैसे ही ब्रह्म भी इस जगत् को अपनी ही शक्ति द्वारा उत्पन्न करता है। यही नहीं, वही इसका पालक है और वही इसका संहार भी करता है। जीव और ब्रह्म का तादात्म्य है और अनेक प्रकार के साधनों और उपासनाओं द्वारा वह ब्रह्म के साथ तादात्म्य का अनुभव करके जगत् के कर्मजंजाल से और बारंबार के जीवन और मरण से मुक्त हो जाता है। मुक्तावस्था में परम आनन्द का अनुभव करता है।
।। हरि ॐ तत् सत् ।। गीता विशेष – 16.14 ।।
Complied by: CA R K Ganeriwala (+91 9422310075)