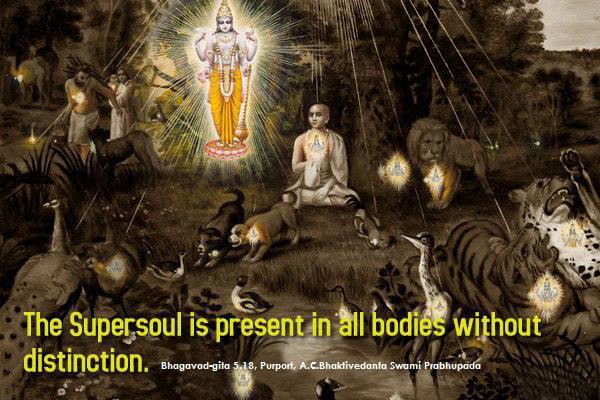।। Shrimadbhagwad Geeta ।। A Practical Approach ।।
।। श्रीमद्भगवत गीता ।। एक व्यवहारिक सोच ।।
।। Chapter 16.13 II
।। अध्याय 16.13 II
॥ श्रीमद्भगवद्गीता ॥ 16.13॥
इदमद्य मया लब्धमिमं प्राप्स्ये मनोरथम् ।
इदमस्तीदमपि मे भविष्यति पुनर्धनम् ॥
idam adya mayā labdham,
imaḿ prāpsye manoratham..।
idam astīdam api me,
bhaviṣyati punar dhanam..।।
भावार्थ:
आसुरी स्वभाव वाले मनुष्य सोचते रहते हैं कि आज मैंने इतना धन प्राप्त कर लिया है, अब इससे और अधिक धन प्राप्त कर लूंगा, मेरे पास आज इतना धन है, भविष्य में बढ़कर और अधिक हो जायेगा। (१३)
Meaning:
This has been gained by me now, these wishes I shall fulfill. This is mine, and this wealth shall be mine later.
Explanation:
In three verses, Krishna talks about the thought pattern of the materialistic person. And what is a thought pattern? Calculation of the money that he possesses; which bank, what things; and what are the interest rates; and the next year, how much it will increase. And just go on projecting and daydreaming; he does not have anything else to think of other than arta and kāmah.
The Sukti Sudhakar states that there are four kinds of people: “The first kind of people is the saintly personalities who sacrifice their self-interest for the welfare of others. The second kind is common people who believe in engaging in the welfare of others, provided it does not harm them. The third kind is the demoniac who do not mind harming others, if it helps fulfil their self-interest. There is also a fourth kind of people who harm others, for no reason (except sadistic delight). There is no suitable name for them.”
Ignoring all morality, the demoniac presume they have a right to enjoy whatever they find pleasurable. They make concerted efforts to orchestrate events to fulfil their ambitions. Realizing that the ritualistic practices of the Vedas will help them become materially affluent, they even perform ritualistic ceremonies to accrue abundance and fame from them. However, like the vulture that flies high but keeps its sight fixed low, the demoniac sometimes rise in social status, but their actions remain mean and lowly. Such people respect power and believe in the principle of “might is right.” Hence, they do not hesitate in even harming or injuring others to eliminate obstacles in the fulfilment of their desires.
In India, when a young boy gets the news that he has gained admission in the engineering college of his choice, a desire automatically pops up in his mind. Once I get through my gruelling 4-year engineering course, I will be happy. As the 4 years come to a close, another desire comes in. I need to get into a good master’s program in the US. When that happens, he feels that he will be happy when he gets a US visa. Once he arrives in the US, he wants a green card. Then he wants a wife, a big house, car and so on. Each time he thinks he will be happy; another desire is waiting in line to be fulfilled.
Shri Krishna wants us to examine our own outlook and find out the level of materialism in it. So, in this shloka and the following two shlokas, he uses the first person to drive this point home. Here, he wants us to inquire into what we think is our ultimate goal, our destination, our objective in life. Most of us will come to a similar conclusion that it is accumulation of wealth so that we can take care of our material desires as well as those of our family.
In fact, Bhagavān also measures the worth of a person not in terms of taking but in terms of giving; and our value increases not in proportion to earning; but in proportion to sharing; but this materialistic person does not know. Therefore, he says this much I have earned and next year how much I will get, calculation using the computer, same calculation again and again; in future I will be able to fulfill these many desires of mine.
But this line of thinking has a flaw in it. Desires are bahushaakha, they multiply infinitely, as we have seen in earlier chapters. Each desire contains the seed of several other desires. If any of those desires is unfulfilled, we invite stress, tension and anxiety into our lives. Now it does not mean that we should not harbour any desires. It just means that we need to apply some system, some framework to ensure that desires are managed and do not get out of hand.
The four stage aashrama system (brahmachaari, grihastha, vaanaprastha and sanyaasi) prescribes the duties of an individual based on their stage in life. When duties are given importance, desires automatically manage themselves. For instance, if one is a householder, then one focuses on what is the essential set of desires for fulfilling one’s duties, rather than deriving joy out of adding more and more desires. And even if some desires are unfulfilled, they do not agitate the mind because the goal is the duty, not the desire.
।। हिंदी समीक्षा ।।
पूर्व श्लोक में असंतोष, लोभ और स्वार्थ को ध्यान में रखते हुए, असुर वृति के लोगो के विचारो का व्यवहारिक वर्णन करते हुए, भगवान कहते है। आसुरी प्रकृतिवाले व्यक्ति लोभ के परायण हो कर मनोरथ करते रहते हैं कि हम ने अपने उद्योग से, बुद्धिमानी से, चतुराई से, होशियारी से, चालाकी से इतनी वस्तुएँ तो आज प्राप्त कर लीं, इतनी और प्राप्त कर लेंगे। इतनी वस्तुएँ तो हमारे पास हैं, इतनी और वहाँ से आ जायँगी। इतना धन व्यापार से आ जायगा। हमारा बड़ा लड़का इतना पढ़ा हुआ है अतः इतना धन और वस्तुएँ तो उस के विवाह में आ ही जायँगी। इतना धन टैक्स की चोरी से बच जायगा, इतना जमीन से आ जायगा, इतना मकानों के किराये से आ जायगा, इतना ब्याज का आ जायगा, आदि आदि।
सभी प्रकार की नैतिकता की उपेक्षा कर आसुरी व्यक्ति यह समझते हैं कि उन्हें जो भी सुखदायक प्रतीत होता है उसका उपभोग करना उनका अधिकार है। वे महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए योजनाओं एवं कार्यक्रमों को अनुकूल बनाने का ठोस प्रयास करते हैं। वे यह समझते हैं कि वेदों में वर्णित धार्मिक रीतियाँ उन्हें भौतिक रूप से समृद्ध बनाने में सहायक होती हैं वे प्राचुर्य सुख समृद्धि और यश प्राप्त करने हेतु धार्मिक अनुष्ठानों का आयोजन करते हैं। किन्तु जिस प्रकार से गिद्ध ऊंची उड़ान भरता है लेकिन अपनी दृष्टि नीचे की ओर स्थिर रखता है, वैसे ही कभी-कभी असुर व्यक्तियों की समाज में प्रतिष्ठा बढ़ती है लेकिन उनके कार्य निम्न और निकृष्ट प्रकृति के होते हैं। ऐसे लोग शक्ति की पूजा करते हैं और ‘जिसकी लाठी उसकी भैंस’ के सिद्धांत में विश्वास रखते हैं। इसलिए वे अपनी कामनाओं की पूर्ति में आने वाली बाधाओं को समाप्त करने हेतु दूसरे लोगों को चोट पहुंचाने में भी संकोच नहीं करते हैं।
तीन श्लोकों में कृष्ण भौतिकवादी व्यक्ति के विचार पैटर्न के बारे में बात करते हैं। और विचार पैटर्न क्या है? उसके पास कितना पैसा है, इसका हिसाब; कौन सा बैंक, कौन सी चीजें; और ब्याज दरें क्या हैं; और अगले साल, यह कितना बढ़ेगा। और बस कल्पना करते रहो और दिवास्वप्न देखते रहो; उसके पास अर्थ और काम के अलावा सोचने के लिए कुछ नहीं है।
दरअसल भगवान भी किसी व्यक्ति का मूल्य लेने से नहीं, बल्कि देने से मापते हैं और हमारा मूल्य कमाने से नहीं, बल्कि बांटने से बढ़ता है; लेकिन यह भौतिकवादी व्यक्ति नहीं जानता। इसलिए वह कहता है कि मैंने इतना कमाया है और अगले साल मुझे कितना मिलेगा, कंप्यूटर से हिसाब लगाता है, बार-बार वही हिसाब लगाता है; भविष्य में मैं अपनी इतनी सारी इच्छाएँ पूरी कर सकूँगा।
सुक्ति सुधाकर में चार प्रकार के मनुष्यों का वर्णन किया गया है
एक सत्पुरुषः परार्थगहस्तकः स्वार्थन परित्यज्य।सामान्यास्तु परार्थमुद्यमभारितः स्वार्थः विरोधेत ये।।
ते मी मानव राक्षसः परहितं स्वार्थाय निनंति ये।ये तुभंति निरार्थकं परहितं ते के न जानीमहे ।।
पहले प्रकार के मनुष्यों में वे पुण्यात्मा हैं जो दूसरों के कल्याण के लिए अपने निजी हित का त्याग करते हैं। दूसरी श्रेणी में साधारण लोग आते हैं जो दूसरे लोगों का कल्याण करने में विश्वास रखते हैं बशर्ते कि इससे उनका कोई अनिष्ट न होता हो। तीसरी श्रेणी असुर लोगों की है जो अपने हितों की पूर्ति हेतु दूसरों को क्षति पहुँचाने में कोई हिचक नहीं करते। चौथी श्रेणी के लोग भी होते हैं जो (केवल कामुकतापूर्ण आनन्द के लिए) अकारण लोगों को कष्ट देते हैं। इनके लिए कोई उपयुक्त नाम नहीं हैं। श्रीकृष्ण ने स्पष्ट रूप से निकृष्ट मानसिकता वाले असुर लोगों का वर्णन किया है। घमंड में अंधे होकर वे इस प्रकार से सोचते हैं”
सामान्य भाषा मे 99 का चक्कर जिसे कहते है, वह यही है। “Time is money” इन लोगो का वेद वाक्य है, क्योंकि यह लोग प्रत्येक व्यवहार को पैसों से तोलते है, फिर चाहे रिश्तेदारी हो, मंदिर, पूजा धर्म हो या आपसी व्यवहार। धन कितना भी आ जाए, इन का लोभ बढ़ता जाता है, वैसे ही इन के मनोरथ भी बढ़ते जाते हैं। जब इनका चिन्तन बढ़ जाता है, तब वे चलते फिरते हुए, कामधंधा करते हुए, भोजन करते हुए, मलमूत्र का त्याग करते हुए और यदि नित्य कर्म (पाठ पूजा जप आदि) करते हैं तो उसे करते हुए भी धन कैसे बढ़े इसका चिन्तन करते रहते हैं। इतनी दूकानें, मिल, कारखाने तो हमने खोल दिये हैं, इतने और खुल जायँ। अंतहीन विचारों एवम चिंताओं के यह सिलसिला लग जाता है। भव्यता, सम्मान और व्यवहार का मापदंड सिर्फ धन ही होता है। कभी कभी बीमारी – मृत्यु जैसे प्रकरण को भी धन की मात्रा से नापा जाता है, कि इस बीमारी में इलाज कितने रुपए का हुआ।
कबीर जी ने इन अनंत इच्छाओं के लिए कहा है – माया मरी न मन मरा,मर-मर गया शरीर।आशा,तृष्णा न मरी कह गए दास कबीर।।
सामान्य लोग इसी प्रकार का जीवन जीते हैं। प्रतिस्पर्धा से पूर्ण इस जगत् में उस व्यक्ति को सफल समझा जाता है, जिस के पास अधिकतम धन हो। सामाजिक प्रतिष्ठा, मान- मर्यादा का माप दंड व्यक्ति के पास किंतना धन है, उस से तोला जाता है। आज सिने जगत या राजनीति या व्यापार में जिस ने भी नैतिक या अनैतिक तरीके से अधिक धन कमा कर रखा है, उस को लोग अधिक सम्मान देते है। अत: मनुष्य को जितना अधिक धन प्राप्त होता है, उस से उस की सन्तुष्टि नहीं होती। धनार्जन की इस धारणा में हास्यास्पद विरोधाभास यह है कि धन प्राप्ति से सन्तोष होने के स्थान पर अधिकाधिक धन की इच्छा बढ़ती जाती है। आज तक किसी भी भौतिकवादी धनी व्यक्ति ने अपने धन को पर्याप्त नहीं माना है। इस के विपरीत स्थितप्रज्ञ पुरुष के लक्षण बताते हुए गीता में कहा गया है कि ज्ञानी पुरुष की परिपूर्णता ऐसी होती है कि जगत् के विषय उसके मन में किंचित् भी विकार उत्पन्न नहीं करते हैं और वही पुरुष वास्तविक शान्ति प्राप्त करता है, न कि कामी पुरुष। इस श्लोक में आसुरी पुरुष का भौतिक वस्तुओं के संबंध में दृष्टिकोण बताया गया है। धन संग्रह की वस्तु न होकर अतिरिक्त दान देने की वस्तु है।
गीता में यह व्यवहारिक ज्ञान का वर्णन अज्ञान के कुचक्र को समझने के लिए किया गया है। जिस मनुष्य का जीवन नित्य नही है, वह ही संग्रहण इस प्रकार करता है मानो यह उस का पुरषार्थ से प्राप्त है। जिस का मरने के बाद संसार का कोई संबंध नहीं रहता, वह भी अपने वंश और बच्चो में अपने को अमरता को महसूस करता है। सांसारिक संबंध और कर्तव्य जीवन के सात्विक गुणों के विकास के लिए होते है, किंतु योगमाया इस में ममता, मोह, लोभ और स्वार्थ घोल कर मनुष्य को अपने कर्तव्य धर्म और मोक्ष के मार्ग से च्युक्त कर देती है। यह अज्ञान की पराकाष्ठा है, जिसे कोई समझ कर भी समझने को तैयार नहीं। अतः इसी को अधिक समझाने के लिए अगले श्लोक में भगवान क्या कहते है, पढ़ते है।
।। हरि ॐ तत सत।। गीता – 16.13।।
Complied by: CA R K Ganeriwala (+91 9422310075)