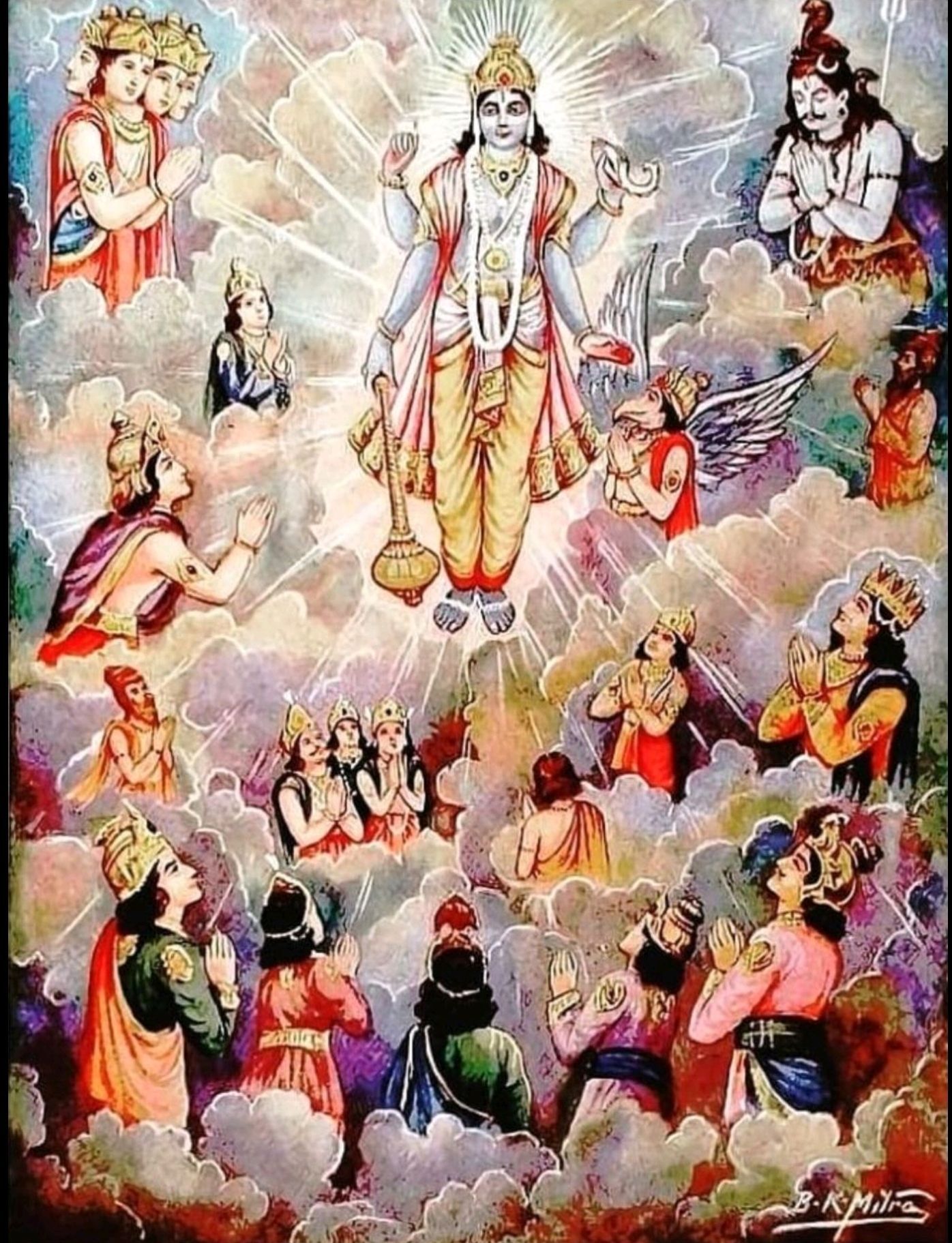।। Shrimadbhagwad Geeta ।। A Practical Approach ।।
।। श्रीमद्भगवत गीता ।। एक व्यवहारिक सोच ।।
।। Chapter 16.07 II
।। अध्याय 16.07 II
॥ श्रीमद्भगवद्गीता ॥ 16.7॥
प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च जना न विदुरासुराः ।
न शौचं नापि चाचारो न सत्यं तेषु विद्यते॥
“pravṛttiḿ ca nivṛttiḿ ca,
janā na vidur āsurāḥ..।
na śaucaḿ nāpi cācāro,
na satyaḿ teṣu vidyate”..।।
भावार्थ:
आसुरी स्वभाव वाले मनुष्य यह नही जानते हैं कि क्या करना चाहिये और क्या नही करना चाहिये, वह न तो बाहर से और न अन्दर से ही पवित्र होते है, वह न तो कभी उचित आचरण करते है और न ही उनमें सत्य ही पाया जाता है। (७)
Meaning:
Whether to engage or to disengage from action, those people with devilish tendencies do not know. Neither purity nor proper conduct nor truth exists in them.
Explanation:
Shri Krishna begins his explanation of the materialistic viewpoint by examining its value system. He says that those people who come from a purely materialistic viewpoint have a shaky value system. In other words, they do not know what to do and what not to do, when to engage in something and when not to. They focus only on artha or wealth and kaama or desire. They forget that there are two other goals in life, dharma or duty and moksha or liberation, and that each goal is to be picked up and left off at a certain stage in life.
Being a natural living being, every human being has got only two purusharthas, they are called arta and kāmaḥ. Arta means what? Money, value for wealth is very natural, even a child has value for money. And the second thing is kāma pleasure or enjoyment; therefore, everybody by birth has a value for artha kama puruṣārtha; and therefore our mind develop its own rāgaḥ-dveṣaḥs. rāgaḥ means likes and dvesha means dislike. Right from birth, our life is governed by rāgaḥ-dveṣaḥs.
But once a particular stage comes, we are capable of discrimination and thinking, this rāgaḥ-dveṣaḥ based life should be changed; and a new value system should replace the old value system; and the new value system that is prescribed by our scriptures is the spiritual value system. And we do not know the importance of spiritual goals, because we are immature people at that time. And therefore, we should be guided by the scriptures which we look upon as Vēdā mātha.
Dharma consists of codes of conduct that are conducive to one’s purification and the general welfare of all living beings. Adharma consists of prohibited actions that lead to degradation and cause harm to society. The demoniac nature is devoid of faith in the knowledge and wisdom of the scriptures. Hence, those under its sway are confused about what is right and wrong action. A thing which is good for me and niṣēda means that which is not good for me. vidhi means kartavyam; niṣeda means akarthavyam or varjaniyam and the Sr̥uti asks us to replace the rāgaḥ-dveṣaḥ based life by vidhi-niṣēda based life.
A typical example of this is the present trend in western philosophy. Having evolved through various schools of thought after the Renaissance, such as Age of Enlightenment, Humanism, Empiricism, Communism, Existentialism, and Skepticism, the present era in western philosophy is labelled as “post-modernism.” The prevalent view of post-modernist thought is that there is no absolute truth. Multitudes have rejected the possibility that such a thing as absolute truth could exist. “All is relative” has become the slogan of the post-modernist era of philosophy. We often hear phrases like “that may be true for you, but it’s not true for me.” Truth is seen as a personal preference or perception that cannot extend beyond a person’s individual boundaries. This viewpoint has a big bearing on the subject of ethics, which deals with the question of right and wrong behavior. If there is no such thing as absolute truth, then there is no ultimate moral rightness or wrongness about anything. Then, people are justified in saying, “It may be right for you but that does not mean it is right for me.”
Now, since such people are unclear about the pros and cons of everything, they are bound to do things in a haphazard and messy way. Shri Krishna says that such people do not have shaucha, they do not have purity. He refers not just to external purity but also internal. When someone does not have a systematic way of thinking through things, there is a strong chance that they will lead messy lives. Furthermore, their conduct towards others, their aacharana, will also be messy and haphazard. They will lack good manners, courtesy and politeness.
It also follows that when someone does not know the pros and cons of anything, they will not place a lot of importance on satyam, truth, doing things the right way. So if they do not get the result they want, they have no qualms in getting their results by lying, cheating and deceit. They do not want to wait for the result, because waiting takes time. If there is a shortcut, they will go for it. Such is the value system of the aasuri, the devilish, the materialistic viewpoint.
Shree Krishna states that the demoniac nature is confused about what is right and what is wrong, and thus, neither purity, nor truth, nor right conduct is found in them. In the following verse, he goes on to describe the predominant views of such people.
।। हिंदी समीक्षा ।।
मनुष्य भी अन्य प्राणियों के समान प्रकृति पुरुष है। हर मनुष्य के पास दो ही पुरुषार्थ होते हैं, उन्हें अर्थ और काम कहते हैं। अर्थ का मतलब क्या है? धन, धन का मूल्य बहुत स्वाभाविक है, यहाँ तक कि एक बच्चे के लिए भी धन का मूल्य होता है। और दूसरी चीज़ है काम सुख या भोग; इसलिए जन्म से ही हर किसी के पास अर्थ काम पुरुषार्थ का मूल्य होता है; और इसलिए हमारे मन में अपने राग-द्वेष विकसित होते हैं। राग का मतलब है पसंद और द्वेष का मतलब है नापसंद। जन्म से ही हमारा जीवन राग-द्वेष से संचालित होता है।
इस अध्याय की समाप्ति पर्यन्त प्राणियों के विशेषणों द्वारा आसुरी सम्पत्ति दिखलायी जाती है, क्योंकि प्रत्यक्ष कर लेने से ही उस का त्याग करना बन सकता है।
धर्म में आचरण के नियम शामिल हैं जो व्यक्ति की शुद्धि और सभी जीवों के सामान्य कल्याण के लिए अनुकूल हैं। अधर्म में निषिद्ध कार्य शामिल हैं जो पतन की ओर ले जाते हैं और समाज को नुकसान पहुंचाते हैं। आसुरी प्रकृति शास्त्रों के ज्ञान और बुद्धि में विश्वास से रहित है। इसलिए, इसके प्रभाव में आने वाले लोग सही और गलत कर्म के बारे में भ्रमित रहते हैं।
किसी व्यक्ति की पहचान का आधार उस का प्राकृतिक शरीर एक बार अवश्य हो सकता है, जिस के कारण वह सज धज कर, विभिन्न भेष भूसा और आज के समय तो कुछ कलाकार संपूर्ण कपड़े उतार कर भी फोटो ग्राफी करवाते है। किंतु उस के व्यक्तित्व की पहचान का आधार प्रवृति, निर्वृती का ज्ञान, शौच, आचार – व्यवहार, सत्य के आचरण पर होता है। इसलिए असुर बड़े दांत, लाल आंखे या अत्यंत बड़े शरीर से नही, कुछ गुणों से पहचाने जाते है।
आसुरी स्वभाववाले मनुष्य, प्रवृत्ति को अर्थात् जिस किसी पुरुषार्थ के साधनरूप कर्तव्यकार्य में प्रवृत्त होना उचित है, उस में प्रवृत्त होने को और निवृत्ति को अर्थात् उस से विपरीत जिस किसी अनर्थकारक कर्म से निवृत्त होना उचित है, उस से निवृत्त होने को भी नहीं जानते। केवल प्रवृत्ति निवृत्ति को नहीं जानते, इतना ही नहीं, उन में न शुद्धि होती है, न सदाचार होता है और न सत्य ही होता है। यानी आसुरी प्रकृतिके मनुष्य अशुद्ध, दुराचारी, कपटी और मिथ्यावादी ही होते हैं।
वह वस्तु जो मेरे लिए अच्छी है और निषेध का अर्थ है वह जो मेरे लिए अच्छी नहीं है। विधि का अर्थ है कर्तव्यम्; निषेद का अर्थ है अकर्तव्यम् या वर्जनीयम् और श्रुति हमें राग:-द्वेष: आधारित जीवन के स्थान पर विधि-निषेध आधारित जीवन अपनाने को कहती है।
यहाँ प्रवृत्ति और निवृत्ति के शब्द क्रमश कर्तव्य कर्म और अकर्तव्य अर्थात् निषिद्ध कर्म हैं।धार्मिक अनुष्ठानकर्ता कर्तव्य पालन और निस्वार्थ समाज सेवा के द्वारा न केवल तात्कालिक लाभ को प्राप्त करता है अपितु अन्तकरण की शुद्धि भी प्राप्त करता है, क्योंकि वह कभी अपने सर्वोच्च लक्ष्य को विस्मृत नहीं होने देता। निषिद्ध कर्मों से विरति ही निवृत्ति कहलाती है। अकर्तव्य का त्याग ही मनुष्य के लिए श्रेयस्कर होता है। असुर लोगों को कर्तव्य और अकर्तव्य का सर्वथा अज्ञान होता है। यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि आसुरी गुणों की सूची अज्ञान से प्रारम्भ होती है। यदि कोई व्यक्ति अज्ञानवशात् किसी प्रकार का अपराध करता है, तो समाज के सहृदय पुरुषों के मन में उसके प्रति क्षमा का भाव सहज उदित होता है। भले ही न्यायालय में उसे क्षमा के योग्य कारण न माना जाये। बाह्य शुद्धि, बहुत कुछ मात्रा में मनुष्य के आन्तरिक व्यक्तित्व की परिचायक होती है। श्रेष्ठ शिक्षा और संस्कारी पुरुष में ही यह शुद्धि हमें देखने को मिलती है। अज्ञानी पुरुष में अन्तर्बाह्य शुद्धि का अभाव होता है। ऐसे अनुशासनविहीन पुरुष का व्यवहार (आचार) भी विनयपूर्ण नहीं हो सकता, क्योंकि बाह्य आचरण मनुष्य के स्वभाव की ही अभिव्यक्ति है। इसलिए भगवान् कहते हैं कि आसुरी लोगों में सदाचार का अभाव स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है। अविवेक, अशौच तथा अनाचार से युक्त पुरुष अपने वचनों की सत्यता का पालन कभी नहीं कर सकता।
वैदिक प्रक्रिया के अनुसार सांसारिक भोग और संग्रह में लगे हुए पुरुषों में भी परमात्मा की प्राप्ति का एक निश्चय नहीं होता। भाव यह है कि आसुरी सम्पदा का अंश रहने के कारण जब ऐसे शास्त्र विधि से यज्ञादि कर्मों में लगे हुए पुरुष भी परमात्मा का एक निश्चय नहीं कर पाते, तब जिन पुरुषों में आसुरीसम्पदा विशेष बढ़ी हुई है अर्थात् जो अन्यायपूर्वक भोग और संग्रह में लगे हुए हैं। उन की बुद्धि में परमात्मा का एक निश्चय होना कितना कठिन है। इसलिए गीता में इस के लिये मनुष्य शब्द का प्रयोग नहीं है क्योंकि जो व्यक्ति देह दृष्टि एवम देह स्वार्थ में ही लिप्त हो कर कर्तव्य- अकर्तव्य को नही जानता वो पशुवत जीवन ही व्यतीत करता है क्योंकि जितनी मात्रा में स्वार्थ की वृद्धि होगी, उतनी ही मात्रा में राग, द्वेष, ईर्षा एवम क्रोध आदि बढ़ेंगे। यहां सभी अपना अपना सत्य ले कर चलते है।
इसका एक विशिष्ट उदाहरण पश्चिमी दर्शन में वर्तमान प्रवृत्ति है। पुनर्जागरण के बाद विभिन्न विचारधाराओं जैसे कि ज्ञानोदय युग, मानवतावाद, अनुभववाद, साम्यवाद, अस्तित्ववाद और संशयवाद के माध्यम से विकसित होने के बाद, पश्चिमी दर्शन में वर्तमान युग को “उत्तर-आधुनिकतावाद” के रूप में लेबल किया गया है। उत्तर-आधुनिकतावादी विचार का प्रचलित दृष्टिकोण यह है कि कोई पूर्ण सत्य नहीं है। बहुत से लोगों ने इस संभावना को अस्वीकार कर दिया है कि पूर्ण सत्य जैसी कोई चीज़ मौजूद हो सकती है। “सब कुछ सापेक्ष है” दर्शन के उत्तर-आधुनिकतावादी युग का नारा बन गया है। हम अक्सर ऐसे वाक्यांश सुनते हैं जैसे “यह आपके लिए सही हो सकता है, लेकिन यह मेरे लिए सही नहीं है।” सत्य को एक व्यक्तिगत पसंद या धारणा के रूप में देखा जाता है जो किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत सीमाओं से आगे नहीं बढ़ सकता है। इस दृष्टिकोण का नैतिकता के विषय पर बहुत प्रभाव पड़ता है, जो सही और गलत व्यवहार के सवाल से निपटता है। यदि पूर्ण सत्य जैसी कोई चीज़ नहीं है, तो किसी भी चीज़ के बारे में कोई अंतिम नैतिक सही या गलत नहीं है। फिर, लोगों को यह कहने में उचित है, “यह आपके लिए सही हो सकता है लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि यह मेरे लिए सही है।” किंतु क्या भौतिकवाद से स्वार्थ इस सीमा तक नहीं पनपता की पद, सम्मान, नियम और राग – द्वेष में जीव आतंकवाद और धर्म के नाम पर विचारहीन कट्टरता को धारण कर के उस के मत को नहीं मानने वालों की हत्या करना सही मान लेता है।
अच्छाई को जानना और उसे ग्रहण करना सभी धर्मो और धार्मिक पुस्तकों में सिखाया जाता है, किंतु मन प्रकृति से जुड़ा है, इसलिए यह हमेशा जीव को अधोगति अर्थात प्राकृतिक क्रियाओं की ओर खींचता है, जो एक सभ्य – विकसित समाज में निषिद्ध मानी जाती है और जिस के कारण जीव को मोक्ष की प्राप्ति न हो कर जन्म – मृत्यु का कष्ट पूर्ण चक्कर चालू रहता है। पशुवत जीवन जीना कोई शौर्य का विषय नहीं है। अपने रहन सहन और व्यवहार में शालीनता न रखते हुए, यदि अच्छे आचरण की अपेक्षा घर, खानदान, समाज या देश के लोगो से की जाए तो यह अपेक्षा ही सब से बड़ी भूल होगी। आज जो लोग ज्ञान की बाते करते है, किसी के गलत कार्य का विरोध करते है, वह स्वयं भी प्रवृति – निवृति, शौच, सदाचार और सत्य का व्यवहार नहीं जानते। जो आप नही करते, वह पर्याप्त नहीं है, जो आप को नही करना चाहिए, वह भी सत्य का आचरण है और भौतिकवादी-मूल्य-व्यवस्था से आध्यात्मिक- मूल्य- व्यवस्था में यह परिवर्तन मनुष्य का दूसरा जन्म माना जाता है। यह परिवर्तन प्रकृति से संस्कृति पुरुष की ओर होता है।
श्री कृष्ण कहते हैं कि आसुरी प्रकृति इस बात को लेकर भ्रमित रहती है कि क्या सही है और क्या गलत, और इस प्रकार, उनमें न तो पवित्रता, न ही सत्य, न ही सही आचरण पाया जाता है। अगले श्लोक में, वे ऐसे लोगों के प्रमुख विचारों का वर्णन करते हैं।
।। हरि ॐ तत सत।। गीता – 16.07।।
Complied by: CA R K Ganeriwala (+91 9422310075)