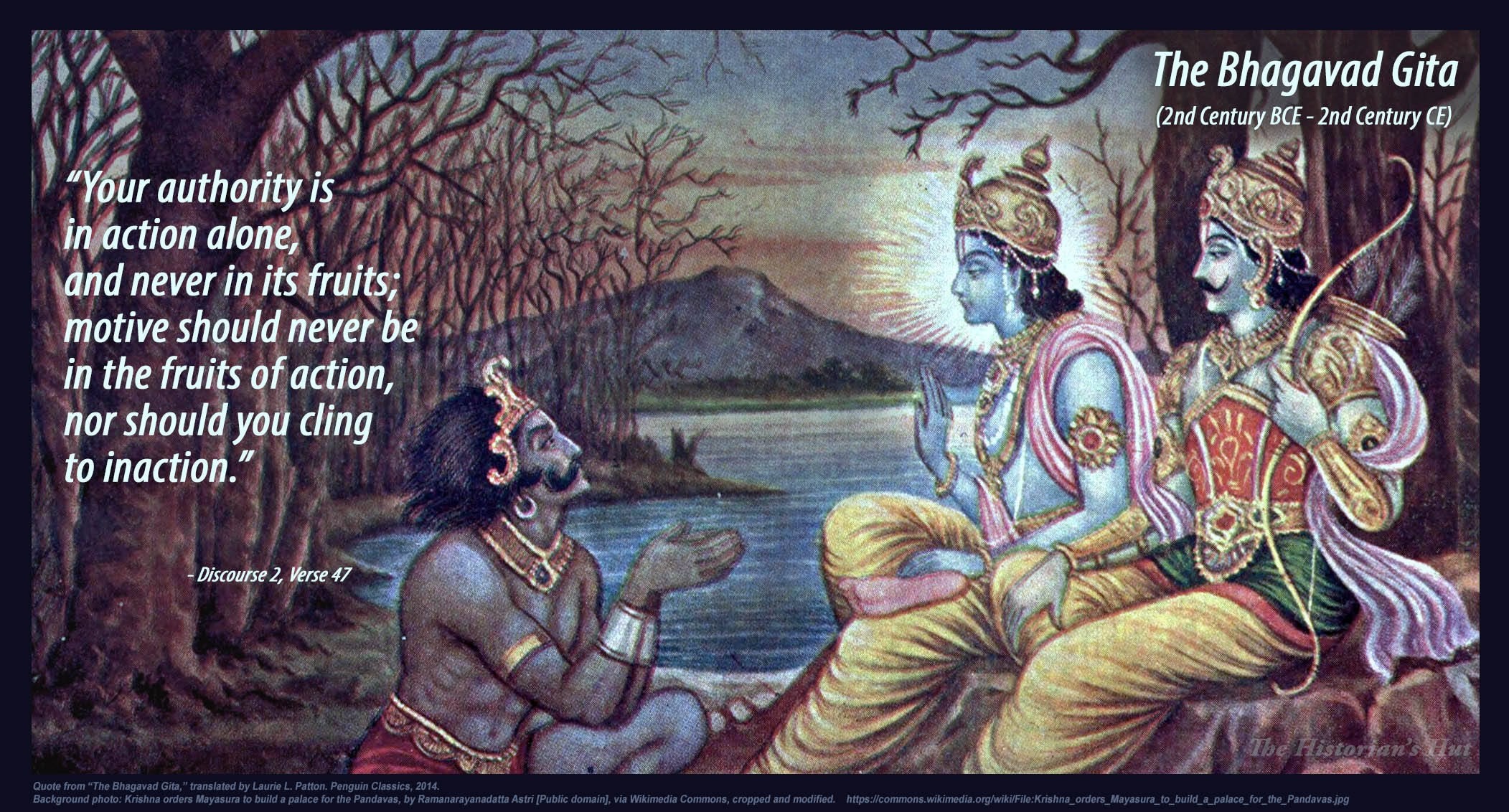।। Shrimadbhagwad Geeta ।। A Practical Approach ।।
।। श्रीमद्भगवत गीता ।। एक व्यवहारिक सोच ।।
।। Chapter 16.03 II Additional II
।। अध्याय 16.03 II विशेष II
।। दैवीय गुण, चरित्र और व्यवहार ।। विशेष गीता अध्याय 16.03 ।।
कुछ लिखने से पहले एक प्रसंग है कि किसी सज्जन पुरुष द्वारा बहेलिए द्वारा पक्षियों को पकड़े जाने से व्यथित किसी सज्जन पुरुष ने पक्षियों को शिक्षित करने का विचार किया। इस कार्य हेतु उस में कुछ तोतों को पकड़ कर सिखाया कि ” बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना फैकेगा, किंतु हमे लालच नहीं करना है, दाना चुगने के लिए जाल में नही फसना है।” शिक्षित तोतों को उस में जंगल में छोड़ दिया। कुछ समय बाद वह जंगल गया, उसे विश्वास था, कि बहेलिया के जाल में कोई तोता नही फसेगा, किंतु उस में आश्चर्य पूर्ण देखा सभी तोते जाल में फसे भी थे और गा भी रहे थे ” बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना फैकेगा, किंतु हमे लालच नहीं करना है, दाना चुगने के लिए जाल में नही फसना है।”
कथन का आशय यही है, दैवीय गुण पढ़ने, विचारने या आत्मभूत हो अन्य को सुनाने के गुण नहीं है। जिस भी मनुष्य में इन दैवीय गुणों का प्रदुर्भाव आत्मसात हो कर, उस के व्यक्तित्व में उस के आचरण, व्यवहार और कर्म में झलकता है, और वह बिना किसी प्रचार और प्रसार के आनंद के साथ रहता है, वही दैवीय गुण संपन्न है। एक तोते की भांति जीव कितना भी वेदों का पाठ करे, भजन करे, यज्ञ करे, किंतु दैवीय गुणों से युक्त हुए बिना उस का अज्ञान समाप्त नहीं हो सकता।
राम चरित मानस या गीता या भागवद के एक एक श्लोक का याद होना, आरती, श्लोक, भजन, कीर्तन में घंटो व्यतीत करना, नित्य स्नान, ध्यान, यज्ञ आदि करते रहना, शुद्धि की ओर प्रयास ही है, यह सफल तभी मानी जा सकती है, जब इस में दिए ज्ञान को अध्ययन करने वाला आत्मसात कर सके। इस विषय हेतु वाद – विवाद में निरर्थक समय व्यतीत करते हुए, अपने को ही सही सिद्ध करने का को चलन आज कल बढ़ गया है, उस से दूर रहना भी दैवीय गुण है।
व्हाट्सएप्प और अन्य सोशल मीडिया में अक्सर हम सुविचारों को एक दूसरे को प्रेषित करते है क्योंकि हमारे संस्कार और आदर्श हमे उन सुविचारों से प्रभावित करते है किंतु आचरण में हमारा राग, द्वेष, स्वार्थ, लोभ, काम और वासना इन सुविचारों के अनुसार कर्म नहीं करने देता। इसलिए अपनी इन कमजोरियों को जीतने के लिए सत्संग, आध्यात्मिक ज्ञान और गुरु का मार्ग दर्शन आवश्यकता होती है।
आज सनातन संस्कृति में हिंदू समाज का ज्ञान स्वार्थ और लोभ में इतना अधिक डूब गया है कि कोई भी यदि चार टोटके लाभ के बता दे तो लोग उसे ही ज्ञानी और धर्म गुरु मान कर पागलों की तरह पीछे पड़ जाते है। उन के लिए धर्म की अस्मिता, ज्ञान या रक्षा का कोई महत्व नहीं। स्वार्थ और लोभ में बहेलिए के जाल में दाना चुगने और गाने वाले पक्षी की जीवन जीने वाला सनातनी, वास्तव में अपने शौर्य को भुला कर लालची और कायर हो गया है।
ज्ञान को आत्मसात करने के लिए श्रवण जिस में पढ़ना भी शामिल है, मनन और चिंतन आवश्यक है। किंतु समाज में ज्ञानी की अपेक्षा धनवान का सम्मान बढ़ जाने से नैतिक मूल्यों का ह्वास हुआ है। जो धनवान है, वह रटे हुए पक्षी की तरह ज्ञान तो देता है किंतु आचरण नहीं करता और समाज में अपनी प्रतिष्ठा धन के बल पर कायम रखने की कोशिश करता है। अक्सर चलचित्र में भी खलनायक को साधु या गीता के वाक्य पढ़ते हुए बताया जाता है। यही सनातन का अपमान सनातन के लोग गर्व से देखते है किंतु कभी किसी अन्य मत में ऐसा विरोधाभास नहीं देखा होगा, क्योंकि वहां अज्ञान भी है तो हठधर्मिता के साथ। और यहां ज्ञान भी है तो मूर्खता के साथ।
देवी संपदा के 26 गुण को धारण करना एवम शब्दतः पालन करना व्यवहारिकता नही। रामायण काल त्रेता युग था, जहां किसी के वचन, आचरण एवम व्यक्तित्व का मूल्यांकन उस के द्वारा कथित वचनों से था, इसलिये पिता द्वारा दिये वचन को राम ने पालन किया। राम-रावण युद्ध मे किसी ने नियमो का उल्लंघन राम ही नहीं, रावण ने भी नहीं किया।
किन्तु द्वापर युग मे भगवान श्री कृष्ण ने किसी गुण से स्वयं को शब्दत: नही बांधा। उन में यह सब गुण उन के लोकसंग्रह के हेतु निष्काम कर्मों में झलकते है। व्यक्तिगत मूल्यों एवम आचरण में लोभ, महत्वाकांक्षा एवम अनीति ने ज्यादा स्थान लिया। इसलिये लोग अपने हित के लिये षड्यंत्र ज्यादा रचते थे। जो व्यक्तिगत मूल्यों में ज्यादा विश्वास भी रखते थे वो उस के सही या गलत का निर्णय न ले कर अपने व्यक्तिगत मूल्यों पर ज्यादा टिके थे, जैसे भीष्म, कर्ण या द्रोणाचार्य। जो दुर्योधन का साथ न चाहते हुए भी दे रहे थे।
जब सामाजिक व्यवस्था दिशाहीन हो तो समाहित भाव से लिया उद्देश्य सर्वोपरि होता है। भगवान श्री कृष्ण ने जनहित के लिये हर गुण के विरुद्ध जा कर समाहित भाव से कर्म करने का उदाहरण दिया। युद्ध हो या शांति, कर्तव्य धर्म के लिये, जन हित मे अपने निजी स्वार्थ को दूर रखते हुए जो भी निष्काम भाव से कर्म किया जाए वो ही देवी संपदा गुण है।
चाणक्य, शिवजी, गुरु गोविंद सिंह आदि अनेक मार्गदर्शकों में हमे इस दिशा में मार्ग दिखाया कि आततायियों के किस प्रकार सामना करना चाहिए। समहितभाव से किये कार्य समाज को बुराइयों से दूर करते है तो इस मे कर्ण, भीष्म, द्रोणाचार्य, अभिमन्यु, बर्बरीक जैसे लोगो के बलिदान हवन कुंड में स्वाहा कर दिए जाते है, चाहे वो व्यक्तिगत स्वरूप में कितने भी महान हो, परन्तु समाहित भाव मे वो जनहित में नही होते।
आज के संदर्भ में यही बात लागू होती है। असमर्थ, अयोग्य एवम देवीसम्पदा गुणों से बाहर आसुरी व्यक्तियों को यदि भारत वर्ष के उत्थान के लिये बाहर करना है, तो जो अच्छे व्यक्ति भी उन के साथ होंगे, उन्हें भी हटाना होगा। इस का अर्थ कदापि नहीं है कि राजनीतिज्ञ उद्देश्य देवी संपदा के गुणों से ऊपर है।
हमे महाभारत के युद्ध से यह समझना चाहिए कि भगवान श्री कृष्ण ने धरती का भार नैतिक मूल्यों के गिरावट के संतुलन के होने दिया। किन्तु देवी सम्पद से युक्त श्री कृष्ण ने इस युद्ध के अंत मे अपने ही कुल का नाश भी गांधारी के श्राप द्वारा स्वीकार किया क्योंकि जब मूल्यों की स्थापना या उद्देश्य की पूर्ति हेतु देवीसम्पद गुणों के बाहर जा कर जनहित कार्य किया जाए तो राम राज्य बन ही नही सकता। राम का जीवन काल जहां 1000 साल का बताते है वहां श्री कृष्ण का जीवन काल 130 वर्षों का ही है। अतः जिस राज्य या देश, धर्म, जाति या विचारधारा की नींव दैवीय प्रवृति पर नही रखी जाए वो सनातन हो ही नही सकती। सनातन सत्य तो देवीसम्पद के गुणों से प्राप्त होगा। समाहित भाव मे भी यदि अनुचित होगा, तो उस जन कल्याण तो हो सकता है, परंतु सनातन सत्य की स्थापना नहीं। सनातन सत्य की स्थापना तो गीता में दिए निष्काम कर्मयोग के ज्ञान से होगी।
जो व्यक्ति समहितभाव रखता है, वो ज्ञान भी रखता है, जो ज्ञान रखता है वो देवीसम्पद गुणों के बिना हो ही नही सकता। भगवान श्री कृष्ण परब्रह हो कर इतनी लीला करते हुए भी, अकर्ता एवम साक्षी रहे। अतः जो अटल सत्य है वही सत्य रहेगा। प्रश्न किसी गुण को समय, काल, स्थान, व्यक्ति, उद्देश्य के अनुसार समंझने का है, जिसे वह ही व्यक्ति समझ सकता है, जो खुद में वेदवित हो, ज्ञानी हो एवम देवीसम्पद गुणों से युक्त हो। यदि ऐसा नही है तो वह व्यक्ति किंतना भी ज्ञानी क्यों न हो, आसुरी प्रवृति का ही माना जाता है, रावण इस का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है।
26 गुणों से युक्त होना, तत्व ज्ञानी के लिए संभव है, जन सामान्य के इन सब गुणों का ज्ञान होना और उस को आत्मसात करते रहने का प्रयास करते रहना प्रर्याप्त है। दैवीय गुण आपस में गूथे है, एक गुण दूसरे गुण को आकर्षित करता है, किसी भी गुण को आचरण में लाने से अन्य गुण स्वत: ही मनुष्य के जीवन में आने लगते है।
आज के भौतिक युग में आचरण में दैवीय गुण का लाभ आसुरी वृति के लोग, दैवीय गुण से युक्त व्यक्ति की कमजोरी मानते है। सहिष्णुता, धर्म निरपेक्षता, दया और सभी धर्मो का सम्मान का भाव आसुरी वृति के लोगो के लिए या मतांधनता का पालन करने वाले लोगो के कमजोरी है। आक्रांता, शत्रु, मतधान्त लोगो के लिए धर्म और सत्य की रक्षा के लिए कट्टर होना भी आवश्यक है।किंतु इस कार्य हेतु जो शांति पूर्वक अपने कार्य को करते रहते है, डींगे नही हांकते, और साहस और विवेक से परिस्थितियों का सामना करते है, वो लोग ही वास्तविक रचनाकार है। आज के समय में सोशल मीडिया पर जो संदेशों को बिना पढ़े, जांचे और समझे बस फॉरवर्ड कर के अपने कर्तव्य की इतिश्री करते है, वो दैवीय गुण के पात्र नहीं।
ज्ञान आचरण और व्यक्तित्व का हिस्सा है। हमे जो प्रभावित या द्रवीण करता है, वह हमारे अच्छे संस्कारों और शिक्षा का परिणाम है, किंतु जब तक वह हमारे जीवन में आचरण और व्यवहार का हिस्सा न बने, एक ढोंग से अधिक नही है। इसलिए दिन भर धार्मिक पोस्ट करने वाला भी व्यापार या समाज में धोका भी दे देता है।
अंत में यह मानते है कि दैवीय गुण अध्यात्म या मोक्ष मात्र के गुण नहीं है, यह गुण किसी भी सफल उद्योगपति, व्यवसायिक, राजनेता, संत, गृहस्थ, निष्काम कर्मयोगी या प्रत्येक जीव के गुण है। सभी में कुछ न कुछ मात्रा में यह गुण रहते ही है, क्योंकि यह वास्तविकता है, इन का अभाव ही आसुरी वृति है, इसलिए जैसे जैसे इन गुणों का प्रभाव बढ़ता है, आसुरी वृति भी समाप्त होती है। सभी गुण समान रूप से भी नही विकसित होते है, कुछ गुण अधिक और गुण कम रहते है। इसलिए इन को प्राप्त करने के लिए समय समय पर आत्मचिंतन करना ही सर्वश्रेष्ठ उपाय है।
यह मेरी व्यक्तिगत टिप्पणी है, अतः सभी अपने अपने विचार रख सकते है।
।। हरि ॐ तत सत ।। गीता – विशेष 16.03 ।।
Complied by: CA R K Ganeriwala (+91 9422310075)