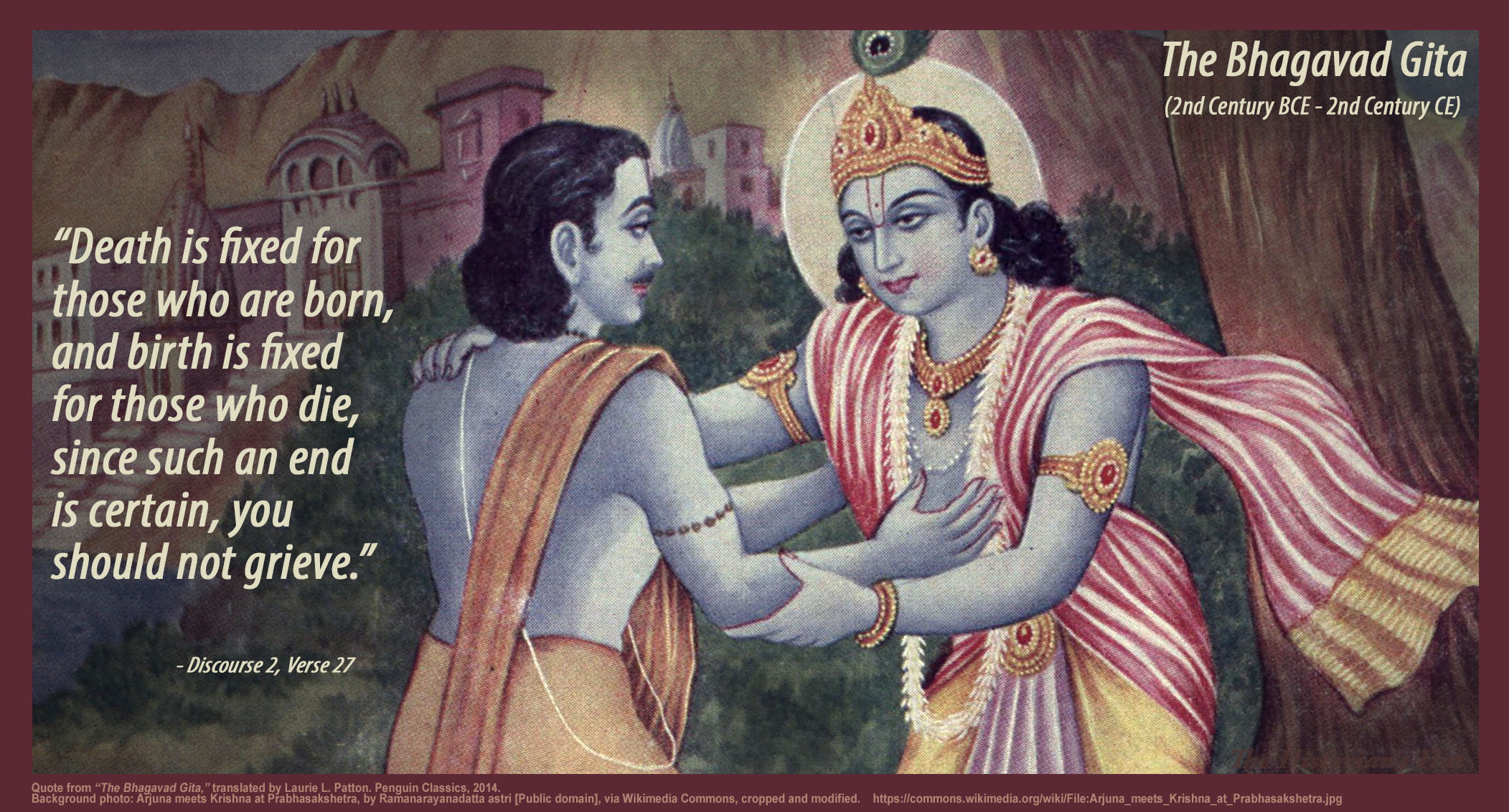।। Shrimadbhagwad Geeta ।। A Practical Approach ।।
।। श्रीमद्भगवत गीता ।। एक व्यवहारिक सोच ।।
।। Chapter 14.26 II
।। अध्याय 14.26 II
॥ श्रीमद्भगवद्गीता ॥ 14.26॥
मां च योऽव्यभिचारेण भक्तियोगेन सेवते ।
स गुणान्समतीत्येतान्ब्रह्मभूयाय कल्पते॥
“māḿ ca yo ‘vyabhicāreṇa,
bhakti-yogena sevate..।
sa guṇān samatītyaitān,
brahma-bhūyāya kalpate”..।।
भावार्थ:
जो मनुष्य हर परिस्थिति में बिना विचलित हुए अनन्य-भाव से मेरी भक्ति में स्थिर रहता है, वह भक्त प्रकृति के तीनों गुणों को अति-शीघ्र पार करके ब्रह्म-पद पर स्थित हो जाता है। (२६)
Meaning:
And he who worships me with the unwavering yoga of devotion, having gone beyond these gunas, becomes fit for attaining brahman.
Explanation:
Since this chapter is coming to an end, let us do a quick recap. We learned that this entire universe, including our mind and body, is nothing but the play of the three gunas of Prakriti – sattva, rajas and tamas. Only when we learn to stand apart from the gunas, when we separate ourselves from the gunas, can we attain liberation from the endless cycle of sorrow known as samsaara. For most of us, such a high degree of discrimination is extremely difficult. Moreover, such discrimination needs to be combined with dispassion as well as total control of the mind and the sense organs.
Knowing the impediments of fulfilling all these requirements, Arjuna wanted to know whether there was a straightforward way of releasing oneself from the influence of the gunas. Shri Krishna says that yes, it is possible. The answer is the yoga of unwavering devotion, which was the topic of chapters seven to twelve. In a nutshell, we detach ourselves from the gunas by attaching ourselves to something higher, which is Ishvara. It is like the child who gives up his toys because he loves poetry now that he is a teenager.
This yoga of devotion is not completely without effort, however. Shri Krishna adds an adjective that we need to bear in mind – avyabhichaarena or unwavering. We have learned about four types of devotees i.e. The curious, the seeker, the scholar and the knowledgeable. We cannot keep Ishvara as our goal from 7 am to 8 am and then start thinking about how to demolish our competitors from 8 am to 11 am. The one and only goal should be Ishvara. If all our goals are within the scope of our svadharma, our prescribed role in this world, they very naturally are part and parcel of our devotion towards Ishvara.
Many people are of the view that if the mind is fixed upon the personal form of God, it will not rise to the transcendental platform. Only when it is attached to the formless Brahman, will the mind become transcendental to the modes of material nature. However, this verse refutes such a view. Although the personal form of God possesses infinite guṇas (qualities), these are all divine and beyond the modes of material nature. Hence, the personal form of God is also nirguṇa (beyond the three material modes). Sage Ved Vyas explains how the personal form of God is nirguṇa: “Wherever the scriptures refer to God as nirguṇa (without attributes), they mean that he is without material attributes. Nevertheless, his divine personality is not devoid of qualities—he possesses infinite divine attributes.”
This verse also reveals the proper object of meditation. Transcendental meditation does not mean to meditate upon nothingness. The entity transcendental to the three modes of material nature is God. And so, only when the object of our meditation is God can it truly be called transcendental meditation.
Having made Ishvara our only goal, and having maintained such an awareness throughout our life, we become fit to attain brahman. How does that happen? The next and last shloka of this chapter addresses this topic.
।। हिंदी समीक्षा ।।
इस अध्याय के अंतिम दो श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण अपने परब्रह्म स्वरूप की बात कहते है। अध्याय तेहरवें से हम जिस क्षेत्र-क्षेत्रज्ञ ज्ञान को पढ़े एवम चौदहवें अध्याय में जिस गुणों को हम ने पढ़ा, वो सांख्य, वेदान्त एवम गीता का कर्म योग का ही सन्यास, ध्यान एवम ज्ञान योग का भाग है। प्रस्तुत श्लोक में भक्ति योग को भी इस मे सम्मलित किया गया है, जो हमे यह बताता है कि किसी भी मार्ग से हम ईश्वर की आराधना करें, एक स्थिति में यह सब मिल कर एक ही हो कर परमात्मा की आराधना है एवम जब तक जीवन है, कर्म नहीं छूटता, इसलिये निष्काम कर्मयोग सभी योग का साधन है, जिस से सत्वगुण हो कर लोकसंग्रह के लिये कर्म किये जायें।
बहुत से लोगों का मानना है कि अगर मन भगवान के साकार रूप पर स्थिर हो जाए तो वह पारलौकिक स्तर तक नहीं पहुंच पाएगा। जब मन निराकार ब्रह्म से जुड़ जाएगा तभी वह भौतिक प्रकृति के गुणों से परे हो पाएगा। हालाँकि, यह श्लोक इस दृष्टिकोण का खंडन करता है। हालाँकि भगवान के साकार रूप में अनंत गुण (गुण) हैं, लेकिन ये सभी दिव्य हैं और भौतिक प्रकृति के गुणों से परे हैं। इसलिए, भगवान का साकार रूप भी निर्गुण (तीन भौतिक गुणों से परे) है। ऋषि वेद व्यास बताते हैं कि भगवान का व्यक्तिगत रूप किस प्रकार निर्गुण है:
यस्तु निर्गुण इत्युक्तः शास्त्रेषु जगदीश्वरः। प्रकृतैर्हेय संयुक्तैर्गुणैर्हीनत्वमुच्यते (पद्म पुराण)।।
“जहां भी शास्त्रों में भगवान को निर्गुण (गुणों के बिना) के रूप में संदर्भित किया गया है, उनका मतलब है कि वह भौतिक गुणों से रहित है। फिर भी, उनका दिव्य व्यक्तित्व गुणों से रहित नहीं है – उनमें अनंत दिव्य गुण हैं।”
हम ने पूर्व में चार प्रकार के भक्तों आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी के बारे में पढ़ा। इसी में ज्ञानी भक्त को और आगे वर्णित करते हुए, गुणातीत भक्त के विषय में
परमात्मा कहते है जो पुरुष अव्यभिचारिणी भक्ति द्वारा अर्थात इष्ट के अतिरिक्त अन्य सांसारिक स्मरणो से सर्वथा रहित हो कर योग द्वारा अर्थात उसी नियत कर्म द्वारा मुझे निरंतर भजता है, वह इन तीनो गुणों का अच्छे प्रकार उल्लंघन करके परब्रह्म में विलीन होने के योग्य होता है। यहां परब्रह्म को एक कल्प माना गया है। परब्रह्म से एकीभाव हो जाना ही वास्तविक कल्प है। अनन्य भाव से नियत कर्म का आचरण किये बिना कोई भी गुणातीत नहीं होता। यह श्लोक अर्जुन के तृतीय प्रश्न का उत्तर है कि दिव्य स्थिति प्राप्त करने का क्या साधन है। यहां यह समझ लेना जरूरी है गुणातीत होना ज्ञान है, किन्तु अव्यभिचारिणी भक्ति दिव्य स्थिति प्राप्त करने का मार्ग है। कपिल मुनि गुणातीत थे किंतु सगर पुत्रो पर क्रोध कर बैठे। इसलिये गुणातीत की सफलता बिना अव्यभिचारिणी भक्ति के पूर्ण नहीं है। यह श्लोक ध्यान के उचित उद्देश्य को भी प्रकट करता है। भावातीत ध्यान का अर्थ शून्यता पर ध्यान करना नहीं है। भौतिक प्रकृति के तीन गुणों से परे जो तत्व है, वह ईश्वर है और इसलिए, जब हमारे ध्यान का उद्देश्य ईश्वर हो, तभी इसे सही मायने में भावातीत ध्यान कहा जा सकता है।
इसलिए मन को गुणातीत करने के लिए परमात्म-चिन्तन में लगाना आवश्यक है। श्री वसिष्ठजी ने कहा – ‘निष्पाप श्रीराम! मन जिस किसी से भी उत्पन्न हुआ हो और जो कुछ भी उसका स्वरूप हो, बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि वह उसे प्रयत्नपूर्वक अपनी मुक्ति के लिए परमात्मा में लगाये । परमात्मा में लगाया हुआ मन वासनारहित एवं शुद्ध हो जाता है। तत्पश्चात वह कल्पनाशून्य होकर परमात्मभाव को प्राप्त हो जाता है । अतः मनुष्य को उचित है कि वह मोक्ष प्राप्ति के लिए मन को परमात्म चिन्तन में लगाये।।’
धर्म का व्यावहारिक शास्त्रीय ग्रंथ होने के कारण गीता में केवल सिद्धान्तों का प्रतिपादन नहीं किया गया है। इसमें प्रत्येक सिद्धान्त के विवेचन के पश्चात् उस साधन का वर्णन किया गया है, जिस के अभ्यास से एक साधक सिद्धावस्था को प्राप्त हो सकता है। प्रकृति के गुणों में अनेक चमत्कार, आकर्षण, भ्रांतियां, सिद्धियां, एवम कर्म है, किन्तु यह समस्त क्रियाएं जीव को गुणातीत नहीं करती। इसलिये ध्यान, पूजा, यज्ञ, सांसारिक कर्म करने वाला जीव इन तीन गुणों में ही जीवन व्यतीत करता रहता है। एक सिद्ध पुरुष भी प्रकृति के गुणों के आकर्षण से मुक्त नहीं हो पाता क्योंकि उस अपना अहम से”मैं” जीवित रहता है। अव्यभिचारिणी भक्ति ही मार्ग है जो इस अहम से मुक्ति दिला कर परब्रह्म की ओर ले जाता है।
परमात्मा कहते है, जो अव्यभिचारी भक्तियोग से मेरी सेवा करता है, उस का अहम नष्ट हो जाता है। ईश्वर से परम प्रीति भक्ति कहलाती है। प्रिय वस्तु में हमारा मन सहजता से रमता है। हमारा सम्पूर्ण स्वभाव हमारे विचारों से पोषित होता है। यथा विचार तथा मन, यह नियम है। इसलिये एकाग्र चित्त से आत्मा के अनन्तस्वरूप का चिन्तन करने से परिच्छिन्न नश्वर अहंकार की समाप्ति और स्वस्वरूप में स्थिति हो जाती है। यह सत्य है कि परमात्मा का अखण्ड चिन्तन एक समान निष्ठा एवं प्रखरता के साथ संभव नहीं होता है। जिस स्थिति में आज हम अपने को पाते हैं, उसमें यह सार्मथ्य नहीं है कि मन को दीर्घकाल तक ध्यानाभ्यास में स्थिर कर सकें। साधकों की इस अक्षमता को जानते हुये भगवान् एक उपाय बताते हैं, जिसके द्वारा हम दीर्घकाल तक ईश्वर का स्मरण बनाये रख सकते हैं। और वह उपाय है सेवा। तृतीय अध्याय में यह वर्णन किया जा चुका है कि ईश्वरार्पण की भावना से किए गए सेवा कर्म ईश्वर की पूजा (यज्ञ) बन जाते हैं।
अखण्ड ईश्वर स्मरण तथा सेवा साधना मन के विक्षेपों को दूर करके उसे ध्यान की सूक्ष्मतर साधना के योग्य बना देती है। तमस और रजस की मात्रा घटती जाती है और उसी अनुपात में सत्त्वगुण प्रवृद्ध होता जाता है। ऐसा सत्त्वगुण प्रधान साधक ध्यान की साधना के योग्य बन जाता है। यह स्वयंप्रकाश आत्मा, पाँचों कोशोंसे विलक्षण (भिन्न) तथा तीनों अवस्थाओंका साक्षी होनेके कारण, सभी विकारोंसे रहित, निर्मल और शुद्धसत्स्वरूप है, उसे ही विद्वान पुरुषोंको अपनी वास्तविक सदानन्द आत्मा समझना चाहिए।
अव्यभिचारिणी भक्ति का उदाहरण भक्त प्रह्लाद का भी जो अनेक संकट में भी भक्ति पर कायम रहा। व्यवहार में हम आसक्ति और कामना में स्वार्थ की भक्ति करते है, भक्ति में कुछ प्राप्त होने की आशा भी रखते है। इसलिए एकनिष्ठ हो कर अपने आचरण, चिंतन और व्यासायिक बुद्धि को साम्य अवस्था में न लाते हुए, भगवद पाठ विभिन्न देवी देवताओं का करते रहते है। इसलिए जब तक बुद्धि स्थिर नही होती, भक्ति का स्वरूप भी अव्यभिचारिणी नही होता, न ही भक्ति अनन्य भक्ति में परिवर्तित होती है। यदि सजग न रहे तो भक्ति अहंकार में भी परिवर्तित हो जाती है। इसलिए गुणातीत होने के लिए भक्ति अव्यभिचारिणी व अनन्य होनी ही चाहिए।
ऐसे साधक से आत्मानुभूति दूर नहीं रहती। अहम ब्रह्मास्मि उत्तम अधिकारी ब्रह्मस्वरूप का अनुभव कर स्वयं ब्रह्म बन जाता है। जैसे स्वप्नद्रष्टा जागने पर स्वयं ही जाग्रत पुरुष बनता है।यह साधक स्वयं ब्रह्म कैसे बनता है, यह आगे पढ़ते है।
।। हरि ॐ तत सत।। गीता – 14.26।।
Complied by: CA R K Ganeriwala (+91 9422310075)