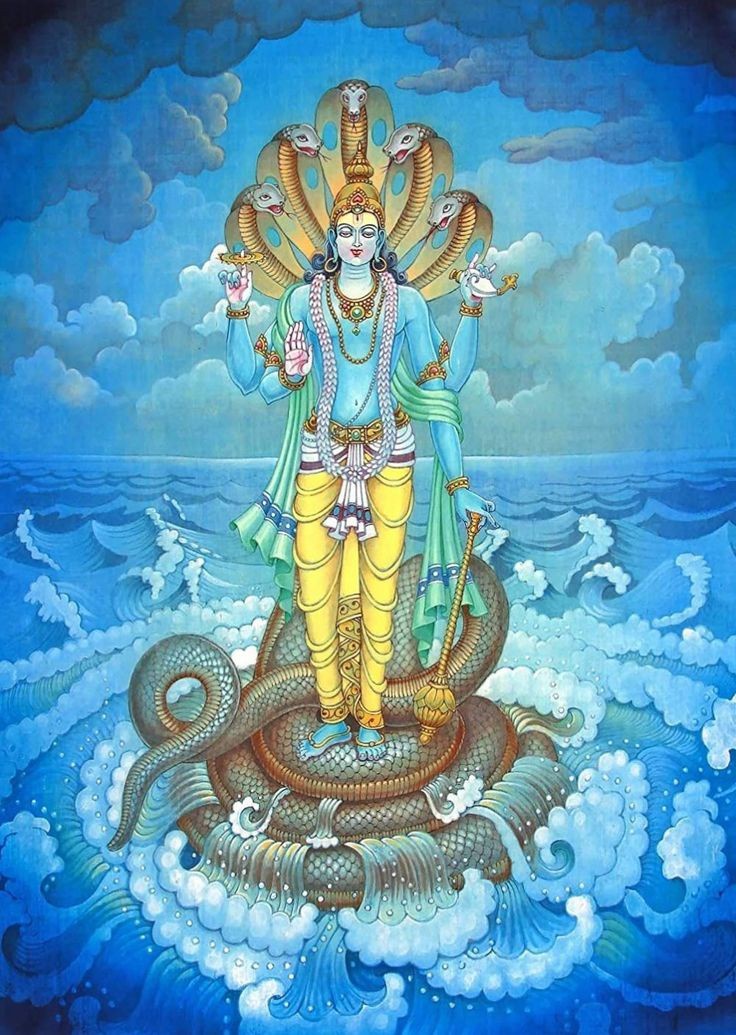।। Shrimadbhagwad Geeta ।। A Practical Approach ।।
।। श्रीमद्भगवत गीता ।। एक व्यवहारिक सोच ।।
।। Chapter 14.16 II
।। अध्याय 14.16 II
॥ श्रीमद्भगवद्गीता ॥ 14.16॥
कर्मणः सुकृतस्याहुः सात्त्विकं निर्मलं फलम् ।
रजसस्तु फलं दुःखमज्ञानं तमसः फलम्॥
“karmaṇaḥ sukṛtasyāhuḥ,
sāttvikaḿ nirmalaḿ phalam..।
rajasas tu phalaḿ duḥkham,
ajñānaḿ tamasaḥ phalam”..।।
भावार्थ:
सतोगुण में किये गये कर्म का फल सुख और ज्ञान युक्त निर्मल फल कहा गया है, रजोगुण में किये गये कर्म का फल दुःख कहा गया है और तमोगुण में किये गये कर्म का फल अज्ञान कहा गया है। (१६)
Meaning:
The result of good action is sattvik and pure, it is said, while the result of rajas is sorrow, and the result of tamas is ignorance.
Explanation:
In this verse, Lord Krishna comes to the next topic; and that is the phalam (result) for the predominance of each guṇa; so the previous two slōkās talked about gathi, now this slōka talk about phalam and the difference between Gathi and Phalam; Gathi is the consequence after death; whereas Phalam is the consequence in this life itself.
The word prakāśhakam means “illuminating.” The word anāmayam means “healthy and full of well-being.” By extension, it also means “of peaceful quality,” devoid of any inherent cause for pain, discomfort, or misery. The mode of goodness is serene and illuminating. Thus, sattva guṇa engenders virtue in one’s personality and illuminates the intellect with knowledge. It makes a person become calm, satisfied, charitable, compassionate, helpful, serene, and tranquil. It also nurtures good health and freedom from sickness. While the mode of goodness creates an effect of serenity and happiness, attachment to them itself binds the soul to material nature.
Rajo guṇa, the mode of passion, which excites the passions of the living being, and binds the soul in innumerable worldly desires and tamo guṇa, the mode of ignorance, which literally wants to kill the soul, by degrading it into sloth, languor, and nascence.
When new year comes around, many people make new year resolutions to lose weight. Many take a gym membership, but most end up using it only for a few days. The ones that consciously develop a habit of going to the gym everyday are the most likely to lose weight. Even if they go to the gym for ten minutes every day, they will lose weight. This is because habits are self-reinforcing. A behaviour creates a habit, which pushes us to repeat the behaviour, which strengthens the habit, and so on.
Similarly, we can shape our mental states by choosing our actions consciously. Shri Krishna says that sattvic or selfless actions generate a sattvic state, rajasic or selfish actions generate a rajasic state, and tamasic or ignorant actions generate a tamasic state. If we are predominantly rajasic by nature, we can improve our state by emphasizing the performance of sattvic actions. If we are predominantly tamasic by nature, we can change it by emphasizing the performance of rajasic actions.
The law of karma holds true in every situation, including this one. If we perform rajasic actions, we will attain temporary joy, which will eventually generate sorrow. It does not take a large amount of raaga dvesha, likes or dislikes, to make us act selfishly. And if we perform tamasic actions, we will continue to live our lives in inertness and ignorance. Only through sattvic actions will we create a state of purity and serenity in our mind.
।। हिंदी समीक्षा ।।
इस श्लोक में भगवान कृष्ण अगले विषय पर आते हैं; और वह है प्रत्येक गुण की प्रबलता का फल; अतः पिछले दो श्लोकों में गति के बारे में बात की गई थी, अब यह श्लोक फल के बारे में तथा गति और फलम के बीच के अंतर के बारे में बात करता है; गति मृत्यु के बाद का परिणाम है; जबकि फलम इस जीवन में ही परिणाम है।
प्रकाशकम् शब्द का अर्थ है “प्रकाशमान।” अनामयम् शब्द का अर्थ है “स्वस्थ और खुशहाली से भरा हुआ।” विस्तार से, इसका अर्थ “शांतिपूर्ण गुण” भी है, जिसमें दर्द, परेशानी या दुख के लिए कोई अंतर्निहित कारण नहीं होता। सत्वगुण शांत और प्रकाशमान होता है। इस प्रकार, सत्वगुण व्यक्ति के व्यक्तित्व में सद्गुण उत्पन्न करता है और बुद्धि को ज्ञान से प्रकाशित करता है। यह व्यक्ति को शांत, संतुष्ट, दानशील, दयालु, मददगार, शांत और शांत बनाता है। यह अच्छे स्वास्थ्य और बीमारी से मुक्ति का पोषण भी करता है। जबकि सत्वगुण शांति और खुशी का प्रभाव पैदा करता है, उनके प्रति आसक्ति ही आत्मा को भौतिक प्रकृति से बांध देती है।
रजो गुण, जो कि वासना का गुण है, जो कि जीव की वासनाओं को उत्तेजित करता है तथा आत्मा को असंख्य सांसारिक इच्छाओं में बांधता है, तथा तमो गुण, जो कि वस्तुतः आत्मा को आलस्य, सुस्ती तथा अज्ञानता में गिराकर उसे मार डालना चाहता है।
वास्तव में कर्म न सात्त्विक होते हैं न राजस होते हैं और न तामस ही होते हैं। सभी कर्म क्रियामात्र ही होते हैं। वास्तव में उन कर्मों को करने वाला कर्ता ही सात्त्विक, राजस और तामस होता है। सात्त्विक कर्ता के द्वारा किया हुआ कर्म सात्त्विक, राजस कर्ता के द्वारा किया हुआ कर्म राजस और तामस कर्ताके द्वारा किया हुआ कर्म तामस कहा जाता है।
जब श्रीरामचन्द्रजी ने गुरूदेव श्री वसिष्ठजी से प्रश्न पूछा –
‘ भगवन! कर्म के द्वारा कर्ता का निर्माण होता है और कर्ता से कर्म, जैसे बीज से अंकुर होता है और अंकुर से बीज । यदि कर्म कि फल अवश्य मिलता है, तब प्राणियों के जन्म आदि में वही हेतु हुआ। फिर आपने उत्पत्ति को अकारण या अज्ञानकल्पित कैसे बताया? मेरे इस संशय का निवारण कीजिए।’
तब श्री रामचंद्र जी को कर्म के विषय में वशिष्ठ जी कहते है।
‘ हे रघुनन्दन! यह संकल्प – विकल्पात्मक मन का विकास ही कर्मों का कारण है – उसी के अनुसार फल प्राप्त होता है। मन के संयोग के बिना किये हुए कर्म फलदायक नहीं होते।।’
‘सृष्टि के आरम्भ में परम- पदरूपी ब्रह्म से मनरूपी तत्त्व उत्पन्न हुआ, तभी से मन के संकल्प के अनुसार जीवों का कर्म भी उत्पन्न हुआ और जीव पूर्व वासना के अनुसार देहवाला होने के कारण देह में अहंभाव से स्थित है। मन से कर्म की उत्पत्ति हुई; इसलिए बीज और वृक्ष की भाँति कारण-कार्यरूप मन और कर्म परस्पर अभिन्न हैं।। ‘
‘इस जगत में क्रिया का होना ही विद्वानों द्वारा कर्म बताया गया है । उस क्रिया का आश्रयभूत देह भी पहले मन ही था अर्थात यह देह भी मन का ही संकल्प होने के कारण मनोरूप ही है। इसी प्रकार क्रिया भी मन का संकल्प होने से मन का ही स्वरूप है।। ‘
‘कर्मों का फल अवश्यम्भावी है। ज्ञानपूर्वक किया हुआ कर्म चाहे पूर्वजन्म का हो या इस जन्म का, वह क्रियारूप पुरुषार्थ ही पुरुष का परम प्रयत्न है। वह कभी निष्फल नहीं होता। जो मुक्त पुरुष है, उसी के कर्म का नाश होनेपर मन का नाश होता है, मन का नाश ही कर्म का अभाव है। जो मुक्त नहीं है, उसके कर्म और मन का नाश कदापि नहीं होता। अग्नि और उष्णता की भाँति सदा परस्पर मिले हुए मन और कर्म, इन दोनों में से एक का अभाव होनेपर दोनों का ही अभाव हो जाता है।। ‘
क्रिया का कर्ता जब भी किसी कर्म को करता है तो उस कर्म में निहित आसक्ति और कामना के साथ कर्तृत्व और भोक्त्त्व भाव से गुण की व्याख्या होती है। निषिद्ध कर्म को छोड़ कर सभी कर्म करने योग्य है।
महाभारत में एक ब्राह्मण को मांस के विक्रेता द्वारा या एक ब्राह्मण को गृहस्थ स्त्री द्वारा दिया ज्ञान, यही सिद्ध करता है कि गुण का प्रकार कर्ता के आत्मिक आचरण और उस के कर्म के प्रति कर्तृत्व एवम भोक्त्व भाव पर निर्भर है। निष्काम भाव से लोकसंग्रह के लिए कर्तव्य धर्म के अनुसार किया कार्य सात्विक या राजसी ही होता है।
प्रकृति एवम जीव का संयोग सृष्टि है जिस में जीव साक्षी एवम अकर्ता है और प्रकृति क्रियाशील। अतः यह तीन सत-रज-तम प्रकृति की क्रिया हुई किन्तु जीव इस मे लिप्त कर्तृत्त्व भाव से होता है। इसलिये सत-रज-तम की हर क्रिया प्रकृति ही करती है और जीव उस मे कर्तृत्त्व भाव रखता है। यदि यह भाव न हो तो जीव एवम प्रकृति पृथक पृथक हो जाएंगे।
इस से यह स्पष्ट है कि प्रकृति के यह तीनों गुण का आधार कर्म न हो कर जीव के लिये कर्तृत्त्व भाव है। इस लिये जिस क्रिया में जिस गुण के अनुरूप भाव होगा वो क्रिया उसी गुण की होगी।
स्वामी रामकृष्ण हंस वैश्या के घर गए किन्तु उन भाव सत का था इसलिये उन का वेश्या के यहाँ जाना भी सात्विक है। भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों के संग रास लीला की किन्तु भाव निश्छल एवम त्यागमय प्रेम का था जिस में काम या वासना नही थी, इसलिये रासलीला भी सात्विक हुई। अतः प्रकृति के यह तीनों गुण कर्म पर आधारित न हो कर भाव पर आधारित है। इसलिये सत के भाव सुख, वैराग्य, अभिमान है, रज के आसक्ति, लोभ, स्पृहा या संग, कर्म है और तम के भाव प्रमाद, आलस्य एवम निंद्रा है।
सत्त्वगुण का स्वरूप निर्मल, स्वच्छ, निर्विकार है। अतः सत्त्वगुण वाला कर्ता जो कर्म करेगा, वह कर्म सात्त्विक ही होगा क्योंकि कर्म कर्ता का ही रूप होता है। इस सात्त्विक कर्म के फलरूप में जो परिस्थिति बनेगी, वह भी वैसे ही शुद्ध, निर्मल, सुखदायी होगी। फलेच्छारहित होकर कर्म करने पर भी जबतक सत्त्वगुण के साथ कर्ताका सम्बन्ध रहता है, तबतक उस की, सात्त्विक कर्ता संज्ञा होती है और तभी तक उस के कर्मों का फल बनता है। परन्तु जब गुणों से सर्वथा सम्बन्ध विच्छेद हो जाता है, तब उसकी सात्त्विक कर्ता संज्ञा नहीं होती और उसके द्वारा किये हुए कर्मों का फल भी नहीं बनता, प्रत्युत उसके द्वारा किये हुए कर्म अकर्म हो जाते हैं।
रजोगुणका स्वरूप रागात्मक है। अतः रागवाले कर्ता के द्वारा जो कर्म होगा, वह कर्म भी राजस ही होगा और उस राजस कर्म का फल भोग होगा। तात्पर्य है कि उस राजस कर्म से पदार्थों का भोग होगा, शरीर में सुखआराम आदिका भोग होगा, संसार में आदरसत्कार आदि का भोग होगा और मरनेके बाद स्वर्गादि लोकों के भोगोंकी प्राप्ति होगी। परन्तु ये जितने भी सम्बन्धजन्य भोग हैं, वे सब के सब दुःखों के ही कारण हैं। इसी दृष्टि से भगवान्ने यहाँ राजस कर्म का फल दुःख कहा है।
तमोगुणका स्वरूप मोहनात्मक है। अतः मोहवाला तामस कर्ता परिणाम, हिंसा, हानि और सामर्थ्य को न देखकर मूढ़ता पूर्वक जो कुछ कर्म करेगा, वह कर्म तामस ही होगा और उस तामस कर्मका फल अज्ञान अर्थात् अज्ञानबहुल योनियों की प्राप्ति ही होगा। उस कर्म के अनुसार उस का पशु, पक्षी, कीट, पतङ्ग, वृक्ष, लता, पहाड़ आदि मूढ़योनियों में जन्म होगा, जिन में अज्ञान (मूढ़ता) की मुख्यता रहती है।
सावधानीपूर्वक अध्ययन करने पर हमें ज्ञात होगा कि अन्तकरण का विचार ही समस्त कर्मों का जनक है विचार बोये गये बीज हैं, तो कर्म हैं अर्जित की गयी उपज। घासपात के बीजों से मात्र घास ही उत्पन्न होगी वैसे ही अशुभ संकल्पों से अशुभ कर्म ही होंगे। बाह्य जगत् में व्यक्त हुए ये अशुभ कर्म दुष्प्रवृत्तियों का संवर्धन करते हैं और इस प्रकार मन के विक्षेप शतगुणित हो जाते हैं। यदि कोई पुरुष सेवा और भक्ति, स्नेह और दया, क्षमा और करुणा का शान्त, सन्तुष्ट, प्रसन्न और पवित्र जीवन जीता है। तो निश्चय ही ऐसा जीवन उसके सात्विक स्वभाव का ही परिचायक है। यह तथ्य जैसे सिद्धान्तत सत्य है वैसे ही लौकिक अनुभव के द्वारा भी सिद्ध होता है। ऐसे आदर्श जीवन जीने वाले पुरुष को अवश्य ही अन्तकरण की शुद्धि प्राप्त होती है।
यहाँ यह प्रश्न सम्भव हो सकता है कि यदि वर्तमान जीवन में कोई व्यक्ति अत्यन्त अधपतित है, तो किस प्रकार वह अपना उद्धार प्रारम्भ कर सकता है। यदि कर्म विचारों की अभिव्यक्ति हैं और अन्तकरण में स्थित विचारों का स्वरूप अशुभ है, तो ऐसे व्यक्ति के विचारों के आमूल परिवर्तन की अपेक्षा हम कैसे कर सकते हैं विश्व के सभी धर्मों में अपनी विधि और निषेध की भाषा में इस प्रश्न का उत्तर एक मत से यही दिया गया है कि सत्य के साधकों, भगवान् के भक्तों और संस्कृति के समुपासकों को सदाचार और नैतिकता का आदर्श जीवन जीने का प्रयत्न करना चाहिए।
वैचारिक परिवर्तन का यह प्रथम चरण है। इसमें कोई सन्देह नहीं कि मन को अनुशासित करना और विचारों के स्वरूप को परिवर्तित करना सरल कार्य नहीं है किन्तु कर्मों के प्रकार को परिवर्तित करना और अपने बाह्य आचरण और व्यवहार को संयमित करना अपेक्षाकृत सरल कार्य है। इसलिए, सदाचार और अनुशासित व्यवहार आत्मोत्थान की महान् योजना के प्रारम्भिक चरण माने गये हैं। सदाचार के पालन से शनैशनै सद्विचारों का निर्माण भी प्रारम्भ हो जाता है।यही कारण है कि सभी राष्ट्रों की संस्कृतियों में बालकों से कुछ नियमों के पालन का आग्रह किया जाता है, जैसे श्रेष्ठजनों का आदर, आज्ञाओं का पालन, असत्य का त्याग, शास्त्रों का स्वाध्याय, शिक्षा स्वच्छता आदि। जब बालक से इन नियमों का पालन करने को कहा जाता है, तब सम्भवत उन्हें ये सब नियम क्रूर नियम प्रतीत होते हैं, जिनका पालन करते हुए उन्हें जीने के लिए बाध्य किया जाता है। तथापि, दीर्घकाल की अवधि में अनजाने ही ये नियम बालकों के विचारों को अनुशासित करते हैं। सदाचार से मन सात्विक और निर्मल बन जाता है। इससे प्राप्त होने वाले फल, मनप्रसाद, न्यूनतम विक्षेप, चित्त की एकाग्रता, श्रद्धा, भक्ति, जिज्ञासा इत्यादि है। विकार और विक्षेप ये मन की अशुद्धियां हैं? जो अशुभ कर्मों से और अधिक प्रवृद्ध होती हैं। सत्कर्म अपने स्वभाव से ही मनोद्वेगों को नष्ट करके मन को शान्त और प्रसन्न करते हैं।
प्रकृति में आप के कर्मो का खाता खुला है, इसलिये आप जिस प्रकार के कर्म करते है, प्रकृति उसी प्रकार की जमा कर्मो की राशि व्याज सहित अगले जन्म में उस योनि में जन्म दे कर लौटाती है। प्रकृति के इस बैंक एकाउंट में जो जैसा जमा करेगा वो वैसे ही फल पायेगा। जो जमा नहीं करता, वो मोक्ष को प्राप्त होता है किंतु खाते को खोलने एवम जमा करने के नियम प्रकृति तय करती है, जीव नही।
सत्त्व, रज और तम इन तीन गुणों का लक्षण क्रमश विवेक, विक्षेप और आवरण है। अत साधक का अधिक से अधिक प्रयत्न सत्वगुण में स्थिति की प्राप्ति के लिए होना चाहिए क्योंकि सक्रिय शान्ति की स्थिति ही सत्त्व है, जो मनुष्य के आन्तरिक जीवन का रचनात्मक क्षण होता है। यही एक मात्र उपाय है जिस से जीव प्रकृति के बैंक खाते में अधिक से अधिक सत्वगुणो की धनराशि जमा कर सके। कर्मो का लेखा जोखा ऐसा है कि बिना उधारी चुकाए, मुक्ति नही मिलती।
सात्त्विक, राजस और तामस कर्मों के मूल में गुणों को बताने के लिये आगे का श्लोक पढ़ते हैं।
।। हरि ॐ तत सत।। गीता – 14.16।।
Complied by: CA R K Ganeriwala (+91 9422310075)