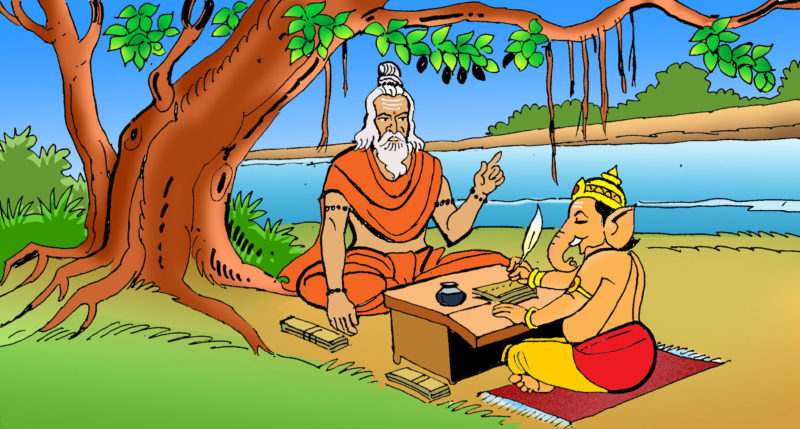।। Shrimadbhagwad Geeta ।। A Practical Approach ।।
।। श्रीमद्भगवत गीता ।। एक व्यवहारिक सोच ।।
।। Chapter 14.12 II
।। अध्याय 14.12 II
॥ श्रीमद्भगवद्गीता ॥ 14.12॥
लोभः प्रवृत्तिरारम्भः कर्मणामशमः स्पृहा ।
रजस्येतानि जायन्ते विवृद्धे भरतर्षभ॥
“lobhaḥ pravṛttir ārambhaḥ,
karmaṇām aśamaḥ spṛhā..।
rajasy etāni jāyante,
vivṛddhe bharatarṣabha”..।।
भावार्थ:
हे भरतवंशीयों में श्रेष्ठ! जब रजोगुण विशेष बृद्धि को प्राप्त होता है तब लोभ के उत्पन्न होने कारण फल की इच्छा से कार्यों को करने की प्रवृत्ति और मन की चंचलता के कारण विषय-भोगों को भोगने की अनियन्त्रित इच्छा बढ़ने लगती है। (१२)
Meaning:
Greed, activity, commencement of actions, unrest, desire. These arise when rajas is predominant, o foremost among the Bharataas.
Explanation:
Shri Krishna addressed Arjuna as “bharatarshabha”, the foremost scion of the Bharata dynasty, and enumerates the marks of a person who is under the influence of raajas. He says that whenever our mind generates thoughts of greed, selfish activity, commencement of action, unrest or uneasiness, and desire for even trivial things, we should realize that we are under the sway of rajas. In fact, we consider this to be our natural state of mind, especially during the waking hours of the day.
Most of us start our day with Pray to GOD, to give us strength, but what for? It is for success and for earning. Because when the mode of passion becomes prominent, we may think, “I must surely progress on the spiritual path, but what is the hurry? At present, I have many responsibilities to discharge, and they are more important.” Success moves us to workaholic and we want our sub ordinate also gives result as per our desire. This creates stage, where we become selfmade person, egoist and starts saying our story of success to next generation. If they do not listen, we fight with them or disappointed. Though the mind’s natural sentiments may be inclined toward the world, yet with the intellect, we have to force it into the spiritual realm. Initially, this may seem difficult, but with practice it becomes easy. This is just as driving a car is difficult initially, but with practice it becomes natural.
If we look at the first half of the shloka in reverse order, we start with spruha, which is a selfish desire for objects that have nothing to do with our duties, like a gold watch. Frequent thoughts for acquiring the gold watch led to ashama or restlessness, where we are not satisfied with our present situation and want to do something else. We then begin to act, karmanaam aarambha, so that we can acquire this gold watch. Our plans may lead us to do another part time job or withdraw from our savings, which is pravritti, engaging in selfish action. Even after we acquire the gold watch, we are not satisfied and want another one. That is lobha, greed, the height of rajasic influence on our mind.
It is not easy to detect whether our actions are prompted by selfishness or not. Only a pure mind that has been cleansed of selfishness through karma yoga, with the aid of a guru, can recognize the subtle difference between sattvic and rajasic actions. Karma yoga teaches us to analyze our qualification and proclivity for selecting an appropriate vocation. If we are trained to become an actor, and are also passionately interested in acting, then that becomes our vocation. There is a baseline level of rajas needed to perform actions towards fulfilling the duties of our vocation, which is perfectly fine. Shri Krishna says that we need to watch for signs where rajas increase beyond that baseline level, where selfishness creeps into our actions.
।। हिंदी समीक्षा ।।
रज गुण की वृद्धि के लक्षण के लिये जीव में जब सुख एवम वैराग्य का स्थान लोभ, सांसारिक प्रवृतियां, कर्मो पर अधिक आकर्षण, विषय भोगों की लालसा, अशांति एवम स्पृहा लेने लगे, तो यह जान लेना चाहिए कि रज गुण सत्त्व एवम तम पर प्रबल हो गया है।
जब रजोगुण प्रबल हो जाता है, तो हम सोचते हैं, “मुझे आध्यात्मिक पथ पर अवश्य प्रगति करनी चाहिए, लेकिन जल्दी क्या है? इस समय मुझे कई जिम्मेदारियाँ निभानी हैं, और वे अधिक महत्वपूर्ण हैं।”
उस के अंदर एक असंतुष्टि रहती है, जिस से वो जितना प्राप्त है उस से अधिक प्राप्त करने की चेष्टा करता है। घर है तो महल चाहिये, पद छोटा है तो सर्वश्रेष्ठ पद चाहिए। धन में तो 99 के चक्कर मे लगा रहता है तथा और और की रट लगी रहती है।
उस मे इन्द्रिय तृप्ति की कोई सीमा नहीं होती एवम सदैव अपने परिवार एवम स्वजनों के साथ भोग विलास द्वारा इंद्रियाओ की तृप्ति के साधन जुटाता रहता है। उस के अंदर इन सब के खोने का डर भी रहता है। धन उपार्जन के समय कर्तव्य- अकर्तव्य का विवेचन छोड़ कर दूसरे के स्वत्व पर भी अधिकार जमाने की इच्छा या चेष्टा करने लगता है।
रजोगुण बढ़ जाने से जीव के अन्तःकरण में सत्व गुण के कार्य प्रकाश, विवेकशक्ति और शांति आदि एवम तमोगुण के कार्य निंद्रा और आलस्य आदि दोनों ही प्रकार के भाव दब जाते है।
रज गुण प्रकृति की मध्यम प्रवृति है जो मनुष्य को कर्मठ बनाती है। मनुष्य सुख सुविधा के प्रकृति को भी चुनौती देता हुआ अपने सामर्थ्य एवम बल पर भौतिक सुविधाओ को बढ़ाता है, विभिन्न प्रकार के अनुसंधान एवम खोज कर के भौतिक उन्नति कर के घर, सड़क, यातायात आदि के साधन जुटाता है एवम वर्चस्व की लड़ाई में युद्ध की सामग्री एवम बल में वृद्धि करता है।
आज के युग मे शिक्षा, उस के पश्चात व्यापार एवम व्यवसाय एवम गृहस्थ जीवन, डॉक्टर, इंजीनियर, CA, नेता, प्रदेश, राज्य, देश एवम विश्व मे अधिकतर कर्मठ व्यक्तित्व रजोगुणी लोगों का है। इस से सत्व की ओर बढ़ने का मार्ग ही निष्काम कर्मयोग है। अर्जुन रजोगुण युक्त श्रेष्ठ योद्धा था, युद्ध लड़ना उस का कर्म था, अतः कर्तव्य धर्म का पालन का विचार रजोगुणी व्यक्तित्व के लिये है जो निष्काम हो अपने कर्तव्य का पालन करे। सकाम होने से वो तमोगुण की ओर बढेगा और निष्काम होने से सत्त्व गुण की ओर।
रजगुण से युक्त प्राणी अनाकारण किसी को नुकसान नही पहुचाता, वह सब के साथ भौतिक साधनों के साथ सुख से रहना चाहता है।
मन की स्वाभाविक भावनाएँ भले ही संसार की ओर झुकी हों, फिर भी बुद्धि के द्वारा हमें उसे आध्यात्मिक क्षेत्र में लाना होगा। शुरू में यह कठिन लग सकता है, लेकिन अभ्यास से यह आसान हो जाता है। यह वैसा ही है जैसे कार चलाना शुरू में कठिन लगता है, लेकिन अभ्यास से यह स्वाभाविक हो जाता है।
सत्वगुण के व्यक्ति में यदि कुछ मात्रा में रजगुण क्रियाशील रहते है तो वह लोकसंग्रह के कार्य करता है, संसार को मुक्ति या मोक्ष का मार्ग दिखाता है। महात्मा बुद्ध, जनक या नानक देव ऐसे ही सत्व गुण युक्त प्राणी थे।
किन्तु जब रज गुण के साथ सत्व गुण की कम मात्रा हो तो भौतिक सुखों के लिये जीव भजन, कीर्तन, उपवास, ध्यान पूजा, यज्ञ एवम दान धर्म करने लगता है। उस का धार्मिक होने एवम उस के लिये कर्म भी करने का उद्देश्य किसी भौतिक वस्तु, समाज, परिवार आदि की सुविधा की प्राप्ति होता है।
परमात्मा ने अर्जुन को विराट रूप दर्शन में सभी योद्धाओं के उन के विराट स्वरूप में समाते हुए दिखा कर कहा था कि जिस को तू मारने की बात करता है वो तो मेरे द्वारा पहले ही मृत्यु को प्राप्त हो गए है, तू इन का निमित्त बन और संसार के राज्य एवम सुख-वैभव का उपभोग कर। रजोगुण व्यक्ति की संसार मे उच्च पदों पर या उच्च व्यापारी, उद्योगपति, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति हो कर संसार के वैभव का उपभोग करते है एवम लोकसंग्रह के लिये कर्म करते है। यह अपनी क्षमता एवम ईश्वर पर विश्वास रख कर आलसी की भांति दैव दैव न पुकारते हुए इतिहास की रचना करते है। प्रकृति के वैभव का आनंद ले कर कर्म करते है।
परमात्मा का कथन स्पष्ट है कि प्रकृति से सामंजस्य कर के निष्काम कर्म योगी उस के वैभव का आनंद एवम सुख ले सकता किन्तु वो उस के आसक्त नही होता। स्वयं भगवान राम एवम कृष्ण राज परिवार में जन्म लिया एवम राज्य के दायित्व को निर्वाह करते हुए, राज्य के सभी साधनों का उपयोग किया। रजोगुणी कर्मयोगी ही होता है इसलिये उसे उन सब संसाधनों को उपयोग करने का अधिकार है जिस के लिये एवम जिस के द्वारा वो कर्म करता है किंतु वह यदि निष्काम है तो उस मे किसी संसाधन पर कर्ता भाव या स्वामित्व का अधिकार न रखते हुए वह स्वयं को प्रकृति के कृत्य का निमित्त ही मानता है। इस प्रकार वह ऊंचे पद एवम स्थान पर प्रकृति के वैभव का सुख एवम आनंद का उपभोग करता है एवम यदि वो सकाम है तो कर्म बंधन के फल को प्राप्त होता है।
निष्काम कर्म की प्रबलता सत्व गुण में भी रहती है, किंतु वहां वह लोकसंग्रह हेतु निष्काम होती है, जिस स्थान पर कर्म करने की प्रबलता लोभ, प्रवृति, कर्मारम्भ (सकाम भाव से कर्म को शुरू करना),अशम (मन की चंचलता) एवम स्पृहा (सांसारिक पदार्थो की इच्छा) के भाव से हो, तो वह रजो गुण की प्रबलता से होती है। यह कर्म की भावना हिंसा, अशांति या किसी को कष्ट या हानि दे कर की जाए तो रजो गुण में तमो गुण का प्रदुर्भाव कहा जा सकता है। जैसे दान मांगना नीच कर्म है किंतु लोकसंग्रह हेतु मदन मोहन मालवीय जी द्वारा दान मांग कर विश्व विद्यालय की स्थापना करना सत्व गुण का कर्म है।
व्यवहार में इस संसार की भौतिक उन्नति रज प्रधान लोगों ने ही की है। धन, नाम, पद और सुख की लालसा व्यक्ति को सांसारिक कर्म की ओर खींचती है। जिस से वह अपने सभी आवश्यकताओं को भुला कर कर्म पर जुट जाता है। याद रहे लक्ष्य लोकसंग्रह का हो तो वही कर्म सत गुण की और ले जाने वाला है और यदि लक्ष्य सांसारिक सुख भोगने की लालसा से जुड़ा है तो तमो गुण की ओर ले जाता है। अत्यधिक कर्म में हम अपने आस पास सभी से कठिन परिश्रम और सही कार्य की आशा रखता है और नही होने पर चिड़चिड़ा और निराशी बना देता है और सही होने पर अहंकारी। फिर हम अपनी सफलता की कहानियां सुनाते फिरते है किंतु सुनने वाले नहीं मिलते। अत्यधिक कर्म निराशा, लोभ, ईर्ष्या और अहंकार का कारण भी है जिस से मन की शांति नष्ट हो जाती है और व्यक्ति चिंताओं से घिर जाता है। जिस से उस का पतन भी शुरू हो जाता है। इसलिए कर्म प्रधान होना किसी भी परिवार, समाज और देश के आवश्यक है किंतु इस की अतिश्योक्ति हानिकारक है।
आगे हम तम गुण के लक्षण को पढ़ते है।
।। हरि ॐ तत सत।। गीता – 14.12।।
Complied by: CA R K Ganeriwala (+91 9422310075)