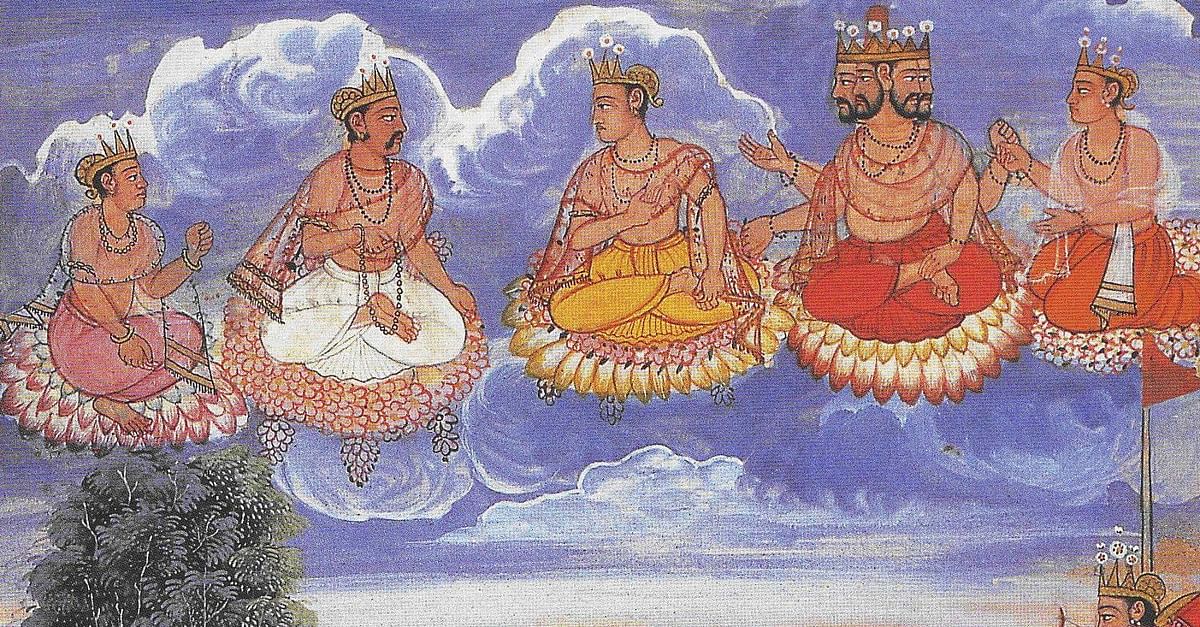।। Shrimadbhagwad Geeta ।। A Practical Approach ।।
।। श्रीमद्भगवत गीता ।। एक व्यवहारिक सोच ।।
।। Chapter 13.29 II
।। अध्याय 13.29 II
॥ श्रीमद्भगवद्गीता ॥ 13.29॥
समं पश्यन्हि सर्वत्र समवस्थितमीश्वरम् ।
न हिनस्त्यात्मनात्मानं ततो याति परां गतिम् ॥
“samaḿ paśyan hi sarvatra,
samavasthitam īśvaram..।
na hinasty ātmanātmānaḿ,
tato yāti parāḿ gatim”..।।
भावार्थ:
जो मनुष्य सभी चर-अचर प्राणीयों में समान भाव से एक ही परमात्मा को समान रूप से स्थित देखता है वह अपने मन के द्वारा अपने आप को कभी नष्ट नहीं करता है, इस प्रकार वह मेरे परम-धाम को प्राप्त करता है। (२९)
Meaning:
For, he who sees Ishvara established equally everywhere, does not kill his self by his own self. That is why he attains the supreme state.
Explanation:
Shri Krishna explains the result of developing an equanimous vision in this shloka. He says that one who sees Ishvara residing equally in everything and everyone, including himself, does not harm or kill his self by his own self. He says that we commit a kind of suicide whenever we do not focus on the imperishable and give too much importance to the perishable. We would very rarely get the urge to commit suicide. So how does this happen?
The mind is pleasure seeking by nature and being a product of the material energy, is spontaneously inclined to material pleasures. If we follow the inclinations of our mind, we become degraded into deeper and deeper material consciousness. The way to prevent this downslide is to keep the mind in check with the help of the intellect. For this, the intellect needs to be empowered with true knowledge.
Whenever our body’s weight increases or decreases, we say “I am fat, I am thin”. Whenever our body falls ill and recovers, we say “I am sick, I am healthy”. Whenever our body is injured and healed, we say “I am injured, I am healed”. We have taken on changes that happen to a mass of flesh and bones as our own changes. By repeatedly taking on this identification to the body due to ignorance of our true nature, we get stuck in an endless cycle of desire, action, birth and death. This entry into the cycle of birth and death is referred to as “killing of one’s self by one’s own self”.
Shri Krishna says that we need to develop samadarshanam, the vision of seeing the imperishable Ishvara in the perishable world. We need to stop identifying with the body, which is not ours to begin with. It belongs to the five elements that make up the universe and will go back to them when it has run its course. We should identify with Ishvara who exists equally in us and in other beings. When we recognize that the Ishvara in us is the same Ishvara in everyone, we will attain the most supreme, the purest state of Ishvara which is the state of brahman, the eternal essence. The instant we realize our identity with brahman, we attain liberation or moksha.
Those, who learn to see God as the Supreme Soul present in all beings, begin to live by this knowledge. They no longer seek personal gain and enjoyment in their relationships with others. They neither get attached to others for the good done by them, nor hate them for any harm caused by them. Rather, seeing everyone as a part of God, they maintain a healthy attitude of respect and service toward others. They naturally refrain from mistreating, cheating, or insulting others, when they perceive in them the presence of God. Also, the humanly created distinctions of nationality, creed, caste, sex, status, and color, all become irrelevant. Thus, they elevate their mind by seeing God in all living beings, and finally reach the supreme goal.
We have seen how to attach ourselves to Ishvara, how to identify ourselves with Ishvara in these shlokas. We also need to detach ourselves from Prakriti. We shall see how to do this in the next two shlokas.
।। हिंदी समीक्षा ।।
एक ही सच्चिदानंदघन परमात्मा सर्वत्र समभाव से स्थित है, अज्ञान के कारण ही भिन्न भिन्न शरीरों में उस की भिन्नता प्रतीत होती है- वस्तुतः उस मे किसी प्रकार का भेद नही है। इस तत्व का ज्ञान ही सर्वत्र समभाव में स्थित परमेश्वर को सम देखना है।
जो सम भाव से नही देखते उन्हें संसार का प्रत्येक जीव अपने से भिन्न दिखता है और विषम बुद्धि से किसी को हितेषी, किसी को प्रिय और किसी को शत्रु समझते है।
अज्ञानी पुरुष प्रकृति से बंधा होने से अपनी देह को ही अपना स्वरूप समझता है और प्रकृति के सुख के लिए कर्म करता है जिस से उसे कर्मफल का बंधन रहने से पुनः पुनः जन्म और मरण को प्राप्त होता है। वैसे ही ज्ञान तो मुक्ति में है किंतु वह ज्ञान भी अपनी कामनाओं के लिए उपयोग करता है, तो उस का ज्ञान भी अज्ञान है। अतः जो जीव ब्रह्म स्वरूप, नित्य, अजन्मा और अकर्ता है, अपने स्वरूप को नही पहचान कर अज्ञान में विषम दृष्टि से संसार को देखता है। समत्व भाव उसे अमरत्व प्रदान करता है और उसे सदचित्तानंद प्रदान कर सकता है, वहां उसे यह संसार और संसार के कर्मो से लगाव रहने से अज्ञान में दुख भोगना पड़ता है।
मन की प्रकृति सुख की कामना करना है और प्राकृत शक्ति की उपज होने के कारण सहज रूप से इसकी रूचि सांसारिक सुखों में होती है। अगर हम अपने मन की इच्छाओं की तृप्ति करते हैं तब हम गहन से गहन लौकिक चेतनाओं के निम्नतम स्तर तक धस जाते हैं। इस अधोपतन को रोकने के उपाय के रूप में बुद्धि की सहायता से मन पर अंकुश लगाना पड़ता है। इसके लिए बुद्धि को सच्चे ज्ञान से सशक्त करना आवश्यक है।
परमात्मा का कथन है कि जितने भी संसार मे चर-अचर प्राणी है, वह सब क्षेत्र-क्षेत्रज्ञ के संयोग से उत्पन्न है जैसे – देव, मनुष्य, पशु, पक्षी, कीट आदि। इन समस्त देहो में जो जीवात्मा को समानाकार, नित्य, ज्ञाता, अणु, चेतन, सब का नियमन करने वाला, शरीर का स्वामी देख लेता है, वह पुरुष आत्मा यानि मन से अपनी आत्मा का हनन नही करता।
जब आप को कोई सर्वोच्च पद प्राप्त हो और आप अपने पद की गरिमा के अनुसार कार्य नहीं करते हो आप अपना सम्मान एवम पद दोनों ही खोते है। ठीक ऐसा ही जब जीव अपने साक्षी, अकर्ता एवम समभाव को छोड़ कर अहंकार एवम कामना के साथ कर्तृत्व भाव से मेरा-तेरा करना शुरू कर देता है तो उसे यह ही माना जाना चाहिये कि उस ने अपने जीव तत्व को खो दिया है, अपनी गरिमा एवम पद का हनन किया है।
सर्वभेद व परिच्छेद विनिमुक्त ईश्वर, शुद्ध चेतन स्वरूप अपने आत्मा को जब हम प्रकृति के रूप में अर्थात देहादि के रूप में ग्रहण करते है और अपनी पहचान सांसारिक नामो एवम कर्मो से करते है तो यही सब पापो एवम हत्याओं के मूल आत्महत्या है और इसी से जन्म मरणादि सब दुखो व क्लेशों की उत्पत्ति होती है। इसलिये जिस ने आपने आत्मा को नही जाना, वही आत्म हत्यारा है।
उदाहरण के तौर पर यदि जीव अपने आत्म स्वरूप को भूल के प्रकृति प्रदत्त शरीर को अधिक मान्यता देगा तो इंद्रियाओ, मन और बुद्धि से इस शरीर की सुख सुविधा एवम कर्म के बंधन में बंध जाएगा। जिस से उस की मुक्ति संभव नही एवम हर बार वह शरीर के मरण के बाद पुनः जन्म लेकर इस संसार के सुख-दुख भोगेगा। इसी को मन द्वारा अपनी आत्मा का हनन कहेंगे। यदि उसे अपना ज्ञान प्राप्त है तो वह निष्काम हो कर्म योगी तत्वविद भाव से जीवन व्यतीत करेगा और मोक्ष को प्राप्त होगा। मुख्य बात यही है कि संसार मे कर्म करते हुए भी निर्लिप्त एवम निष्काम रहना एवम किसी भी किस्म की कामना से मुक्त रहना। जिस से यह सांसारिक शरीर से मोह ही नही। जिस ने यह जान लिया कि शरीर की मृत्यु- मृत्यु नहीं है क्योंकि वह यह शरीर ही नही है वो अपने आप की हत्या से मुक्त है। किंतु जिस में यह माना कि मेरी मृत्यु मेरा यह शरीर है उस ने अपने नित्य स्वरूप की हत्या कर दी और अब वह जन्म मरण के कुचक्र में फस गया।
वे लोग जो भगवान को सभी जीवों में प्रकट परमात्मा के रूप में देखना सीख लेते हैं और इस सत्य ज्ञान से जीवन निर्वाह करना आरम्भ करते हैं तब वे फिर कभी दूसरों के साथ अपने संबंधों में व्यक्तिगत लाभ और सुख की अपेक्षा नहीं करते। वे न तो दूसरे के अच्छे कार्यों के कारण उनके प्रति आसक्त होते हैं और न ही उनके द्वारा स्वयं को किसी भी प्रकार की क्षति पहुँचाने के कारण उनसे द्वेष करते हैं। अपितु इसके विपरीत वे सभी को भगवान के अंश के रूप में देखते हैं और अन्य लोगों का सम्मान और उनकी सेवा करने का शुद्ध मनोभाव बनाए रखते हैं। जब उन्हें अपने भीतर भगवान की उपस्थिति का बोध हो जाता है तब वे स्वाभाविक रूप से दुर्व्यवहार, धोखा-धड़ी, दूसरों का निरादर और दूसरों को अपमानित करने जैसे विकारों से दूर रहते हैं। उनके लिए मानव निर्मित राष्ट्रीयता, योनि, जाति, लिंगभेद, पद प्रतिष्ठा, रंग भेद, अमीर-गरीब आदि सबका अन्तर अनावश्यक हो जाता है। इस प्रकार से वे सभी जीवों में भगवान की उपस्थिति का बोध करते हुए अपने मन को उन्नत करते हैं और अंततः परम लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं।
सच्चिदानंदघन ब्रह्म में अभिन्न भाव से रहना वाला जीव इस प्रकार अपने अस्तित्व का विनाश या हत्या नही करता, वरन ज्ञान से समभाव हो जीवन व्यतीत करता है और मोक्ष को प्राप्त करता है।
श्री वसिष्ठजी आगे कहते हैं-
‘ जैसे तरंगशून्य जल के भीतर तरंगें स्थित हैं, उसी प्रकार परब्रह्म परमात्मा में सृष्टि- शब्दार्थ से शून्य सृष्टियाँ स्थित हैं। जैसे वायु अपने में ही स्पन्दन की कल्पना करती है , उसी प्रकार परमार्थ- चिन्मय ब्रह्म अपनी ज्ञानवृत्ति से अपने ही गूढ़ स्वरूप को प्रपंच के रूप में अभिव्यक्त कर देता है।।’
वाणी को मन में, मन को बुद्धि में, बुद्धि को उस के साक्षी- अन्तरात्मा में हम लय करें और अन्तरात्माको निर्विकल्प ब्रह्म में विलीन करके परमशान्तिका अनुभव करें।।
देह, प्राण, इन्द्रिय, मन, बुद्धि आदि उपाधियों की जिस-जिस वृत्तिके साथ योगीका संयोग होता है, वह उसी-उसी भावके साथ एकाकार हो जाता है।।
जब मननशील साधकका चित्त सब उपाधियों से निवृत्त हो जाता है तो उसको पूर्ण उपरतिका आनन्द प्रतीत होने लगता है, जिससे उसके चित्त में सच्चिदानंदरस हिलोरें मारने लगता है।।
परब्रह्म परमात्मा के स्वरूप का वर्णन करते हुए श्री वसिष्ठ जी कहते हैं ‘ रघुनन्दन! तुम जिस रूप में स्थित होकर क्रिया, रूप, रंग, रस, गन्ध, स्पर्श और चेतन को जानते हो, वह प्रदाता चेतन भी वही है और जिसे जानते हो, वे भी परमात्मदेव ही हैं । द्रष्टा, दर्शन और दृश्य के मध्य में साक्षीरूप से जिसका दर्शन होता है, उसे तुम एकाग्रचित्त होकर अपना आत्मा ही समझो। वह परब्रह्म परमात्मा अजन्मा, अजर, अनादि, सनातन, नित्य, कल्याणमय, निर्मल, अमोघ, सबका परम वन्दनीय, समस्त कलनाओं से शून्य, कारणों का भी कारण, अनुभवरूप, अवेद्य, ज्ञानस्वरूप, विश्वरूप तथा अन्तर्यामी है ।।’
जगत की ब्रह्म से अभिन्नता, परमार्थ-तत्व का लक्षण, महाप्रलय में जगत के अधिष्ठान का विचार तथा जगत की बहुरूपता के विषय में श्री वसिष्ठजी कहते हैं –
‘ रघुनन्दन ! यह जगत न तो कभी परब्रह्म से उत्पन्न होता है और न उसमें लीन ही होता है । यह सद्ब्रह्म ही सदा अपने आप में प्रतिष्ठित है । निश्चल होने के कारण, शान्त आकारवाले महासागर के जल में जिस प्रकार बड़ी- बड़ी लहरें विद्यमान होती हैं , उसी प्रकार निराकार ब्रह्म में उसी के समान यह विश्व स्थित है । पूर्ण से पूर्ण का प्रसार होता है; जो पूर्ण में स्थित है, वह पूर्ण ही है। अतः विश्व कभी उत्पन्न हुआ ही नहीं और जो उत्पन्न हुआ है, वह तत्स्वरुप (ब्रह्मस्वरूप) ही है।।’
जो इस तत्व को जान लेता है, वह ही ब्रह्म को जान कर उस को प्राप्त होता है। ब्रह्म को गहराई में जानने के लिए, नासदीय सुक्त को भी समझना चाहिए, क्योंकि जिस को प्राप्त होना है, जो इस समस्त रचना का आधार है, वह स्वयं में कैसा है।
नासदीय सूक्त – वेद में हमारे ऋषि- मुनियों की ज्ञान दृष्टि का द्योतक उस परमब्रह्म के विचार का है। समस्त वेदान्त शास्त्र का रहस्य यही है कि नेत्रों को या सामान्यतः सब इंद्रियाओ को गोचर होने वाले विकारी और विनाशी नामरूपात्मक अनेक दृश्यो के फंदे मे न फस कर, ज्ञान दृष्टि से यह समझना आवश्यक है कि इस दृश्य के परे कोई न कोई एक और अमृत तत्व है। ऋषि का अमृत मंथन हमे यही ज्ञान देता है कि जब तक हम अपने अन्तःकरण को पूर्ण रूप से जागृत नही करते, तब तक समभाव या क्षेत्र-क्षेत्रज्ञ के ज्ञान के प्रति हमारी उपलब्धि एक रटू तोते की भांति होगी जो प्रवचन के नाम पर श्रेष्ठ एवम उच्च कोटि की बाते तो करते है किंतु आचरण में सामान्य व्यक्ति की भांति मोह एवम अहंकार में रहते है। देश मे अनेक साधु संत भी लगभग इसी प्रकार के है किंतु जिन्होंने ज्ञान के लिये संसार को त्याग कर परमात्मा की शरण ली है, वो निश्चय ही प्रगति कर के ज्ञान को प्राप्त कर लेंगे। ज्ञान पूर्णतः अन्तःकरण की वस्तु है जिसे पुस्तको, लिखने, पढ़ने, अभ्यास एवम ज्ञानी पुरुष के शरणागति से सीखा तो जा सकता है किंतु अन्तःकरण में उतारने के कड़े अभ्यास की जरूरत है।
नासदीय सूक्त ऋषि के बेबाक होने व स्पष्टता से जो नही समझ मे आता एवम जो समझ रहा है, उस का भी उत्कृष्ट उदाहरण है, जब तक अंतर्मन की गहराई तक आत्मतत्व को नही समझ सकते, समभाव का भी उत्पन्न होना उतना ही दुर्लभ है।
स्वामी रामकृष्ण परमहंस के शरीर पर उभरते कोड़ों के निशान, जो किसी किसान द्वारा बैल पर डाले गए, इस बात का द्योतक है।
संत ज्ञानेश्वर द्वारा भैंसे से वेद मंन्त्र का उच्चारण, समभाव दृष्टि से संभव था।
समभाव करुणा, दया, निश्छल प्रेंम से उपजा बीज है जो राधा- कृष्ण या गोकुल में गोपियों और कृष्ण का था।
वेदान्त हमें जगत् से पलायन नहीं सिखाता, बल्कि वह इस दृश्यमान जगत् का पुनर्मूल्यांकन करने का उपदेश देता है। सामान्यत जगत् की ओर देखने की हमारी दृष्टि हमारे प्रिय विचारों एवं भावनाओं से रंजित होती है। स्पष्ट है कि उस स्थिति में हम जगत् को यथार्थ रूप में नहीं देखते। इस अज्ञान की दृष्टि का त्यागकर ज्ञान की दृष्टि से विश्व को देखने का अर्थ वर्तमान काल के सुस्त और उदास, दुखी कुरूप जगत् में ही पूर्णता और आनन्द, दिव्यता और पवित्रता का दर्शन करना है। दुर्व्यवस्थित प्रमाणों के द्वारा परमार्थ सत्य का विपरीत दर्शन ही यह जगत् है, जो द्रष्टा जीव को ही पीड़ित करता रहता है।उपाधियों के साथ तादात्म्य करके जीवभाव को प्राप्त आत्मा जब देखता है, तब उसे नानाविध सृष्टि दिखाई देती है। भ्रान्तिजनित यह जगत् कभी उसे खिसियाते और नृत्य करते हुए तो कभी चीखते और हुंकारते हुए प्रतीत होता है। इन सब दुखपूर्ण परिवर्तनों के मध्य ही पारमार्थिक सत्य स्वरूप को पहचानने से ही सभी विक्षेपों, अर्थहीन लक्ष्यों और परिश्रमों की समाप्ति हो सकती है, क्योंकि वह परमेश्वर ही सर्वत्र समान रूप से स्थित देखता है। ज्ञान के अपने इस अनुभव के कारण फिर ज्ञानी पुरुष को कोई दुख अथवा भय नहीं होता।
व्यवहार में समभाव होने से कर्तव्य धर्म के पालन में कोई अड़चन नहीं होती, प्रकृति ही समस्त क्रिया करती है किंतु वह किसी न किसी निमित्त को तलाशती है। कर्म के फल का नही, किंतु इंद्रिय, मन और बुद्धि हमे कर्म का अधिकार देते हैं, अतः प्रकृति के लिए किस प्रकार का निमित्त होना है, वह आप के अधिकार में हैं, जो कर्मठ, आलस्य छोड़ कर सात्विक विचारो से निमित्त बनते है, वे प्रकृति के उच्च कार्य के अधिकारी भी होते है और सांसारिक सुखों का आनंद निर्लिप्त भाव से प्राप्त करते है। बिना प्रयोजन के कोई काम सिद्ध नहीं होता, किंतु प्रयोजन लोकसंग्रह का बिना कर्तृत्व एवम भोक्त्व भाव का तो हो ही सकता है।
आगे जब जीव और प्रकृति पृथक पृथक है तो जीव को प्रकृति से मुक्त कैसे होना है, पढ़ते है।
।। हरि ॐ तत सत।। 13.29।।
Complied by: CA R K Ganeriwala (+91 9422310075)