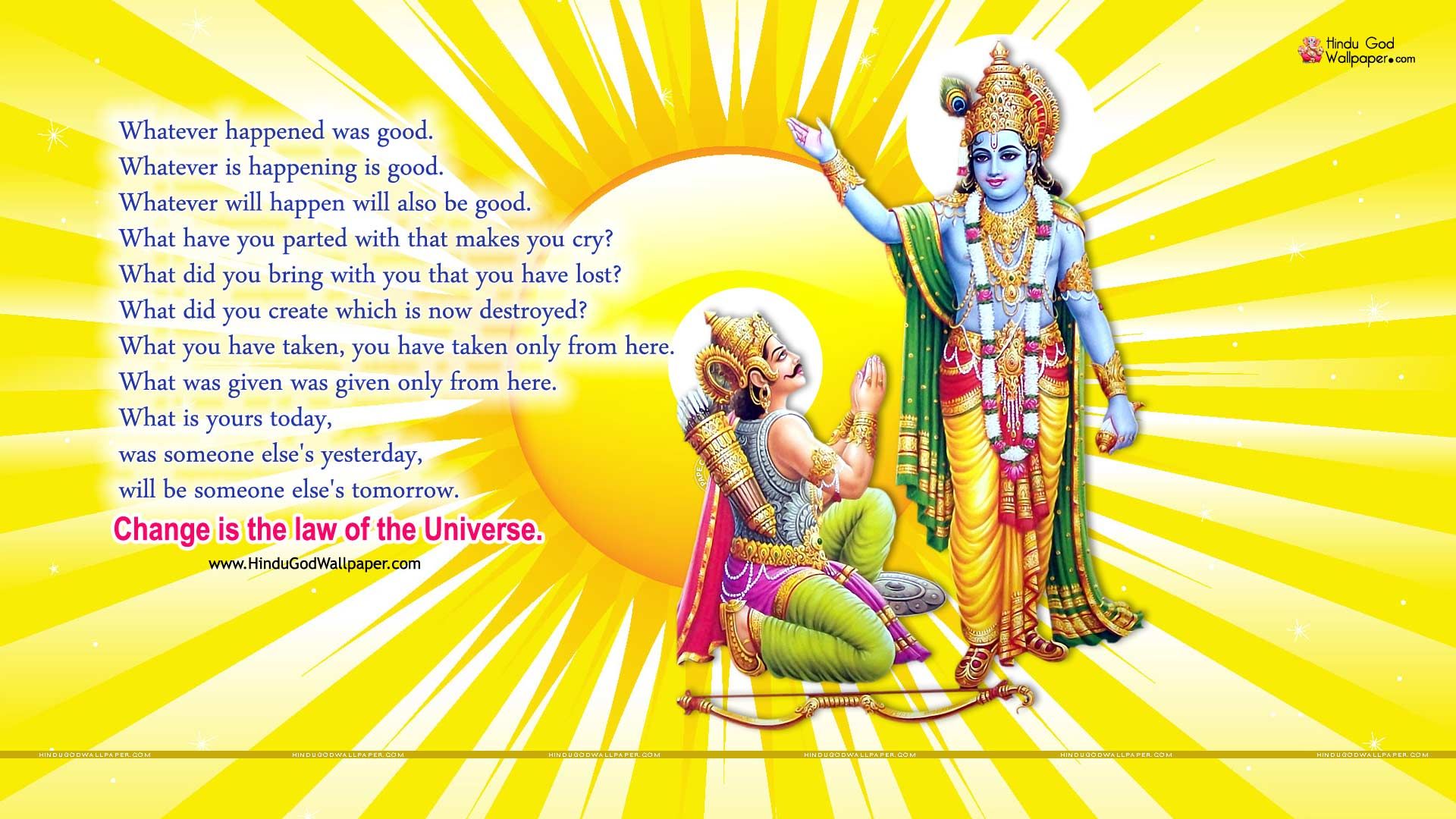।। Shrimadbhagwad Geeta ।। A Practical Approach ।।
।। श्रीमद्भगवत गीता ।। एक व्यवहारिक सोच ।।
।। Chapter 13.22 II
।। अध्याय 13.22 II
॥ श्रीमद्भगवद्गीता ॥ 13.22॥
पुरुषः प्रकृतिस्थो हि भुङ्क्ते प्रकृतिजान्गुणान् ।
कारणं गुणसंगोऽस्य सदसद्योनिजन्मसु ॥
puruṣaḥ prakṛti-stho hi,
bhuńkte prakṛti-jān guṇān..।
kāraṇaḿ guṇa-sańgo ‘sya,
sad-asad-yoni-janmasu..।।
भावार्थ:
भौतिक प्रकृति में स्थित होने के कारण ही प्राणी, प्रकृति के तीनों गुणों से उत्पन्न पदार्थों को भोगता है और प्रकृति के गुणों की संगति के कारण ही जीव उत्तम और अधम योनियाँ में जन्म को प्राप्त होता रहता है। (२२)
Meaning:
Purusha, when seated in Prakriti, experiences the qualities born of Prakriti. Attachment to these qualities is the cause of his birth in good and evil wombs.
Explanation:
Puruṣah (conscious) and Prakriti (Nature) both are beginningless. But nature has dissimilarity with consciousness in four manners: Puruṣah is conscious principle, Prakr̥ti is inert; Puruṣah is changeless principle, Prakr̥ti is changing principle; Puruṣah is without any attribute, attributeless whereas the Prakr̥ti has all the attributes and finally Puruṣah is satyam, Prakr̥ti is mithya. So Nirguṇa, Nirvikāra, Satya, cētana tatvam Puruṣa. Saguṇa, Savikāra, Mithya, Acētana tatvam Prakr̥ti.
Therefore, originally, before the creation evolves or the world evolves, the puruṣah was neither the subject, nor the prakr̥ti was object; there was no subject- object transaction at all, before the creation evolved. Then when did the puruṣah get the subject status? When the universe evolved, naturally the body was also created, the mind also is created and after the creation of the body and mind, the all- pervading puruṣa got enclosed within the body- mind- enclosure. Previously the enclosures were not there, therefore this consciousness was an all-pervading unenclosed consciousness; but after the creation of body- mind, we have got enclosed consciousness. Previously it was unenclosed consciousness. Now it is body mind enclosed consciousness; and that becomes the subject- principle. And then the whole world become object. Therefore, consciousness becomes a subject
The Vedas state that there are 8.4 million species of life in the material world. All these bodily forms are transformations of the material energy. Hence, material nature is responsible for all the cause and effect in the world. The soul gets a bodily form (field of activity) according to its past karmas, and it identifies itself with the body, mind, and intellect. Thus, it seeks the pleasure of the bodily senses. When the senses come in contact with the sense objects, the mind experiences a pleasurable sensation. Since the soul identifies with the mind, it vicariously enjoys that pleasurable sensation. In this way, the soul perceives the sensations of both pleasure and pain, through the medium of the senses, mind, and intellect.
Imagine that two young brothers and their grandmother are watching a boxing match on TV. One brother is a huge fan of boxer A, and the other brother of boxer B. The two brothers get so involved in the match that they feel they themselves are in the boxing ring. The brothers start throwing punches in the air, mimicking the actions of the boxers. Also, when boxer A punches boxer B, the first brother feels exhilaration whereas the second brother feels pain. All this time, their grandmother is watching the match without any of these reactions.
This involvement with the boxers doesn’t end with the match. Boxer A always likes to wear a headband, so the first brother starts to wear headbands in the house. Boxer B always snaps his fingers at the end of every sentence, so the second brother begins to do that as well, much to the annoyance of his parents. Both the brothers have become so infatuated with their boxers that they take on their likes and dislikes. We may think that such behaviour only happens with children and teenagers, but something similar has happened to all of us, causing us to get trapped in samsaara.
We are stuck twice in samsaaraa. First, Shri Krishna says that the eternal essence has mistakenly identified itself with one body due to avidyaa or ignorance, just like the brother identified himself with boxer A. Instead of watching the IMAX movie of the universe like the grandmother, we get stuck to one character in that movie. When the eternal essence as though gets deluded with ignorance, it becomes the Purusha, and becomes “seated in Prakriti”. It forgets it real nature as infinite, indivisible and blissful. It assumes the properties of our body and thinks itself to be finite, divisible and sorrowful.
Second, having identified with a finite body, having taken the “upaadhi” or conditioning of a body, we get attached to the play of Prakriti, the play of the three gunaas or qualities. We get so attached to the forms of Prakriti that we generate selfish desires in order to repeatedly contact these forms, which are nothing but objects and people. Seeking a shinier car is a mistaken attempt to find joy in the car instead of understanding our true nature as joy itself. We become the brother who starts wearing a headband to feel happy, just because boxer A does so, when the brother was happy even before he knows what boxing was.
So then, how do we get out of this twostep problem of samsaara which causes us to “take birth in good and evil wombs”? We solve step one – attachment to gunaas – through vairaagya or dispassion, we learn to slowly wean ourselves off the influence of the three gunaas. We then solve step two – ignorance of our true nature – through jnyaana or knowledge, when we learn of our real nature as the eternal essence and internalize it through meditation.
An illustration of Purusha getting entangled in Prakriti is taken up next.
।। हिंदी समीक्षा ।।
प्रकृति और पुरुष यद्यपि दोनो ही अनादि है और दोनो में कारण और कार्य का कोई संबंध भी नही होने के बावजूद कुछ असमानताएं भी है। इसलिए मूलतः, सृष्टि के विकास के पहले या जगत के विकास के पहले, पुरुष न तो विषय था, न प्रकृति वस्तु थी; सृष्टि के विकास के पहले, विषय- वस्तु का कोई लेन-देन ही नहीं था। फिर पुरुष को विषय का दर्जा मिला, जब ब्रह्माण्ड का विकास हुआ, तो स्वाभाविक रूप से शरीर भी बना, मन भी बना और शरीर और मन की रचना के बाद, सर्वव्यापी पुरुष शरीर- मन- परिक्षेत्र में बंद हो गया। पहले कोई सीमा या परिक्षेत्र नहीं थे; इसलिए यह चेतना सर्वव्यापी असंलग्न चेतना थी; लेकिन शरीर- मन की रचना के बाद, हम जीव के स्वरूप में परिक्षेत्र में बंद चेतना को पाते है। पहले यह असंलग्न चेतना थी। अब यह शरीर- मन- संलग्न चेतना है; और यह पुरुष विषय- तत्त्व हो गया और फिर सारा जगत् वस्तु बन गया। इसलिए चेतना विषय बन गई।
प्रकृति और पुरुष अनादि होते हुए भी चार असामान्य विशेषताएं भी रखते हैं। पुरुष चेतन तत्त्व है, प्रकृति जड़ है; पुरुष अपरिवर्तनीय सिद्धांत है, प्रकृति परिवर्तनशील सिद्धांत है; पुरुष किसी भी गुण से रहित है, निर्गुण है जबकि प्रकृति में सभी गुण हैं और अंततः पुरुष सत्य है, प्रकृति मिथ्या है। अतः निर्गुण, निर्विकार, सत्य, चेतना तत्वम् पुरुष। सगुण, सविकार, मिथ्या, अचेतन तत्वं प्रकृति।
इसलिए प्राकृत शक्ति ब्रह्मा के निर्देशानुसार असंख्य तत्त्वों और जीवन रूपों का निर्माण करती है। वेद में वर्णन है कि भौतिक जगत में 84 लाख योनियाँ पायी जाती हैं। इन सबके शरीर रूपों का रूपान्तरण प्राकृतिक ऊर्जा द्वारा होता है इसलिए प्राकृत शक्ति संसार के सभी कारणों और परिणामों के लिए उत्तरदायी है। आत्मा अपने पूर्व कर्मों के अनुसार शरीर अर्थात कर्म क्षेत्र प्राप्त करती है और यह अपनी पहचान शरीर, मन और बुद्धि के रूप में करती है इसलिए यह शरीर के सुखों की कामना करती है जब इन्द्रियाँ अपने विषयों के संपर्क में आती है तब मन सुखद अनुभूति का बोध करता है क्योंकि आत्मा मन के साथ पहचानी जाती है इसलिए वह परोक्ष रूप से इन सुखद अनुभूति का आनंद लेती है। इस प्रकार से आत्मा को मन, इन्द्रियों और बुद्धि द्वारा सुख और दुख दोनों की अनुभूति का बोध होता है।
प्रकृति जनित सत्व, रज और तम ये तीनो गुण तथा गंध रूप जितने भी सांसारिक पदार्थ है-इन्हें प्रकृति जनित गुण माना गया है। पुरुष प्रकृतिस्थ हो कर प्रकृति से बने हुए स्थूल, सूक्ष्म और कारण इन से सम्बंध बना लेता है। इसलिये जब तक यह सम्बन्ध है तब तक ही पुरुष प्रकृति का भोक्ता है एवम सम्बन्ध छूट जाने से वह स्वरूप नित्य असंग ही है।
पुरुष सचेतन और ज्ञाता है, तथापि केवल निर्गुण होने के कारण स्वयं कर्म करने के कोई साधन उस के पास नही है। और प्रकृति काम करने वाली है तथापि जड़ एवम अचेतन होने के कारण वह नही जानती, की क्या करना चाहिये। इस प्रकार यह लंगड़े एवम अंधे की वह जोड़ी है, जैसे ही अंधे के कंधे पर लंगड़ा बैठे और वे दोनों एक दूसरे की सहायता से मार्ग चलने लगे, वैसे ही अचेतन प्रकृति और चेतन पुरुष का संयोग हो जाने पर सृष्टि का कार्य प्रारंभ हो जाता है।
जिस प्रकार नाटक की रंगभूमि में प्रेक्षकों के मनोरंजन के नटी विभिन्न स्वांग रज कर नाचती है, उसी प्रकार पुरुष को लुभाने के लिये प्रकृति भी अपने सत्व- रज- तम गुणों की न्यूनाधिक से अनेक रूप धारण कर के उस के सामने लगातार नाचती रहती है। प्रकृति के इस नाच को देख कर, मोह से भूल जाने के कारण, या वृथाभिमान के कारण, जब तक पुरुष इस प्रकृति के कर्तृत्व को स्वयं अपना कर्तृत्व मानता रहता है, और जब तक वह सुख-दुख के काल मे स्वयं अपने को फसा कर रखता है उसे मोक्ष या मुक्ति प्राप्त नही हो सकती।
किन्तु जिस समय पुरुष को यह ज्ञान हो जाये, की त्रिगुणात्मक प्रकृति एवम वह स्वयं भिन्न भिन्न है। वह मुक्त ही है; क्योंकि यथार्थ में पुरुष न तो कर्ता है और न ही बंधा ही है। वह तो स्वतंत्र और निसर्गत: केवल या अकर्ता है। जो कुछ भी होता है वह सब प्रकृति ही का खेल है। यहां तक कि मन और बुद्धि भी प्रकृति के ही विकार है, इसलिये बुद्धि को जो ज्ञान होता है, वह ही प्रकृति के कार्य का फल है। सत्व- रज- तम ये प्रकृति के गुण है और बुद्धि को ज्ञान सत्व गुण प्राप्त होने से ही होता है।
पुरुष निर्गुण है और प्रकृति उस के दर्पण, यदि दर्पण स्वच्छ है तो ही पुरुष दर्पण में अपनी छवि निर्गुण देख सकता है।
अब हम कर्मात्मक मूल प्रकृति से उन नियमो को जानने का प्रयत्न करते है जिन के अनुसार मनुष्य को कर्मो के फल भोगने पड़ते है। इसी को कर्म विपाक कहते है।
इस का पहला नियम यही है कर्म का आरंभ होने के बाद उस का व्यापार अखंड चलता है। यद्यपि सृष्टि का संहार होने पर भी यह कर्म बीज रूप में बना रहता है एवम सृष्टि का आरंभ होने पर पुनः कर्म बीज से अंकुरित हो जाता है। महाभारत का कथन है कि पूर्व की सृष्टि में प्राणी ने जो जो कर्म किये होंगे, ठीक वे ही कर्म उसे चाहे इच्छा हो या न हो, फिर यथा पूर्व प्राप्त होते है। कर्म की गति कठिन है ही, कर्म का बंधन भी उस से बड़ा कठिन है। कर्म से कोई मुक्त नही है। वायु, सूर्य, चंद्र, ब्रह्मा- विष्णु- महेश सगुण देवता सभी कर्मो से बंधे है।
मायात्मक कर्म में एक बार मनुष्य के फस जाने से, फिर चाहे वह किसी भी रीति से हो, नाम रूपात्मक देह का नाश होने पर भी कर्म के परिणाम के कारण उसे सृष्टि में भिन्न भिन्न रुपों अर्थात विभिन्न जीव रूप का मिलना कभी नही छूटता। कर्म शक्ति का कभी भी नाश नही होता, इस लिये जो शक्ति एक नाम रूप में वो विभिन्न नाम रूप में क्रमशः नाम रूप के अंत मे मिलती रहती है। यह नाम रूप निर्जीव या सजीव कोई भी हो सकता है। आध्यत्म दृष्टि से इस नाम रूपात्मक परम्परा को ही जन्म- मरण का चक्र या संसार कहते है और इन नाम रूप को समिष्ट रूप से ब्रह्म एवम व्यष्टि रूप से जीवात्मा कहा करते है।
गुणों का सङ्ग ही अर्थात् गुणों में जो आसक्ति है वही इस भोक्ता पुरुष के अच्छी बुरी योनियों में जन्म लेने का कारण है। अच्छी और बुरी योनियों का नाम सदसत् योनि है, उन में जन्मों का होना सदसद्योनिजन्म है, इन भोग्यरूप सदसद्योनि जन्मों का कारण गुणों का सङ्ग ही है। अथवा संसार पद का अध्याहार कर के यह अर्थ कर लेना चाहिये कि अच्छी और बुरी योनियों में जन्म लेकर गुणों का सङ्ग करना ही इस संसार का कारण है। देवादि योनियाँ सत् योनि हैं और पशु आदि योनियाँ असत् योनि हैं। प्रकरण की सामर्थ्य से मनुष्य योनियों को भी सत् असत् योनियाँ मानने में ( किसी प्रकारका ) विरोध नहीं समझना चाहिये।
अतः यह कहना कि आत्मा न तो जन्म धारण करता है और न ही मरता है अर्थात वह नित्य एवम स्थायी है, किन्तु कर्म बंधन के उसे एक नाम रूप से दूसरे नाम रूप में जा कर अपने कर्मो के फल को भोगना ही पड़ता है। यह कर्म फल जीव के नाम रूप तक ही नही, वरन उस से उत्पन्न अन्य नाम रूपों अर्थात पुत्र, पुत्रियों, नाती, नातियों एवम रिस्तेदारो तक को भी भोगना पड़ता है।
जैसे कई रोग वंश परंपरा से चलते है वैसे ही कई पूर्व जन्म के दोष के कारण हम कह उठते कि यह पितर दोष से कष्ट है। यही कर्म वाद की सच्चाई है।
सारी सृष्टि परमेश्वर की इच्छा से ही चल रही है, तो कहना होगा कि कर्म फल भी देने वाला और कोई नही परमात्मा ही है। इसलिये भगवान ने कहा भी है मै जिस का निश्चय कर दिया करता हूँ वही इच्छित फल मनुष्य को मिलता है। कर्म का फल कर्मो की योग्यता के अनुसार ही परमात्मा तय करता है।
अत संसार की आत्यन्तिक निवृत्ति के लिए जो ज्ञानमार्ग है, उस के दो अंग हैं विवेक और वैराग्य। साधक को चाहिए कि वह विवेक के द्वारा आत्मज्ञान प्राप्त करे और वैराग्य के द्वारा मिथ्या आसक्ति का त्याग करे।
और मुख्य बात यह भी है कि इस की तुलना स्वप्नावस्था से की गयी है।
एहि बिधि जग हरि आश्रित रही । यद्यपि असत्य देत दुःख अहि।। (रामचरितमानस)
जौ सपनें सिर काटइ कोई।बिनु जागें न दूरी दुख होई ।।(रामचरितमानस)
संसार भगवान द्वारा स्थिर है। यह भले ही जो असत्य है उसका भ्रम उत्पन्न करता है और आत्मा को दुख देता है। यह उसी प्रकार से है जैसे कि किसी का स्वप्न में सिर कट गया हो और इससे उसे तब तक कष्ट होता रहता है जब तक कि स्वप्न देखने वाला वह व्यक्ति नींद से जाग नहीं जाता और स्वप्न समाप्त नहीं हो जाता। इस स्वप्नावस्था में शरीर के साथ अपनी पहचान करने वाली आत्मा को अपने पूर्व और वर्तमान के कर्मों के अनुसार सुख और दुख की अनुभूति होती है। परिणामस्वरूप इसे दोनों प्रकार के अनुभवों के लिए उत्तरदायी माना जाता है।
अगले श्लोक में परमात्मा का ही साक्षात् निर्देश करते हुए भगवान् श्रीकृष्ण क्या कहते हैं, हम पढ़ेंगे।
।। हरि ॐ तत सत ।।11.22।।
Complied by: CA R K Ganeriwala (+91 9422310075)