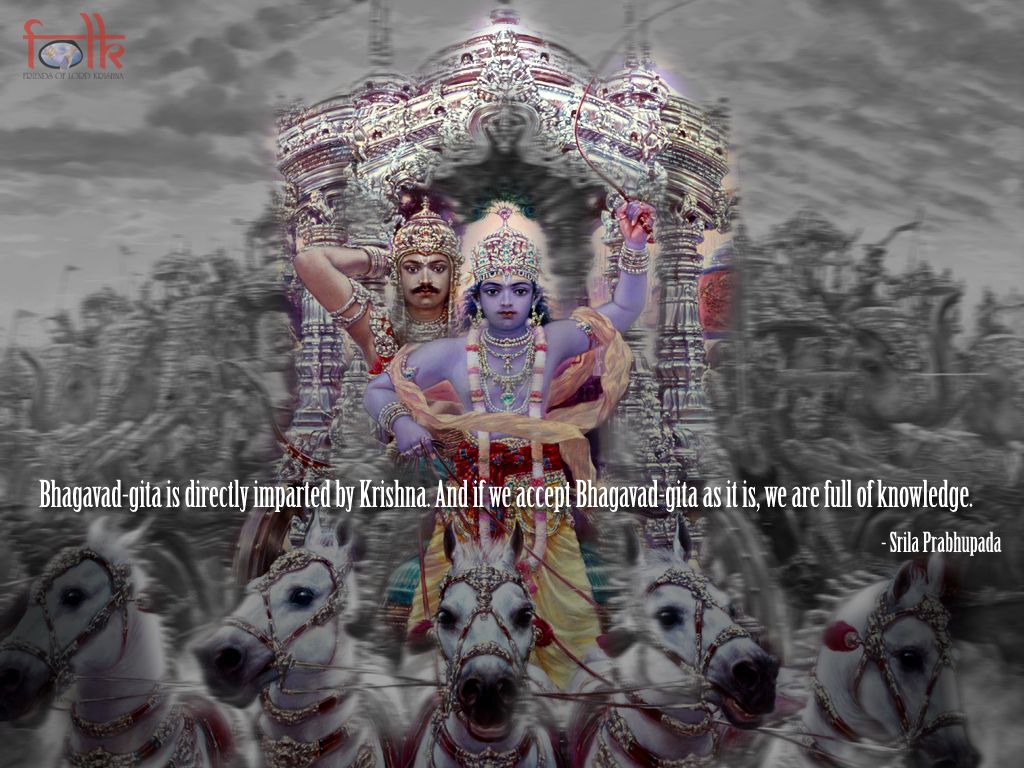।। Shrimadbhagwad Geeta ।। A Practical Approach ।।
।। श्रीमद्भगवत गीता ।। एक व्यवहारिक सोच ।।
।। Chapter 09.28 II
।। अध्याय 09.28 II
॥ श्रीमद्भगवद्गीता ॥ 9.28॥
शुभाशुभफलैरेवं मोक्ष्य से कर्मबंधनैः ।
सन्न्यासयोगयुक्तात्मा विमुक्तो मामुपैष्यसि ॥
“śubhāśubha-phalair evaḿ,
mokṣyase karma- bandhanaiḥ..।
sannyāsa- yoga- yuktātmā,
vimukto mām upaiṣyasi”..।।
भावार्थ:
इस प्रकार तू समस्त अच्छे और बुरे कर्मों के फ़लों के बन्धन से मुक्त हो जाएगा और मन से सभी सांसारिक कर्मो को त्याग कर (सन्यास-योग के द्वारा) मन को परमात्मा में स्थिर करके विशेष रूप से मुक्त होकर मुझे ही प्राप्त होगा। (२८)
Meaning:
In this manner, you will be free from the bonds of action and their auspicious and inauspicious results. Having engaged in this yoga of renunciation, you will be liberated and attain me.
Explanation:
What happens when we incorporate devoted worship into our life? Shri Krishna says that we shall be free of the results of action. Our actions give us results in the form of joy, sorrow, profit, loss, win, loss. Freedom from results leads to liberation and attainment of Ishvara. This is the ultimate result of living a worshipful life.
When we walk on the earth, we unknowingly kill millions of tiny living entities. In our occupational duties, no matter how careful we are in the fulfilment of our duties, we still end up harming the environment and hurting others. Even if we eat a cup of yogurt, we still incur the sin of destroying the living entities that reside in it. Some religious sects try to reduce this involuntary killing by tying a cloth over their mouth. Even this does not fully eliminate the destruction of living entities in our breath.
When we perform our actions with the intention of fulfilling our self-interest, we are culpable for the sins we commit, knowingly or unknowingly. In accordance with the law of karma, we have to reap their karmic reactions. Good works can also be binding because they oblige the soul to go to the celestial abodes to enjoy their results.
This shloka takes us back to the topic of renunciation. In an earlier portion of the Gita, Shri Krishna had redefined “sannyaasa” or renunciation as giving up of the attitude of doership, not the giving up of action and retiring to a hermitage. By submitting our actions and their results in Ishvara hands, we automatically attain renunciation because we have come to know that it is Ishvara who is doing and enjoying everything.
As an illustration, let’s consider our boss at work. If we do not have confidence in our boss’s authority and his ability to lead us, our job becomes complicated, heavy and burdensome. Before we begin a task, we are worried whether we are doing the right things, and also fear the consequences of making a mistake. But if we trust our boss’s authority and his ability to give us right direction, we work effortlessly and fearlessly knowing that we are carrying out the boss’s command, and that he will take care of us if something goes wrong.
Similarly, once we realize that it is the infinite Ishvara that is directing everything, our actions automatically become effortless and fearless. It is like working for the most powerful CEO or the most powerful President, it gives us that kind of a confidence and peace of mind. We know that Ishvara is making us do the right things, and that he will take responsibility for the results and the consequences.
Shree Krishna gives a simple solution for destroying all karmic reactions of work. He uses the word sanyās yog, meaning renunciation of selfishness. He says that when we dedicate our actions for the pleasure of the Lord, we are freed from the fetters of both good and bad results.
Those who establish themselves in such consciousness are called yog yuktātmā (united in consciousness with God). Such yogis become jīvan mukt (liberated in consciousness) even in this body. And, upon leaving their mortal frame, they receive a divine body and eternal service in the divine Abode of God.
Now, if Ishvara is running everything, does that mean that he is partial to those who surrender to him and those who do not? This is taken up next.
।। हिंदी समीक्षा ।।
पूर्व श्लोक में वर्णित पांच प्रकार के कर्म जिस में दो लौकिक और तीन श्रोत कर्म है। लौकिक का अर्थ जीवन निर्वाह एवम संसार मे अपने अस्तित्व, रुचि, शिक्षा एवम ज्ञान के अनुसार व्यवसाय, व्यापार, समाज, देश एवम धर्म के अनुसार कर्म एवम जीवन की निरंतरता के लिये भोजन आदि और श्रोत कर्म यज्ञ, दान एवम तप। जब जीव को अपरा प्रकृति से लगाव हो जाता है तो उसे इस मे इंद्रियाओ द्वारा क्षणिक सुख मिलता है और वह अहम से अपने को कर्ता एवम भोक्ता मानता है। जब सब कुछ परमात्मा को समर्पित हो तो उस मे कर्ता या भोक्ता भाव नही होता। यह ठीक वैसा ही है जैसा नॉकरी करनेवाले को मालूम रहता है वो जो कुछ कर रहा है वो अपने मालिक के लिये कर रहा है, इसलिये उस मे कर्ता या भोक्ता भाव न हो कर कर्तव्य भाव ही रहता है।
हमे पहले भी कहा गया था कि कर्म पर तेरा अधिकार है और फल पर नही, न ही हमे कर्म का हेतु बनना है और न ही हमे कर्म का श्रेय लेना है। क्योंकि प्रत्येक दशा में कर्म के प्रति कोई भी कामना और आसक्ति बंधन का कारण होती है किंतु कर्म का फल तो कार्य – कारण के सिद्धांत से उत्पन्न होगा ही। प्रत्येक जीव कर्म विमुक्त भी नही हो सकता। इसलिए कर्म को सेवक भाव से परमात्मा का कार्य ही समझते हुए करना ही एक मात्र निष्काम कर्म का उपाय है।
भगवान श्री कृष्ण ने श्रद्धा एवम विश्वास के साथ पूर्ण समपर्ण की बात कही जिस में उन्होंने स्पष्ट किया कि परमात्मा प्रेम एवम भाव के भूखे है, धन, ऐष्वर्य और दिखावे के नही। फिर उन्होंने मन को उन में स्थिर करते हुए निष्काम कर्म करते हुए अपना प्रत्येक कर्म उन को अर्पण करने को कहा। अब यहां भगवान श्री कृष्ण सर्वस्व त्याग की बात कह रहे है। सर्वस्व त्याग का अर्थ है अपनी कामना, अपने अहम अर्थात भोगकत्व एवम कर्तृत्व भाव का त्याग।
जब आप ने अपने समस्त कर्म भगवान को अर्पित कर दिए और मन को परमात्मा की ओर स्थिर करना शुरू कर दिया तो यहां कर्ता परमात्मा ही होगा एवम भोक्ता भी परमात्मा ही होगा। अहम का कोई स्थान नहीं। जब मै और तू नही बस तू ही तू है तो वहां तो भोक्ता एवम कर्ता भी एक ही है। परमात्मा से संयुक्त होना ही सन्यास है।
जैसे सांख्ययोगी सम्पूर्ण कर्मों को मन से नवद्वारवाले शरीर में रखकर स्वयं सुखपूर्वक अपने स्वरूप में स्थित रहता है, ऐसे ही भक्त कर्मों के साथ अपने माने हुए सम्बन्ध को भगवान् में रख देता है। तात्पर्य यह हुआ कि जैसे कोई सज्जन अपनी धरोहर को कहीं रख देता है, ऐसे ही भक्त अपने सहित अनन्त जन्मों के संचित कर्मों को, उनके फलों को और उनके सम्बन्ध को भगवान् में रख देता है। इसलिये इस को संन्यासयुक्त कर्मयोग कहा गया है।
व्यवहार में यदि कोई संरक्षण प्राप्त हो, तो व्यक्ति की काम करने की क्षमता का विकास होता है। परमात्मा से बढ़ कर कोई संरक्षक नही हो सकता। मैं परमात्मा का हूँ और परमात्मा मेरे है, यही भाव ने मीरा को भक्तिमार्ग में अमर कर दिया। कठिन से कठिन कार्य भी व्यक्ति निर्भय हो कर पाता है।
कार्य- कारण के नियम से कोई भी कर्म का फल नही हो यह नही हो सकता। किन्तु जब श्रद्धा, प्रेम, विश्वास, स्मरण एवम समर्पण भाव से अपने समस्त कर्म, क्रियाए, कामनाएं, आसक्ति एवम अहम परमात्मा को अर्पित कर के यदि जीवात्मा सेवक भाव स्वीकार कर ले, तो परमात्मा का कहना है, इस प्रकार अर्पण करने से तू शुभ अशुभ कर्मफलों से मुक्त हो जायगा। शुभ अशुभ कर्म फलों से मुक्त होने पर तू मेरे को प्राप्त हो जायगा। तात्पर्य यह हुआ कि सम्पूर्ण कर्मफलों से मुक्त होना तो प्रेम प्राप्ति का साधन है और भगवान् की प्राप्ति होना प्रेम की प्राप्ति है।
भक्ति द्वारा ऊपर की ओर उठने की यह स्थिति आप को ज्ञान मार्ग से उठने की स्थिति तक ले जाती है अर्थात ज्ञान मार्ग जिसे हम पूर्व के अध्याय में पढ़ चुके है और अब श्रद्धा एवम विश्वास का यह भक्ति मार्ग आगे चल कर एक ही हो जाता है। जो गति ज्ञानी को प्राप्त होती है वो ही भक्त को प्राप्त होती है। राजा जनक कर्तृत्व अभिमान एवम कर्मफलासक्ति को त्याग कर दोनो कर्मो को सन्यास युक्त हो कर करते थे, इसलिये उन्हें भी जो मोक्ष ज्ञानयुक्त ब्रह्मसन्ध को प्राप्त था, वही ज्ञान सन्यासयुक्त कर्मयोग से प्राप्त हुआ। अर्जुन के प्रश्न में उसे युद्ध छोड़ कर सन्यास की भावना एवम ज्ञान एवम कर्मयोग में क्या श्रेष्ठ है, उत्तर में यही बताया गया कि ज्ञान या भक्ति किसी भी मार्ग में अपने कर्तव्यकर्म का त्याग करना उचित नहीं है।
किस प्रकार अर्पण की भावना से जीवन जीते हुए, मनुष्य परम पुरुषार्थ को प्राप्त कर सकता हैं जो कि निदिध्यासन और यज्ञ की भावना का निश्चित फल हैं। यह सर्वविदित तथ्य हैं कि जो कर्म का कर्ता होता हैं, वही कर्मफल का भोक्ता भी होता है। यदि सुख स्वर्ण की जंजीर है तो दुख लोह की बेड़ी, किन्तु दोनों है तो बेड़ी ही। अत यदि हम कर्तृत्वाभिमान से कर्म करें, तो फलोपभोग के लिए भी हमें बाध्य होना पडेगा। इसलिए वेदान्त का सिद्धांत है कि निरहंकार भाव से कर्म किये जाने पर उनसे शुभ या अशुभ दोनों ही प्रकार की वासनाएं उत्पन्न नहीं होती।भगवान् श्रीकृष्ण यहाँ कहते हैं, तुम शुभ अशुभ रूप कर्म के बन्धन से मुक्त हो जाओगे। कारण यह है कि अहंकार के अभाव में साधक के किये नये कर्मो से वासनाओं में वृद्धि नहीं होती और साथ ही साथ पूर्व संचित वासनाओं का शनैशनै क्षय हो जाता है। संक्षेप में, उस साधक का चित्त अधिकाधिक शुद्ध होता जाता है शास्त्रीय भाषा में इसे चित्तशुद्धि कहते हैं। मन के शुद्ध होने पर उसकी एकाग्रता की शक्ति में वृद्धि हो जाती हैं।विकास की अगली सीढ़ी यह हैं कि इस चित्तशुद्धि के फलस्वरूप साधक की आत्मानात्मविवेक की सार्मथ्य में अभिवृद्धि होती है। फिर वह संन्यास और योग के जीवन का आचरण करता हुआ अपने सांसारिक, व्यवहारिक, व्यवसायिक, सामाजिक एवम दैनिक कर्म करता है।
व्यवहारिक जीवन मे दुख-सुख का मूल कारण राग, कामना, आसक्ति और अहम है। जो प्राप्त है, वही पर्याप्त है, किन्तु आशा के अनुकूल न होने से दुख, क्षोभ, क्रोध, निराशा जन्म लेती है और आशा से अधिक होने से लोभ और अहम जन्म लेता है। किन्तु जब समस्त कार्य परमात्मा को समर्पित कर के पूर्ण निष्ठा, ईमानदारी, लग्न, दक्षता और मेहनत से किया जाए, तो उस के कारण दुख उत्पन्न होता ही नही है। यही आनन्द मय जीवन की कुंजी है।
कुछ लोगो का मत है कि कर्म और भक्ति से मोक्ष नहीं मिल सकता, जब तक ज्ञान उत्पन्न न हो, इसलिए सन्यासी आत्मशुद्धि के पश्चात ज्ञान मार्ग की ओर अग्रसर होता है और यही निष्काम कर्म योगी और समर्पित भक्ति मार्ग में भी आवश्यक है। किंतु परमात्मा को समर्पित जीव का योगक्षेम परमात्मा वहन करता है तो वह ही उसे ज्ञान भी प्रदान करता है। अतः परमात्मा के अत्यंत करीब तक पहुंचने वाला ही अहम ब्रह्मास्मी अर्थात परमात्मा के स्वरूप को प्राप्त करता है। यही फिर कर्म सन्यास ज्ञान योग है।
परमात्मा कभी अपनी रचना या प्राणियों में विभेद नही करता, किन्तु भक्त जब अपने को परमात्मा को अर्पित कर देता है, तो यह विभेद किस प्रकार का उत्पन्न होता है, आगे पढ़ते है।
।। हरि ॐ तत सत।। 9.28।।
Complied by: CA R K Ganeriwala (+91 9422310075)