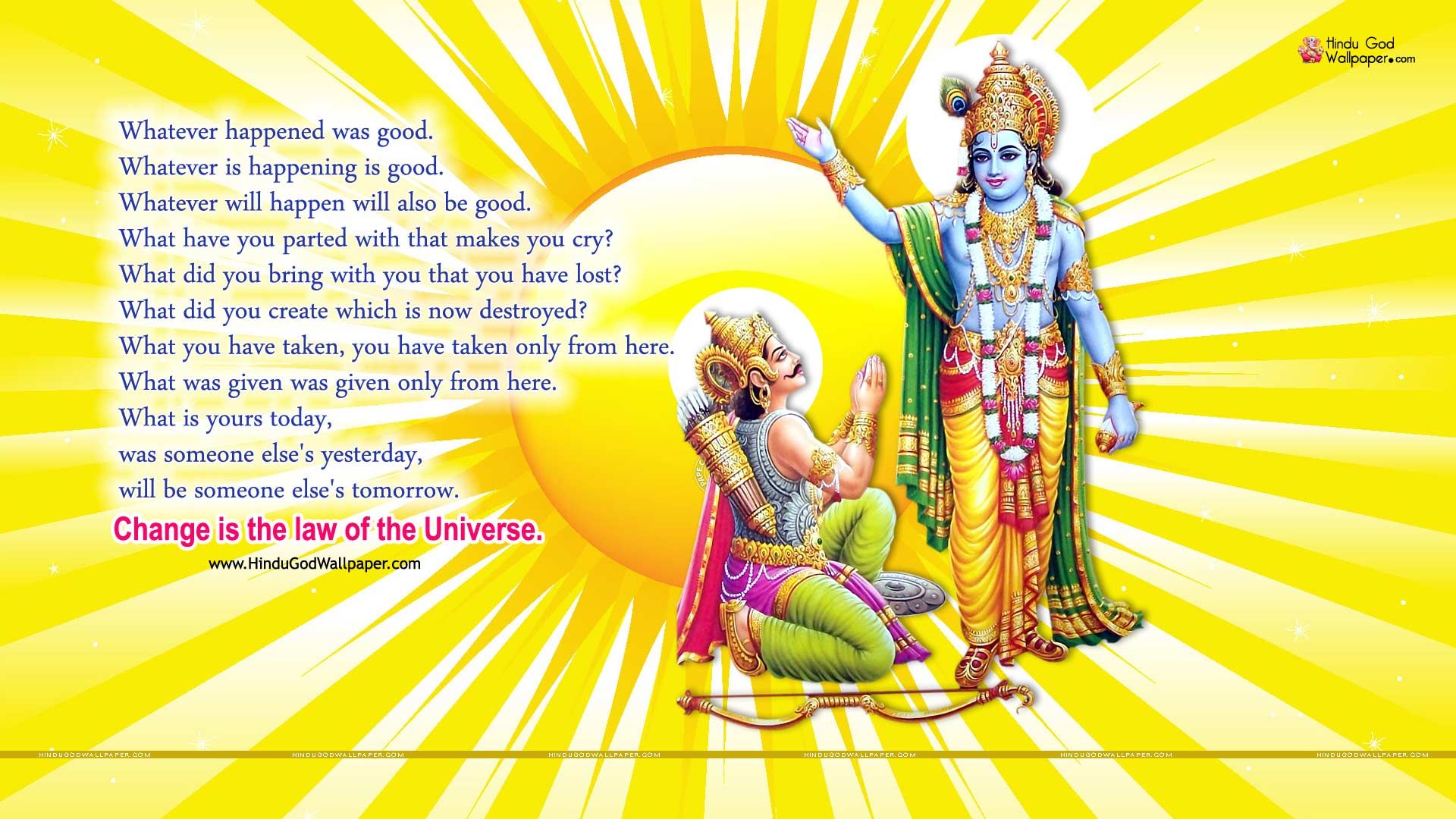।। Shrimadbhagwad Geeta ।। A Practical Approach ।।
।। श्रीमद्भगवत गीता ।। एक व्यवहारिक सोच ।।
।। Chapter 08.08 II
।। अध्याय 08.08 II
॥ श्रीमद्भगवद्गीता ॥ 8.8॥
अभ्यासयोगयुक्तेन चेतसा नान्यगामिना ।
परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थानुचिन्तयन्॥
“abhyāsa- yoga- yuktena,
cetasā nānya-gāminā..।
paramaḿ puruṣaḿ divyaḿ,
yāti pārthānucintayan”..।।
भावार्थ:
हे पृथापुत्र! जो मनुष्य बिना विचलित हुए अपनी चेतना (आत्मा) से योग में स्थित होने का अभ्यास करता है, वह निरन्तर चिन्तन करता हुआ उस दिव्य परमात्मा को ही प्राप्त होता है । (८)
Meaning:
With the mind engaged in constant practice of yoga, not diverting from it, contemplating the supreme divine person, (one) attains (him), O Paartha.
Explanation:
Now that we know that the ultimate goal is upaasana, or constant meditation on Ishvara, how do we actually go about doing it? Shri Krishna described three kinds of meditation in the upcoming shlokas.
To perform upaasana, we need the support of either name or form, since it is extremely difficult to meditate upon something that is intangible. In the following three shlokas, Shri Krishna elaborates upon the technique of meditation on form. Here, he recalls the technique that was presented to us in the sixth chapter – abhyaasa yoga. In this technique, the mind is trained to focus exclusively on one thing. If it diverts to something else, then we bring it back to our object of meditation.
So then, what is the form that we meditate upon? We can meditate upon any form that we have a closeness to. It could be Lord Rama, Krishna, Hanuman or any deity. The deity should come to our mind effortlessly. There is no compulsion to choose one over the other. But as discussed earlier, we should be clear that the deity is an indicator or pointer to Ishvara, the supreme divine person being the words used in this shloka. We should not get stuck at the level of the deity we have chosen.
The devotee can constantly think of the object of worship, the Supreme Lord, in any of His features Narayana, Krishna, Rama, etc. by chanting Hare Krishna. This practice will purify him, and at the end of his life, due to his constant chanting, he will be transferred to the kingdom of God. Yoga practice is meditation on the Supersoul within; similarly, by chanting Hare Krishna one fixes his mind always on the Supreme Lord. The mind is fickle, and therefore it is necessary to engage the mind by force to think of Krishna. One example often given is that of the caterpillar that thinks of becoming a butterfly and so is transformed into a butterfly in the same life.
For those of us who are not so familiar with these deities, we can read scriptures like the Puraanaas that have wonderful stories describing the lives and exploits of these deities. Growing up in India, our generation was fortunate to read Amar Chitra Katha comics that presented these stories in a format that appealed to us as kids. They are available all over the world now.
When one is continuously engaging in devotion, with complete surrender to God, their purified mind will gradually get fully absorbed in God- consciousness. Such souls receive the divine grace of God that liberates them from the bondage of maya. Then God bestows upon these souls His unlimited divine bliss, divine knowledge, and divine love. They become God- realized while they are still alive and live a complete life. Eventually, when they die, their soul ascends to the Divine Abode of God.
As we increase our prowess in meditation, our notion of Ishvara also grows. To help us meditate upon Ishvara in all his grandeur, Shri Krishna gives us a pointer to this type of meditation in the next shloka that describes the form of the param purusha, the supreme being.
।। हिंदी समीक्षा ।।
पूर्व श्लोक में मन-बुद्धि युक्त योग करते हुए अपने कर्म अर्थात युद्ध करने की प्रेरणा देने के बाद यहाँ इस बात पर बल दिया गया कि मन- बुद्धि युक्त योग को प्राप्त करने के यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा एवम ध्यान अर्थात अष्टांग योग का निरंतर अभ्यास करते रहना चाहिए। भगवत सम्बन्धी सजातीय वृत्तियों की आवृत्ति एवं विजातीय वृत्तियों की निवृत्ति का नाम ही अभ्यास योग है।
इस अभ्यास द्वारा चित्त विभिन्न पदार्थो या देवी देवताओं की ओर न लगा कर एक मात्र परमात्मा पर लगा देना चाहिये। यह स्मरण इतना सूक्ष्म होना चाहिए कि इष्ट के अतिरिक्त किसी अन्य वस्तु या देवी देवताओं का स्मरण या मन मे तरंग भी न हो।
अभ्यास में लगे हुए स्थिर चित्त द्वारा परमात्मा का निरंतर सूक्ष्म ध्यान अपने स्वाभाविक एवम वर्ण धर्म के अनुसार कर्तव्यकर्म करते हुए करना ही अनुचिंतन है।
अभ्यास में मन लगने से प्रसन्नता होती है और मन न लगने से खिन्नता होती है। यह अभ्यास तो है पर अभ्यासयोग नहीं है। अभ्यासयोग तभी होगा जब प्रसन्नता और खिन्नता – दोनों ही न हों। अगर चित्त में प्रसन्नता और खिन्नता हो भी जायँ तो भी उनको महत्त्व न दे केवल अपने लक्ष्यको ही महत्त्व दे। अपने लक्ष्य पर दृढ़ रहना भी योग है।
भूखे मरने से उचित भीख मांगना है और कुछ नही करने से अच्छा कर्म करते रहना है। ऐसे ही ध्यान लगाने के सगुण उपासना उचित है यही सगुण उपासना निर्गुण उपासना में परिवर्तित होती है। निर्गुण उपासना से सविकल्प समाधि लगती है और सविकल्प समाधि निर्विकल्प समाधि लगती है। निर्विकल्प समाधि से जीव में असंग के ज्ञान की प्राप्ति होने लगती है और तत् त्वं असि अर्थात उसे ब्रह्म तत्व मैं ही हूं का ज्ञान उत्पन्न होने लगता है।
निर्गुण उपासना से निर्विकारता, असंगता, स्वप्रकाशता, नित्यता, पूर्णता, एकता आदि उदार धर्म जिन का विभिन्न शास्त्रों में वर्णन आता है, स्वत: ही उपासक को प्राप्त होने लगते है। अमृत बिंदु उपनिषद में इसी निर्गुण उपासना के लिए निर्विकल्प समाधि को योगाभ्यास सिद्ध करने को कहा गया है। क्योंकि सगुण उपासना से निर्गुण उपासना अधिक ऊंची है।
अतः जो जप तप, तीर्थाटन, भजन कीर्तन अधिक करते है और निर्गुण उपासना का योगाभ्यास नही करते या निर्गुण उपासना आत्म तत्व के ज्ञान के नही करते, वे उन लोगो की श्रेणी में आते है जो गुड को फेंक कर हाथ को चाटते है। ज्ञान की प्राप्ति निर्गुण उपासना से ही अधिक सिद्ध होती है। जिन का मन व्याकुल रहता है या जो ममता, मोह में फसे हुए है, इन के सांख्य के योगाभ्यास द्वारा आत्मज्ञान हेतु परब्रह्म का निर्विकल्प समाधि से योग करना ही श्रेष्ठ है।
मरते समय जो भी आसक्ति, विचार चलता है, वही प्राण में रुक जाता है और इंद्रियों का व्यापार बंद हो जाता है। इसलिए प्राण उसी के अनुसार अगला जन्म तलाश कर लेते है। इसलिए निर्गुण उपासना को योग से करने से अंत काल में निर्गुण ब्रह्म का ध्यान रह जाता है, जिस से जीव को ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है। तापनीय उपनिषद में निष्काम निर्गुण उपासना से मुक्ति की बात कही गई है।
भगवान कहते है, हे पार्थ ! अभ्यास योगयुक्त अनन्यगामी चित्त द्वारा अर्थात् चित्तसमर्पण के आश्रयभूत मुझ एक परमात्मा में ही विजातीय प्रतीतियों के व्यवधान से रहित तुल्य प्रतीति की आवृत्ति अर्थात सजातीय वृत्तियों का आवृति का नाम अभ्यास है वह अभ्यास ही योग है ऐसे अभ्यासरूप योग से युक्त उस एक ही आलम्बन में लगा हुआ विषयान्तर में न जानेवाला जो योगी का चित्त है उस चित्त द्वारा शास्त्र और आचार्य के उपदेशानुसार चिन्तन करता हुआ योगी परम निरतिशय – दिव्य पुरुषको -जो आकाशस्थ सूर्यमण्डलमें परम पुरुष है – उसको प्राप्त होता है।
यहां माँ द्वारा उस के पुत्र है प्रेम का उदाहरण भी दे सकते कि वो समस्त कार्य करती हुई अपने पुत्र में मोह में एकचित हो कर उस का ख्याल रखती है। इसी प्रकार अभ्यास द्वारा एक चित्त हो कर एक परमात्मा का ध्यान रखते हुए जीव को अपना कर्तव्य कर्म करते रहना चाहिये। मीरा ने भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप की सगुण उपासना प्रेम से की थी।
यथार्थ गीता में स्मरण एवम युद्ध मे युद्ध को मायावी विजातीय प्रवृति जैसे काम-क्रोध, राग-द्वेष आदि के विरुद्ध बताया है। किंतु कर्मयोगी को विजातीय प्रवृति के साथ विरुद्ध युद्ध करते हुए भी अपने कर्तव्य धर्म का पालन करना ही चाहिये। यही निष्काम भाव से कर्म है, यही अकर्ता भाव से कर्म है, यही समर्पण भाव से कर्म है, यही सृष्टि यज्ञ चक्र के नियम से कर्म है एवम यदि मन- बुद्धि योग चित भाव से कर्म है। यही कर्तव्य धर्म के पालन के अनुसार कर्म है।
व्यवहारिकता में कुछ भी प्राप्त करना हो तो परिश्रम, एकाग्रता, लक्ष्य के प्रति समर्पण आदि की आवश्यकता तो होती है किन्तु निपुणता केवल निरन्तर अभ्यास से ही प्राप्त होती है, अभ्यास से ही आप सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी, उद्योगपति, वक्ता या अन्वेषण आदि कर सकते है, वैसे ही मन का नियंत्रण, कर्म करते हुए सूक्ष्म ह्रदय से स्मरण अभ्यास से प्राप्त हो सकता है, इसी पर भगवान श्री कृष्ण का भी अधिक बल के है कि अंत समय मे परमात्मा का ही स्मरण हो, तो अभ्यास के साथ अपना अपना कर्तव्य धर्म का पालन करते रहना चाहिये। सब कर्मो को त्याग कर सन्यासी बन जाने से भी अंत समय मे परमात्मा का स्मरण बिना अभ्यास के सम्भव नही।
परमात्मा ही अधियज्ञ है, वह ही समस्त यज्ञ का भोक्ता है। वह ही ह्रदय में हमेशा विद्यमान रहता है। उस परमेश्वर अर्पण बुद्धि से जन्म भर निष्काम कर्म करने वाले कर्मयोगी अंत काल मे भी जिस दिव्य स्वरूप परम पुरुष परमात्मा का स्वरूप का स्मरण करते हुए परमात्मा को प्राप्त होता है, परमात्मा को प्राप्त होना एवम स्मरण किस प्रकार का है इसे हम आगे पढ़ते है।
।। हरि ॐ तत सत ।।8.08।।
Complied by: CA R K Ganeriwala ( +91 9422310075)