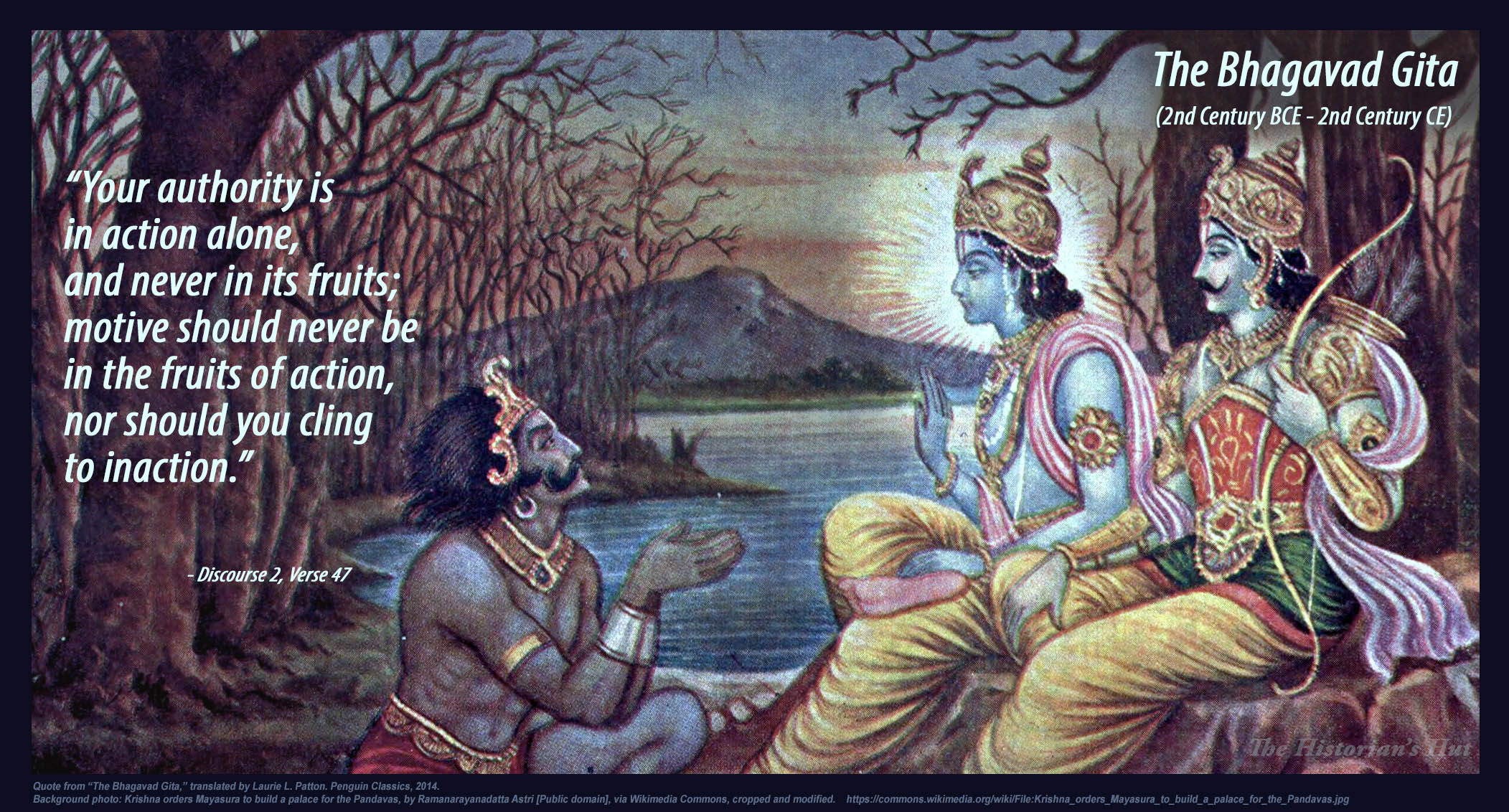।। Shrimadbhagwad Geeta ।। A Practical Approach ।।
।। श्रीमद्भगवत गीता ।। एक व्यवहारिक सोच ।।
।। Chapter 07. 12 ।I Additional II
।। अध्याय 07. 12 ।। विशेष II
।। प्रकृति एक परिचय और गुण ।। विशेष – 7.12 ।।
प्रकृति, व्यापकतम अर्थ में, प्राकृतिक, भौतिक या पदार्थिक जगत या ब्रह्माण्ड हैं। “प्रकृति” का सन्दर्भ भौतिक जगत के दृग्विषय से हो सकता है और सामन्यतः जीवन से भी हो सकता हैं। प्रकृति का अध्ययन, विज्ञान के अध्ययन का बड़ा हिस्सा है। यद्यपि मानव प्रकृति का हिस्सा है, मानवी क्रिया को प्रायः अन्य प्राकृतिक दृग्विषय से अलग श्रेणी के रूप में समझा जाता है। गीता में अध्याय 14 में प्रकृति के तीनों गुणों का वर्णन है, किंतु प्रकृति ही सृष्टि का महत्वपूर्ण घटक है जिस में परब्रह्म माया से संपूर्ण सृष्टि के संकल्प को साकार कर रहा है।
प्रकृति के नियम
आइंस्टीन ने एक बार कहा था कि ब्रह्मांड के बारे में सब से अबूझ बात यह है कि यह समझ में आने योग्य है। इसका मतलब यह है कि प्रकृति के नियम न केवल पृथ्वी पर बल्कि ब्रह्मांड पर भी लागू होते हैं। समय के साथ यह देखा गया है कि ब्रह्मांड में हर जगह, हर कण कुछ नियमों का पालन करता है जिन्हें प्रकृति के नियम कहा जाता है।
ब्रह्मांड में प्रत्येक कण एक पैटर्न का पालन करता है, जिस के कारण विज्ञान का अध्ययन बहुत हद तक वैध है। इस का अर्थ यह भी है कि प्रत्येक कण या वस्तु स्वतंत्र रूप से कार्य नहीं करती है। भौतिकी के नियम प्रकृति के मूलभूत नियम हैं जो हमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन जैसे कणों के गुणों और उन्हें नियंत्रित करने वाली शक्तियों के बारे में बताते हैं। नियमों के बिना किसी के लिए ब्रह्मांड को समझना असंभव होगा।
भौतिकी के नियम
प्रकृति के सबसे बुनियादी और निचली परत के नियम भौतिकी के नियम हैं। होम्स के नियम हमें बताते हैं कि करंट, वोल्टेज और प्रतिरोध एक दूसरे से कैसे संबंधित हैं और वे एक विद्युत सर्किट कैसे बनाते हैं।
ऐसा माना जाता है कि सभी नियम भौतिकी के अधिक मौलिक नियमों से प्राप्त हुए हैं, और समय के साथ, इन कानूनों की अधिक से अधिक खोज होती रहती है।
यह भी माना जाता है कि समीकरणों या कानूनों का एक समूह होता है, जिसे बाकी सभी कानूनों के लिए मानक कानून माना जाता है और अन्य सभी कानून उनसे प्राप्त किए जा सकते हैं।
कभी-कभी प्रकृति के नियमों की स्वतंत्रता पर सवाल उठाया जाता है, कि क्या केवल एक ही मानक कानून है या स्वतंत्र कानूनों का एक समूह है।
जीव विज्ञान के नियम
जीव विज्ञान के बुनियादी नियमों में से एक विकास का नियम है। भौतिकी के नियमों के विपरीत, यह किसी समीकरण या कुछ चर और स्थिरांक का वर्णन नहीं करता है जो विकास का वर्णन करते हैं।
विकास की अवधारणा कानून के लिए बहुत सहज है। यह दर्शाता है कि समय के साथ चीज़ें कैसी होंगी, कुछ प्रजातियाँ कैसे बदल सकती हैं या नहीं बदल सकती हैं, और प्रजातियाँ एक-दूसरे के साथ कैसे प्रतिस्पर्धा करती हैं। ऐसा लगता है मानो विकास का नियम ज्ञात तथ्यों के एक समूह के कारण सामने आया या उत्पन्न हुआ।
रसायन विज्ञान के नियम
रसायन विज्ञान में, प्रकृति के नियमों को उन टिप्पणियों के एक समूह के रूप में देखा जाता है जो प्रकृति से बनाए गए थे। वे प्रकृति में चीजों के व्यवहार के सारांश की तरह हैं।
तो, इन अवलोकनों के आधार पर, कुछ निश्चित धारणाएँ हैं।
सबसे पहले, एक प्रयोग कुछ निश्चित परिस्थितियों में किया जाता है, जिसके आधार पर कुछ निश्चित अवलोकन किए जाते हैं, जिन्हें परिकल्पना का नाम दिया जाता है। फिर, यदि ये व्यवहार और परिकल्पनाएँ सार्वभौमिक हैं या कई मामलों में सच होती हैं, तो उन्हें सिद्धांत कहा जाता है।
प्रकृति के नियमों की उत्पत्ति
ब्रह्माण्ड कल नहीं बना था. यह अरबों वर्षों से अस्तित्व में है, और प्रकृति के नियम भी ऐसे ही हैं। प्रकृति के इन नियमों को किसी ने नहीं बनाया; वे वैसे ही अस्तित्व में हैं जैसे ब्रह्मांड में है।
कुछ लोग भ्रमित हो सकते हैं कि यदि ये नियम अपरिहार्य हैं, तो उन्हें गणितीय समीकरणों में कैसे दर्शाया जाता है? प्रकृति को यह गणित कैसे पता चला? गणित की खोज नहीं हुई थी. बल्कि इस का आविष्कार कानूनों की बेहतर समझ के लिए किया गया था। अत: प्रकृति इन समीकरणों का पालन नहीं करती। बल्कि ये समीकरण उस बड़ी वास्तविकता की छाप हैं जो वहां मौजूद है। इसी प्रकार योग, ध्यान, चक्र, समाधि और सिद्धियां आदि भी प्रकृति से नियम से है, जिस पर अन्वेषण द्वारा यह क्रिया मशीनों और दवाइयों के माध्यम से की जा सके। पहले भी असुर भी ध्यान और योग से अनेक सिद्धियां प्राप्त कर लेते थे।
निष्कर्ष
प्रकृति के नियमों को एक पैटर्न या एक अवलोकन के रूप में देखा जाता है जो कुछ प्रयोगों को निष्पादित करके बनाया गया था। ये पैटर्न इस ब्रह्मांड में मौजूद हर चीज़ के लिए सत्य हैं। कुछ लोगों का मानना है कि ये नियम उस वर्तमान ब्रह्मांड के निर्माण के साथ ही बने थे जिसमें हम रहते हैं। यदि वर्तमान ब्रह्मांड का गठन अलग तरीके से हुआ होता, तो कानून अलग हो सकते थे। प्रकृति के नियमों पर भौतिकी, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान के परिप्रेक्ष्य से चर्चा की गई, जिन्हें विज्ञान के निर्माण खंड माना जाता है।
परिवर्तन प्रकृति का नियम है। जिस प्रकार से प्रकृति स्वयं में बदलाव करती है । समय समय पर अपने रुप में बदलाव लाती है कभी पतजड़ का मौसम तो कभी गर्मी का समय तो बरसात का तो कभी ठंड का मौसम आने से प्रकृति का सौन्दर्य इस हरियाली से है वो इस परिवर्तन से हमेंशा बनी रहती है ।
पुरुष और प्रकृति
सारा संसार प्रकृति को समझने में फँसा है। पुरुष और प्रकृति को तो अनादि से खोजते आए हैं। लेकिन वे योें हाथ में आ जाएँ, ऐसे नहीं हैं। क्रमिक मार्ग में पूरी प्रकृति को पहचान ले उस के बाद में पुरुष की पहचान होती है। उस का तो अनंत जन्मों के बाद भी हल निकले ऐसा नहीं है। जबकि अक्रम मार्ग में ज्ञानी पुरुष सिर पर हाथ रख दें, तो खुद पुरुष होकर सारी प्रकृति को समझ जाता है। फिर दोनों सदा के लिए अलग-अलग ही रहते हैं। प्रकृति की भूलभूलैया में अच्छे-अच्छे फँसे हुए हैं, और वे करते भी क्या? प्रकृति द्वारा प्रकृति को पहचानने जाते हैं न, उस का कैसे पार पाएँ?
पुरुष होकर प्रकृति को पहचानना है, तभी प्रकृति का हर एक परमाणु पहचाना जा सकता है।
प्रकृति अर्थात् क्या? प्र = विशेष और कृति = किया गया। स्वाभाविक की गई चीज़ नहीं। लेकिन विभाव में जाकर, विशेष रूप से की गई चीज़, वही प्रकृति है।
प्रकृति तो स्त्री है, स्त्री का रूप है और ‘खुद’(सेल्फ) पुरुष है। कृष्ण भगवान ने अर्जुन से कहा कि त्रिगुणात्मक से परे हो जा, अर्थात् त्रिगुण, प्रकृति के तीन गुणों से मुक्त, ‘तू’ ऐसा पुरुष बन जा। क्योंकि यदि प्रकृति के गुणों में रहेगा, तो ‘तू’ अबला है और पुरुष के गुणों में रहा, तो ‘तू’ पुरुष है।
‘प्रकृति लट्टू जैसी है।’ लट्टू यानी क्या? डोरी लिपटती है, वह सर्जन, डोरी खुले, तब घूमता है, वह प्रकृति। डोरी लिपटती है, तब कलात्मक ढंग से लिपटती है, इसलिए खुलते समय भी कलात्मक ढंग से ही खुलेगी। बालक हो, तब भी खाते समय निवाला क्या मुँह में डालने के बजाय कान में डालता है? साँपिन मर गई हो, तब भी उस के अंडे टूटने पर उनमें से निकलने वाले बच्चे निकलते ही फन फैलाने लगते हैं, तुरंत ही। इस के पीछे क्या है? यह तो प्रकृति का अजूबा है।
प्रकृति का कलात्मक कार्य, एक अजूबा है। प्रकृति इधर-उधर कब तक होती है? उसकी शुरूआत से ज़्यादा से ज़्यादा इधर-उधर होने की लिमिट है। लट्टू का घूमना भी उसकी लिमिट में ही होता है। जैसे कि, विचार उतनी ही लिमिट में आते हैं। मोह होता है, वह भी उतनी लिमिट में ही होता है। इसलिए प्रत्येक जीव की नाभि, सेन्टर है और वहाँ आत्मा आवृत्त नहीं है। वहाँ शुद्ध ज्ञानप्रकाश रहा हुआ है। यदि प्रकृति लिमिट से बाहर जाए, तो वह प्रकाश आवृत्त हो जाता है और पत्थर हो जाता है, जड़ हो जाता है। लेकिन ऐसा होता ही नहीं है। लिमिट में ही रहता है। यह मोह होता है, इसलिए उसका आवरण छा जाता है। चाहे जितना मोह टॉप पर पहुँचा हो, लेकिन उसकी लिमिट आते ही फिर नीचे उतर जाता है। यह सब नियम से ही होता है। नियम से बाहर नहीं होता।
प्रकृति के तीन गुण से ( सत्त्व , रजस् और तमस् ) सृष्टि की रचना हुई है या यह माने की प्रकृति ही यह तीन गुण है। ये तीनों घटक सजीव-निर्जीव, स्थूल-सूक्ष्म वस्तुओं में विद्यमान रहते हैं । इन तीनों के बिना किसी वास्तविक पदार्थ का अस्तित्व संभव नहीं है। किसी भी पदार्थ में इन तीन गुणों के न्यूनाधिक प्रभाव के कारण उस का चरित्र निर्धारित होता है।
गुण का शाब्दिक अर्थ है “गुण”। योग दर्शन और आयुर्वेद में, 3 गुण प्रकृति के आवश्यक गुण हैं जो सभी प्राणियों और चीजों में मौजूद हैं। प्रत्येक गुण एक विशिष्ट विशेषता से जुड़ा हुआ है:
सत्त्व = पवित्रता और ज्ञान
राजस = गतिविधि और इच्छा
तमस = अंधकार और विनाश
ये शक्तियाँ हर समय हमारे भीतर मौजूद रहती हैं और कुछ स्थितियों और अनुभवों पर हमारी प्रतिक्रियाओं में प्रकट होती हैं। हालाँकि, गुणों में से एक हमेशा अन्य दो की तुलना में अधिक प्रभावशाली होता है।
गुण शब्द से हमें किसी एक पदार्थ की प्रतीति न हो कर, उस गुण को धारण करने वाले अनेक पदार्थों की एक साथ प्रतीति होती है। जैसे खारा कह देने से तमाम खारे पदार्थों की प्रतीति होती है, न कि केवल नमक की। इस तरह हम देखते हैं कि गुण का अर्थ है किसी पदार्थ का स्वभाव। लेकिन साँख्य के त्रिगुण गुणवत्ता या स्वभाव नहीं हैं। यहाँ वे प्रकृति के आवश्यक घटक हैं। सत्व, रजस् और तमस् नाम के तीनों घटक प्रकृति और उस के प्रत्येक अंश में विद्यमान रहते हैं। इन तीनों के बिना किसी वास्तविक पदार्थ का अस्तित्व संभव नहीं है। किसी भी पदार्थ में इन तीन गुणों के न्यूनाधिक प्रभाव के कारण उस का चरित्र निर्धारित होता है। हमें अन्य तत्वों के बारे में जानने के पूर्व साँख्य सिद्धांत के इन तीन गुणों के बारे में कुछ बात कर लेनी चाहिए। सत्व का संबंध प्रसन्नता और उल्लास से है, रजस् का संबंध गति और क्रिया से है। वहीं तमस् का संबंध अज्ञान और निष्क्रीयता से है।
गुणों का मूल्यांकन वस्तु की शुद्धता के आधार पर है। जैसे 24 कैरट का सोना शुद्ध कह सकते है, जब कि इस मे 2 से 8 कैरट अशुद्धता आभूषण बनाने में उपयोगी होने से “रज” या उपयोगी मान सकते है, किन्तु इस से अधिक अशुद्धता होने से सोने का वर्गीकरण बेकार अनुपयोगी में होने लग जायेगा। यही सत-रज-तम गुण जड़ से ले कर चेतन्य सभी प्राणी में विभिन्न मात्रा में फैले है। जिन की कोई स्थिर मात्रा नही और बदलता रहना,इन का गुण है।
सत्वगुण का अर्थ “शुद्धता”, “पवित्रता” तथा “ज्ञान” है। सत्व नाम अर्थात अच्छे कर्मों की ओर मोड़ने वाला गुण का है। तीनों गुणों ( सत्त्व , रजस् और तमस् ) में से सर्वश्रेष्ठ गुण सत्त्व गुण हे सात्विक मनुष्य – किसी कर्म फल अथवा मान सम्मान की अपेक्षा अथवा स्वार्थ के बिना समाज की सेवा करना ।
सत्त्वगुण दैवी तत्त्व के सबसे निकट है । इसलिए सत्त्व प्रधान व्यक्ति के लक्षण हैं – प्रसन्नता, संतुष्टि, धैर्य, क्षमा करने की क्षमता, अध्यात्म के प्रति झुकाव । एक सात्विक व्यक्ति हमेशा वैश्विक कल्याण के निमित्त काम करता है। हमेशा मेहनती, सतर्क होता है । एक पवित्र जीवनयापन करता है। सच बोलता है और साहसी होता है।
सत्व प्रकृति का ऐसा घटक है जिस का सार पवित्रता, शुद्धता, सुंदरता और सूक्ष्मता है। सत्व का संबंध चमक, प्रसन्नता, भारन्यूनता और उच्चता से है। सत्व अहंकार, मन और बुद्धि से जुड़ा है। चेतना के साथ इस का गहरा संबंध है। परवर्ती साँख्य में यह कहा जाता है कि चेतना के साथ इस का गहरा संबंध अवश्य है लेकिन इस के अभाव में भी चेतना संभव है। यहाँ तक कि बिना प्रकृति के भी चेतना का अस्तित्व है। लेकिन यह कथन मूल साँख्य का प्रतीत नहीं होता है अपितु यह परवर्ती सांख्य में वेदान्त दर्शन का आरोपण मात्र प्रतीत होता है जो चेतना के स्वतंत्र अस्तित्व की अवधारणा प्रस्तुत करता है।
रजस् प्रकृति का दूसरा घटक है जिस का संबंध पदार्थ की गति और कार्रवाई के साथ है। भौतिक वस्तुओं में गति रजस् का परिणाम हैं। जो गति पदार्थ के निर्जीव और सजीव दोनों ही रूपों में देखने को मिलती वह रजस् के कारण देखने को मिलती है। निर्जीव पदार्थों में गति और गतिविधि, विकास और ह्रास रजस् का परिणाम हैं वहीं जीवित पदार्थों में क्रियात्मकता, गति की निरंतरता और पीड़ा रजस के परिणाम हैं।
रजस् का अर्थ क्रिया तथा इच्छाएं है। राजसिक मनुष्य – स्वयं के लाभ तथा कार्यसिद्धि हेतु जीना । जो गति पदार्थ के निर्जीव और सजीव दोनों ही रूपों में देखने को मिलती वह रजस् के कारण देखने को मिलती है। निर्जीव पदार्थों में गति और गतिविधि, विकास और ह्रास रजस् का परिणाम हैं वहीं जीवित पदार्थों में क्रियात्मकता, गति की निरंतरता और पीड़ा रजस के परिणाम हैं।
तमस् प्रकृति का तीसरा घटक है जिस का संबंध जीवित और निर्जीव पदार्थों की जड़ता, स्थिरता और निष्क्रीयता के साथ है। निर्जीव पदार्थों में जहाँ यह गति और गतिविधि में अवरोध के रूप में प्रकट होता है वहीं जीवित प्राणियों और वनस्पतियों में यह अशिष्टता, लापरवाही, उदासीनता और निष्क्रियता के रूप में प्रकट होता है। मनुष्यों में यह अज्ञानता, जड़ता और निष्क्रियता के रूप में विद्यमान है।
तमस् का अर्थ अज्ञानता तथा निष्क्रियता है। तामसिक मनुष्य – दूसरों को अथवा समाज को हानि पहुंचाकर स्वयं का स्वार्थ सिद्ध करना | तम प्रधान व्यक्ति, आलसी, लोभी, सांसारिक इच्छाओं से आसक्त रहता है ।
तमस् गुण के प्रधान होने पर व्यक्ति को सत्य-असत्य का कुछ पता नहीं चलता, यानि वो अज्ञान के अंधकार (तम) में रहता है। यानि कौन सी बात उसके लिए अच्छी है वा कौन सी बुरी ये यथार्थ पता नहीं चलता और इस स्वभाव के व्यक्ति को ये जानने की जिज्ञासा भी नहीं होती।
गुण कहाँ पाए जाते हैं?
गुण माया (संसार की माया और उसके सभी विकर्षणों) के हर हिस्से में मौजूद हैं। उन्हें दिन, मौसम, भोजन, विचारों और कार्यों में देखा जा सकता है। उदाहरण के लिए, सुबह का समय सत्त्वगुण लाता है, दोपहर का समय राजसिक हो जाता है और रात का समय तमस लाता है।
इसलिए, रजस और तमस के बिना शुद्ध सत्त्व नहीं हो सकता, न ही तमस और सत्व के बिना शुद्ध रजस हो सकता है। सत्व हमें खुशी के साथ आसक्ति से बांधता है , राजस हमें गतिविधि से जोड़ता है, और तमस हमें भ्रम से जोड़ता है। जब तक हम तीनों गुणों में से किसी एक से प्रभावित होते हैं, तब तक हम माया के बंधन में रहते हैं।
गुण हमें कैसे प्रभावित करते हैं?
तीन गुण हमें गहराई से प्रभावित करते हैं। वे हमारे बारे में हर चीज़ को प्रभावित करते हैं , हमारे विचारों और कार्यों से लेकर आदतों और गतिविधियों तक जो हमें वह बनाती हैं जो हम हैं। इसका मतलब यह है कि जो भी गुण आपके भीतर अधिक मौजूद है, वह इस बात को प्रभावित करेगा कि आप दुनिया को कैसे देखते हैं । उदाहरण के लिए, मुख्य रूप से तामसिक व्यक्ति हर चीज़ को नकारात्मक और विनाशकारी के रूप में देखेगा। दूसरी ओर, जो व्यक्ति अधिक सात्विक है, उसका दृष्टिकोण सकारात्मक होगा और वह हर चीज में आनंद और खुशी ढूंढेगा।
गुण की पहचान – कथा
एक छोटे, गरीब गाँव में, तीन दोस्तों ने बेहतर जीवन का सपना देखा। इसलिए, वे भारतीय गर्मियों की तेज़ धूप में चलते हुए, शहर का पता लगाने के लिए निकल पड़े। दोपहर तक, वे भूखे-प्यासे थे, और पास के जंगल में विश्राम के लिए रुक गए।
एक पेड़ की छाया के नीचे उनकी नजर फलों से लदे आम के पेड़ पर पड़ी। इसे अपनी भूख-प्यास मिटाने का वरदान समझकर सबसे पुराना मित्र पेड़ के पास पहुंचा। उसने जमीन पर पके आम देखे, उन्हें उठाया और उनका स्वाद लिया और इस उपहार के लिए भगवान को धन्यवाद दिया। फिर उन्होंने इस उम्मीद में बीज बोए कि वे भविष्य के यात्रियों को लाभ पहुंचाने के लिए एक पेड़ बन सकते हैं।
यह सत्व गुण है
इसके बाद दूसरा दोस्त पेड़ के पास चला गया। उसने देखा कि वह आमों और लकड़ियों को बाजार में बेच सकता है, जिससे खुद को फायदा हो सकता है। इसलिए, कुछ आमों का आनंद लेने के बाद, उसने अपने चतुर विचार पर गर्व करते हुए, फलों से भरी एक शाखा तोड़ दी और उसे ले गया।
यह राजस गुण है
आख़िरकार तीसरा दोस्त पेड़ के पास गया। स्वयं पेड़ उगाने के अपने असफल प्रयासों के बावजूद पेड़ की सफलता से ईर्ष्या करते हुए, उसने द्वेषवश इसे नष्ट करने का फैसला किया। लेकिन, उसने जो आम तोड़े वे कच्चे और खट्टे थे। वह नहीं जानता था कि अंतर कैसे बताया जाए, और सीखने के बजाय, उसने अपने क्रोध को अपने कार्यों पर हावी होने दिया और पेड़ को आग लगा दी।
यह तमो गुण है
इस कहानी में, तीन दोस्त तीन अलग-अलग गुणों का प्रतिनिधित्व करते हैं – कृतज्ञता और ज्ञान (सत्व), स्वार्थ (रजस), और नकारात्मक अहंकार (तमस)। हममें से प्रत्येक को इन गुणों में से एक द्वारा निर्देशित किया जाता है , जो हमारे सोचने, महसूस करने और कार्य करने के तरीके को प्रभावित करता है।
कृष्ण भगवान ने गीता में कहा है कि, ‘वेद तीन गुणों से बाहर नहीं हैं, वेद तीन गुणों को ही प्रकाशित करते हैं।’ कृष्ण भगवान ने ‘नेमीनाथ’ से मिलने के बाद गीता कही थी, उससे पहले वे वेदांती थे। उन्होंने गीता में कहा, ‘त्रैगुण्य विषयो वेदो निस्त्रैय गुण्यो भवार्जुन,’ यह गज़ब का वाक्य कृष्ण ने कह दिया है! ‘आत्मा जानने के लिए वेदांत से परे जाना,’ कह दिया है! उन्होंने ऐसा कहा कि, ‘हे अर्जुन! आत्मा जानने के लिए तू त्रिगुणात्मक से परे हो।’ त्रिगुणात्मक कौन-कौन से? सत्व, रज और तम। वेद इन्हीं तीन गुणवाले हैं, इसलिए तू उनसे परे हो जाएगा तभी तेरा काम होगा। और फिर ये तीन गुण द्वंद्व हैं, इसलिए तू त्रिगुणात्मक से परे हो जा और आत्मा को समझ! आत्मा जानने के लिए कृष्ण ने वेदांत से बाहर जाने को कहा है, लेकिन लोग समझते नहीं है। चारों ही वेद पूरे होने के बाद वेद इटसेल्फ क्या कहते हैं? दिस इज़ नोट देट, दिस इज़ नोट देट, तू जिस आत्मा को ढूँढ रहा है वह इसमें नहीं है। ‘न इति, न इति,’ इसलिए तुझे यदि आत्मा जानना हो तो गो टु ज्ञानी।
कृष्ण भगवान ने कहा है कि, ‘यह जगत् भगवान ने नहीं बनाया है, लेकिन स्वभाविक रूप से बन गया है!’
मूल-साँख्य के अनुसार प्रधान (आद्य प्रकृति) में ये तीनों घटक साम्यावस्था में थे। आपसी अंतक्रिया के परिणाम से भंग हुई इस साम्यावस्था ने प्रकृति के विकास को आरंभ किया जिस से जगत (विश्व Universe) का वर्तमान स्वरूप संभव हुआ। हम इस सिद्धान्त की तुलना आधुनिक भौतिक विज्ञान द्वारा प्रस्तुत विश्व के विकास (Evolution of Universe) के सर्वाधिक मान्य महाविस्फोट के सिद्धांत (Big-Bang theory) के साथ कर सकते हैं। दोनों ही सिद्धांतों में अद्भुत साम्य देखने को मिलता है।
अब एक परम गणितीय मॉडल बनाने का प्रयास किया जा रहा है जो स्पष्ट रूप से ब्रह्मांड की कार्यक्षमता का प्रतिनिधित्व करेगा। वैज्ञानिक किसी अंतिम नियम के अस्तित्व में विश्वास नहीं करते। उनका मानना है कि प्रकृति के वर्तमान नियम अतीत में हमारे ब्रह्मांड में जो कुछ हुआ उसका परिणाम हैं। यदि चीजें वास्तव में जो हुआ उससे भिन्न होतीं, तो ये कानून भिन्न हो सकते थे। इसका मतलब यह है कि प्रकृति के नियम समय के साथ बदल सकते हैं।
अंतिम विचार
आत्मज्ञान या समाधि प्राप्त करने में खुद को तीन गुणों से मुक्त करना और माया के भ्रम से परे सत्य को समझना शामिल है। एक व्यक्ति जो गुणों से ऊपर उठ चुका है, वह जीवन के द्वंद्वों, जैसे दर्द और सुख, से अप्रभावित रहता है। भगवद गीता के बुद्धिमान शब्दों में:
“जब कोई शरीर में उत्पन्न होने वाले तीन गुणों से ऊपर उठ जाता है;
व्यक्ति जन्म, बुढ़ापा, रोग और मृत्यु से मुक्त हो जाता है; और आत्मज्ञान प्राप्त करता है” (भगवद गीता 14.20)
यह संक्षिप्त परिचय गीता को समझने के आवश्यक है क्योंकि गीता पढ़ते समय हम जो भी अर्थ या भावार्थ समझते है, वह हमारी प्रकृति के गुण के अनुसार होती है। जब तक सात्विक गुण नही प्राप्त होता, धर्म या ज्ञान का प्रत्येक कार्य कामना या आसक्ति के साथ ही होता है।
।। हरि ॐ तत सत ।। विशेष 7.12 ।।
Complied by: CA R K Ganeriwala ( +91 9422310075)