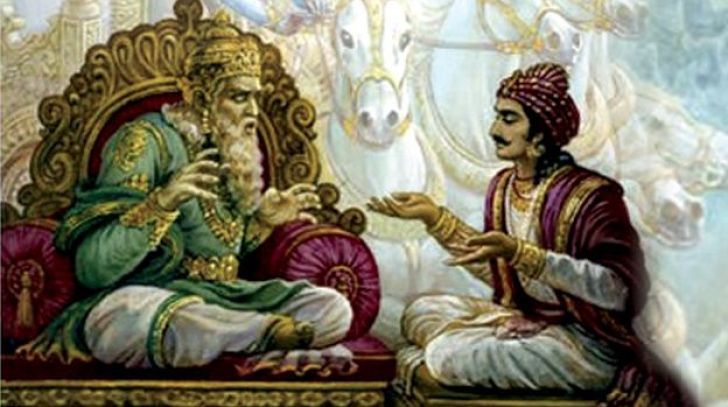।। Shrimadbhagwad Geeta ।। A Practical Approach ।।
।। श्रीमद्भगवत गीता ।। एक व्यवहारिक सोच ।।
।। Chapter 04.28।।
।। अध्याय 04.28 ।।
॥ श्रीमद्भगवद्गीता ॥ 4.28॥
द्रव्ययज्ञास्तपोयज्ञा योगयज्ञास्तथापरे ।
स्वाध्यायज्ञानयज्ञाश्च यतयः संशितव्रताः ॥
“dravya-yajñās tapo-yajñā,
yoga-yajñās tathāpare..।
svādhyāya-jñāna-yajñāś ca,
yatayaḥ saḿśita-vratāḥ”..।।
भावार्थ :
कुछ मनुष्य धन-सम्पत्ति के दान द्वारा, कुछ मनुष्य तपस्या द्वारा और कुछ मनुष्य अष्टांग योग के अभ्यास द्वारा यज्ञ करते हैं, कुछ अन्य मनुष्य वेद-शास्त्रों का अध्ययन करके, कुछ ज्ञान में निपुण होकर और कुछ मनुष्य कठिन व्रत धारण कर के यज्ञ करते है। (२८)
Meaning:
Others offer sacrifice of materials, austerity and yoga, and other seekers with a resolute will offer the sacrifice of knowledge through study of scriptures.
Explanation:
In Indian philosophy the Yog Darśhan is one of the six philosophical treatises written by six learned sages. Jaimini wrote “Mimsnsa Darśhan,” Ved Vyas wrote “Vedant Darśhan,” Gautam wrote “Nyaya Darśhan,” Kanad wrote “Vaiśheṣhik Darśhan,” Kapil wrote “Sankhya Darśhan,” and Patañjali wrote “Yog Darśhan.” The Patañjali Yog Darśhan describes an eight-fold path, called aṣhṭaṅg yog, for spiritual advancement, starting with physical techniques and ending in conquest of the mind.
Human beings differ from each other in their natures, motivations, activities, professions, aspirations, and sanskars (tendencies carrying forward from past lives). Shree Krishna brings Arjun to the understanding that sacrifices can take on hundreds of forms, but when they are dedicated to God, they become means of purification of the mind and senses and elevation of the soul.
Shri Krishna gives us a choice of four more yajnyas in this shloka.
First, he talks about the sacrifice of wealth, or as it is more commonly known – charity. As we saw in the second chapter, lobha or the tendency to hoard can destabilize our mind, and strengthen the ego. Therefore, giving away wealth or even our time to a higher ideal checks this tendency to hoard. But charity has to be done with the attitude that I am giving away what was not mine to begin with. If one donates with a view to gain publicity and so on, that is a selfish or rajasic type of charity.
Secondly, Shri Krishna mentions austerity or tapas. In this type of yajyna, the urge of the sense organs to go out into the world is checked, so that the ego is weakened. There are three avenues for conducting tapas: the body, senses and mind. In physical tapas, we use the energy of our body to do seva or service the world. In sense- related tapas, we keep a strong leash on our senses and organs. For example, we can practice austerity on speech by always speaking truth, saying what’s beneficial to someone, and creating disturbance in anybody’s mind. In mental tapas, we control our mind by not giving attention to negative thoughts and emotions, and not letting others trigger such emotions in us.
Third, Shri Krishna gives us the option of practicing a detailed regimen of spiritual practice or yoga. It could be bhakti yoga (which we will see later), karma yoga, raaja yoga of Patanjali and so on.
Finally, we can practice study of the scriptures, which is also known as jnyaana yajnya. A daily reading of the Gita, Ramayana or any other such spiritual text with utmost attention, concentration, understanding and discipline is also a yajnya. Here also, the ego becomes weak because the intellect gains a firmer and stronger position in relation to the ego, strengthened by daily exposure to the scriptures.
Jnana yajna. Some persons are inclined toward the cultivation of knowledge. This propensity finds its perfect employment in the study of scriptures for enhancing one’s understanding and love for God. sa vidya tanmatiryaya (Bhagavatam 4.29.49)[v25] “True knowledge is that which increases our devotion to God.” Thus, studiously inclined sadhaks engage in the sacrifice of knowledge, which when imbued with the spirit of devotion, leads to loving union with God. Tapo yajnaḥ; tapas means mastery of the sense organs.it should not enforced self-denial;
The common thread of all the yajnyas mentioned is that of weakening the hold of the ego, which is nothing but weakening of the notion of “I-ness” and “mine-ness”.
।। हिंदी समीक्षा ।।
सनातन धर्म विभिन्न विचारधाराओं का क्रमिक विकास है, जब बुद्धि, मन, इंद्रियां और शरीर के सभी अंगों की आवश्यकता और विकास की बात वेदांत करता है तो वह प्रकृति में और प्रकृति के परे मुक्ति को खोजता है। इसलिए सनातन संस्कृति विभिन्न दर्शन शास्त्र का समूह है जिस में जैमिनी के मीमांसा, गौतम के न्याय शास्त्र, कणाद के वैशेषिक, पतंजलि के योग,कपिल के सांख्य शास्त्र एवम वेदव्यास के वेदांत शास्त्र का समावेश है। यह कालांतर में उन्नति की ओर प्रशस्त है, इसलिए मीमांसा से ले कर वेदांत शास्त्र में विरोध नही है, अपितु जिस में जो सत्य लगा उस को स्वीकृत किया गया। क्योंकि सभी का लक्ष्य मुक्ति ही है।
अहिंसा, सत्य, अस्तेय (चोरीका अभाव) ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह (भोगबुद्धि से संग्रह का अभाव) ये पाँच यम हैं जिन्हें महाव्रत के नाम से कहा गया है। शास्त्रों में इन महाव्रतों की बहुत प्रशंसा महिमा है। इन व्रतों का सार यही है कि मनुष्य संसार से विमुख हो जाय। इन व्रतों का पालन करने वाले साधकों के लिये यहाँ संशितव्रताः पद आया है। इसके सिवाय इस श्लोक में आये चारों यज्ञों में जो जो पालनीय व्रत अर्थात् नियम हैं उन पर दृढ़ रह कर उनका पालन करनेवाले भी सब संशितव्रताः हैं। यज्ञ के माध्यम से तप यानि अकर्म करने वालो को भगवान ने इस प्रकार बताया है।
जीव को आकर्षण चाहे प्रकृति का रहे किंतु वह परब्रह्म का अंश है, इसलिए वह मुक्ति के नाम पर सुख को खोजता है। वह सुख शारीरिक, मानसिक, भौतिक या आध्यात्मिक या मोक्ष का भी हो सकता है। इसलिए उस के यज्ञ कामना और कामना रहित दोनो प्रकार के होते है। परमात्मा कामना सहित यज्ञ करने वालो को भी निराश नहीं करता और उसे उस के यज्ञ के अनुसार फल प्रदान करता है।
द्रव्ययज्ञ यहां द्रव्य शब्द को उस के व्यापक अर्थ में समझना चाहिये। ईमानदारी से अर्जित किये धन का समाज सेवा में भक्तिभाव सहित विनियोग करने को द्रव्ययज्ञ कहते हैं। यह आवश्यक नहीं कि इस में केवल अन्न या धन का ही दान हो। द्रव्य शब्द के अर्थ में वे सब वस्तुएं समाविष्ट हैं जो हमारे पास हैं जैसे भौतिक सम्पत्ति प्रेम और सद्विचार। ईश्वर की पूजा समझ कर अपनी इन भौतिक मानसिक एवं बौद्धिक सम्पदाओं का समाजसेवा में सदुपयोग करना ही द्रव्ययज्ञ कहलाता है। अत इस यज्ञ के अनुष्ठान के लिए साधक का धनवान होना आवश्यक नहीं है। दरिद्र अथवा शरीर से अपंग होते हुए भी हम जगत् के कल्याण की कामना कर सकते हैं और हृदय से प्रार्थना कर सकते हैं। हार्दिक सहानुभूति का एक शब्द कृपा का एक कटाक्ष स्नेह सिंचित स्मिति अथवा मैत्रीपूर्ण सदव्यवहार पाषाणी मन से दी हुई बड़ी धनराशि से भी अधिक महत्व का होता है। द्रव्य यज्ञ में यदि अहम है जैसे नाम कमाने की लालसा तो वो यज्ञ नही व्यापार होगा। ऐसा दान राजस या तामस होगा। पाप या अनैतिक तरीके से कमाए धन से यदि द्रव्य यज्ञ किया जाए तो उस का परिणाम में धन के स्तोत्र का भी प्रभाव होता है।
तपोयज्ञ कुछ साधक गण अपना तपोमय जीवन ईश्वर को अर्पित करते हैं। विश्व में ऐसा कोई धर्म नहीं जो किसी न किसी प्रकार से तप या व्रत का जीवन जीने का उपदेश न करता हो। ये व्रत परमेश्वर प्रीत्यर्थ ही किये जाते हैं। यह तो सब जानते ही हैं कि भक्त द्वारा किये गये भोग के त्याग से समस्त विश्व के पालन और पोषणकर्त्ता करुणासागर परमात्मा का कोई विशेष प्रयोजन सिद्ध होने का नहीं तथापि साधकगण उसे ईश्वरार्पण करते हैं जिससे उन्हें आत्मसंयम और चित्त शुद्धि प्राप्त हो। कोई कोई तप शरीर के लिये अत्यन्त पीड़ादायक होते हैं फिर भी यदि उन्हें समझ कर किया जाय तो इन्द्रिय संयम प्राप्त हो सकता है। तप शारीरिक, मानसिक एवम बौद्धिक किया जा सकता है।
योगयज्ञ अपने मन से निकृष्ट प्रवृत्तियों का त्याग कर के उत्कृष्ट जीवन जीने के सतत् प्रयत्न का नाम है योग। इस की प्राथमिक साधना है अपने हृदय के इष्ट भगवान् की भक्ति पूर्वक पूजा करना। इस का ही नाम है उपासना। निष्काम भावना से उपासना का अनुष्ठान करने पर साधक की अध्यात्म मार्ग में प्रगति होती है इसलिये इसे योग कहा गया है और यज्ञ भावना से इस का अनुष्ठान करने के कारण यहां योगयज्ञ कहा गया है। पतंजलि का अष्टांग योग इस श्रेणी में आता है।
स्वाध्याय यज्ञ प्रतिदिन शास्त्रों का अध्ययन करना स्वाध्याय कहलाता है। शास्त्रों के अध्ययन के बिना हम न तो अपने लक्ष्य को ही निर्धारित कर सकते हैं और न ही साधना अभ्यास का अर्थ ही समझ सकते हैं। ज्ञानरहित यन्त्रवत् साधना से अपेक्षित प्रगति नहीं हो सकती। यही कारण है कि सभी धर्मों में दैनिक स्वाध्याय पर विशेष बल दिया जाता है। आत्मानुभव के पश्चात् भी ऋषि मुनि अपना अधिकांश समय शास्त्राध्ययन तथा उसके गम्भीर चिन्तन, मनन और निध्यासन में व्यतीत करते हैं। अध्यात्म दृष्टि से स्वाध्याय का अर्थ है स्वयं का अध्ययन अर्थात् आत्म निरीक्षण के द्वारा अपनी दुर्बलताओं को समझना जिस से उन का परित्याग किया जा सके। साधक के लिये यह आत्मविकास का एक साधन है तो सिद्ध पुरुषों के लिये आत्मानुभव में रमण का।
ज्ञानयज्ञ गीता में यह शब्द अनेक स्थानों पर प्रयुक्त है और व्यास जी ने जिन मौलिक शब्दों का प्रयोग गीता में किया है उन में से यह एक है। वह साधना ज्ञानयज्ञ कहलाती है जिसमें साधक ज्ञान की अग्नि प्रज्वलित करके उसमें अपने अज्ञान की आहुति देता है।
आत्मानात्म विवेक के द्वारा अनात्म वस्तु का निषेध एवं आत्मा के पारमार्थिक सत्य स्वरूप का प्रतिपादन इस यज्ञ के अंग हैं। निदिध्यासन में इसी का अभ्यास किया जाता है।आत्मोन्नति के उपर्युक्त पाँच साधनों का लाभ दृढ़ निश्चयी एवं उत्साहपूर्ण अभ्यासी साधकों को ही मिल सकता है। इन साधकों को केवल ज्ञान अथवा आत्मविकास की इच्छामात्र से कोई प्रगति नहीं हो सकती। पूर्ण लगन से जो निरन्तर साधना का अभ्यास करते हैं केवल वे ही साधक अध्यात्म के मार्ग पर सफलतापूर्वक आगे बढ़ सकते हैं।
भगवान श्री कृष्ण द्वारा कर्मयोगी जो मोक्ष को प्राप्त करना चाहते है अलग अलग तरीके से कर्म में अपनी अपनी क्षमता से लगे हुए है। यह बात पुनः दोहराना उचित होगा कि स्वार्थ एवम अहम की दृष्टि से कोई भी कार्य यज्ञ, हवन या आहुति में नही आता क्योंकि इस मे जीव प्रकृति के अधीन कार्य करता है जो कर्म बंधन करते है। यदि मंदिर में आप सांसारिक सुख या लालसा ले कर जाते है, कीर्तन भजन धन कमाने के लिए करते है या उपवास, व्रत और तप कोई फल की कामना से करते है तो वो यज्ञ नही है। साधनोपदेश के क्रम में अब अगले श्लोक में भगवान् प्राणायाम की विधि बताते हैं।
।। हरि ॐ तत सत।। 4.28।।
Complied by: CA R K Ganeriwala ( +91 9422310075)