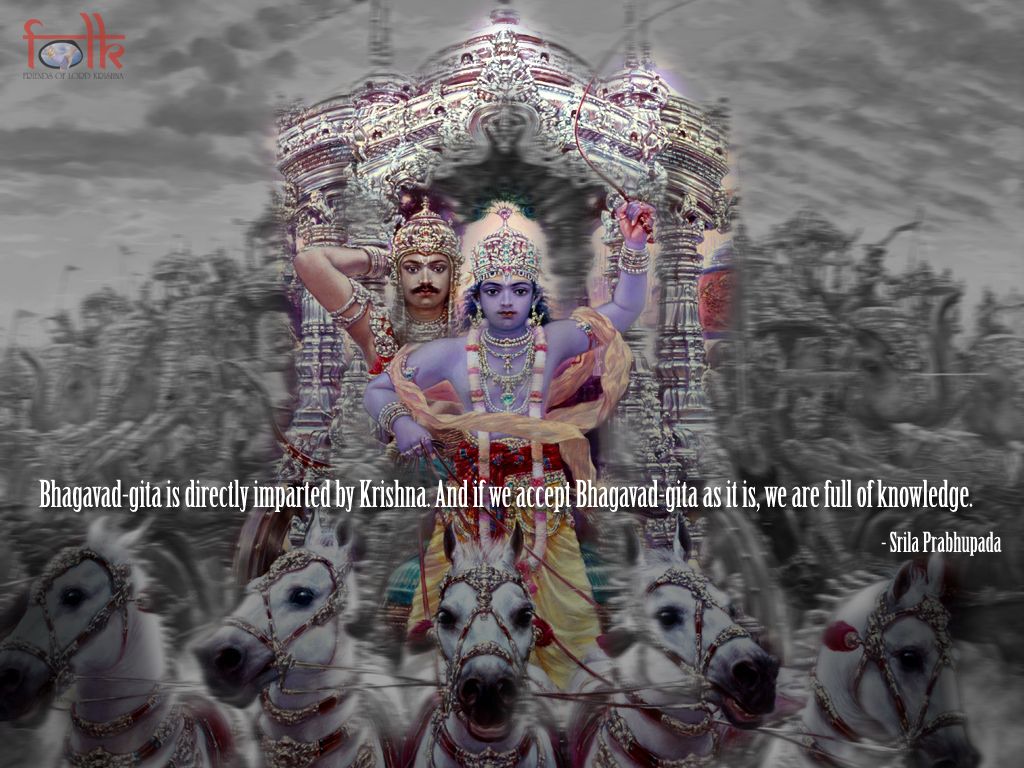।। Shrimadbhagwad Geeta ।। A Practical Approach ।।
।। श्रीमद्भगवत गीता ।। एक व्यवहारिक सोच ।।
।। Chapter 04.22।।
।। अध्याय 04.22 ।।
॥ श्रीमद्भगवद्गीता ॥ 4.22॥
यदृच्छालाभसंतुष्टो द्वंद्वातीतो विमत्सरः ।
समः सिद्धावसिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते ॥
“yadṛcchā-lābha-santuṣṭo,
dvandvātīto vimatsaraḥ..I
samaḥ siddhāv asiddhau ca,
kṛtvāpi na nibadhyate”..II
भावार्थ :
जो मनुष्य स्वत: प्राप्त होने वाले लाभ से संतुष्ट रहता है, जो सभी द्वन्द्वो से मुक्त और किसी से ईर्ष्या नही करता है, जो सफ़लता और असफ़लता में स्थिर रहता है यधपि सभी प्रकार के कर्म करता हुआ कभी बँधता नही है। (२२)
Meaning:
Content in whatever comes of its own accord, transcending duality, free from envy, balanced in success and in failure; (he) is not bound even when performing actions.
Explanation:
So this verse can be taken as either a grihastha-jnani sloka or a sanyasi-jnani sloka; in both ways one can interpret; Sankaracarya takes this verse as the description of a sanyasi-jnani. But this can be taken as a grihastha-jnani also.
While progressing in our project, we may encounter several situations, some of which we expected and some that we did not. Shri Krishna guides us on how to deal with these situations in this shloka.
By definition, karma yoga inspires us to work relentlessly. The output of our project may be sometimes favourable, and sometimes not. The follower of karma yoga knows that he is one of the many variables that determine the output of his work, and is therefore content with whatever comes his way. He does not let unfavourable outcomes impact his level of work. This is the “prasaada buddhi” that we say earlier.
While living in this world, nobody can hope to neutralize the dualities to have only positive experiences. Then how can we successfully deal with the dualities that come our way in life? The solution is to take these dualities in stride, by learning to rise above them in equipoise in all situations. This happens when we develop detachment to the fruits of our actions, concerning ourselves merely with doing our duty in life without yearning for the results. When we perform works for the pleasure of God, we see both positive and negative fruits of those works as the will of God, and joyfully accept both.
Favourable and unfavourable, success and failure, heat and cold, praise and criticism – this is duality. It arises because our mind tends to label one aspect of nature as positive, and reject the other as negative. But the follower of karma yoga knows that nothing is absolutely good or bad. It is all part of Ishvaraa and therefore remains equanimous. This is nothing but “samatva buddhi”.
Our mind has a natural tendency to compare ourselves with others like us. If it perceives us “better” than others, it generates pride. If it perceives us “inferior” to others, it generates envy. The follower of karma yoga knows that ultimately we are all part of the same higher ideal – Ishvaraa. Any envy generated in the mind only strengthens the ego. So he never lets envy distract him from his work. It is a quality that he does not encourage.
He welcomes whatever happens in life as a result of his karma; so yadrcchālābhasantuṣṭaḥ; satisfied with whatever comes to him as a result of his action; because we should remember that the events in our life are not totally controlled by us.
There are one set of people, who claim that they can decide my future; then the second extreme is the fatalistic type, who say that nothing is under my control. One takes hundred percent responsibility; another takes zero percent responsibility. Gita says both extremes are wrong. Then what is the right attitude; I am only one of the contributory factors with regard to my future. We do not have the total control, then what are the other factors which will control. All the other factors put together, we call daivam. Because the other factors are numerous to enumerate. Right from weather onwards; right from war somewhere else; everything can influence today’s condition. That means the whole world is interconnected and therefore the number of factors that will determine my future is so numerous that instead of enumerating them; we have put all the extraneous factors into one huge bag and we call it daivam; or prārabhdam or īśvara iccha, God’s will.
Whatever comes as karma phalam, it is according to the Law of the Lord that I have to accept that does not mean that we should not work for improving the situation. If the failure happens, I have to accept it because it has happened; and therefore it is choiceless. But at the same time, with regard to the next result; I have got control and therefore I can do, whatever has to be done. Therefore accept the present; work for the future; accept the present; work for the future. So worry cannot change the present; worry cannot change the future also. Present requires acceptance; future requires hard work. This is the simple philosophy of Gītā; present including past, requires acceptance; future requires hard work. Both of them do not require worry. Therefore Krishna said; aśōcyānanvaśōcastvaṁ;
According to our śāstrā, competition is not a healthy thing; even though nowadays they say competition alone brings the best out of the people, our śāstrā is not very much in favour of that; śāstrā feels that it is like drug induced power; so when a person takes certain banned drugs in olympic games etc. it is called performance enhancing drugs; but still they ban. Why should they ban?; even though it increases the performance. Side effects are not good; they are powerfully negative. The same is competition, which put us into desire of end result.
So the refrain here is that such a follower of karma yoga will continue to perform actions in this world, yet remain unattached because he never lets external situations destabilize his equanimity.
।। हिंदी समीक्षा ।।
प्रस्तुत श्लोक ज्ञान कर्म योग सन्यास का होने से सांख्य अर्थात सन्यास में भी और कर्म योगी में समान रूप से लागू होता है। इसलिए शंकराचार्य जी द्वारा सन्यासी के लिए जो व्याख्या है, वह कर्मयोगी के लिए भी है।
आदि गुरु शंकराचार्य ने इस श्लोक की व्याख्या इस प्रकार की है कि योगी पुरुष के बारे में भगवान बताते है कि जिस ने समस्त संग्रह का त्याग कर दिया है ऐसे संन्यासी के पास शरीरनिर्वाह के कारण रूप अन्नादि का संग्रह नहीं होता इसलिये उस को याचनादि द्वारा शरीर निर्वाह करने की योग्यता प्राप्त हुई। इस पर बिना याचना किये बिना संकल्प के अथवा बिना इच्छा किये प्राप्त हुए इत्यादि वचनों से जो शास्त्र में संन्यासी के शरीर निर्वाह के लिये अन्नादि की प्राप्ति के द्वार बतलाये गये हैं उन को प्रकट करते हुए कहते हैं जो बिना माँगे अपने आप मिले हुए पदार्थ से संतुष्ट है अर्थात् उसी में जिस के मन का यह भाव हो जाता है कि यही पर्याप्त है जो द्वन्द्वों से अतीत है अर्थात् शीतउष्ण आदि द्वन्द्वों से सताये जाने पर भी जिस के चित्त में विषाद नहीं होता जो ईर्ष्या से रहित अर्थात् निर्वैरबुद्धिवाला है और जो अपने आप प्राप्त हुए लाभ की सिद्धिअसिद्धि में भी सम रहता है जो ऐसा शरीर स्थिति के हेतुरूप अन्नादि के प्राप्त होने या न होने में भी हर्षशोक से रहित समदर्शी है और कर्मादि में अकर्मादि देखनेवाला यथार्थ आत्मदर्शननिष्ठ एवं शरीर स्थिति मात्र के लिये किये जाने वाले और शरीरादि द्वारा होने वाले भिक्षाटनादि कर्मों में भी मैं कुछ नहीं करता गुण ही गुणों में बर्त रहे हैं इस प्रकार सदा देखनेवाला है वह यति अपने में कर्तापन का अभाव देखने से अर्थात् आत्मा को अकर्ता समझ लेने से वास्तव में भिक्षाटनादि कुछ भी कर्म नहीं करता है। ऐसा पुरुष लोक व्यवहार की साधारण दृष्टि से तो सांसारिक पुरुषों द्वारा आरोपित किये हुए कर्तापन के कारण भिक्षाटनादि कर्मों का कर्ता होता है। परंतु शास्त्र प्रमाण आदि से उत्पन्न अपने अनुभव से ( वस्तुतः ) वह अकर्ता ही रहता है। इस प्रकार दूसरों द्वारा जिस पर कर्तापन का अध्यारोप किया गया है ऐसा वह पुरुष शरीर निर्वाह मात्र के लिये किये जाने वाले भिक्षाटनादि कर्मों को करता हुआ भी नहीं बँधता क्योंकि ज्ञानरूप अग्निद्वारा उस के ( समस्त ) बन्धनकारक कर्म हेतुसहित भस्म हो चुके हैं।
गीता में सन्यास भाव से की गई आदि गुरु शंकराचार्य द्वारा यह व्याख्या योगी को कर्म करने से भी रोकने जैसी लगती है क्योंकि जब योगी पुरुष का देह से संबंध नही रहता तो वो मात्र जीवन निर्वाह हेतु ही कर्म करता है। किंतु योगी पुरुष के लक्षण भगवान ने कर्मयोगी के लिए अन्य प्रकार से ही बताए है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं को अव्यक्त ब्रह्म के सृष्टि यज्ञ चक्र के लिए निरंतर कर्म करते हुए बताया है, अपने जीवन मे कर्म के सभी साधनों को उपयोग में लिया है वो द्वारकाधीश भी बने । राजा जनक, इक्षवाकु, मनु, सूर्य आदि अनेक कर्मयोगियों का जीवन हमारे समक्ष उदाहरण के लिये प्रस्तुत है। अतः हम कह सकते है कर्म योगी संतुष्ट होता है, उसे कोई लालसा एवम अहम बांध नही सकता। वो अपने लिए भविष्य हेतु कुछ भी संग्रह नही करता और जो भी मिल जाये उस के लिये पर्याप्त है। उस के कार्य लोक संग्रह के लिए होते है इसलिये उस को कोई भी कर्म बंधन नही लगता और कार्य कारण के नियमानुसार भी उसे उस के कर्म का कोई फल नही बाँधता। उस का अहम एवम मोह उस की ज्ञानाग्नि के समक्ष भस्म हो चुके होते है। अतः किसी भी कर्म की सफलता, असफलता, प्रसिद्धि या बदनामी, दुख, तकलीफ हानि लाभ कुछ भी उस को प्रभावित नही करते। वो कर्म करते हुए भी निःद्वन्द भाव से कर्म करता है। इसलिये उस के कर्म उस को बांधते नहीं है।
कर्मयोगी की तरह इस श्लोक की व्याख्या में यही सिद्ध है कि कर्म की निपुर्णता और कठिन परिश्रम से उसे लक्ष्य तक पहुंचाने का तो अधिकार किसी भी जीव को है, किंतु उस के सफल या असफल होने का या परिणाम जीव के हाथ में नही है। समय, स्थान और साधन हर समय एक समान नही होते, इसलिए किसी कार्य के परिणाम में अनेक प्राकृतिक और अन्य जीवों के संयुक्त क्रियाओं का समावेश होता है। इन्हे सामूहिक तौर पर दैवीय गुण या अधिदेव कह सकते है।
फिर यदि पूर्ण योग्यता, कर्मठता, लग्न और आलस्य त्याग कर यदि कोई कार्य करना ही कर्मयोगी का कर्तव्य कर्म है, जो परिणाम प्राप्त हो, वह प्रसाद के समान स्वीकार करना ही कर्मयोग है। कर्मयोगी निष्काम भाव से लोकसंग्रह के लिए कार्य प्रकृति का एक भाग हो कर करता है, उस में उस की कोई कामना, आसक्ति, मोह, लोभ आदि कुछ नही होता। यदि कार्य लक्ष्य के अनुसार परिणाम न दे तो उस का कार्य अपने कर्म को और अधिक परिश्रम, लग्न, योग्यता और एकनिष्ठ को करना चाहिए। अर्जुन को युद्ध करने के यदि प्रकृति ने निमित्त बनाया है तो उसे युद्ध जीतने के अपने पूर्ण कौशल से करना ही ज्ञान कर्म योग सन्यास है जिस का परिणाम जो भी परमात्मा द्वारा प्राप्त हो, उसे हरि इच्छा मान कर आगे बढ़ना है।
अहंकार से परे आत्मस्वरूप में स्थित पुरुष इच्छा तथा फलासक्ति से प्रेरित होकर कर्म नहीं करता। कर्मों को करने से प्राप्त फल से ही वह सन्तुष्ट रहता है। अहंकाररहित अवस्था का अर्थ है अन्तकरण पर पूर्ण संयम। स्वभाविक ही शीतउष्ण सिद्धिअसिद्धि सुखदुख इत्यादि द्वन्द्वात्मक अनुभव उसे व्यथित नहीं कर सकते क्योंकि वे सब मन की बाह्यजगत् के साथ होने वाली प्रतिक्रियायें मात्र हैं।मन के प्रभावहीन होने पर बुद्धि अपने पूर्वाग्रह ईर्ष्या और मत्सर आदि से ज्ञानी पुरुष को प्रभावित नहीं कर सकती। सामान्यत सिद्धि में हमें हर्षातिरेक और असिद्धि में अत्यन्त विषाद होता है। परन्तु जब अविद्याजनित अहंकार पूर्णरूप से दैवी स्वरूप को प्राप्त हो जाता है तब वह पुरुष सफलता और असफलता में समान भाव से स्थित रहता है। ऐसा ज्ञानी पुरुष कर्म करके भी कर्मफलों से नहीं बंधता।जब आत्मज्ञानी पुरुष हमारे मध्य रहता हुआ कर्म करता है तब उसका व्यवहार सामान्य जनों के समान ही प्रतीत होता है तथापि उसके कर्मों में एक विशेष शक्ति और प्रभाव दिखाई पड़ता है जो उसे कर्मक्षेत्र में सामान्य से कहीं अधिक सफलता प्रदान करता है।
भगवान राम से ले कर कृष्ण राजा रहे, जनक ने राज्य का संचालन किया। अतः संतुष्टि जो आत्मा से प्राप्त है, यहाँ उस का आशय भी यही है, योगी पुरुष किसी भी आशा, कामना , भोक्तत्व, कर्तृत्त्व भाव से कर्म न करते हुए, लोकसंग्रह के लिये कर्म करता है। वह लोकसंग्रह के कार्य हेतु प्रकृति द्वारा प्रदत्त सभी साधनों का उपयोग और उपभोग भी अपने लक्ष्य की प्राप्ति हेतु करता है, किंतु साधन या सुविधा के होने या न होने पर भी, उसे कुछ न करने या न करने का भी सुख – दुख नही होता। दुःख कामनाओ को जन्म देने वाला है क्योंकि दुखी मनुष्य में दुःख से कुछ न कर पाने की कामना या मलाल उसे योगी बनने से रोक देता है। दुःख में मनुष्य ईर्ष्या, घृणा, बदला लेने की भावना आदि भी तामसी गुण पाल लेता है। अतः योगी पुरुष न दुखी होता है और न ही सुखी होता है, वह अपने कर्म को परब्रह्म के दिव्य कर्म समझ कर करता रहता है। उस के कर्म सांसारिक लोग सदाहरण समझते है, किन्तु उस को इस कि कोई परवाह नही होती। सत्व गुण प्रधान होने से निठल्ले या आलस्य के तमो गुण के परे, वह कर्म परमात्मा को समर्पित भाव से कर्तव्य समझ कर करता है।
स्वामी राम कृष्ण परमहंस भी इसी प्रकार के योगी पुरूष थे जिस का चरित्र यदि कोई पढ़े का तो दिव्य कर्म वाला युग पुरुष कैसा होता है, जान सकता है।
तीसरे अध्याय के नवें श्लोक के पूर्वार्ध में भगवान् ने व्यतिरेक रीति से कहा था कि यज्ञ से अतिरिक्त कर्म मनुष्य को बाँधते हैं। अब तेईसवें श्लोक के उत्तरार्ध में उसी बात को अन्वय रीति से कहते हैं। जिसे हम आगे पढ़ेंगे।
।। हरि ॐ तत सत।। 4.22।।
Complied by: CA R K Ganeriwala ( +91 9422310075)