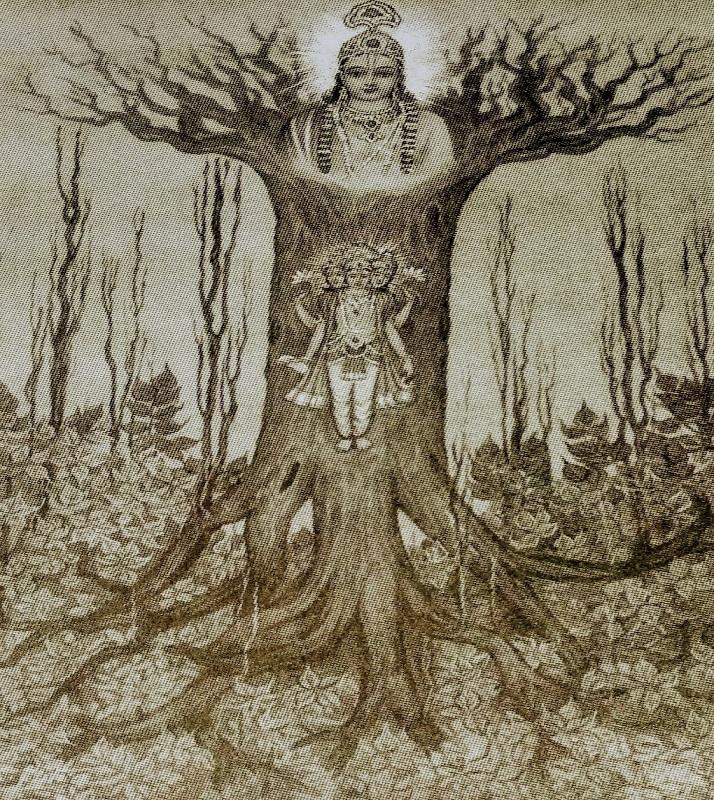।। Shrimadbhagwad Geeta ।। A Practical Approach ।।
।। श्रीमद्भगवत गीता ।। एक व्यवहारिक सोच ।।
।। Chapter 04.19।।
।। अध्याय 04.19 ।।
॥ श्रीमद्भगवद्गीता ॥ 4.19॥
यस्य सर्वे समारम्भाः कामसंकल्पवर्जिताः ।
ज्ञानाग्निदग्धकर्माणं तमाहुः पंडितं बुधाः ॥
“yasya sarve samārambhāḥ,
kāma-sańkalpa-varjitāḥ..।
jñānāgni-dagdha-karmāṇaḿ,
tam āhuḥ paṇḍitaḿ budhāḥ”..।।
भावार्थ :
जिस मनुष्य के निश्चय किये हुए सभी कार्य बिना फ़ल की इच्छा के पूरी लगन से सम्पन्न होते हैं तथा जिसके सभी कर्म ज्ञान-रूपी अग्नि में भस्म हो गए हैं, बुद्धिमान लोग उस महापुरुष को पूर्ण-ज्ञानी कहते हैं। (१९)
Meaning:
One who begins all actions devoid of desire and resolve, and whose actions have been burnt in the fire of knowledge, he is called a sage (even) by the wise.
Explanation:
In the following six shlokas, Shri Krishna gives us extremely practical guidelines to fully internalize the message of this chapter, which is that only by renouncing the sense of doer ship and enjoyers hip can one achieve detachment from action. They are simple, clear, actionable messages.
when the soul is illumined with divine knowledge, it realizes that the bliss it seeks will be attained not from the objects of the senses, but in loving service to God. It then strives to perform every action for the pleasure of God. “Whatever you do, whatever you eat, whatever you offer as oblation to the sacred fire, whatever you bestow as a gift, and whatever austerities you perform, O son of Kunti, do them as an offering to me.” (Bhagavad Gita 9.27) Since such an enlightened soul renounces selfish actions for material pleasures and dedicates all actions to God, the works performed produce no karmic reactions. They are said to be burnt in the fire of divine knowledge.
In fact, the true service comes, true work comes out only when there is fullness; and a person’s contribution with fullness will be immensely greater because he does not have any axe to grind; because otherwise whatever activity I take, there will be a tinge of selfishness. Because I want to get something out of it; but Krishna says, a jñāni alone can contribute with contentment and now the question is: if jñāni has contentment, then what will be the driving force; our scriptures say then the driving force will be purely of compassion; the greatness of wisdom is: the more a person becomes wiser, the more he identifies with the whole world; ignorance makes my mind smaller, selfish, bothered about me and my family; but in the case of a jñāni, because of universal identification, there is universal compassion; which is his nature. He does not show compassion; but compassion becomes his nature; just as a mother has got an instinctive love for the child; just as the tiger loves the baby; anybody comes around, it attacks; it is not born out of will; it is nature-driven.
Imagine that we are about to undertake on a new project that is part of our field of work, our svadharma. It could be a presentation at work, a new job, moving to a new city and so on. At each step of the project, our mind entertains different questions. We can use this series of shlokas as a guide throughout the project.
Initially, our mind is fully focused on executing the project in the spirit of karma yoga. But after a while, it will get distracted and tend to wander towards material objects. This distraction will eventually lead to lack of efficiency in our project. Shri Krishna addresses how to deal with this aspect of the mind.
The common meaning of the word “sankalpa” is decision or resolve. Let’s examine the deeper meaning. Whenever we think about an object, there is a constant labelling going on in our mind on whether the object is “good” or “bad”. After having gone back and forth, we label something as “good”. This labelling is called sankalpa.
Why does this labelling happen? It is because our intellect has been superseded by our mind and senses. For example, a bitter medicine may benefit the body holistically. The intellect knows this. But the sense of taste will not like it. Furthermore, this sankalpa or labelling gives rise to kaama, or desire for that object. And herein lies the seed of selfish action that distracts us from the goal. Sankalpa and kaama are interrelated, any one of them indicates the present of the other, but both give rise to selfish action.
Therefore, Shri Krishna urges us to “burn” our selfish actions with the fire of knowledge. In other words, he wants our intellect to guide us in our svadharma, and stop the mind from labelling objects as good or bad. If something comes to us as part of our svadharma, we must accept it with prasaada buddhi. Like the lotus that remains in the pond and is untouched by the water, we must continually remind ourselves that our eternal essence is different and separate from all actions. Actions are going on by themselves in nature. Therefore, we should remain alert at all times, and should reinstate the supremacy of the intellect over the senses whenever the senses move towards external objects.
That is what Dayanand Svāmi beautifully says: I have rejected myself and when I cannot accept myself, I cannot accept the world also; I find fault with every person, every job, every set up, every house, and whatever it is; the problem is not with the world, self-rejection expresses in the form of world rejection. And self-acceptance, expresses in the form of world acceptance. Again Swamiji beautifully says: a jñāni is at home with himself as he is and therefore at home with the world as it is and therefore no more dreaming and projections; he lives in the present day and I am fine as I am; and I enjoy doing whatever I can do, and whatever I have to do. Therefore he does not travel from unhappiness to happiness; therefore his travel is from happiness to happiness to happiness only. What a beautiful state of mind; so happily he succeeds; happily he fails also; happily he gets things done; and happily he is not able to get things done also.
।। हिंदी समीक्षा ।।
पिछले अध्यायों में हम ने पढ़ा कि किसी भी कार्य शक्ति के पीछे कामना एवम संकल्प शक्ति रहती है जिस से हम प्रेरित हो कर कार्य करने लगते है। इस संकल्प शक्ति के साथ अहम की इस कार्य को मै कर रहा हूँ एवम लालसा यानि मोह की इस से मुझे यह फायदा होगा जुड़ा रहता है और यही कर्म है। यदि यह कार्य बिना लालसा या मोह एवम अहम के साथ किया जाए तो इस को लोक संग्रह यानि जन हित के लिए किया कार्य मानेगे। और यदि यह कार्य बिना संकल्प एवम कामना के साथ किया जाए तो इसे अकर्म मानेगे।
इसे हम इस प्रकार भी कह सकते है कि विषयों का बारबार चिन्तन होने से उन की बार बार याद आने से उन विषयों में ये विषय अच्छे हैं काम में आने वाले हैं, जीवन में उपयोगी हैं और सुख देनेवाले हैं ऐसी सम्यग्बुद्धि का होना संकल्प है और ये विषय पदार्थ हमारे लिये अच्छे नहीं हैं हानिकारक हैं ऐसी बुद्धि का होना विकल्प है। ऐसे संकल्प और विकल्प बुद्धि में होते रहते हैं। जब विकल्प मिट कर केवल एक संकल्प रह जाता है तब ये विषय पदार्थ हमें मिलने चाहिये ये हमारे होने चाहिये इस तरह अन्तःकरण में उन को प्राप्त करने की जो इच्छा पैदा हो जाती है उस का नाम काम (कामना) है। कर्मयोग से सिद्ध हुए महापुरुष में संकल्प और कामना दोनों ही नहीं रहते अर्थात् उस में न तो कामनाओं का कारण संकल्प रहता है और न संकल्पों का कार्य कामना ही रहती है। अतः उस के द्वारा जो भी कर्म होते हैं वे सब संकल्प और कामना से रहित होते हैं। संकल्प और कामना ये दोनों कर्म के बीज हैं। संकल्प और कामना न रहने पर कर्म अकर्म हो जाते हैं
अतः जब व्यक्ति कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म को प्राप्त कर लेता है तो उस के अहम, मोह, कामना एवम संकल्प कुछ भी नही रहता, तब उस का चेतन अपने आत्म स्वरूप आत्मा से एकाकार होने लगता है। इस प्रकार का व्यक्ति कर्म करते हुए भी कार्य कारण के सिंद्धान्त के अनुसार किसी भी बंधन से मुक्त होता है, उस का प्रकृति जन्य शरीर, मन, बुद्धि प्रकृति के त्रियामी गुणों से कार्य करते है किंतु वो साक्षी भाव से सभी कार्यो को होते हुए देखता है। अनेक महापुरुष जनक इत्यादि एवम वेदों के रचयिता ऋषि मुनि जन संग्रह के लिए कार्य करते गए किन्तु उन को इस संसार मे कोई नही जानता और क्योंकि वो संकल्प एवम कामना रहित हो कर कार्य कर रहे थे इसलिए उन्हें कोई जाने यह लालसा भी नही थी। ऐसे की अनेक ज्ञानी पंडित इस संसार मे लोकसंग्रह के कार्य कर रहे है जिन्हें इस प्रकृति के अतिरिक्त कोई नही जानता।यह लोग आत्मा को साक्षी मान कर लोकसंग्रह के करते है अतः भगवान के दिव्य कर्म के अनुसार ही कार्य करते हुए मोक्ष को प्राप्त होते है। वेदव्यास जी ने सभी वेदों को लिपिबद्ध किया, 12 पुराणों की रचना की आदि किंतु उन का संकल्प, मोह, लालसा आदि कुछ नही था।
अकर्म एवम संकल्प के लिये विवेकशील बुद्धि की आवश्यकता है। कर्म एवम अकर्म का ज्ञान भी विवेकशील बुद्धि से होता है। आसक्ति एवम निष्काम भी विवेकशील बुद्धि से होता है। यह विवेकशील बुद्धि का अर्थ ही वह बुद्धि जो किसी कामना, आसक्ति या पूर्वाग्रह से ग्रसित न हो। गीता किसी धर्म विशेष का ग्रंथ भी इसलिये है कि यह व्यक्तित्व विकास के लिये किसी भी धार्मिक मान्यता में बंध कर कार्य करने को नही कहती। अन्य धर्म ईसाई या मुस्लिम धर्म मे बुद्धि को उन के ग्रन्थ में लिखी मान्यताओं पर चल कर मोक्ष का मार्ग बताती है, गीता वही मार्ग निष्काम भाव से, आसक्ति रहित बुद्धि से प्राप्त करने को कहती है जिस से किसी भी कर्म को करने से पहले उस का ज्ञान होना चाहिए कि यह कर्म बन्धन कारक है या नही, लोकसंग्रह का कर्म है या नही। इस कर्म को करने का संकल्प में कोई अहम, आसक्ति या कामना है या नही। जीव को अपना यथार्थ स्वरूप का ज्ञान होने के मुक्त वातावरण चाहिए, यदि वह किसी भी नियम, कर्मकांड, पद्धिति, मोह या विचारधारा के बन्धन में है तो उस का संकल्प भी उसी विचारधारा के बन्धन में होगा। साक्षी, अकर्ता, नित्य एवम दृष्टा स्वरूप जब भी कर्म के लिये अवतरित होता है तो वह जो भी संकल्प करता है, जो भी कर्म करता है, वह सब अकर्म ही होते है। क्योंकि उस मे उस की कोई कामना, अहम या आसक्ति नही होती, वह कर्म प्रकृति द्वारा लोकसंग्रह हेतु किया जाता है।
अतः भगवान श्री कृष्ण कहते है कर्म में प्रवृति हेतु काम यानि इच्छा व संकल्प ही है और काम व संकल्प का मूल परिच्छिन्न अहंकार है। अज्ञान के प्रभाव से पुरुष जब अपने आप को अपने वास्तविक आत्मस्वरूप से भिन्न कुछ कल्पना करता है, तभी काम उत्पन्न होता है और काम से संकल्प बनता है। परंतु जब ज्ञानाग्नि प्रज्ज्वलित हो कर अज्ञान को भस्म कर देती है और ‘सर्व मैं ही हूँ’ इस ज्ञान की प्रौढ़ता से अहंता का आसन परिच्छिन्न अहंकार से उखड़ कर सर्व साक्षी अपने आत्मा में जम जाता है, तब वह सम्पूर्ण कार्य कारण की एक मात्र सत्ता अपने आत्मा को ही देखता है और तब अज्ञान कर के प्रतीयमान अहंकार रूप कर्ता काम व संकल्परूप निमित तथा कर्म रूप कार्य ये सभी त्रिपुट श्रृंखला शिथिल हो जाती है। फिर तो क्या कर्ता, क्या निमित्त और क्या कर्म सभी की अधिष्ठानरूप वह अपने आत्मा को ही देखता है। इस प्रकार जिस के कर्म ज्ञानाग्नि से भस्म हो कर संकल्पवर्जित हो रहे हो, उसी को ज्ञानी जन पंडित कहते है।
हमे याद रहे कि कुछ लोग कहते है कि कृष्ण अपनो से युद्ध करने के अर्जुन को उसका रहे है। किंतु यदि हम ज्ञान कर्म सन्यास को समझ सके तो हमे यह ज्ञात होना चाहिए कि क्रियाएं प्रकृति करती है और निमित्त किसी योग्य जीव को बनाती है। अर्जुन योद्धा और अनुसुय होने योग्य था। अतः युद्ध का चुनाव उस का नही है, क्षत्रिय होने से युद्ध में युद्ध करना उस का कर्तव्य कर्म है जो उसे संकल्प रहित, मोह, लालसा आदि को छोड़ कर ज्ञानी की भांति करना है। यही सृष्टि यज्ञ चक्र है किंतु क्या हम जब भी किसी कार्य के लिए निमित्त होते है तो हम संकल्प, मोह और कामना के बिना कार्य कर पाते है? क्योंकि जो ऐसा करते है उन्हे ही ज्ञानी कहा गया है और मैं हनुमान प्रसाद पोद्दार जी को इसी स्वरूप में आदर्श मानता हूं।उन के जैसे और भी होंगे, उन्हें प्रणाम भी करता हूं।
।। हरि ॐ तत सत।। 4.19।।
Complied by: CA R K Ganeriwala ( +91 9422310075)