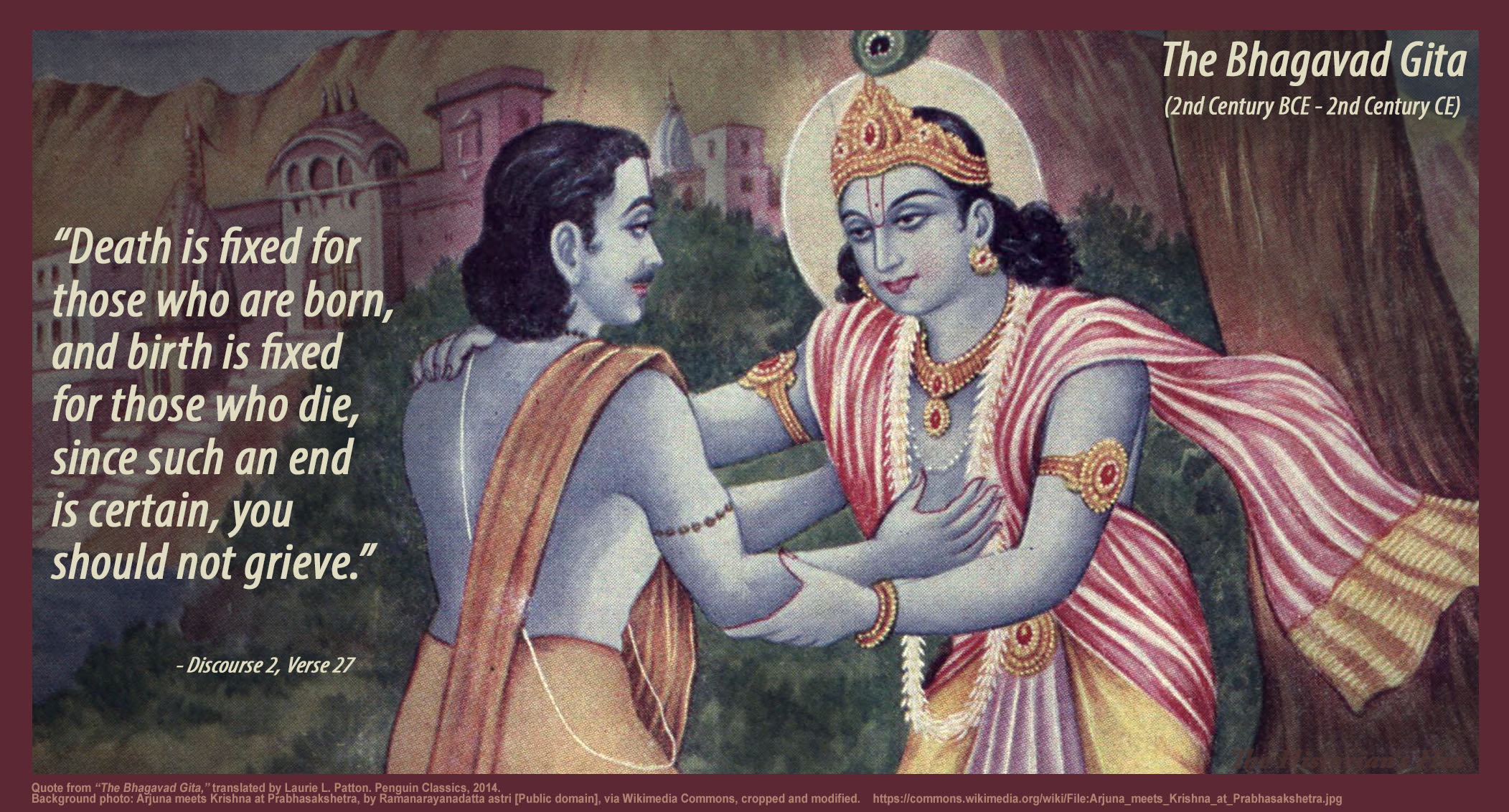।। Shrimadbhagwad Geeta ।। A Practical Approach ।।
।। श्रीमद्भगवत गीता ।। एक व्यवहारिक सोच ।।
।। Chapter 04.14।।
।। अध्याय 04.14 ।।
॥ श्रीमद्भगवद्गीता ॥ 4.14॥
न मां कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्मफले स्पृहा ।
इति मां योऽभिजानाति कर्मभिर्न स बध्यते ॥
“na māḿ karmāṇi limpanti,
na me karma-phale spṛhā..।
iti māḿ yo ‘bhijānāti,
karmabhir na sa badhyate”..।।
भावार्थ :
कर्म के फल में मेरी आसक्ति न होने के कारण कर्म मेरे लिये बन्धन उत्पन्न नहीं कर पाते हैं, इस प्रकार से जो मुझे जान लेता है, उस मनुष्य के कर्म भी उसके लिये कभी बन्धन उत्पन्न नही करते हैं। (१४)
Meaning:
Actions do not stain me, nor do I covet fruits of action. One who knows me in this manner is never bound by actions.
Explanation:
So far, Shri Krishna clarified and elaborated upon key topics within karmayoga. First he gave the paramparaa or tradition of the teaching. He then revealed his nature as Ishvaraa, and explained the method by which he manifests as an avataara. Finally, he explained how he responds in the exact manner that one approaches him.
Krishna says that karma cannot disturb me. Not only karma cannot disturb me; karma phalam also cannot disturb me; karma also can give tension; and karma phalam can give regrets or disappointments; so both are not there for me; therefore Krishna says: karmas do not affect me; by creating tension; anxiety. And not only that; I do not have even the concern over the results of action. So I am not concerned about the result of action; because every action is going to create an appropriate result; and the Lord will never do any injustice to me, because as they say: I always get what I deserve; never what I desire. Therefore Lord is always just and therefore whatever has to happen according to karma, it will happen; therefore I am not concerned about the result.
As we get further into karmayoga, we slowly begin to lost our attachment to the fruits of our action, which is the first stage in karmayoga. In this chapter, Shri Krishna urges us to move to the next stage in this journey where we begin to lose the notion of doership.To highlight this point, Shri Krishna says that as Ishvaraa, even he knows that actions are happening in prakriti, and therefore he is not the doer of those actions, but he is beyond all action. He puts this poetically by saying that actions do not “stain” him.
Why is Ishvara beyond all action? At its core, any action happens when there is an imbalance or vacuum. Wind travels from high pressure areas to low pressure areas. Electric current moves when there is a difference in voltage. The mind creates a thought because of our vaasanaas. But Ishvara is all-complete and self-sufficient. Therefore, he does not need to act. He is only a witness.
Pure personalities are never tainted by defects even in contact with impure situations and entities, like the sun, the fire, and the Ganges.” The sun does not get tainted if sunlight falls on a puddle of urine. The sun retains its purity, while also purifying the dirty puddle. Similarly, if we offer impure objects into the fire, it still retains its purity—the fire is pure, and whatever we pour into it also gets purified. In the same manner, numerous gutters of rainwater merge into the holy Ganges, but this does not make the Ganges a gutter—the Ganges is pure and in transforms all those dirty gutters into the holy Ganges. Similarly, since actions are performed by prakriti, there is no impact to Ishvaraa. Shri Krishna reminds us that just like he knows that he is not the doer or enjoyer of actions, so should we have the exact same conviction.
Activities bind one in karmic reactions when they are performed with the mentality of enjoying the results. However, God’s actions are not motivated by selfishness; his every act is driven by compassion for the souls. Therefore, although he administers the world directly or indirectly, and engages in all kinds of activities in the process, he is never tainted by any reactions. Lord Krishna states here that he is transcendental to the fruitive reactions of work.
Material activities never taint the devotees of God who are fully satisfied in serving the dust of his lotus feet. Nor do material activities taint those wise sages who have freed themselves from the bondage of fruitive reactions by the power of Yog. So where is the question of bondage for the Lord himself who assumes his transcendental form according to his own sweet will?”
So here incidentally we have to note, planning for the result is one thing; worrying over the result is another. Vedanta is never against planning; planning is extremely important; without planning you cannot do anything. Planning leads to efficiency, worrying leads to deficiency.
।। हिंदी समीक्षा ।।
नित्य शुद्ध और परिपूर्ण आत्मा को किसी प्रकार की अपूर्णता का भान नहीं हो सकता जो किसी इच्छा को जन्म दे। इस दृष्टि से श्रीकृष्ण भगवान् कहते हैं कर्म मुझे दूषित नहीं कर सकते और न मुझे कर्मफल में कोई आसक्ति ही है। इच्छा अथवा कर्म का बन्धन जीव अहंकार के लिये ही हो सकता है। मन और बुद्धि की उपाधियों से युक्त चैतन्य आत्मा ही जीव कहा जाता है। इन उपाधियों के दोषयुक्त होने पर जीव ही दूषित हुआ समझा जाता है। इसे एक दृष्टान्त के द्वारा हम भली भांति समझ सकेंगे। यदि किसी पात्र में रखे जल में सूर्य प्रतिबिम्वित होता है तो उस प्रतिबिम्ब की स्थिति पूर्णतया उस जल की स्थिति पर निर्भर करती है। जल के शान्त अस्थिर अथवा मैले होने पर वह प्रतिबिम्ब भी स्थिर क्षुब्ध अथवा धुंधला दिखाई देगा। परन्तु महाकाश स्थित वास्तविक सूर्य पर इस चंचलता अथवा निश्चलता का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसी प्रकार इच्छा आसक्ति आदि का प्रभाव अहंकार पर ही पड़ता है। नित्य मुक्त चैतन्य स्वरूप आत्मा इन सबसे किसी प्रकार भी दूषित नहीं होती।
भगवान् के कर्म तो दिव्य हैं मनुष्य भी अपने कर्मों को दिव्य बना सकता है। जब कर्मों में मलिनता (कामना ममता आसक्ति आदि) होती है तब वे कर्म बाँधनेवाले हो जाते हैं। जब मलिनता के दूर हो जाने पर कर्म दिव्य हो जाते हैं तब वे उसे नहीं बाँधते। इतना ही नहीं वे कर्म उस कर्ता को और दूसरों को भी (उसके अनुसार आचरण करनेसे) मुक्त करनेवाले हो जाते हैं। अपने कर्मों को दिव्य बनाने का सरल उपाय है संसार से मिली हुई वस्तुओं को अपनी और अपने लिये न मानकर (संसार की और संसार के लिये मानते हुए) संसार की सेवा में लगा देना। विचार करना चाहिये कि हमारे पास शरीर आदि जितनी भी बाह्य वस्तुएँ हैं उन सब को हम साथ लाये नहीं और जायँगे तब साथ ले जा सकते नहीं उनके रहते हुए उनमें इच्छानुसार परिवर्तन कर सकते नहीं उन्हें इच्छानुसार रख सकते नहीं अर्थात् उनपर हमारा कोई आधिपत्य नहीं है। इसी प्रकार जन्म जन्मान्तरों से साथ आये सूक्ष्म और कारण शरीर भी परिवर्तनशील और प्रकृति के कार्य हैं इसलिये उन के साथ भी हमारा सम्बन्ध नहीं है। वे वस्तुएँ अपने लिये भी नहीं हैं।
यहाँ सूक्ष्म बात यह है परमात्मा के दिव्य कर्म को जो जानता है, का अर्थ यही है कि यह उस के व्यवहार एवम नित्य कर्म में शामिल हो। यदि हम किसी ज्ञान को आधार मान कर कर्म करते है तो हम में अहम या कर्ता भाव बना रहता है जो हमे बताता है कि हम अनासक्त है। किंतु जो अनासक्त है वह कभी ही कह सकता की वह अनासक्त है क्योंकि उस मे कर्ता भाव ही नही है। वह दिव्य कर्म को बर्तता ही है। इसलिये उस के कर्म बंधन कारक नही होते।
इसे अन्य उदाहरण से समझे कि आकाश में सभी रचनाये होती रहती है किंतु आकाश कहीं भी लिप्यमान नही होता। अनासक्ति एवम अहमत्याग का भाव दोनो का समावेश होने से ही कर्म दिव्य हो जाते है।
अन्य उदाहरण ले कि कोई सोने का हार आप को दे किन्तु इस मे आप की कोई रुचि नही है किन्तु बात का ज्ञान या भाव है कि मेरी सोने के हार में रुचि नही है तो भी यह रुचि या आसक्त भाव बंधन कारक है। क्योंकि आप की आसक्ति उस के त्याग से जुड़ी है।
किसी कार्य को करने के लिए कर्ता और उस के फल की आसक्ति होने से कर्ता को कर्म का बंधन है। किंतु कोई भी क्रिया योजनाबद्ध तरीके से उत्तम तकनीकी से किया जाए तो इसे आसक्ति नही कहेंगे। यह सत्व गुण की पहचान है। इसलिए कर्ता भाव न रखना या उस कर्म के फल के प्रति आसक्ति न रखने का यह अर्थ कदापि नहीं हो सकता कि कर्म के प्रति भी उदासीनता हो जाए। कर्तव्य कर्म को उत्तम प्रकार से करना कर्मयोग है जिस से हम अपेक्षित परिणाम को प्राप्त कर सके। अर्जुन को युद्ध कर्तव्य कर्म करने के लिए कहा गया था, अर्जुन का चुनाव प्रकृति ने इसलिए किया था कि वह एक अनुसूय, श्रेष्ठ योद्धा और कर्मशक्ति की ऊर्जा से भरा हुआ था। युद्ध उसे जीतने के लिए ही करना है किंतु उस के परिणाम की उसे कोई चिंता भी नही होनी चाहिए और श्रेय की लालसा भी नही होनी चाहिए। इसलिए कर्म के प्रति आसक्ति भाव का त्याग और कर्ता भाव का त्याग सूर्य की भांति हो, जो नित्य संसार में जीवन का संचार करने उदय होता है।
सृष्टिरचना में भगवान् का कुछ भी व्यय नहीं होता। वे ज्यों के त्यों ही रहते हैं। इसलिये उन्हें अव्ययम कहा गया है।जीव भी भगवान् का अंश होने से अव्यय ही है। विचार करें कि शरीरादि सब वस्तुएँ संसार की हैं और संसार से ही मिली हैं। अतः उन्हें संसार की ही सेवा में लगा देने से अपना क्या व्यय हुआ हम तो (स्वरूपतः) अव्यय ही रहे। इसलिये यदि साधक शरीर इन्द्रियाँ मन बुद्धि धन सम्पत्ति आदि मिले हुए सांसारिक पदार्थों को अपना और अपने लिये न माने तो फिर उसे अपनी अव्ययता का अनुभव हो जायगा। कर्म करते हुए भी कर्म कर्मसामग्री और कर्मफल से अपना कोई सम्बन्ध न रहना ही कर्मों की दिव्यता है। उत्पत्ति विनाशशील वस्तु मात्र कर्मफल है। भगवान् कहते हैं कि जैसे मेरी कर्मफल में स्पृहा नहीं है ऐसे ही तुम्हारी भी कर्मफलमें स्पृहा नहीं होनी चाहिये।
फलेच्छा का त्याग करके केवल दूसरोंके लिये कर्म करने से कर्तृत्व और भोक्तृत्व दोनों ही नहीं रहते। कर्तृत्व भोक्तृत्व ही संसार है। अतः इनके न रहने से मुक्ति स्वतःसिद्ध ही है।
पूर्वश्लोक में अपना उदाहरण देकर अब आगे के श्लोक में भगवान् मुमुक्षु पुरुषों का उदाहरण देते हुए अर्जुन को निष्काम भावपूर्वक अपना कर्तव्य कर्म करने की आज्ञा देते हैं।
।। हरि ॐ तत सत ।। 4.14।।
Complied by: CA R K Ganeriwala ( +91 9422310075)