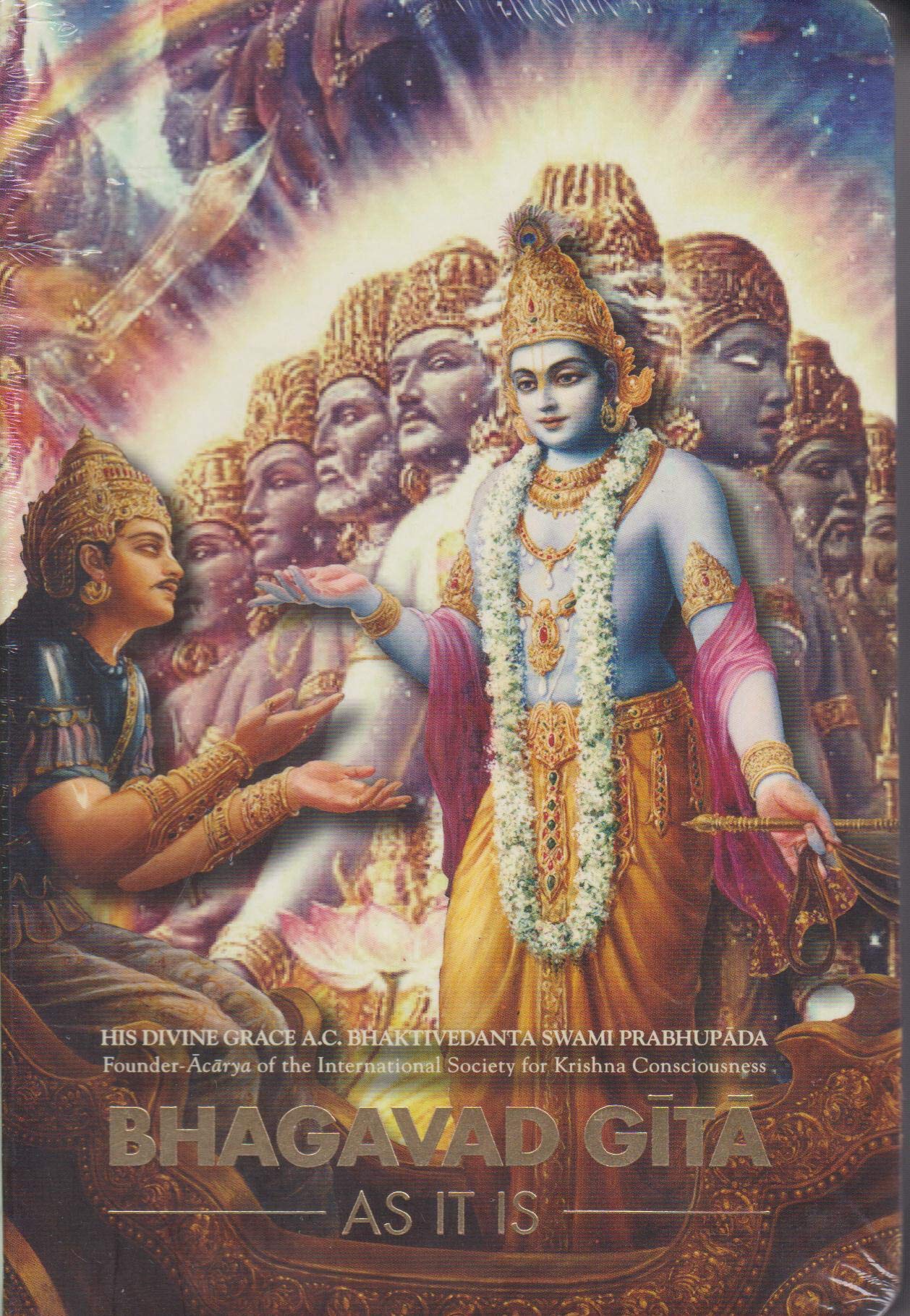।। Shrimadbhagwad Geeta ।। A Practical Approach ।।
।। श्रीमद्भगवत गीता ।। एक व्यवहारिक सोच ।।
।। Chapter 03.25।।
।। अध्याय 03.25 ।।
॥ श्रीमद्भगवद्गीता ॥ 3.25॥
सक्ताः कर्मण्यविद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत ।
कुर्याद्विद्वांस्तथासक्तश्चिकीर्षुर्लोकसंग्रह॥
“saktāḥ karmaṇy avidvāḿso,
yathā kurvanti bhārata..।
kuryād vidvāḿs tathāsaktaś,
cikīrṣur loka-sańgraham”..।।
भावार्थ :
हे भरतवंशी! जिस प्रकार अज्ञानी मनुष्य फ़ल की इच्छा से कार्य (सकाम-कर्म) करते हैं, उसी प्रकार विद्वान मनुष्य को फ़ल की इच्छा के बिना संसार के कल्याण के लिये कार्य करना चाहिये ॥ २५॥
Meaning:
Just as an ignorant individual performs action with attachment, O Bhaarata, so does a wise person perform action without attachment, wishing for the welfare of society.
Explanation:
Here, Shri Krishna offers a guideline for Arjuna in regards to working with other people. He says that one who is working with the attitude of karmayoga should learn to work in harmony with others who may have not yet understood or learned that technique. In other words, Shri Krishna warns us from adopting a “holier-than-thou” attitude with others when performing action.
Also, in this verse the expression saktaḥ avidvansaḥ has been used for people who are as yet in bodily consciousness, and hence attached to worldly pleasures, but who have full faith in the Vedic rituals sanctioned by the scriptures. They are called ignorant because though they have bookish knowledge of the scriptures, they do not comprehend the final goal of God-realization. Such ignorant people perform their duty scrupulously according to the ordinance of the scriptures, without indolence or doubt.They are called ignorant because though they have bookish knowledge of the scriptures, they do not comprehend the final goal of God-realization.
So Krishna has pointed out that an ignorant person, As Ajnani does karma; a jnani also should do karma; only the purpose is different; ajnani does karma to get purity, knowledge and liberation; in stages; that is the route that is visualised by him; when jnani performs karma, it is not for purity, knowledge or liberation, because jnani has got all the three; his aim is what? Educating the society with regard to proper living; serving as a model; but both should do karma.
Now a person may like to know, if both of them are performing karma, what will be the difference in their attitude? The attitudinal difference between jnani’s karma and ajnani’s karma; and what is difference? Krishna says: when Ajnani is doing karma, ajnani has not attained liberation; he is not happy with himself; bondage means self-insufficiency; self-incompleteness; self-dissatisfaction; not being at home with myself. And naturally, he wants to discover fullness and happiness; therefore he performs action for happiness; Whereas when a jñāni performs action, he is not doing with a sense of incompleteness, because jñāni by definition is one who has jñānam.
When we say jñānan in Vēdāntic context, the jñānam is my nature is fullness; my nature is security; my nature is peace. Whatever I am seeking in life, all those are my intrinsic nature. “aham pūrṇaḥ asmi; aham amṛtahaḥ asmi;” I do not require any external support to fulfill me; to complete me; it is with the sense of fullness that jñāni performs action; and therefore he does not do action for happiness but he does action with happiness; therefore the difference is only in the preposition; that is the only difference. In one, for, in the other, with; when I do for happiness, I am Mr. Samsari. If I do with happiness, I am Mr. Muktaḥ;
For instance, imagine a little girl playing by herself, and pretending to make tea in a small cup. She brings an empty cup to her aunt and asks her to drink that tea. The aunt should enjoy that fake tea, not start questioning the reality of that team. There is no need to do so, the child is doing what is appropriate. Similarly, just because one is studying karmayoga does not make him or her eligible to behave differently with others.
Now, most of our actions are either performed individually or in a team. If we are performing actions individually, it is very straightforward to adopt the attitude of karmayoga. If we are working in a team, we could be playing the role of peers, leaders or followers. In all three of these situations, Shri Krishna urges us to maintain the attitude of karmayoga regardless of whether our peers, leaders or followers have the very same attitude. Their attitude in no way should impact the efficiency of our work.
This “live and let live” approach is extremely practical and sensible. But is there a reason behind it? Shri Krishna will explain in the next verse.
।। हिंदी समीक्षा ।।
हम सब अपने अपने कार्यक्षेत्रों में जीवनपर्यन्त पूर्ण उत्साह एवं रुचि के साथ कर्म करते रहते हैं। एक सामान्य मनुष्य निरन्तर कर्म के दबाव अथवा तनाव में अपने आप को थकाकर क्षीण कर लेता है। शारीरिक स्वास्थ्य ऋतु परिवर्तन की पीड़ा तथा जीवन के अन्य सुखदुख की चिन्ता न कर के वह निरन्तर अधिक से अधिक धनार्जन तथा उसके उपभोग के लिए प्रयत्नशील रहता है। श्रीकृष्ण कहते हैं कि आत्मज्ञानी पुरुष भी अज्ञानी के समान उत्साहपूर्वक अथक कर्म करता है। दोनों के कार्यों में एकमात्र अन्तर यह है कि अज्ञानी पुरुष कर्म फलों में आसक्त हुआ कर्म करता है तो ज्ञानी पुरुष पूर्ण रूप से अनासक्त हुआ केवल विश्व के कल्याण के लिये कर्मरत होता है।यह संभव है कि सामान्य मनुष्य को ज्ञानी और अज्ञानी के कर्मों के मध्य सूक्ष्म भेद विशेष महत्त्व का प्रतीत न हो जब तक कि उसका ध्यान इस ज्ञान की सार्वभौमिक उपयोगिता की ओर आकर्षित नहीं किया जाय। कर्मफल के प्रति आसक्ति और चिन्ता ही वे छिद्र हैं जिनके माध्यम से कर्त्ता की शक्ति बिखर जाती है और जीवन में उसे केवल असफलता ही हाथ लगती है। ज्ञानी पुरुष भी शरीर मन और बुद्धि से ही समस्त कर्म करता है परन्तु वह मन की शक्ति को व्यर्थ में गंवाता नहीं। मन का यह स्वभाव है कि वह किसी न किसी वस्तु के साथ आसक्त होकर ही कार्य करता है।
इस श्लोक में वर्णित अनासक्ति का अर्थ है मिथ्या विषयों के प्रति मन में आकर्षण का अभाव। इसे प्राप्त करने का उपाय है मन को उच्च और श्रेष्ठ लक्ष्य की ओर प्रवृत्त करना। अत श्रीकृष्ण जब अनासक्त होकर कर्म करने का उपदेश देते हैं तब उसका उपाय भी बताते हैं कि विद्वान् पुरुष को लोक कल्याण की इच्छा से कर्म करना चाहिए।अत्यधिक अहंकार केन्द्रित होने पर ही आसक्ति कल्याण के मार्ग में बाधक बनती है। जिस सीमा तक हम अपनी दृष्टि को व्यापक करते हुए किसी बड़ी योजना अथवा समाज के लिये कार्य करते हैं उसी सीमा तक आसक्ति का दुखदायी विष समाप्त होकर युग को आनन्द विभोर करता है। अनेक प्रकार के विष मिश्रित रूप में जीवन रक्षक औषधि का काम करते हैं जब कि वही विष अपनें तीव्र रूप में तत्काल मृत्यु का कारण बन जाते हैं। अत्यधिक आत्मकेन्द्रित इच्छायें मनुष्य को हानि पहुंचाती हैं परन्तु अपने को ऊँचा उठाकर सम्पूर्ण जगत् के साथ तादात्म्य स्थापित होने पर उसी मनुष्य के कर्म दिव्यता की आभा से मंडित होकर उसके दुखों एवं दुर्बलताओं को दूर कर देते हैं।
हम अपने जीवन मे सभी लोगो से मिलते है जो हम से प्रेम, द्वेष, स्पर्धा एवम अनासक्ति रखते है, यह सभी अपने अपने कार्य करते है। कुछ को फल की आशा है कुछ अपना कर्तव्य मान कर कार्य करते है। किन्तु कार्य सभी किसी न किसी लक्ष्य की पूर्ति के लिए करते है। जब अनाशक्त भाव से कार्य किया जाए तो लक्ष्य प्राप्ति के बाद हम अपने अगले कार्य मे लग जाते है बिना समय गवाए की इस से मुझे या किसी को क्या लाभ हानि हुई। किन्तु आसक्ति भाव से करने से व्यक्ति अपनी लाभ हानि से अपने कर्म की तुलना करता है और फिर आगे का कर्म करने की सोचता है।
अतः अनाशक्त भाव रखने वाले को भी कर्म तो आसक्त भाव रखने वाले के समान ही करना चाहिए, किन्तु दोनों की भावना अलग अलग होती है। एक स्वयं के लिये धन, प्रसिद्धि, सुख सुविधा के लिए कार्य करता है और उस के फल को भोगता हुआ बंधन में कार्य करता है और दूसरा लोकसंग्रह के कार्य करता है और उस को कार्य के फल पर कोई आसक्ति नही होती। इस लिये मन के विकारों से दूर रहता है।
गीता इस श्लोक से यह प्रतिपादित करती है कि कर्म फल के इच्छा एवम विषयो में आसक्ति जहां इस संसार मे अज्ञानी लोगो को कर्म करने के प्रेरित करती है, वही जिस व्यक्ति है अपना सम्बन्ध आत्मा से जोड़ लिया है उस के कर्म करने का कोई औचित्य नही रहने के बाद भी उसे कर्तव्य धर्म के अनुसार अपना कर्म लोकसंग्रह हेतु करते रहना चाहिये। ऐसे व्यक्ति को अज्ञानी लोग अनुशरण भी करते है, इसलिये आत्म ज्ञानी लोकसंग्रह के लिये कर्तव्यधर्म समझ कर कार्य करते रहना ही चाहिये। उन के कर्म की प्रवृति में अनुशासन, कार्यक्षमता एवम कार्यकुशलता, नियमितता में आसक्ति नही होने के बावजूद भी कोई कमी नही होंनी चाहिए।
ज्ञानी व्यक्ति अज्ञानी व्यक्ति को हेय दृष्टि से भी नही देखता और उस के द्वारा किए कार्य में सहयोग ही देता है। अज्ञानी व्यक्ति शास्त्र और कर्मों का किताबी ज्ञान पूर्ण रखता है किंतु वह प्रकृति के बंधन से मुक्त नहीं होता इसलिए वह सभी कार्य सात्विक स्वरूप में अपनी इच्छाओं की पूर्ति अर्थात धन, कीर्ति, पद, सांसारिक प्रसन्नता और अपने परिवार के लिए करता है। ज्ञानी भी अज्ञानी की भांति कर्म तो करता हुआ दिखता है किंतु निष्काम और निर्लिप्त होने के कारण उस के कार्य लोक संग्रह के होते है।
एक अज्ञानी डॉक्टर अपने मरीज का इलाज धन कमाने के लिए अधिक से अधिक बिल बना कर करता है और ज्ञानी डॉक्टर कम से कम खर्चे में मरीज को शीघ्र लाभ हो, इसलिए करता है। अंतर उद्देश्य का है जिस में एक अपनी परिस्थिति से असंतुष्ट है और स्वार्थ और मोह में है, दूसरा अपनी परिस्थिति से संतुष्ट है।
यही एक महत्वपूर्ण कथन भी है कि बिना स्वार्थ के भी हम को कार्य सफल होने के लिये करना है। हार या विफलता को चुनोती समझ कर पूर्ण क्षमता से करना है। यही कारण है वैज्ञानिक एक बार अविष्कार में लग जाये तो खाना-पीना तक भूल कर सफ़ल होने के कार्य करते है। अर्जुन को युद्ध करना तो है ही, किन्तु युद्ध क्षत्रिय की भांति जीतने के लिये अनासक्त भाव से करना है। अनासक्ति का कही भी यह मतलब नहीं होता कि कार्य के प्रति उदासीनता का भाव हो। युद्ध में अर्जुन की उपस्थिति एक योद्धा की है, इस लिए एक ज्ञानी पुरुष के अनुसार उसे निष्काम और निरासक्त होकर युद्ध करना है, क्योंकि वह श्रेष्ठ योद्धा है और उस के कार्य बाद में सामान्य जन के लिए अनुसरण का कारण बनेगा।
ज्ञानी और अज्ञानी में क्या अन्तर है इसको भगवान् आगे के श्लोकमें बताते हैं।
।। हरि ॐ तत सत।। 3.25 ।।
Complied by: CA R K Ganeriwala ( +91 9422310075)