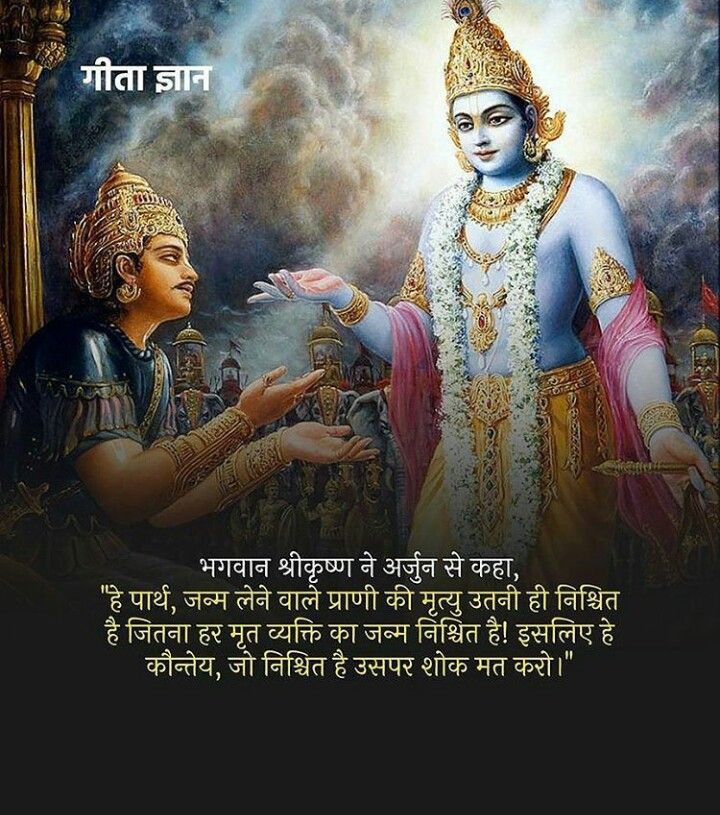।। Shrimadbhagwad Geeta ।। A Practical Approach ।।
।। श्रीमद्भगवत गीता ।। एक व्यवहारिक सोच ।।
।। Chapter 03.10 ।।
।। अध्याय 03. 10 ।।
॥ श्रीमद्भगवद्गीता ॥ 3.10॥
सहयज्ञाः प्रजाः सृष्टा पुरोवाचप्रजापतिः ।
अनेन प्रसविष्यध्वमेष वोऽस्त्विष्टकामधुक् ॥
“saha-yajñāḥ prajāḥ sṛṣṭvā,
purovāca prajāpatiḥ..I
anena prasaviṣyadhvam,
eṣa vo ‘stv iṣṭa-kāma-dhuk”..II
भावार्थ :
सृष्टि के प्रारम्भ में प्रजापति ब्रह्मा ने यज्ञ सहित देवताओं और मनुष्यों को रच कर उन से कहा कि तुम लोग इस यज्ञ द्वारा सुख-समृध्दि को प्राप्त करो और यह यज्ञ तुम लोगों की इष्ट (परमात्मा) संबन्धित कामना की पूर्ति करेगा॥१०॥
Meaning:
In ancient times, Prajaapati created humanity along with yajna. He said “through this (yajna) let everyone prosper, and may it become your fulfiller of wishes”.
Explanation:
A life of sacrifice is prescribed by the vēdās themselves for the harmony and progress of the society. Such a life of contribution; such a life of sacrifice; such a life of sharing called yajña way of life, is prescribed by the vēdās themselves, for whose benefit? For our own benefit. i.e. why we say that the vēdās are like a manual, which has come along with the creation itself.
There should be a manual given to the human beings, so that he will know how to live in the world and get maximum benefit out of the world. Maximum benefit means what? Dharma-artha-kāma, even mokṣaḥ-puruṣārthaḥ, he should attain. If Bhagavān does not give the manual, we do not know how to handle the world, as we are seeing how our life is environment unfriendly life it is; now they are coining the word, eco-friendly and eco-unfriendly; and we only are polluting this creation; creating ozone holes; creating all kinds of problems, destroying whom? Ourselves only, therefore we do not know how to handle the world.
Since manufacturer alone will know what is the ideal way of handling his product, and if he is giving instructions, not for his own benefit, it is only meant for the benefit of the user.
Now users have to read mannual to know specification, coution to follow in do and do not form, it’s utilisation and operating system etc. But instead he starts reading as holy book for our worship. In foreign, people are doing research and we are feeling proud of having research material.
Similarly who has manufactured this world? Not any one of the human beings. Human beings cannot create anything except some confusion.
Human cannot create anything, and that too this wonderful world, no ordinary human intelligence can create, we are not even able to fully understand the creation, where is the question of creating this world.
All the elements of nature are integral parts of the system of God’s creation. All the parts of the system naturally draw from and give back to the whole. The sun lends stability to the earth and provides heat and light necessary for life to exist. Earth creates food from its soil for our nourishment and also holds essential minerals in its womb for a civilized lifestyle. The air moves the life force in our body and enables transmission of sound energy. We humans too are an integral part of the entire system of God’s creation. The air that we breathe, the Earth that we walk upon, the water that we drink, and the light that illumines our day, are all gifts of creation to us. While we partake of these gifts to sustain our lives, we also have our duties toward the integral system. Shree Krishna says that we are obligated to participate with the creative force of nature by performing our prescribed duties in the service of God. That is the yajña he expects from us.
A common question for many of us is: “I understand the concept of selfless dedication. However, how do I know that I will be able to fulfill my material needs if I give up caring for the fruits of action altogether?” Shri Krishna has the answer : perform actions with selfless dedication or yajna, and your material needs will be provided for automatically.
If we work for a corporation, we do several different things everyday to fulfill our job responsibilities: respond to emails, attend meetings, draft project plans, make excel documents and so on. Do we ever think : “how much money will I get paid for opening this email? how much money do I get for attending this meeting?” If we have done our job right, the results will automatically come to us in the form of a monthly salary.
Shri Krishna explains that yajna is embedded within the fabric of humanity since time immemorial. It is a universal law. Once invoked, that law provides us with all that we need in this world. It becomes the “fulfiller of wishes”. And the key to invoke that universal law is to perform selfless action dedicated to a higher ideal.
This is the essence of karmayoga.
Footnotes;
1. Some commentators interpret the word “isthakaamadhuk” to mean “kaamadhenu”, the mythological cow that grants any wish asked of her. But even with this interpretation, the essence of this shloka remains unchanged.
।। हिंदी समीक्षा ।।
ब्रह्माजी प्रजा (सृष्टि) के रचयिता एवं उसके स्वामी हैं अतः अपने कर्तव्य का पालन करने के साथ वे प्रजा की रक्षा तथा उस के कल्याण का विचार करते रहते हैं। कारण कि जो जिसे उत्पन्न करता है उस की रक्षा करना उस का कर्तव्य हो जाता है। ब्रह्माजी प्रजा की रचना करते उस की रक्षा में तत्पर रहते तथा सदा उसके हित की बात सोचते हैं। इसलिये वे प्रजापति कहलाते हैं।
संसार की रचना के बाद यह जटिल प्रश्न था कि इस का निर्वाह कैसे होगा। इसलिये सृष्टि चक्र के नियम बनाये गए और प्रकृति की हर रचना को एक दूसरे के प्रति आश्रित बताया गया। यही सृष्टि का यज्ञ चक्र बना और इस यज्ञ चक्र में कर्म की अनिवार्यता सिद्ध की गई। यही कर्म जीव को कैसे करना चाहिए, हम भगवान श्री कृष्ण से सुन रहे है।
इस सम्पूर्ण ब्रह्मांड की रचना, ब्रह्म के संकल्प को मूर्त रूप देने के लिए ब्रह्मा जी की। कंप्यूटर के हार्डवेयर के साथ ऑपरेटिंग एवम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है, वह ब्रह्म ने महामाया और प्रकृति के कार्य – कारण के नियम बना कर किया। सूर्य, पहाड़, समुंद्र, नदिया, वायु, पशु, पक्षी, वनस्पति का सौंदर्य किस का मन नहीं मोह लेता। फिर मनुष्य बनाया, जिसे बुद्धि दे कर प्रकृति की सर्वोच्च रचना बनी। इस समस्त रचना बना पाना किसी भी मनुष्य के लिए संभव नही किंतु अहंकार में वह यही सोचता है कि वह ही समस्त रचना का न केवल मालिक है, वरन उसे ही एक मात्र उपभोग का अधिकार है।
जिस प्रकार उत्पादन कर्ता अपने प्रोडक्ट का एक आचार संहिता (मैन्युफैक्चरिंग एंड यूटिलाइजेशन मैनुअल ) भी प्रोडक्ट के साथ देता है, वैसे ही वेदों की रचना कर के इस रचना का उपभोग करने का वर्णन किया गया है। वेद ही हमे बताते है कि हम प्रकृति के ही नियम से बंधे है और प्रकृति में वनस्पति से ले कर पृथ्वी, जल, आकाश, सूर्य और चंद्र आदि अपनी शक्तियों का उपयोग बाटने के लिए करते है। वे जो कुछ प्रकृति से लेते है, वह प्रकृति को लौटा देते है। किंतु जीव की बुद्धि मालिन होने से वह प्रकृति के नियम का पालन नहीं करता और अपने ब्रह्म स्वरूप को भूल कर लोभ, स्वार्थ, काम, राग या द्वेष और संचय में लगा रहता है। उस का लोभ प्रकृति को नुकसान तक पहुंचाने में लगा है, जिस के परिणाम भी अब सामने आने लग गए है। यही उस का अज्ञान भी है।
जब मनुष्य उत्पाद कर्ता वेदों और उपनिषदों के विरुद्ध जा कर, ओजोन परत को नष्ट करता है, बड़े बड़े बम बनाता है और युद्ध करता है। नदी, नाले पर गलत बांध बनाता है या पहाड़ों को गलत तरीके से काटता है तो प्रकृति स्वयं उस को भूकंप, बाढ़, आदि से संतुलित करती है।
उत्पादकर्ता की पुस्तक वेद ही क्यों, अन्य धर्म के ग्रंथ क्यो नही। क्योंकि विज्ञान, चिकित्सा, रसायन, अर्थशास्त्र, संगीत और गान आदि के साथ इस की रचना अत्यंत प्राचीन और प्रमाणित विधि से जो अन्य किसी भी धर्म ग्रंथ में नही मिलती। यह बात अलग के वेद पढ़ कर सनातन धर्मी हिंदू ज्ञान को प्राप्त करने की बजाय, इन की पूजा और भक्ति करने लगे। उत्पाद पुस्तक उत्पादन की विशेषताओं, उपयोग की विभिन्न विधियों और do or do not की बारीकियों से पढ़ा जाता है, किंतु हम इसे धार्मिक पुस्तक बना कर पूजन विधि से पढ़ते लगे और इस की श्रुतियों में चमत्कार खोजने लगे। जबकि विदेशों में, यहां तक नासा में वेदों पर अन्वेषण होता है। भारतीय अज्ञान की पराकाष्ठा यह भी है, मनुष्य वेदों की प्रामाणिकता पर बहस भी करता है, जैसे संपूर्ण प्रकृति के रहस्य वो जानता है। गीता वेदों और उपनिषदों का सार अर्थात दूध है किंतु गीता के श्लोक रटना या इस के पाठ से चमत्कार की आशा लगाना भी अज्ञान ही है। इस लिए वह प्रकृति का निर्लिप्त भाव से उपभोग भी नही कर पाता।
ब्रह्माजी मनुष्यों से कहते हैं कि तुम लोग अपने अपने कर्तव्य पालन के द्वारा सब की वृद्धि करो उन्नति करो ऐसा करने से तुम लोगों को कर्तव्य कर्म करने में उपयोगी सामग्री प्राप्त होती रहे उस की कभी कमी न रहे। जब संसार मे स्वार्थ, लोभ, मोह और कामना नही होगा तो समृद्धि का प्रवेश वहॉं होना ही है। इस से प्रकृति का उपभोग निर्लिप्त भाव से भोगने का आनंद भी प्राप्त होगा।
अर्जुन की कर्म न करने में जो रुचि थी उसे दूर करने के लिये भगवान् कहते हैं कि प्रजापति ब्रह्माजी के वचनों से भी तुम्हें कर्तव्य कर्म करने की शिक्षा लेनी चाहिये। दूसरों के हित के लिये कर्तव्य कर्म करने से ही तुम्हारी लौकिक और पारलौकिक उन्नति हो सकती है।
प्रवृति प्रधान भागवत धर्म के तत्व का ही गीता में प्रतिपादन किया गया है। परंतु भागवत धर्म मे यज्ञओ में की जाने वाली हिंसा गह्य मानी गई है, इसलिये पशु यज्ञ के स्थान पर प्रथम द्रव्यमय यज्ञ शुरू हुआ, और अंत मे जपमय और ज्ञानमय यज्ञ को श्रेष्ठ माना गया।
भगवान कृष्ण यहां यह स्पष्ट करना चाहते कि कर्मयोग का जो ज्ञान आज वो अर्जुन को दे रहे है वो नया नही है यह तो सृष्टि की मूल भूत आवश्यकता है, परोपकार की भावना एवम अनासक्ति भाव से ही सृष्टि के सभी प्राणी मिल जुल कर रह सकते है, यहां स्वामी विवेकानंद जी कहते है, – दूसरों के प्रति हमारे कर्तव्य का अर्थ है–दूसरों की सहायता करना, संसार का भला करना। अब प्रश्न उठता है कि हम संसार का भला क्यों करें?
वास्तव में बात यह है कि ऊपर से तो हम संसार का उपकार करते हैं, परन्तु असल में हम अपना ही उपकार करते हैं। हमें सदैव संसार का उपकार करने की चेष्टा करनी चाहिए, और कार्य करने में यही हमारा सर्वोच्च उद्देश्य होना चाहिए। परन्तु यदि ध्यानपूर्वक देखा जाय, तो प्रतीत होगा कि इस संसार को हमारी सहायता की बिलकुल आवश्यकता नहीं। यह संसार इसलिए नहीं बना कि हम अथवा तुम आकर इसकी सहायता करें। एक बार मैंने एक उपदेश पढ़ा था, वह इस प्रकार था–” यह सुन्दर संसार बड़ा अच्छा है, क्योंकि इसमें हमें दूसरों की सहायता करने के लिए समय तथा अवसर मिलता है।” ऊपर से तो यह भाव सचमुच सुन्दर है, परन्तु यह कहना कि संसार को हमारी सहायता की आवश्यकता है, क्या घोर ईश्वर-निन्दा नहीं है? यह सच है कि संसार में दुःख-कष्ट बहुत हैं, और इसलिए लोगों की सहायता करना हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ कार्य है; परन्तु आगे चलकर हम देखेंगे कि दूसरों की सहायता करने का अर्थ है अपनी ही सहायता करना। मनुष्य परमात्मा का स्वरूप है, इस का ज्ञान होने से प्रकृति और मोक्ष का अर्थ समझ में आने लगता है। किंतु जो प्रकृति के अज्ञान से ज्ञान प्राप्त करने की चेष्टा करते है, उन्हे इस को समझ पाना कठिन है।
मुझे स्मरण है, एक बार जब मैं छोटा था, तो मेरे पास कुछ सफेद चूहे थे। वे चूहे एक छोटे-से सन्दूक में रखे गये थे और उस सन्दूक के भीतर उनके लिए छोटे छोटे चक्के बना दिये गये थे। जब चूहे उन चक्कों को पार करना चाहते, तो वे चक्के वहीं के वहीं घूमते रहते, और वे बेचारे चूहे कभी भी बाहर नहीं निकल पाते। बस यही हाल संसार का तथा संसार के प्रति हमारी सहायता का है। उपकार केवल इतना ही होता है कि हमें नैतिक शिक्षा मिलती है। संसार न तो अच्छा है, न बुरा। बात इतनी ही है कि प्रत्येक मनुष्य अपने लिए अपना अपना संसार बना लेता है। यदि एक अन्धा संसार के बारे में सोचने लगे, तो वह उसके समक्ष या तो मुलायम या कड़ा प्रतीत होगा, अथवा शीत या उष्ण। हम सुख या दुःख की समष्टि मात्र हैं; यह हमने अपने जीवन में सैकड़ों बार अनुभव किया है। बहुधा नौजवान आशावादी होते हैं, और वृद्ध निराशावादी। तरुण के सामने अभी उसका सारा जीवन पड़ा है। परन्तु वृद्ध की केवल यही शिकायत रहती है कि उसका समय निकल गया; कितनी ही अपूर्ण इच्छाएँ उसके हृदय में मचलती रहती हैं, जिन्हें पूर्ण करने की शक्ति उसमें आज नहीं। परन्तु है दोनों ही मूर्ख। हमारी मानसिक अवस्था के अनुसार ही हमें यह संसार भला या बुरा प्रतीत होता है। स्वयं यह न तो भला है, न बुरा। अग्नि स्वयं न अच्छी है, न बुरी। जब यह हमें गरम रखती है, तो हम कहते हैं, ‘यह कितनी सुन्दर है!’ परन्तु जब इससे हमारी उँगली जल जाती है, तो इसे हम दोष देते हैं। परन्तु फिर भी स्वयं न तो यह अच्छी है, न बुरी। जैसा हम इसका उपयोग करते है, तदनुरूप यह अच्छी या बुरी बन जाती है। यही हाल इस संसार का भी है। संसार स्वयं पूर्ण है। पूर्ण होने का अर्थ यह है कि उसमें अपने सब प्रयोजनों को पूर्ण करने की क्षमता है। हमें यह निश्चित जान लेना चाहिए कि हमारे बिना भी यह संसार बड़े मजे से चलता जायगा; हमें इसकी सहायता करने के लिए माथापच्ची करने की आवश्यकता नहीं।
परन्तु फिर भी हमें सदैव परोपकार करते ही रहना चाहिए। यदि हम सदैव यह ध्यान रखें कि दूसरों की सहायता करना एक सौभाग्य है, तो परोपकार करने की इच्छा एक सर्वोत्तम प्रेरणा-शक्ति है। एक दाता के ऊँचे आसन पर खड़े होकर और अपने हाथ में दो पैसे लेकर यह मत कहो, “ऐ भिखारी, ले, यह मैं तुझे देता हूँ।” परन्तु तुम स्वयं इस बात के लिए कृतज्ञ होओ कि तुम्हें वह निर्धन व्यक्ति मिला, जिसे दान देकर तुमने स्वयं अपना उपकार किया। धन्य पानेवाला नहीं होता, देनेवाला होता है। इस बात के लिए कृतज्ञ होओ कि इस संसार में तुम्हें अपनी दयालुता का प्रयोग करने और इस प्रकार पवित्र एवं पूर्ण होने का अवसर प्राप्त हुआ। समस्त भले कार्य हमें शुद्ध बनने तथा पूर्ण होने में सहायता करते हैं। और सच पूछो तो हम अधिक से अधिक कर ही कितना सकते हैं? या तो एक अस्पताल बनवा देते हैं, सड़कें बनवा देते हैं या सदावर्त खुलवा देते हैं, बस इतना ही तो? हम गरीबों के लिए एक कोष खोल देते हैं, दस-बीस लाख रुपये इकट्ठा कर लेते हैं। उसमें से पाँच लाख का एक अस्पताल बनवा देते हैं, पाँच लाख नाच-तमाशे में फूंक देते हैं और शेष का आधा कर्मचारी लूट लेते हैं; बाकी जो बचता है, वह किसी तरह गरीबों तक पहुँचता है! परन्तु उतने से हुआ क्या? आँधी का एक झोंका तो तुम्हारी इन सारी इमारतों को पाँच मिनट में नष्ट कर दे सकता है–फिर तुम क्या करोगे? एक भूकम्प तो तुम्हारी तमाम सड़कों, अस्पतालों, नगरों और इमारतों को धूल में मिला दे सकता है। अतएव इस प्रकार की संसार की सहायता करने की खोखली बातों को हमें छोड़ देना चाहिए। यह संसार न तो तुम्हारी सहायता का भूखा है और न मेरी। परन्तु फिर भी हमें निरन्तर कार्य करते रहना चाहिए, निरन्तर परोपकार करते रहना चाहिए। क्यों?–इसलिए कि इससे हमारा ही भला है। यही एक साधन है, जिससे हम पूर्ण बन सकते हैं। यदि हमने किसी भिखारी की कुछ दिया हो, तो वास्तव में उसके ऊपर हमारा कुछ नहीं आता, हमारे ऊपर ही उसका आता है, हम पर उसका आभार है, क्योंकि उसने हमें इस बात का अवसर दिया कि हम अपनी दया उस पर काम में ला सकें। यह सोचना निरी भूल है कि हमने संसार का भला किया, अथवा कर सकते हैं, या यह कि हमने अमुक अमुक व्यक्तियों की सहायता की। यह निरी मूर्खता का विचार है; और मूर्खता के विचारों से दुःख उत्पन्न होता है। हम कभी कभी सोचते हैं कि हमने अमुक मनुष्य की सहायता की और इसलिए आशा करते हैं कि वह हमें धन्यवाद दे; पर जब वह हमें धन्यवाद नही देता, तो उससे हमें दुःख होता है। हम जो कुछ करें, उसके बदले में किसी भी बात की आशा क्यों रखें? बल्कि उलटे हमें उसी मनुष्य के प्रति कृतज्ञ होना चाहिए, जिसकी हम सहायता करते हैं–उसे साक्षात् नारायण मानना चाहिए। मनुष्य की सहायता द्वारा ईश्वर की उपासना करना क्या हमारा परम सौभाग्य नहीं है? यदि हम वास्तव में अनासक्त हैं, तो हमें यह वृथा प्रत्याशाजनित कष्ट क्यों होना चाहिए? अनासक्त होने पर तो हम प्रसन्नतापूर्वक संसार में भलाई कर सकते हैं। अनासक्ति से किये हुए कार्य से कभी भी दुःख अथवा अशान्ति नहीं आयगी। वैसे तो संसार में अनन्त काल तक सुख-दुःख का चक्र चलता ही रहेगा, फिर हम इसकी सहायता के लिए कुछ करें या न करें, उससे कुछ बनने बिगड़ने का नहीं।
कर्मयोग में अनासक्ति भाव से कार्य करना व्यक्ति का मूल स्वभाव होना चाहिए और अपने जीवन निर्वाह का कार्य क्योंकि बंधनकारी है, जितना आवश्यक है उतना ही होना चाहिए।
कौरव या पांडव एक ही परिवार के होने बावजूद युद्ध भूमि में एक दूसरे के विरुद्ध सिर्फ स्वार्थ एवम मोह के लिए खड़े थे अतः यह सब लोग प्रजापति यानि सृष्टि रजियता के नियम के विरुद्ध हो गए, इन को नष्ट होना ही था।
।। हरि ॐ तत सत ।। 3.10 ।।
Complied by: CA R K Ganeriwala ( +91 9422310075)