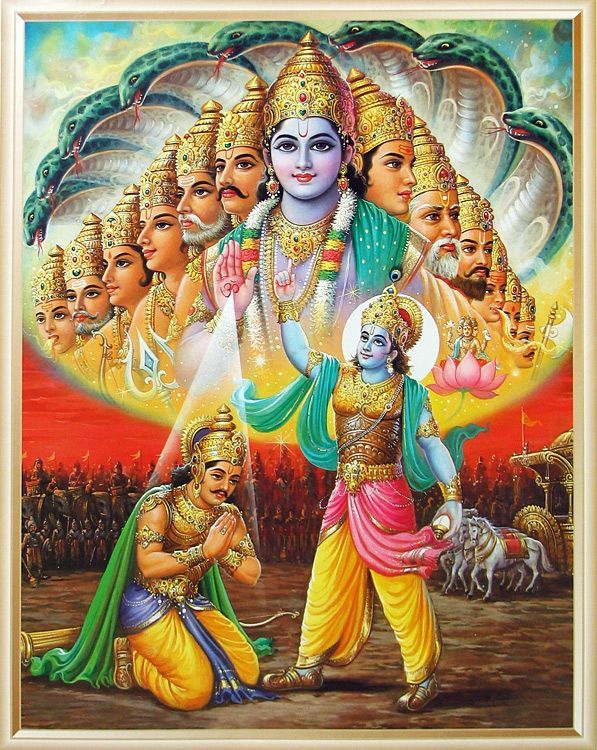।। Shrimadbhagwad Geeta ।। A Practical Approach ।।
।। श्रीमद्भगवत गीता ।। एक व्यवहारिक सोच ।।
।। Chapter 02. 64-65 ।।
।। अध्याय 02. 64-65 ।।
॥ श्रीमद्भगवद्गीता ॥ 2.64-65॥
रागद्वेषवियुक्तैस्तु विषयानिन्द्रियैश्चरन् ।
आत्मवश्यैर्विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति ॥64II
प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते ।
प्रसन्नचेतसो ह्याशु बुद्धिः पर्यवतिष्ठते ॥65II
“rāga-dveṣa-vimuktais tu,
viṣayān indriyaiś caran..I
ātma-vaśyair vidheyātmā
prasādam adhigacchati”..II64II
“prasāde sarva-duḥkhānāḿ,
hānir asyopajāyate..I
prasanna-cetaso hy āśu,
buddhiḥ paryavatiṣṭhate”..II65II
भावार्थ :
किन्तु सभी राग-द्वेष से मुक्त रहने वाला मनुष्य अपनी इन्द्रियों के संयम द्वारा मन को वश करके भगवान की पूर्ण कृपा प्राप्त कर सकता है।
इस प्रकार भगवान की कृपा प्राप्त होने से सम्पूर्ण दुःखों का अन्त हो जाता है तब उस प्रसन्न-चित्त मन वाले मनुष्य की बुद्धि शीघ्र ही एक परमात्मा में पूर्ण रूप से स्थिर हो जाती है। ॥६४-६५॥
Meaning:
But, the one whose mind and senses are under control, is devoid of attraction or revulsion. He moves around objects and gains the state of tranquility.
Having gained tranquility, all of his sorrows are destroyed. His mind is joyful and his intellect soon becomes steady.
Explanation:
In the last shloka, Shri Krishna explained the “ladder of fall”, or how constant thinking about material objects leads to a fall from equanimity. In this set of shlokas, he explains the exact opposite scenario, where bringing the senses and the mind under control brings us to a state of happiness. Here’s the sequence of events:
Bring senses and mind under control -> one becomes devoid of attraction and revulsion -> he can experience the material world without any problem -> his mind becomes tranquil -> his intellect becomes steady -> he has no more sorrow -> he attains the state of happiness.
Attachment and aversion are two sides of the same coin. Aversion is nothing but negative attachment. Just as, in attachment, the object of attachment repeatedly comes to one’s mind; similarly, in aversion, the object of hatred keeps popping into the mind. So attachment and aversion to material objects both have the same effect on the mind—they dirty it and pull it into the three modes of material nature. When the mind is free from both attachment and aversion, and is absorbed in devotion to God, one receives the grace of God and experiences his unlimited divine bliss. On experiencing that higher taste, the mind no longer feels attracted to the sense objects, even while using them. Thus, even while tasting, touching, smelling, hearing, and seeing, like all of us, the sthita prajña is free from both attachment and aversion.
So, if one continues to pursue one’s svadharma, and stay devoted to a higher ideal, one gets to a stage of equanimity. We have learned this in earlier shlokas. But then, what next? This set of shlokas tells us that performance of svadharma has a purifying effect – it is like a flame that burns away our vasanaas. As the vasanaas burn away, our minds remain situated in equanimity – and that’s when our sorrows diminish.
We are always looking at quick fixes to be happy – new job, new friends, read a new book, move to a new place etc. But what comes across in these shlokas is that a long-term state of happiness cannot be found in a quick fix solution. All we can do is follow our svadharma, fix a higher goal, and keep at it.
The intellect was accepting this only on the basis of knowledge as stated in the scriptures, but now after by grace, God who is sat-chit-ānand bestows his divine knowledge, divine love, and divine bliss, it gets the experience of perfect peace and divine bliss. This convinces the intellect beyond any shadow of doubt, and it becomes steadily situated in God. By God’s grace, when we experience the higher taste of divine bliss, the agitation for sensual happiness is extinguished. Once that hankering for material objects ceases, one goes beyond all suffering and the mind becomes tranquil.
Regular meaning of prasāda we receive from the temple. That is the extended meaning of the word prasāda is prasanna chittam. Shanthiḥ. Samatvam. Poise, Balance, Equanimity is called prasādaḥ. Prasādaḥ will produce two fold benefit. The first benefit is destruction of all sorrows and samatvam bring in happiness or joy.
The eight shlokas including this one comprise the answer to the fourth of Arjuna’s four questions, “how does a person of steady wisdom walk”, in other words, how does such a person control his mind?
।। हिंदी समीक्षा ।।
यदि हम पिछले श्लोक का पुन: अवलोकन करे तो हम ज्ञात होगा कि अर्जुन की जिज्ञासा स्थितप्रज्ञ मनुष्य के बारे में थी। कृष्ण जी ने बताया कि 1. वो निष्काम एवम निरासक्त होता है, 2. वो बिना फल की आशा है कार्य करता है, 3. जो फल प्राप्त है उस से संतुष्ट है 4. अपनी इन्द्रियों को नियंत्रण में रखता है।
इन्द्रियों के नियंत्रण के विषय मे पुनः बताया कि इन को वश में करना अत्यंत कठिन है जब तक मन मे राग एवम द्वेष है, यह कभी भी और कंही भी पुनः मनुष्य पर हावी हो सकती है अतः इंद्रियां यानी राग द्वेष तभी समाप्त होगा जब बुद्धि पूर्ण रूप से भगवान को समर्पित हो। यदि राग द्वेष के साथ रहते है तो क्या होता है।
अब इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते है कि स्थितप्रज्ञ राग द्वेष से दूर हो कर भगवान में रमा रहता है तो उस मे भगवद कृपा से चिर आनन्द समा जाता है। वास्तव में सत चित्त आनंद की स्थिति भगवान में रमे हुए मनुष्य को उन की कृपा रूपी प्रसाद से ही प्राप्त होती है। भगवद कृपा हमेशा जीव पर बरसती रहती है, आवश्यकता निष्ठा के साथ उस के प्रति समर्पण की है। एक बार निष्ठा हो जाए तो सद गुण और विषयों से विरक्ति स्वयमेव आ जाती है और मन वैरागी हो जाता है।
आसक्ति रहते हुए विषयों का चिन्तन करने मात्र से पतन हो जाता है और यहाँ कहते हैं कि आसक्ति न रहने पर विषयों का सेवन करने से उत्थान हो जाता है। वहाँ तो बुद्धि का नाश इन्द्रियों में लिप्त होने से बताया था और यहाँ बुद्धि का परमात्मा में स्थित होना बताया है।
इंद्रियों का दमन यदि संभव नही तो उन को भगवान के प्रति मोड़ देने से विषयों के प्रति आसक्ति का क्षय होने लगता है।
साधक का अन्तःकरण अपने वश में रहना चाहिये। अन्तःकरण को वशीभूत किये बिना कर्मयोग की सिद्धि नहीं होती प्रत्युत कर्म करते हुए विषयों में राग होने की और पतन होने की सम्भावना रहती है। वास्तव में देखा जाय तो अन्तःकरण को अपने वश में रखना हरेक साधक के लिये आवश्यक है। कर्मयोगी के लिये तो इस की विशेष आवश्यकता है।
रागद्वेषरहित होकर विषयों का सेवन करने से साधक अन्तःकरण की प्रसन्नता(स्वच्छता) को प्राप्त होता है। यह प्रसन्नता मानसिक तप है जो शारीरिक और वाचिक तप से ऊँचा है। अतः साधक को न तो रागपूर्वक विषयों का सेवन करना चाहिये और न द्वेषपूर्वक विषयों का त्याग करना चाहिये क्योंकि राग और द्वेष इन दोनों से ही संसार के साथ सम्बन्ध जुड़ता है।
मान लीजिये आप को आमरस बहुत पसंद है, यदि राग रखेंगे और न परोसा जाए तो मन मे खिन्नता आएगी यदि राग नही है तो सामने आने पर और न आने पर चित की प्रसनता समान रहेगी। बुद्धि यदि परमात्मा से युक्त है तो आप जो भी कार्य करते है उस के सेवक हो कर और कर्ता के भाव से दूर रहते है। आप को कार्य के कर्तव्य भाव का ज्ञान है किंतु जो प्राप्त है वो पर्याप्त है का भाव आप के मन के भाव को विचलित नही करता और आप उस स्थिति का आनंद के साथ उपभोग करते है।
खाने या घूमने या किसी भी कार्य मे मीन मेख निकालने वाला व्यक्ति न हो आप उस स्थिति का आनंद लेते है अन्यथा असंतुष्ट व्यक्ति के कारण परेशान होते है, यह राग द्वेष में लिप्त आप की बुद्धि ही असंतुष्ट व्यक्ति का कार्य करती है अन्यथा कोई भी आप को आनंद के लिए नही रोक सकता।
जितने भी दुःख हैं वे सब के सब प्रकृति और प्रकृति के कार्य शरीर संसार के सम्बन्ध से ही होते हैं और शरीर संसार से सम्बन्ध होता है सुख की लिप्सा से। सुख की लिप्सा होती है खिन्नता से। परन्तु जब प्रसन्नता होती है तब खिन्नता मिट जाती है। खिन्नता मिटने पर सुख की लिप्सा नहीं रहती। सुख की लिप्सा न रहने से शरीर संसार के साथ सम्बन्ध नहीं रहता और सम्बन्ध न रहने से सम्पूर्ण दुःखों का अभाव हो जाता है। तात्पर्य है कि प्रसन्नता से दो बातें होती हैं संसार से सम्बन्धविच्छेद और परमात्मा में बुद्धि की स्थिरता।
पूजन विधि के अन्त में प्रसाद वितरण की क्रिया इस सिद्धान्त की ही द्योतक है। पूजन अथवा यज्ञ करते समय मनुष्य को संयमित रहकर ईश्वर का ध्यान करना चाहिये जिस के फलस्वरूप वह मन में अपूर्व शान्ति का अनुभव करता है। वास्तव में इसको ही ईश्वर प्रसाद कहा जाता है। वेदान्ती चित्तशुद्धि को प्रसाद समझते हैं। रागद्वेष के अभाव में विक्षेपों का अभाव स्वाभाविक है और यही है चित्तशुद्धि का प्रसाद जिसे प्राप्त करने पर आनंद ही आनंद है।
प्रस्तुत इन दो श्लोक से यह स्पष्ट है कि कर्मयोगी का विषयो से राग – द्वेष मिटा कर निरासक्त भाव से कर्म करने को जोर दिया है, जब कि सन्यास मार्ग में विषयो के साथ कर्मो के भी त्याग की बात की जाती है। सन्यास मार्ग विषयो के त्याग का मार्ग है जबकि कर्मयोग विषयो पर आसक्ति के त्याग का मार्ग है। कर्मयोग सन्यास मार्ग के अनुरूप ही संयम एवम तप का मार्ग होते हुए भी संसार मे रहते हुए, नियत कर्म लोकसंग्रह हेतु करते रहने का योग अर्थात युक्ति बताता है। जो अर्जुन की उस दुविधा का उत्तर है जो अपने कर्तव्य धर्म का पालन न करते हुए, पलायन से सन्यास मार्ग धारण करने की बात करता है।
।। हरि ॐ तत सत ।। 2. 64-65 ।।
Complied by: CA R K Ganeriwala ( +91 9422310075)