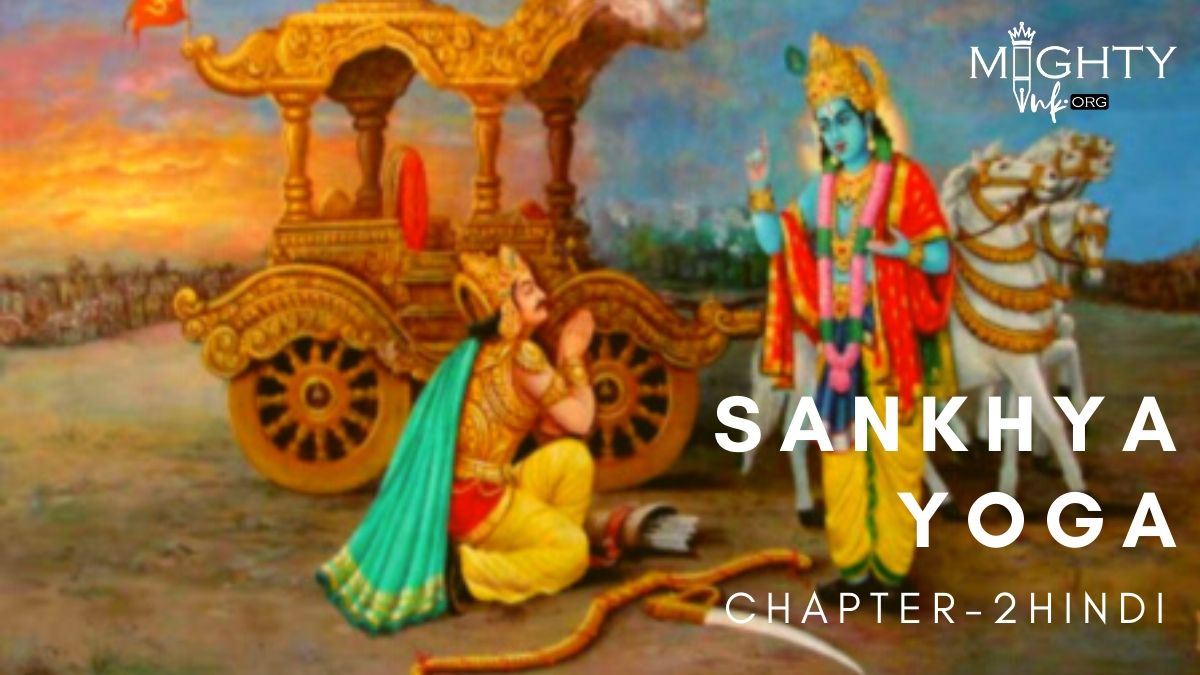।। Shrimadbhagwad Geeta ।। A Practical Approach ।।
।। श्रीमद्भगवत गीता ।। एक व्यवहारिक सोच ।।
।। Chapter 02. 29।।
।। अध्याय 02. 29 ।।
॥ श्रीमद्भगवद्गीता ॥ 2.29॥
आश्चर्यवत्पश्यति कश्चिदेन माश्चर्यवद्वदति तथैव चान्यः ।
आश्चर्यवच्चैनमन्यः श्रृणोति श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित् ॥
āścarya-vat paśyati kaścid enam,
āścarya-vad vadati tathaiva cānyaḥ..I
āścarya-vac cainam anyaḥ śṛṇoti,
śrutvāpy enaḿ veda na caiva kaścit..II
भावार्थ :
कोई इस आत्मा को आश्चर्य की तरह देखता है, कोई इसका आश्चर्य की तरह वर्णन करता है तथा कोई इसे आश्चर्य की तरह सुनता है और कोई-कोई तो इसके विषय में सुनकर भी कुछ नहीं समझ पाता है ॥ २९॥
Meaning:
Some perceive this (eternal essence) as a wonder, and similarly indeed, others speak of it as a wonder; it is a wonder that some hear about this, and after hearing about it, some understand this and some do not.
Explanation:
Shri Krishna was getting ready to conclude the topic of the eternal essence. Therefore, he wanted to remind Arjuna about it, and also instill a sense of deep curiosity and interest in him. In this shloka, Shri Krishna did both of those things.
Four types of spiritual seekers are pointed out here. Firstly, there are seekers who have heard about the eternal essence through the Gita or through other means. Usually, most of them will hear about it and forget about it. But there will be some that will become interested in it, and will want to hear more – this is the second category. Of those seekers, some will try to gain an intellectual understanding about it and having done so, will be so enthralled with it that they will keep speaking about it to other people. This is the third category.
But the most devoted and advanced seekers will ultimately perceive the eternal essence directly, and the perception would have occurred without any sense organs. When this happens, there would be no words to describe it. The closest one could come to describing it is when we see something so wonderful that it renders us speechless, like a breathtaking painting or a waterfall.
Every human being is knowingly or unknowingly looking for only certain fundamental goals in life. one may want success in business; another may want success in politics, another may want to extend his family; even though the goals are superficially different, fundamentally, the goals are the same i.e. sense of fulfilment in life, the second basic goal is a sense of discovery of security And finally, discovery of happiness; thus fulfilment, security, happiness etc. are the basic goals that everyone has. And according to Vēdānta all these basic goals are represented by one word, i.e. ātma, or Brahman. In fact, Brahman or ātma is another word for fulfilment. It is another word for security. It is another word for happiness. Therefore, a person knowingly or unknowingly is seeking what? ātma alone. And what is the greatest wonder in that seeking? The goal that is ātma which is sought after by everyone happens to be the very nature of the seeker. So the sought, that is the goal; which is called peace, security, fulfilment, etc. which is otherwise called ātma, the ātma happens to be one’s own intrinsic self. In fact, in Sanskrit, the word ātma means Self; and therefore the greatest wonder is that everyone is seeking himself or herself without knowing that he is seeking himself or herself.
All the time, we should remember, ātma is not an object that is being talked about but it is the very subject about which Krishna is talking. Therefore looking for the ātma is the basic mistake; this is called objectification orientation. In Sanskrit it is called परोक्ष बुद्धि parokṣha buddhiḥ. Objectification orientation: you imagine some mysterious Brahman; mysterious truth and look for some mysterious thing to happen in your meditation. Some people say that they saw some ring, ring, etc. I saw flash appearing and disappearing; all the time we expect something to happen; either in the form of an event or in the form of an object and whatever you experience is not ātma because, it is an object. And when I negate everything, you tend to conclude that if you negate everything, then it must be शून्यम śūnyam; nothing is there.
The soul, being a fragmental part of God, is more amazing than the things of the world because it is transcendental to material existence. Just as God is divine, its fragment, the soul, is also divine. For this reason, mere intellectual prowess is not enough to comprehend the soul, since the existence and nature of the soul are difficult to grasp. The Kaṭhopaniṣhad states:
“A teacher who is self-realized is very rare. The opportunity to hear instructions about the science of self-realization from such a teacher is even rarer. If, by great good fortune, such an opportunity presents itself, students who can comprehend this topic are the rarest.” Hence, an enlightened teacher is never discouraged when, despite sincere efforts, the majority of the people are either not interested in, or cannot understand the science of the soul.
Note that the meter has changed in this verse to indicate its importance.
।। हिंदी समीक्षा ।।
प्रत्येक मनुष्य के जीवन के कुछ उद्देश्य यही होते है कि वह अपने आप को जानना और समझना चाहता है, वह जिस विषय में रुचि रखता हो, उस में सफलता की इच्छा रखता है, दूसरा सामान्य उद्देश्य सुरक्षा है जिस में स्वयं और परिवार फिर समाज और देश की बात करता है और तीसरा उद्देश्य वह आनंद चाहता है। इन सब के लिए वह अपने को तलाश कर रहा है। जब उसे यह कहा जाए कि जिसे वह तलाश रहा है, वो और कोई नही उस की आत्मा अर्थात खुद की पहचान को तलाश रहा है तो उसे आश्चर्य के साथ विश्वास भी नही होता। आत्मा को जान पाना ही वास्तविक सफलता, सुरक्षा और आनंद है। इस के लिए हम लोग आध्यात्मिक जगत से भौतिक जगत में और भौतिक जगत से आध्यात्मिक जगत में भटकते रहते है। इसलिए जब गीता या वेदों द्वारा आत्मा स्वयं को जानने की बात की जाती है जिस से उसे सफलता, सुरक्षा और आनंद की प्राप्ति स्थायी मिल सके तो इसे वह आश्चर्य की तरह देखता है, वर्णन करता है, सुनता है या फिर सब कर के भी समझ नही पाता। वास्तव में सफलता, सुरक्षा और आनंद अपने को जानने और पहचानने का विषय है, जिसे आत्म तत्व से जाना जा सकता है और आश्चर्य यही है कि जो स्वयं में उपस्थित है, उसे हम भुला कर, लापरवाह होकर, अरुचिकर और महत्वपूर्ण न समझ कर नही ध्यान देते और सांसारिक वस्तुओं में खोजने लगते है। जब की सांसारिक वस्तुएं साधन है, साध्य नहीं।
कोई ध्यान लगा कर,कोई मूर्ति बना कर पूजा द्वारा, कोई कर्म से और कोई योग, सन्यास और यज्ञ याग से इस को जानने और करने में लगा है तो कोई कुछ भी करने और मानने को तैयार नहीं। व्यक्ति आत्मा को वस्तु की भांति स्वयं से अलग खोजता है, कभी ॐ की ध्वनि में, कभी दीपक के प्रकाश में, कभी किसी घटना में, यह सब परोक्ष बुद्धि के लक्षण है। जो स्वयं है, वह बाहर अपने को खोजता है, यही आत्मा के विषय में आश्चर्य है क्योंकि जब कोई बताए भी तो विश्वास नही करता, मानता भी नही है। उसे लगता है, वह जो कर रहा है वही सत्य है। जो स्वयं प्रकाशमान आत्मा है, वह ही प्रकृति के अज्ञान में भ्रमित हो कर, स्वयं को बाहर प्रकृति में खोज रहा है। जिस ने खोजना बंद कर दिया, जिस ने अपने अज्ञान को मिटा दिया, उस ने अपने को भी प्राप्त कर लिया। आत्मा अर्थात अपने को खोजना, हरेक जीव अपने अपने तरीके और बुद्धि से करता है।
गीता का यह श्लोक कठोपनिषद (1.2.7) से मिलता है। आत्मा की अनुभूति लेने वाले चार प्रकार के प्राणी बताए गए है। जिस की रामसुखदास जी ने विस्तार से वर्णन किया है। आत्मा आत्म चिंतन का विषय है एवम मन बुद्धि एवम इन्द्रियों द्वारा इस को सिर्फ समझ सकते है किंतु इस को प्राप्त नही हो सकते। अतः जिन्होंने इसे प्राप्त किया वो मौन है किंतु जिन्होंने इस मार्ग पर आगे बढे वो सिर्फ दिशा निर्देश है, मंजिल तो स्वयं को प्राप्त करनी होती है।
प्रथम
इस देहि अर्थात आत्मा को कोई आश्चर्य की तरह जानता है। तात्पर्य यह है कि जैसे दूसरी चीजें देखने सुनने पढ़ने और जानने में आती हैं वैसे इस देही का जानना नहीं होता। कारण कि दूसरी वस्तुएँ इदंता से ( यह करके) जानते हैं अर्थात् वे जानने का विषय होती हैं पर यह देही इन्द्रिय मनबुद्धि का विषय नहीं है। इस को तो स्वयं से अपनेआप से ही जाना जाता है। अपने आप से जो जानना होता है वह जानना लौकिक ज्ञान की तरह नहीं होता प्रत्युत बहुत विलक्षण होता है।
पश्यति पद के दो अर्थ होते हैं नेत्रों से देखना और स्वयं के द्वारा स्वयं को जानना। यहाँ पश्यति पद स्वयं के द्वारा स्वयं को जानने के विषय में आया है।जहाँ नेत्र आदि करणों से देखना (जानना) होता है वहाँ द्रष्टा (देखनेवाला) दृश्य (दीखनेवाली वस्तु) और दर्शन (देखनेकी शक्ति) यह त्रिपुटी होती है। इस त्रिपुटी से ही सांसारिक देखना जानना होता है। परन्तु स्वयं के ज्ञान में यह त्रिपुटी नहीं होती है अर्थात् स्वयं का ज्ञान करणसापेक्ष नहीं है। स्वयं का ज्ञान तो स्वयं के द्वारा ही होता है अर्थात् वह ज्ञान करणनिरपेक्ष है।
जैसे आईने के सामने बैठ कर स्वयम को देखे और सोचे कौन किस को देख रहा है। मैं हूँ ऐसा जो अपने होनेपन ज्ञान है इस में किसी प्रमाण की या किसी करण की आवश्यकता नहीं है। इस अपने होनेपन को इदंता से अर्थात् दृश्यरूप से नहीं देख सकते। इसका ज्ञान अपने आपको ही होता है। यह ज्ञान इन्द्रियजन्य या बुद्धिजन्य नहीं है। इसलिये स्वयं को (अपनेआपको) जानना आश्चर्यकी तरह होता है।
स्थूल सूक्ष्म और कारण ये तीन शरीर हैं। अन्नजलसे बना हुआ स्थूलशरीर है। यह स्थूलशरीर इन्द्रियोंका विषय है। इस स्थूल शरीर के भीतर पाँच ज्ञानेन्द्रियों पाँच कर्मेन्द्रियाँ पाँच प्राण मन और बुद्धि इन सत्रह तत्त्वों से बना हुआ सूक्ष्म शरीर है। यह सूक्ष्म शरीर इन्द्रियों का विषय नहीं है प्रत्युत बुद्धि का विषय हैं। जो बुद्धि का भी विषय नहीं है जिस में प्रकृति स्वभाव रहता है वह कारण शरीर है। इन तीनों शरीरों पर विचार किया जाय तो यह स्थूल शरीर मेरा स्वरूप नहीं है क्योंकि यह प्रतिक्षण बदलता है और जानने में आता है। सूक्ष्म शरीर भी बदलता है और जानने में आता है अतः यह भी मेरा स्वरूप नहीं है। कारण शरीर प्रकृतिस्वरूप है पर देही (स्वरूप) प्रकृति से भी अतीत है अतः कारण शरीर भी मेरा स्वरूप नहीं है। यह देही जब प्रकृति को छोड़कर अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है तब यह अपने आप से अपने आपबको जान लेता है। यह जानना सांसारिक वस्तुओं को जानने की अपेक्षा सर्वथा विलक्षण होता है इसलिये इसको आश्चर्यवत् पश्यति कहा गया है।
द्वितीय
यहाँ भगवान् ने कहा है कि अपने आप का अनुभव करने वाला कोई एक ही होता है कश्चित् और आगे सातवें अध्याय के तीसरे श्लोक में भी यही बात कही है कि कोई एक मनुष्य ही मेरे को तत्त्व से जानता है। इन पदों से ऐसा मालूम होता है कि इस अविनाशी तत्त्व को जानना बड़ा कठिन है दुर्लभ है। परन्तु वास्तव में ऐसी बात नहीं है। इस तत्त्व को जानना कठिन नहीं है दुर्लभ नहीं है प्रत्युत इस तत्त्वको सच्चे हृदय से जानने वाले की इस तरफ लगने वाले की कमी है। यह कमी जानने की जिज्ञासा कम होनेके कारण ही है।
ऐसे ही दूसरा पुरुष इस देही का आश्चर्य की तरह वर्णन करता है क्योंकि यह तत्त्व वाणी का विषय नहीं है। जिस से वाणी भी प्रकाशित होती है वह वाणी उस का वर्णन कैसे कर सकती है जो महापुरुष इस तत्त्व का वर्णन करता है वह तो शाखा चन्द्र न्याय की तरह वाणी से इस का केवल संकेत ही करता है जिस से सुनने वाले का इधर लक्ष्य हो जाय। अतः इसका वर्णन आश्चर्य की तरह ही होता है।
सब के सब अनुभवी तत्त्वज्ञ महापुरुष उस तत्त्व का विवेचन कर के सुनने वाले को उस तत्त्व तक नहीं पहुँचा सकते। उस की शंकाओं का तर्कों का पूरी तरह समाधान करने की क्षमता नहीं रखते। अतः वर्णन करने वाले की विलक्षण क्षमता का द्योतन करने के लिये ही यह अन्यः पद दिया गया है।
तृतीय
दूसरा कोई इस देही को आश्चर्य की तरह सुनता है। तात्पर्य है कि सुननेवाला शास्त्रों की लोक लोकान्तरों की जितनी बातें सुनता आया है उन सब बातों से इस देही की बात विलक्षण मालूम देती है। कारण कि दूसरा जो कुछ सुना है वह सब का सब इन्द्रियाँ मन बुद्धि आदिका विषय है परन्तु यह देही इन्द्रियों आदिका विषय नहीं है प्रत्युत यह इन्द्रियों आदि के विषय को प्रकाशित करता है। अतः इस देही की विलक्षण बात वह आश्चर्य की तरह सुनता है।
यहाँ अन्यः पद देने का तात्पर्य है कि जाननेवाला और कहनेवाला इन दोनों से सुननेवाला (तत्त्व का जिज्ञासु) अलग है।
चतुर्थ
इस को सुन कर के भी कोई नहीं जानता। इस का तात्पर्य यह नहीं है कि उसने सुन लिया तो अब वह जानेगा ही नहीं। इस का तात्पर्य यह है कि केवल सुन करके (सुनने मात्र से) इस को कोई भी नहीं जान सकता। सुनने के बाद जब वह स्वयं उस में स्थित होगा तब वह अपने आप से ही अपने आप को जानेगा। शास्त्रों पर श्रद्धा स्वयं शास्त्र नहीं कराते और गुरुजनों पर श्रद्धा स्वयं गुरुजन नहीं कराते किन्तु साधक स्वयं ही शास्त्र और गुरुपर श्रद्धा विश्वास करता है स्वयं ही उन के सम्मुख होता है। अगर स्वयं के सम्मुख हुए बिना ही ज्ञान हो जाता तो आज तक भगवान् के बहुत अवतार हुए हैं बड़े बड़े जीवन्मुक्त महापुरुष हुए हैं उनके सामने कोई अज्ञानी रहना ही नहीं चाहिये था। अर्थात् सब को तत्त्वज्ञान हो जाना चाहिये था पर ऐसा देखने में नहीं आता। श्रद्धाविश्वासपूर्वक सुनने से स्वरूप में स्थित होने में सहायता तो जरूर मिलती है पर स्वरूप में स्थित स्वयं ही होता है। अतः उपर्युक्त पदों का तात्पर्य तत्त्वज्ञान को असम्भव बताने में नहीं प्रत्युत उसे करण निरपेक्ष बताने में है।
मनुष्य किसी भी रीति से तत्त्व को जानने का प्रयत्न क्यों न करे पर अन्त में अपने आप से ही अपने आप को जानेगा। श्रवण मनन आदि साधन तत्त्व के ज्ञान में परम्परागत साधन माने जा सकते हैं पर वास्तविक बोध करण निरपेक्ष (अपने आप से) ही होता है।
ज्ञानेन्द्रियों के द्वारा जानना नहीं होता प्रत्युत देखना होता है जो कि व्यवहार में उपयोगी है। स्वयं के द्वारा जो जानना होता है वह दो तरहका होता है एक तो शरीर संसार के साथ मेरी सदा भिन्नता है और दूसरा परमात्मा के साथ मेरी सदा अभिन्नता है। दूसरे शब्दों में परिवर्तनशील नाशवान् पदार्थों के साथ मेरा किञ्चिन्मात्र भी सम्बन्ध नहीं है और अपरिवर्तनशील अविनाशी परमात्मा के साथ मेरा नित्य सम्बन्ध है। ऐसा जानने के बाद फिर स्वतः अनुभव होता है। उस अनुभव का वाणी से वर्णन नहीं हो सकता। वहाँ तो बुद्धि भी चुप हो जाती है।
प्रस्तुत श्लोक यह स्पष्ट करता है तत्वदर्शन लिख कर, पढ़ कर, सुनकर, या देख कर नही होता है। यह इन्द्रियों से अगोचर है, इसलिये इस तत्व को जानना तभी सम्भव है जब स्वयम ही मन को शुद्ध एवम बुद्ध किया जाए। कल्पनातीत विषय को समझना, पढ़ना, मनन करना सभी आश्चर्यजनक ही है।
अब तक देह और देही का जो प्रकरण चल रहा था उस का आगे के श्लोक में उपसंहार करते हैं। श्लोक 30 से आत्मा के विषय मे अपना उपदेश समाप्त करते हुए आगे के कुछ श्लोक अर्जुन को सामान्य एवम व्यवहारिक ज्ञान पर दिए गए है वो युद्ध भूमि को इंगित कर के है।
।। हरि ॐ तत सत ।। 2.29।।
Complied by: CA R K Ganeriwala ( +91 9422310075)