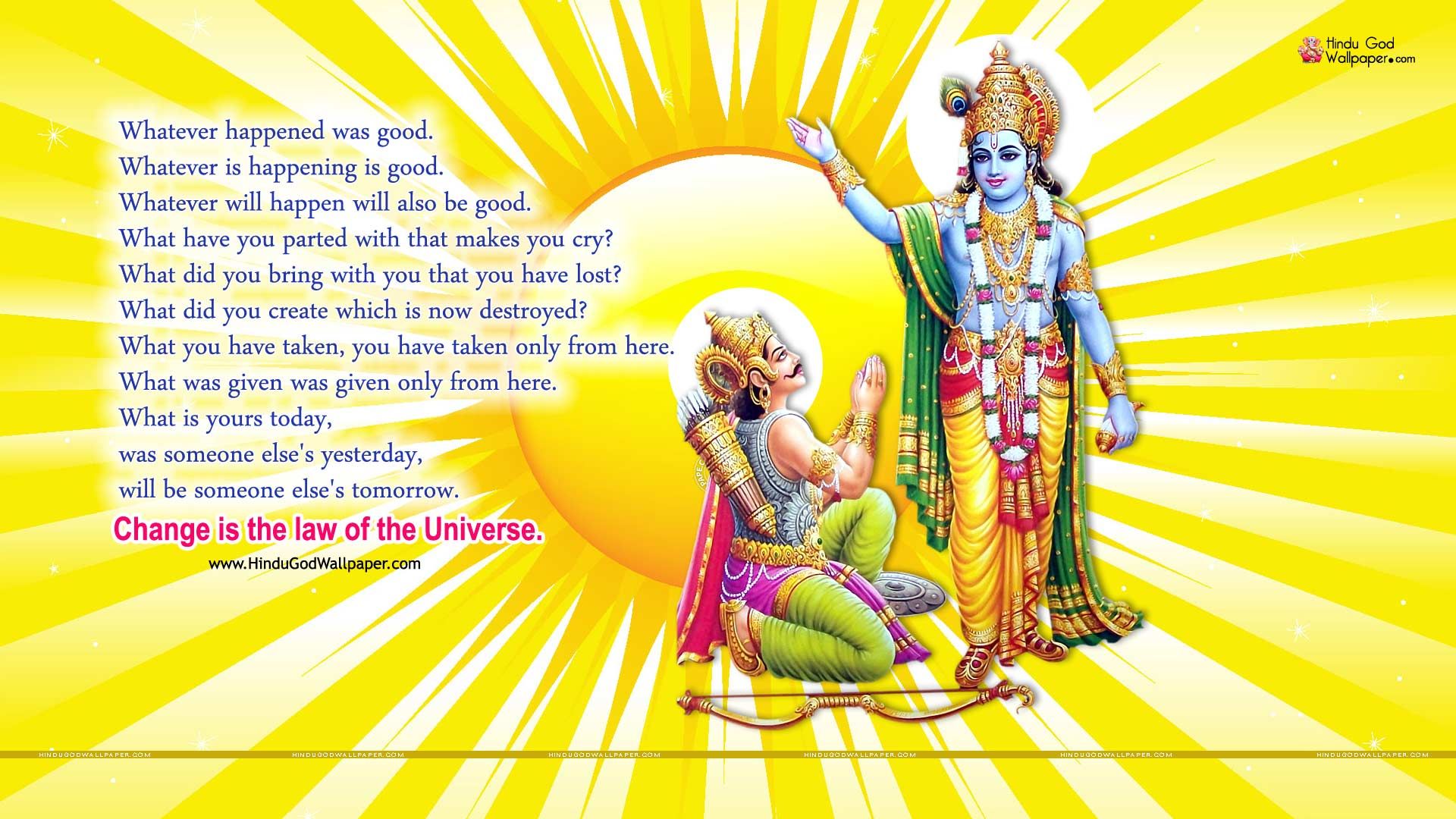।। Shrimadbhagwad Geeta ।। A Practical Approach ।।
।। श्रीमद्भगवत गीता ।। एक व्यवहारिक सोच ।।
।। Chapter 03.17 ।। Additional II
।। अध्याय 03. 17 ।। विशेष II
।। सृष्टि यज्ञ चक्र, वेद, धर्म और अज्ञान ।। विशेष – 3.17 ।।
कल की अतिभौतिवाद विचार धारा के मनन को आगे बढ़ाते है, यह कुछ लंबा है किंतु अति भौतिकवाद और ज्ञान का अंतर समझने में सहायक होगा।
धर्म, नीतिशास्त्र एवम पूर्वजो के आचरण, ग्रंथो का आधार ले कर समस्त कार्य या कर्म नही किये जा सकते। क्योंकि आत्मा का ज्ञान होना ही मोक्ष है तो करने को कुछ बचता ही है, फिर जो भी कर्म होगा, वह नियत एवम लोकसंग्रह का निमित मात्र हो कर होगा।
आदि शंकराचार्य जी कहते है
आत्मा की उपाधिरूप जो अविद्या है , उस की दो बड़ी भारी शक्तियाँ हैं – आवरण और विक्षेप। इन दो शक्तियों से ही आत्मा के ऊपर संसार का आरोपण होता है। अविद्या के तीन गुण हैं – सत्त्व , रज और तम । तमोगुण का धर्म आवरण है , जिस से यह ही आत्मस्वरूप के आवरण का कारण है । उस को मूल – अविद्या के नाम से कहा जाता है , जिस के द्वारा संसार महामोह को प्राप्त हो।अविद्या दो प्रकार की होती है – मूल-अविद्या और तूल-अविद्या । समष्टि-अविद्या का नाम मूल- अविद्या है और प्रत्येक जीवगत्- व्यष्टि -अविद्या का नाम तूल- अविद्या है । जिसको तत्त्वज्ञान की प्राप्ति हो जाती है , उसकी वह तूल-अविद्या नष्ट हो जाती है । इसलिए एक की मुक्ति होने में , सबकी मुक्ति का प्रसंग नहीं आता।
आत्म-अनात्म का विवेकी हो , बड़ी-बड़ी युक्तियों को जानने वाला तार्किक हो अथवा जिसने सम्यक रूप से आत्मा के तत्त्व को सुना हो और चाहे ज्ञानवान पण्डित ही क्यों न हो – यदि उसके ज्ञानचक्षु आवरण शक्ति से ढ़क जायें , तो इनमें से कोई भी अपने में स्थित आत्मा को नहीं जान पाता।।
अविद्या की दूसरी शक्ति — विक्षेप , रजोगुण के कारण है । यह शक्ति पुरुष की निरन्तर प्रवृत्ति का कारण होती है। विक्षेप शक्ति, आत्मा में स्थूल से बुद्धि पर्यन्त समस्त असत् ( मिथ्या ) वस्तुओं को आरोपित करती है। जैसे निद्रा अत्यंत सावधान व्यक्ति को भी अपने वश में कर लेती है ; वैसे ही आवरण – शक्ति अन्तःकरण में विक्षेप-शक्ति को बढ़ाती हुई आत्मा को ढक लेती है।
आवरण नामवाली बड़ी भारी शक्ति के द्वारा स्वच्छरूप आत्मा के आवरणयुक्त हो जानेपर, पुरुष अज्ञान से अनात्मा देह आदि में ‘यह मैं ही हूँ ‘, ऐसा मानकर आत्मपन का ज्ञान स्थापित कर बैठता है । जैसे सुषुप्तिकाल में भासनेवाले देह में ‘ यही मैं हूँ , यही मेरी आत्मा है ‘ , ऐसी बुद्धि होती है ; वैसे ही यह पुरुष उस अनात्मा के जन्म-मरण, भूख-प्यास , भय, थकावट आदि धर्मों को आत्मा में आरोपित करते है।
अतः शाब्दिक या पढ़ाई के ज्ञान से मनुष्य बुद्धिमान तो हो सकता है किंतु आत्मज्ञानी नही। गीता यदि एक बार पढ़ने से समझ में आ जाए तो उस की बुद्धि में अर्जुन की भांति परमात्मा में लीन होनी चाहिए।
कृष्ण अर्जुन को युद्ध के लिये कह रहे है क्योंकि वह नियत है और अर्जुन को योगी की भांति युद्ध के लिये कह रहे है। यही भौतिक जगत में हम परिवार, समाज या देश के समय अपने कर्तव्य धर्म के निर्धारण में तय करते है। जब नियति हमे कर्म को करने के लिए निमित्त बनाती है, तो उस को ज्ञानी की भांति करना या अज्ञानी की भांति राग – द्वेष में करना मनुष्य के अधिकार में है। इसलिए जिस का भाव निर्लिप्त नहीं होता, वह यही समझता है कि कृष्ण भगवान अर्जुन को युद्ध के लिए उसका रहे है, जब की नियति ने उन का भविष्य पहले से ही तय कर रखा है।
व्यास जी ने महाभारत में अनेक स्थानों पर भिन्न भिन्न कथाओं द्वारा यह प्रतिपादन किया है शूरता, धैर्य, दया, शील, मित्रता, समता आदि सब सद्गुण अपने अपने विरुद्ध गुणों के अतिरिक्त देश काल आदि से मर्यादित है। यह नही समझना चाहिए कि कोई एक ही सदगुण सभी समय शोभा देता है। भृतहरि का कथन है संकट के समय धैर्य, अभ्युदय के समय अर्थात जब शासन का सामर्थ्य तो तब क्षमा, सभा मे वक्तृता और युद्ध मे शूरता शोभा देती है। शांति के समय उत्तर के सामान बक बक करने वाले पुरुष कुछ कम नही है।
घर बैठे बैठे अपनी स्त्री की नथनी में से तीर चलाने वाले कर्मवीर बहुतेरे होंगे, उन में से रण भूमि पर धनुधर कहलाने वाला एक आध ही देख पड़ता है। आज व्हाट्सएप्प पर दिन रात चैटिंग करने वाले और सामाजिक चेतना के नाम पर बिना सोचे, परखे संदेश भेजने वाले शूरवीर अनेक है, किंतु कर्म क्षेत्र में वे अपनी चैटिंग के अनुसार ही कार्य और सामाजिक व्यवहार करते होंगे, इस की संभावना नगण्य है।हाथी के दांत की भांति दिखावा ज्यादा किंतु उपयोगिता या आचरण नही।
कुछ लोग विरोध करना या प्रत्येक कर्मवीर के विरुद्ध बोलना या लिखना अपना धर्म ही बना लेते है, जिन से बहस करना, अपनी ही मर्यादा का हनन होता है। इन के लिये धर्म ज्ञान प्रधान नही होता।
धर्म समय और स्थान की आवश्यकता के अनुसार समाज की कार्य करने की प्रवृति है, जिस में सभी लोग सात्विक भाव में रह सके।व्यास जी कहते है युगमान के अनुसार कृत, त्रेता, द्वापर और कली के धर्म भी भिन्न भिन्न होते है। महाभारत में एक कथा है प्राचीन काल मे स्त्रियों के लिये विवाह की मर्यादा नही थी, वे इस विषय मे स्वतंत्र एवम अनावृत थी। परंतु जब इस आचरण का बुरा परिणाम देख पड़ा तब श्वेतकेतु ने विवाह की मर्यादा स्थापित की और मदिरापान का निषेध भी पहले पहले शुक्राचार्य ही ने किया। तात्पर्य यह है कि जिस समय नियम जारी नही थे उस समय के धर्म अधर्म का और उस के बाद के धर्म अधर्म का विवेचन भी भिन्न रीति से किया जाना चाहिए।
कालमान के अनुसार देशाचार, कुलाचार और जाति धर्म का विचार करना पड़ता है क्योंकि आचार ही सब धर्मों की जड़ है। तथापि आचारों में भी बहुत भिन्नता हुआ करती है। भीष्म पितामह के अनुसार ऐसा कोई भी आचार नही मिलता जो हमेशा सब लोगो को समान हितकारी हो। आचार संहिता काल के अनुसार तय होती है। भीष्म द्वारा अपने पिता के लिए आजीवन अविवाहित रहने जैसी प्रतिज्ञा की आज के संदर्भ में चाहे कोई कितनी भी आलोचना करे, किंतु उस काल में पिता और पुत्र की मर्यादा में यह भीष्म प्रतिज्ञा थी।
काम, क्रोध और लोभ यह तीनों नरक के द्वार है। इन से हमारा नाश होता है इसलिए इन का त्याग करना चाहिए। वही गीता में भगवान ने अपने स्वरूप के वर्णन में कहा है “है अर्जुन, प्राणी मात्र में जो काम धर्म के अनुकूल है वो मैं ही हूँ।” मनु ने भी यही कहा है जो अर्थ और काम धर्म के विरुद्ध हो उस को त्याग देना चाहिये। यदि सब प्राणी कल से काम का त्याग कर दे और मृत्यु पर्यंत ब्रह्मचर्य व्रत से रहने का निश्चय कर ले सौ पचास वर्ष में सारी सजीव सृष्टि का लय हो जायेगा और जिस सृष्टि की रक्षा के लिए भगवान बार बार अवतार धारण करते है उस के अल्पकाल में ही उच्छेदन हो जायेगा।
यही बात वृद्ध को सम्मान देने एवम अनुशरण के लिये भी लागू है। इसी प्रकार जो अपने से श्रेष्ठ लोग व्यवहार करे या आचरण करे, वही धर्म हो जरूरी नहीं। परशुराम जी द्वारा मातृहत्या, भगवान राम द्वारा धोबी के कहने से सीता का त्याग, प्रह्लाद द्वारा पिता के विरुद्ध हरि भजन आदि अनुशरण के आचरण नही देते। यदि अपने ही बड़े धर्म विरुद्ध आचरण करे तो उन का आचरण पालन उचित धर्म के अनुसार ही करना चाहिए, जो सब के हित में हो।
महाभारत में भीष्म अपनी प्रतिज्ञा से बंधे अपने वचन का धर्म निभा रहे थे, कर्ण मित्रता धर्म निभा रहा था, द्रोणाचार्य सेवक का धर्म निभा रहे थे। धर्म के दृष्टिकोण से यह तीनों ज्ञानी, धर्मनिष्ठ और वीर योद्धा थे किंतु इन का अधर्म यही था कि यह लोग व्यक्तिगत रूप में चाहे कितने भी सही हो, साथ स्वार्थ, अधर्मी, लोभी और दुष्ट प्रवृति के लोग दुर्योधन के पक्ष से युद्ध कर रहे थे। इसलिए धर्म जब समूह में कार्य होता है तो व्यक्तिगत नही हो कर सामूहिक प्रयास के उद्देश्य से तय होता है। रावण का भी साथ देने वाला अधर्मी हो कर मारा गया।
सर्वधर्म सदभाव की बात सभी ने सुनी है, किंतु क्या कोई ऐसा धर्म है, जो सभी पर समान रूप से लागू है। मनुष्य के वर्ण, आश्रम, कार्य और लिंग और आयु भी धर्म को निर्धारित करते है। बड़ो और छोटों का धर्म, सैनिक का धर्म, नारी का धर्म, शिक्षक का धर्म, व्याध का धर्म आदि सभी अलग अलग है। फिर युद्ध भूमि में खड़े अर्जुन के धर्म की तुलना, परिवार में साथ साथ रह रहे सभी परिवार जनों के साथ कैसे की जा सकती है। मताधंतता में लिप्त हो कर कोई विधर्मी आप के अपने धर्म को नष्ट करे तो सहिष्णुता और दया के भाव से कोई अपनी रक्षा कैसे कर सकता है, वहां वीरों की भांति लड़ना ही धर्म होगा, यही अर्जुन का कर्तव्य है, यही आम व्यक्ति का कर्तव्य अर्थात धर्म है, यदि स्वार्थ में कोई विधर्मी के साथ भी खड़ा हो तो फिर वह चाहे कितना भी योग्य, पूजने और शक्तिशाली क्यों न हो, उस से अपनी और अपने परिवार की रक्षा करना क्षत्रिय का धर्म है।
अतः धर्म की दो परिभाषाएं होनी है, जिस में एक वह पारलौकिक मार्ग जिस पर चल कर व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। यह मार्ग पृथक पृथक भी हो किंतु पहुंचते एक ही स्थान पर होंगे। व्यक्ति की पहचान उस के द्वारा अपनाए मार्ग से होगी। दूसरा अर्थ सांसारिक कर्तव्य का पालन है जिस को व्यक्ति अपने लक्ष्य और कर्म के लिए सामाजिक नियम से तय करता है, इस में कुछ संशय हो तो वह पहले महान लोगो से बताए, मार्ग को अपनाता है। यही धर्म काम, अर्थ और मोक्ष के मार्ग की ओर भी जाता है।
धर्म और न्याय दोनों का अपना अपना महत्व है। शाब्दिक परिभाषा में दोनों को ही स्वार्थ, लोभ और मोह के साथ प्रयोग में लाया जाता है और दोनों ही उसी के अनुसार तय होते है जो शक्तिशाली हो। यह संसार है। किंतु वेदों में धर्म और न्याय वही तय कर सकता है, जो निरासक्त और निर्लिप्त हो। यही गीता द्वारा हमे संदेश दिया जा रहा है कि निरासक्त और निर्लिप्त बनो किंतु इस के साथ शक्तिशाली भी बनो जिस से अधर्म और अन्याय का प्रतिरोध कर सको।
कर्मयोग के अनुसार, बिना फल उत्पन्न किये कोई भी कर्म नष्ट नहीं हो सकता। प्रकृति की कोई भी शक्ति उसे फल उत्पन्न करने से रोक नहीं सकती। यदि मैं कोई बुरा कर्म करूं, तो उस का फल मुझे भोगना ही पड़ेगा; विश्व में ऐसी कोई ताकत नहीं, जो इसे रोक सके। इसी प्रकार, यदि मैं कोई सत्कार्य करूं, तो विश्व में ऐसी कोई शक्ति नहीं, जो उसके शुभ फल को रोक सके। कारण से कार्य होता ही है; इसे कोई भी रोक नहीं सकता। अब हमारे सामने कर्मयोग के सम्बन्ध में सूक्ष्म एवं गम्भीर विषय उपस्थित होता है। हमारे सत् और असत् कर्म आपस में घनिष्ठ रूप से सम्बद्ध हैं; इन दोनों के बीच हम निश्चित रूप से एक रेखा खींचकर यह नहीं बता सकते कि अमुक कार्य नितान्त शुभ है और अमुक अशुभ। ऐसा कोई भी कर्म नहीं है, जो एक ही समय शुभ और अशुभ दोनों फल न उत्पन्न करे। यही देखिये, मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ; सम्भवतः आपमें से कुछ लोग सोचते होंगे कि मैं एक भला कार्य कर रहा हूँ। परन्तु साथ ही साथ शायद मैं हवा में रहनेवाले असंख्य छोटे छोटे कीटाणुओं को भी नष्ट करता जा रहा हूँ। और इस प्रकार एक दृष्टि से मैं बुरा भी कर रहा हूँ। हमारे निकट के लोगों पर, जिन्हें हम जानते है, यदि किसी कार्य का प्रभाव शुभ पड़ता है, तो हम उसे शुभ कार्य कहते है। उदाहरणार्थ, आप लोग मेरे इस व्याख्यान को अच्छा कहेंगे, परन्तु वे कीटाणु ऐसा कभी न कहेंगे। कीटाणुओं को आप नही देख रहे हैं, पर अपनेआप को देख रहे हैं। मेरी वक्तृता का जैसा प्रभाव आप पर पड़ता है, वह आप स्पष्ट देख सकते हैं, किन्तु उसका प्रभाव उन कीटाणुओं पर कैसा पड़ता है. यह आप नही जानते। इसी प्रकार, यदि हम अपने असत् कर्मों का भी विश्लेषण करें, तो हमें ज्ञात होगा कि सम्भवतः उनसे भी कहीं न कहीं किसी न किसी प्रकार का शुभ फल हुआ है –“जो शुभ कर्मों में भी कुछ न कुछ अशुभ, तथा अशुभ कर्मों में भी कुछ न कुछ शुभ देखते हैं, वास्तव में उन्होंने कर्म का रहस्य समझा है।”
उपरोक्त विचार आतिभोतिकवादी विचार धारा के अंतर्गत कर्मयोगी को मनन करते हुए, अनाशक्त भाव की ओर बढ़ने के लिए है।
कर्मयोगी एक लक्ष्य पूर्ति के जीवन जीता है और अपने कर्मो द्वारा अपने लक्ष्य के शिखर पर पहुच जाता है और उसे उस के आगे कुछ करने की चाह नही रहती। यहां से उस की यात्रा अनाशक्त भाव के कर्म की शुरू होती है किंतु लक्ष्य प्राप्ति के लिये त्रिगुण प्रकृति में उसे सत का मार्ग ही चुनना होता है जिस का माप दंड यहां चर्चा के लाया गया है। अर्जुन को कर्तव्य पालन में अपने रिश्तेदारों के विरुद्ध युद्ध करने का आदेश भी उस समय काल का आचरण है।
जरूरत है इस पर मनन करने की, क्योंकि यह हमारे गीता अध्ययन में भगवान कृष्ण के उपदेश को समझने में सहायक होगा। किसी भी दशा में आतिभौतिकवाद सत्य को धर्म, आचरण एवम निष्काम भाव मे बदल नही सकता। नित्य अकर्ता है, अजन्मा है, सत्य है वो अवकाश, आकाश, वायु, अग्नि जल, पृत्वी, मन, बुद्धि, शरीर के किसी भी भाग का हिस्सा नहीं, यह सब सृष्टि यज्ञ चक्र के भागीदार है, नित्य के नही।
अतः गीता कर्मयोग में कर्म की प्रधानता पर जोर देती है, सन्यास मार्ग में ज्ञान की प्राप्ति के बाद जब आत्मा से सम्बन्ध जुड़ गया तो कर्म की आवश्यकता नही रह जाती, किन्तु प्रश्न यही है कि कर्म की आवश्यकता व्यक्तिगत है कि सृष्टि यज्ञ चक्र की आवश्यकता है। यही भगवान श्री कृष्ण श्लोक 17-19 में कहते है कि ज्ञानी को कर्म की आवश्यकता न भी तो भी उसे लोकसंग्रह हेतु, सृष्टि के यज्ञ च्रक में निमित हो कर योगी की भांति कर्म करते रहना चाहिए।
अतिभौतिकवादी एवम कर्म संयासी योग का भेद भी यही है कि कर्म क्यों और किस प्रकार करते रहना चाहिए, इस का पूर्ण ज्ञान होना ही चाहिये।
।। हरि ॐ तत सत ।। विशेष 3.17 ।। क्रमश: ।।
Complied by: CA R K Ganeriwala ( +91 9422310075)