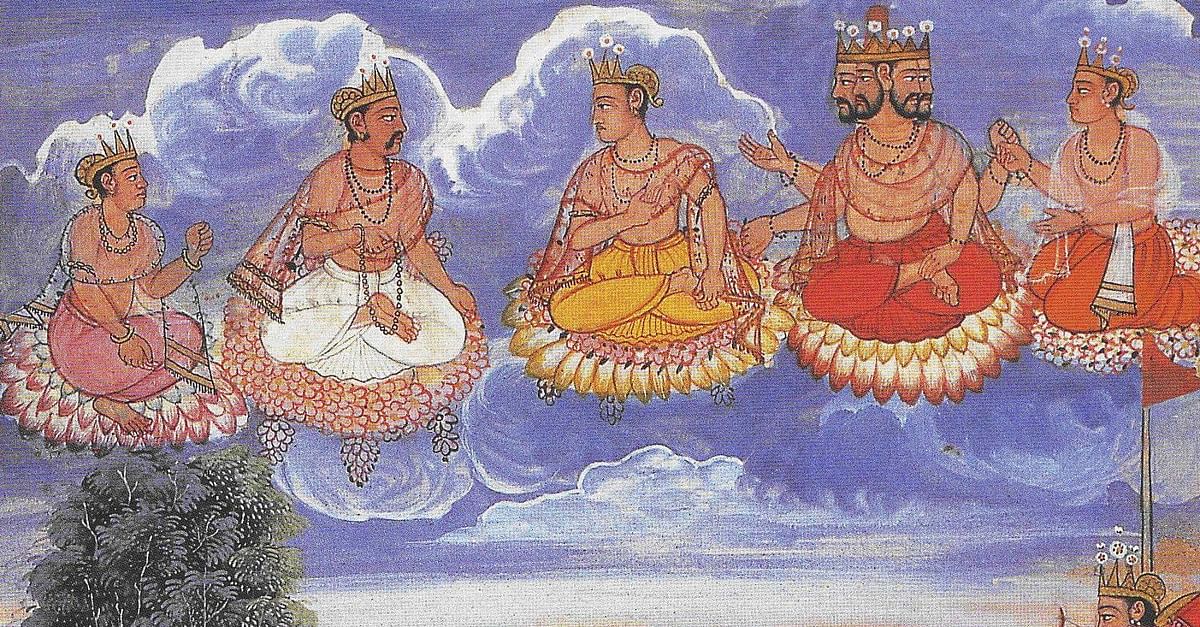।। Shrimadbhagwad Geeta ।। A Practical Approach ।।
।। श्रीमद्भगवत गीता ।। एक व्यवहारिक सोच ।।
।। Chapter 02. 38 ।।
।। अध्याय 02. 38 ।।
॥ श्रीमद्भगवद्गीता ॥ 2.38॥
सुखदुःखे समे कृत्वा लाभालाभौ जयाजयौ ।
ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमवाप्स्यसि ॥
“sukha-duḥkhe same kṛtvā,
lābhālābhau jayājayau..I
tato yuddhāya yujyasva,
naivaḿ pāpam avāpsyasi”..II
भावार्थ :
सुख या दुख, हानि या लाभ और विजय या पराजय का विचार त्याग कर युद्ध करने के लिये ही युद्ध कर, ऎसा करने से तू पाप को प्राप्त नही होगा॥३८॥
Meaning:
Treat joy or sorrow, gain or loss, victory or defeat with equanimity, and then engage in war. By doing so, you will not incur sin.
Explanation:
This is one of the most important shlokas in the second chapter, and perhaps in the entire Gita. In essence, Shri Krishna instructed Arjuna to maintain equanimity, an “even keel” attitude, not just in war, but in any circumstance in life.
Shree Krishna now moves deeper into the science of work. Arjun had expressed his fear that by killing his enemies he would incur sin. Shree Krishna addresses this apprehension. He advises Arjun to do his duty, without attachment to the fruits of his actions. Such an attitude to work will release him from any sinful reactions.
Let us take stock of where we are. We had seen that Shri Krishna was covering 4 main topics: 1) Informing Arjuna that his logic and reasoning was incorrect 2) Explaining the correct logic and reasoning to Arjuna 3) Providing practical guidance to implement this correct logic and reasoning 4) Describing the attributes of the individual who follows this teaching. We are currently in the set of shlokas covering topic 2 – the correct reasoning and logic.
After the first sub- topic of the eternal essence concluded, we explored the second sub-topic of svadharma. Shri Krishna is now about to conclude this sub-topic by pointing us to the ultimate goal of our spiritual efforts.
As somebody was telling that previously they thought that Intelligence Quotient, called IQ is responsible for the success of a person but later they are finding that more than IQ what a person requires is EQ. You know what EQ. Emotional quotient is. EQ in Gita is called samatvam.Therefore he says: सुखदुखे समे कृत्व sukhaduḥkhē samē kṛtvā prepare yourselves to build your EQ.
The entire Vedah is divided into two portion; religion and philosophy. Religion is a way of life;।philosophy is the right view of life. If a person has to efficiently act in the world, most important characteristic is learning to be balanced in mind; therefore, samatvaṃ as karma yoga is being introduced in this sloka which will be elaborated in the later verses;
Having reoriented ourselves with the scheme of the second chapter, lets now examine the current shloka. On first glance, the lesson in this shloka seems unapproachable and impossible to carry out, to some extent.
We encounter joy, sorrow, victory, defeat, gain and loss almost everyday, even several times a day. And each time we encounter any of these situations, we get emotionally and sometimes even physically affected by them. At work, a meeting with your boss does not go well. But on another day, your boss gives you an exemplary speech on a project well executed. How can we possible treat these as equal?
Shri Krishna fully understands this point. Here, he only lays out the ultimate goal for us: the goal of equanimity, or treating each and every life situation equally without getting agitated. Now that we know what the goal is, he will gently guide us through a path of practical advice throughout the rest of the teaching in the Gita.
Anyone who has completely surrendered unto Krishna, Mukunda, giving up all other duties, is no longer a debtor, nor is he obliged to anyone — not the demigods, nor the sages, nor the people in general, nor kinsmen, nor humanity, nor forefathers.” (Bhag. 11.5.41)
if I expected a person to come and help and if he does not help me, I can look at the situation from two angles; I can find fault with that person, who cheated me, or I can find fault with myself, that I expected such a thing to happen. That I was not prepared to face the other thing. In my lack of preparation, is exposed by this bitter experience. That is why somebody nicely said. Adversity introduces a person to himself. Every adversity exposes my limitations.
The samatvaṁ is very important because a person’s thinking power will be functional when the mind is samaḥ. When the mind is विषमः viṣamaḥ, disturbed, the first thing what happens is the discriminative power goes, for not only the decisions will go wrong; still worse, the man will lose the capacity to learn from every experience. As they say, the very life is like a university. That every experience can teach us a lesson; especially tragic experiences teach much more than happy experiences. As they say, a knife can be sharpened only when it is rubbed against a rough surface. When the knife is rubbed against a sponge, nothing happens but when it is rough surface; it increases the shine and sharpness. Similarly, we can learn much more from adverse circumstances than happy circumstances and if I have to learn valid lessons from such experiences, I should be able to have a relatively calm mind and therefore, Krishna emphasises the capacity to maintain the emotional balance is the most important virtue that is required.
So as we read the rest of the second chapter, if we think we have lost sight of the goal, let’s remember this shloka.
।। हिंदी समीक्षा ।।
सम्पूर्ण गीता के साररूप इस द्वितीय अध्याय में सांख्ययोग के पश्चात् इस श्लोक में कर्मयोग का दिशा निर्देश है।
यह श्लोक गीता के प्रमुख श्लोकों में एक है जिसे याद रखना चाहिये। इसी अध्याय में आगे भक्तियोग का भी संक्षेप में संकेत किया गया है।
यह प्रथम अवसर है जब श्रीकृष्ण इस श्लोक में आत्मोन्नति की साधना का स्पष्टरूप से वर्णन करते हैं। इसलिये इस का सावधानीपूर्वक अध्ययन गीता के समस्त साधकों के लिये अत्यन्त उपयोगी सिद्ध होगा।
अर्जुन को यह आशंका थी कि युद्ध में कुटुम्बियों को मारने से हमारे को पाप लग जायगा, पर भगवान् यहाँ कहते हैं कि पाप का हेतु युद्ध नहीं है, प्रत्युत अपनी कामना है। अतः कामना का त्याग कर के तू युद्ध के लिये खड़ा हो जा। कृष्ण अर्जुन को कर्तव्य पालन के लिये युद्ध करने को कह रहे थे, युद्ध दुर्योधन भी कर रहा है, द्रोण, भीष्म, कर्ण और अनेक महारथी कर रहे है किंतु जिस युद्ध को अर्जुन से कृष्ण करने को कह रहे है, उस को अब स्पष्ट करते है।
शरीर मन और बुद्धि इन तीन उपाधियों के माध्यम से ही हम जीवन में विभिन्न अनुभव प्राप्त कर सकते हैं। इन तीन स्तरों पर प्राप्त होने वाले सभी अनुभवों का समावेश इस श्लोक में कथित तीन प्रकार के द्वन्द्वों में किया गया है। अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थितियों को सुख और दुख के रूप में अनुभव करना बुद्धि की प्रतिक्रिया है लाभ और हानि ये मन की कल्पनायें हैं जिस कारण वस्तु की प्राप्ति पर हर्ष और वियोग पर शोक होना स्वाभाविक है भौतिक जगत् की उपलब्धियों को यहाँ जयपराजय शब्द से सूचित किया है। श्रीकृष्ण का उपदेश यह है कि मनुष्य को इस प्रकार की विषम परिस्थितियों में सदैव मन के सन्तुलन को बनाये रखना चाहये। इसके लिये सतत जागरूकता की आवश्यकता है। मनुष्य को पंडित अर्थात विवेकशील और धीर हो कर समभाव होना चाहिये।
बुद्धिमत्ता या ज्ञान को सर्वश्रेष्ठ अवश्य कहा गया है किंतु मात्र ज्ञान से व्यवहारिक जीवन सफल नहीं होता, सफलता के लिए भावनात्मक नियंत्रण भी आवश्यक है। यही वेदों एवम गीता में समत्व भाव है। जिस ने अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना सीख लिया, वही कर्तव्य कर्म भी बिना सुख – दुख, लाभ – हानि, सफलता – असफलता आदि के कुशलता पूर्वक कर सकता है।
समुद्र स्नान के इच्छुक व्यक्ति को समुद्र स्नान करने की कला ज्ञात होनी चाहिये अन्यथा समुद्र की उत्तुंग तरंगे उस व्यक्ति को व्यथित कर देंगी और उसे जल समाधि में खींच ले जायेंगी किन्तु बड़ी लहरों के नीचे झुकने और छोटी लहरों पर सवार होने की कला जो व्यक्ति जानता है वही समुद्र स्नान का आनन्द उठा सकता है। यह आशा करना कि समुद्र की लहरें शान्त हो जायें अथवा स्नान के समय कष्ट न पहुँचाये अपनी सुविधा के लिये समुद्र को उसके स्वरूप का त्याग करने के आदेश देने के समान है किन्तु अज्ञानी पुरुष जीवन में यही चाहता है कि किसी प्रकार की समस्यायें उसके सामने न आयें जो सर्वथा असम्भव है। जीवन के समुद्र में सुख दुख लाभहानि और जय पराजय की लहरें उठना अनिवार्य है अन्यथा पूर्ण गतिहीनता ही मृत्यु है। जीवन में जितना हम विपरीत परिस्थितियों में सीखते है, उतना हम अनुकूल परिस्थितियों में नही सीख पाते।
यदि जीवन का स्वरूप ही एक उफनते तूफानी समुद्र के समान है तो उसमें उठती उत्तुंग तरंगों के आघातों अथवा गहन गह्वरों से विचलित हुये बिना जीवन जीने की कला हमको सीखनी चाहिये। इन उठती हुई तरंगों में किसी एक के साथ भी तादात्म्य स्थापित कर लेना मानो समुद्र की सतह पर उसके साथ इधरउधर बहते जाना है और न कि उस प्रकाश के स्तम्भ के समान स्थिर रहना है जो वहीं विक्षुब्ध लहरों के बीच निश्चल खड़ा रहता है और जिसकी नींव समुद्र तल की चट्टान पर निर्मित होती है। भगवान् श्रीकृष्ण अर्जुन को युद्ध करने के लिये प्रेरित करते हैं किन्तु साथ में इस समत्व भाव का उपदेश भी देते हैं अन्यथा कर्म में प्रवृत्त हुआ व्यक्ति अनेक अवसरों पर अपनी ही नकारात्मक प्रवृत्तियों का शिकार बन जाता है। मन के इस समभाव के होने पर ही मनुष्य वास्तविक स्फूर्ति और प्रेरणा का जीवन जी सकता है और ऐसे व्यक्ति की उपलब्धियां ही सच्ची सफलता की आभा से युक्त होती हैं।
यह सुविदित तथ्य है कि सभी कार्य क्षेत्रों में जो कर्म स्फूर्ति और प्रेरणा युक्त होते हैं उनकी अपनी ही दैवी चमक होती है जिनकी न प्रतिकृति हो सकती है और न ही उसे बारम्बार दोहराया जा सकता है। किसी भी कार्य क्षेत्र का व्यक्ति चाहे वह कवि हो या कलाकार चिकित्सक हो या वक्ता जब अपनी सर्वश्रेष्ठ उपलब्धि या कृति प्रस्तुत करता है तब वह सर्वसम्मति से प्रेरणा का कार्य ही स्वीकार किया जाता है। इस प्रकार हम जब दैवी प्रेरणा के आनन्द से अविभूत कोई कार्य कर रहे होते हैं तब हमारी कल्पनायें विचार और कर्म अपनी एक निराली ही सुन्दरता से ओतप्रोत होते हैं जिन्हें एक यन्त्र के समान पुन दोहराया नहीं जा सकता।
प्रसिद्ध चित्रकार दा विन्सी अपनी श्रेष्ठ कृति मन्द स्मितवदना मोनालिसा का चित्र दोबारा चित्रित नहीं कर सका महाकवि कीट्स की लेखनी उड़ते हुये बुलबुल के गान को दूसरी बार नहीं लिख पायी बीथोवेन पियानों पर फिर एक बार वही मधुर स्वर झंकृत नहीं कर सका भगवान् श्रीकृष्ण ने भी अर्जुन के प्रार्थना करने पर युद्ध के पश्चात् दोबारा गीता सुनाने में अपनी असमर्थता स्वीकार की।
पाश्चात्य विचारकों के लिये प्रेरणा संयोग की कोई रहस्यमय घटना है जिस पर मानव का कोई नियन्त्रण नहीं रहता जबकि भारतीय मनीषियों के अनुसार दैवी प्रेरणा का जीवन मनुष्य का वास्तविक लक्ष्य है जिसे वह अपने आत्मस्वरूप के साथ पूर्णतया तादात्म्य स्थापित करके जी सकता है। समत्व भाव का वह जीवन जहाँ हम जीवन में आने वाली परिस्थितियों से अप्रभावित अपने मन और बुद्धि के साक्षी बनकर रहते हैं अहंकार की विस्मृति के क्षण हैं और तब हमारे कर्म उषकाल की जगमगाती आभा से समृद्ध होते हैं। सामान्य मनुष्य की धारणा होती है कि अहंकार के अभाव में हम कार्य करने में अकुशल या असमर्थ बन जायेंगे परन्तु यह मिथ्या धारणा है। प्रेरणा की आभा ही सामान्य सफलता को भी महान् उपलब्धि की ऊँचाई तक पहुँचाती है।
प्राचीन हिन्दू योगियों ने एक साधना का आविष्कार किया जिसके अभ्यास से मन और बुद्धि की युक्तता एवं समता सम्पादित की जा सकती है। इस साधना को योग कहते हैं। वैदिक काल के लोगों को इसका ज्ञान था तथा इसका अभ्यास करके वे योगी का जीवन जीते थे। उन्होंने असाधारण उपलब्धियों को अर्जित करके राष्ट्र के लिये स्वर्णयुग का निर्माण किया।
भारत जैसे देश में वैदिक काल में निश्चित ही आस्तिक दर्शन प्रचलित होगा परन्तु उसकी उपयोगिता जीवन के सभी क्षेत्रों में समान रूप से है। यदि उसकी सार्वक्षेत्रीय उपयोगिता न हो तो वह वास्तविक अर्थ में दर्शन ही नहीं है। अधिक से अधिक उसे किसी श्रेष्ठ पुरुष का जीवन विषयक मत माना जा सकता है जिसका सीमित उपयोग हो किन्तु तत्त्वज्ञान के रूप में वह कभी स्वीकार नहीं हो सकता।
अब तक के उपदेश में भगवान् ने वे सभी आवश्यक तर्क अर्जुन के समक्ष प्रस्तुत किये जिनको समझकर प्राप्त परिस्थितियों में स्वबुद्धि से उचित निर्णय लेने में वह समर्थ हो सके। सभी भौतिक परिस्थितियों के मूल्यांकन में केवल आध्यात्मिक दृष्टिकोण को ही अन्तिम प्रमाण नहीं माना जा सकता। जीवन की प्रत्येक परिस्थिति या चुनौती का मूल्यांकन आध्यात्मिक दृष्टि के साथसाथ बुद्धि के स्तर पर तर्क मन के स्तर पर नैतिकता और भौतिक स्तर पर परम्परा और सामाजिक रीति रिवाज की दृष्टि से भी करना आवश्यक है। इन सब के द्वारा बिना किसी विरोधाभास के यदि किसी एक सत्य का संकेत मिलता है तो निश्चय ही वह दिव्य मार्ग है जिस पर मनुष्य को प्रत्येक मूल्य पर चलने का प्रयत्न करना चाहिये।
केवल नैतिकता की भावना से युद्ध की ओर देखने से अर्जुन उस परिस्थिति को उचित रूप में समझ नहीं सका। शत्रुपक्ष में खड़े अपने ही बन्धुबान्धवों को विनष्ट करना नैतिकता के विरुद्ध था। किन्तु भावावेशजनित मन की भ्रमित अवस्था में उसने अन्य दृष्टिकोणों पर विचार नहीं किया जिससे वह पुन संयमित हो सकता था। ऐसे अवसर पर जो करने योग्य है वही करता हुआ अर्जुन भगवान् कृष्ण की शरण में जाता है। श्रीकृष्ण उसके मार्गदर्शन का उत्तरदायित्व अपने ऊपर लेकर जीवन के सभी दृष्टिकोणों को उसके सामने प्रस्तुत करते हैं। सम्पूर्ण गीता में श्रीकृष्ण मनुष्य को प्राप्त विवेकशील बुद्धि की भूमिका निभाते हैं जो कठोपनिषद् की भाषा में देहरूपी रथ का योग्य सारथि है।
इस प्रकार आध्यात्मिक बौद्धिक नैतिक और पारम्परिक दृष्टियों से विचार करने के पश्चात् पूर्व के श्लोक में भगवान अर्जुन को युद्ध करने की सम्मति देते हैं। जिस भावना से कर्म करना चाहिये उसका विवेचन इस श्लोक में श्रीकृष्ण ने किया है। शरीरादि अनात्म उपाधियों के साथ तादात्म्य करने से जो चिन्तायें विक्षेप व्याकुलतायें होती हैं उनसे ऊपर उठकर सभी विषम परिस्थितियों में समभाव में स्थित होकर कर्म करना चाहिये।
मन के समत्व भाव में रहने से जीवन की वास्तविक सफलता निश्चित होती है। इसके पूर्व हम देख चुके हैं कि जीवन में किस प्रकार पूर्व संचित वासनायें क्षीण हो सकती हैं। जगत् में सभी जीव अपनीअपनी वासनाओं का क्षय करने के लिये ही विभिन्न शरीर धारण किये हुये हैं। इस प्रकार वृक्ष पशु अथवा मनुष्य सभी वासनाओं के भण्डार हैं।
सब परिस्थितियों में समभाव में स्थित हुआ मन वासनाओं के निस्सारण का मार्ग बनता है। यह द्वार जब अहंकार और स्वार्थ से अवरुद्ध होता है तब वासनाक्षय के स्थान पर असंख्य नयी वासनाएँ उत्पन्न होती जाती हैं। द्वन्द्वों के कारण हुआ विक्षेप अहंकार के जन्म और वृद्धि के कारण है। कर्मयोग की भावना से कर्म करते हुये जीवन जीने पर अन्तकरण की शुद्धि प्राप्त होती है। इस कर्मयोग का विस्तृत विवेचन गीता के तृतीय अध्याय में है।
तत्त्वज्ञान और सामान्यजन की दृष्टि से विचार करने के पश्चात् भगवान् अर्जुन को कर्मयोग की भावना से युद्ध करने का उपदेश देते हैं। तत्त्वज्ञान को समझ कर उसे जीवन में जीना ही व्यावहारिक धर्म है।
अनित्य का पुनः जन्म कार्य कारण के सिंद्धांत के अनुसार उन अतृप्त वासनाओ के कारण होता है जिन्हें मृत्यु के पूर्व नित्य या शरीर नही कर पाता। यह श्लोक में सम भाव रखने का उपदेश अतृप्त भावनाओ को नियंत्रित करने की ओर एक कदम आगे बढ़ाता है जिस से हम मुक्त हो कर कर्म कर सके।
इसके पश्चात् इस अध्याय में वेदान्त ज्ञान का व्यवहार में उपयोग करने के उपायों एवं साधनों का निरूपण किया है।
।। हरि ॐ तत सत ।। 2.38 ।।
Complied by: CA R K Ganeriwala ( +91 9422310075)