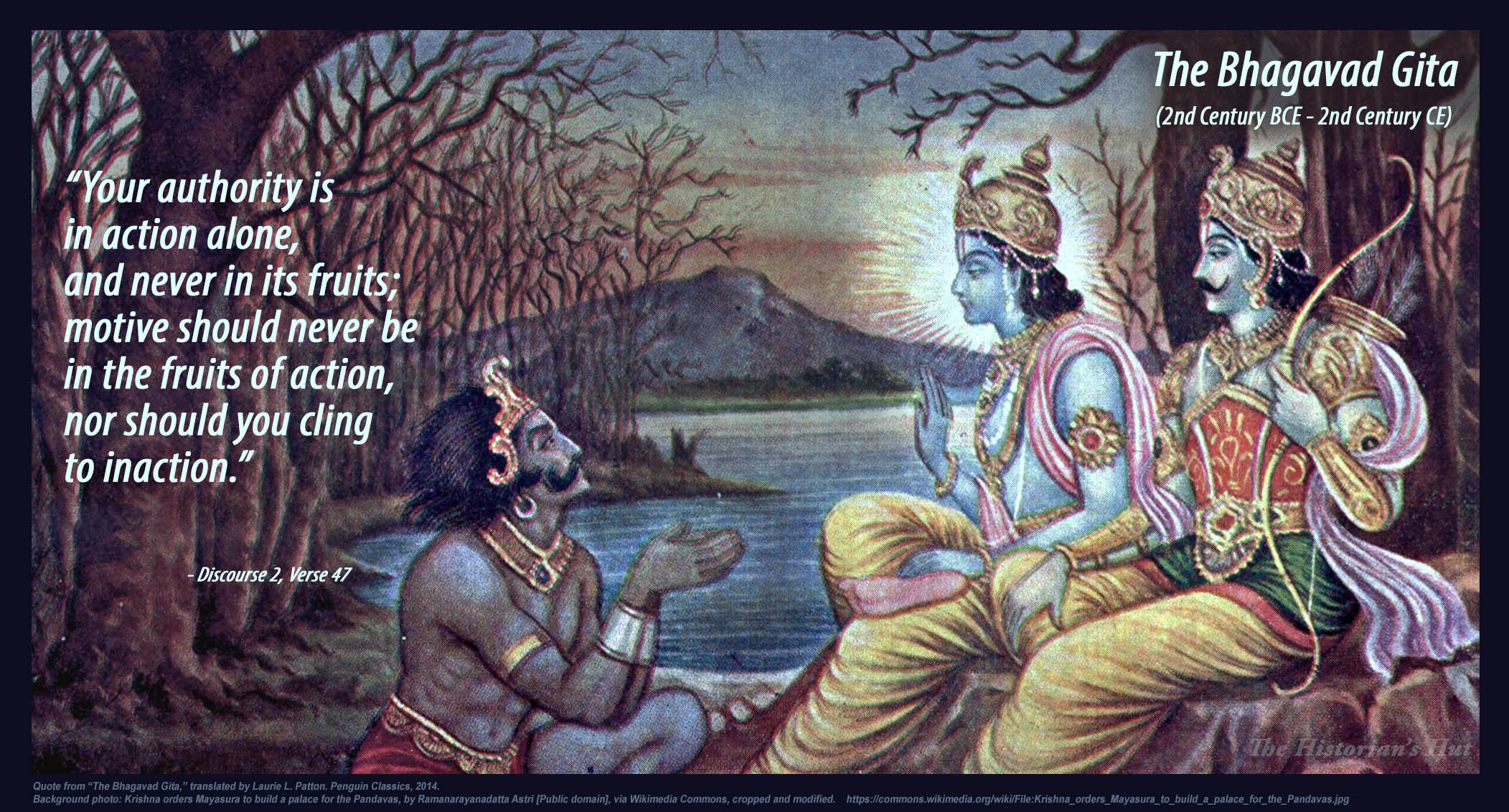।। Shrimadbhagwad Geeta ।। A Practical Approach ।।
।। श्रीमद्भगवत गीता ।। एक व्यवहारिक सोच ।।
।। Chapter 18.45 II
।। अध्याय 18.45 II
॥ श्रीमद्भगवद्गीता ॥ 18.45॥
स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धिं लभते नरः।
स्वकर्मनिरतः सिद्धिं यथा विन्दति तच्छृणु॥
“sve sve karmaṇy abhirataḥ,
saḿsiddhiḿ labhate naraḥ..।
sva- karma- nirataḥ siddhiḿ,
yathā vindati tac chṛṇu”..।।
भावार्थ:
अपने- अपने स्वाभाविक कर्मों में तत्परता से लगा हुआ मनुष्य भगवत्प्राप्ति रूप परमसिद्धि को प्राप्त हो जाता है। अपने स्वाभाविक कर्म में लगा हुआ मनुष्य जिस प्रकार से कर्म करके परमसिद्धि को प्राप्त होता है, उस विधि को तू सुन ॥४५॥
Meaning:
Engaged in his own duty, each person attains the foremost accomplishment. How one can attain this accomplishment by being content in his duty, that you hear from me.
Explanation:
The Vedas recognized the system of varna as a means for every individual to realize their potential. They enabled everyone to contribute to society as per their mental makeup and aptitude. Every action performed in accordance with one’s duty yielded a meritorious fruit or punya, and every, and every action that went against one’s duty yielded a demerit or a paapa. The net result of punyas and paapas decided the fate of every individual. One would gain a life that was better or worse than the current one based on their actions.
Swa-dharma is the prescribed duties based upon our guṇas and station in life. Performing them ensures that we use the potential abilities of our body and mind in a constructive and beneficial manner. This leads to purification and growth and is auspicious for the self and society. And since the prescribed duties are in accordance with our innate qualities, we feel comfortable and stable in discharging them. Then, as we enhance our competence, the swa-dharma also changes, and we step into the next higher class. In this manner, we keep advancing by dutifully executing our responsibilities.
Shri Krishna says whatever be the profession in which you are, you do not have to change at all. You have only to change the attitude with which you undertake those activities. He emphasises, to continue in your profession and to remain in your own profession. Selection of your profession always depends on your nature. You have develped certain nature by your hard work and dedication and some part of nature is inherent due to your birth in certain country means place, family and society or you can say, you get it from your ealier life as your fruit of karma.
1) Further, you have developed skill and excellence in any field only by long practice. If I keep on changing the profession, I will not get excellence in any field. Therefore, take your own time to choose the correct profession; but once you have chosen, you must be stick to it and do the hard work to touch the peak.
But there is more to the performance of duty than the cycle of action, reaction and rebirth. Shri Krishna says that performance of duty can become the gateway towards liberation. As we have seen earlier, the Gita enables each and every individual, regardless of their occupation or stage in life, to pursue the path of liberation. We do not have to renounce our actions and become sadhus or monks. We just have to keep doing our duty. The result of doing our duty is samsiddhi, perfection, the foremost accomplishment.
2) Shri Krishna says in one’s own chosen profession, He is always abhirataḥ; the word abhiratah means one should learn to be fully involved with fully dedication. You do more and more research in improving the quality and in improving the facility.
3) Therefore in any field choosen by you, you can try to put your heart and soul, i.e. the meaning of the word; “abhirataḥ;” ’रं’ raṁ means reveling, enjoying, abhiraṁ, intimately enjoying; which means putting your heart and soul, in whatever you are undertaking; abhirataḥ; by taking to that and then convert Karma into karma yōga, you do not have to change your profession.
It is also be noted, if you have selected wrong profession, in which you do not have any interest, but as inherentance business, you have to go for profession according to your swadharma first. because your profession needs dedication.
4) By changing the attitude and by doing it properly you can gradually grow spiritually. Even the most worldly activity can contribute to inner growth; if it is properly handled. It brings you towards purity of mind, or to put in technical language, sādhanā catuṣṭaya saṁpathi or to put in another language, jñāna yōgyatha; or to put it in another language, more and more interest in spiritual knowledge. So, interest in spritual knowledge should increase, that is the indication of successful karma yōga.
The ultimate goal of karma yoga is purification of the mind. It cleans the mind of all its impurities in the form of selfish desires created by raaga and dvesha, likes and dislikes. It is this purification of the mind that becomes the foremost accomplishment, samsiddhi, for one who is performing karma yoga. But mere performance of duty will not result in samsiddhi. There is something else needed, which Shri Krishna will reveal in the next shloka.
।। हिंदी समीक्षा ।।
वेदों ने वर्ण व्यवस्था को हर व्यक्ति के लिए अपनी क्षमता को साकार करने के साधन के रूप में मान्यता दी। उन्होंने हर किसी को अपनी मानसिक बनावट और योग्यता के अनुसार समाज में योगदान करने में सक्षम बनाया। अपने कर्तव्य के अनुसार किए गए हर कार्य से पुण्य मिलता है और अपने कर्तव्य के विरुद्ध किए गए हर कार्य से पाप या पाप मिलता है। पुण्य और पाप का कुल परिणाम हर व्यक्ति के भाग्य का फैसला करता है। अपने कर्मों के आधार पर व्यक्ति को वर्तमान जीवन से बेहतर या बदतर जीवन मिलता है।
नियत कर्म प्रकृति के गुणों से तय होती है, अतः वर्ण व्यवस्था में प्रत्येक गुण के लिये आवश्यक तत्व जान लेने के बाद भगवान श्री कृष्ण सभी वर्णों को समान सम्मान देते हुए मुक्ति का मार्ग बतलाते है। वह कहते है कि मनुष्य की जैसी स्वतःसिद्ध स्वाभाविक प्रकृति (स्वभाव) है, उस में अगर वह कोई नयी उलझन पैदा न करे, रागद्वेष न करे तो वह प्रकृति उसका स्वाभाविक ही कल्याण कर दे। तात्पर्य है कि प्रकृति के द्वारा प्रवाह रूप से अपने आप होनेवाले जो स्वाभाविक कर्म हैं, उन का स्वार्थ त्यागपूर्वक प्रीति और तत्परता से आचरण करे परन्तु कर्मों के प्रवाह के साथ न राग हो, न द्वेष हो और न फलेच्छा हो। रागद्वेष और फलेच्छा से रहित होकर क्रिया करने से करने का वेग शान्त हो जाता है और कर्म में आसक्ति न होने से नया वेग पैदा नहीं होता। इस से प्रकृति के पदार्थों और क्रियाओँ के साथ निर्लिप्तता (असंगता) आ जाती है। निर्लिप्तता होने से प्रकृति की क्रियाओं का प्रवाह स्वाभाविक ही चलता रहता है और उन के साथ अपना कोई सम्बन्ध न रहने से साधक की अपने स्वरूप में स्थिति हो जाती है, जो कि प्राणिमात्र की स्वतःस्वाभिवक है। अपने स्वरूप में स्थिति होने पर उस का परमात्मा की तरफ स्वाभाविक आकर्षण हो जाता है। परन्तु यह सब होता है कर्मों में अभिरति होने से, आसक्ति होने से नहीं।
स्व-धर्म हमारे गुणों और हमारे जीवन की अवस्थाओं पर आधारित निर्धारित कर्त्तव्य है। इन्हें सम्पन्न करना यह सुनिश्चित करता है कि हम अपने शरीर और मन की सशक्त योग्यताओं का उपयोग रचनात्मक और लाभदायक ढंग से करते हैं। यह शुद्धिकरण और विकास की ओर ले जाता है और समाज एवं आत्मा के लिए शुभ होता है। चूंकि हमारे निर्धारित कर्त्तव्य हमारे जन्मजात गुणों के अनुरूप होते हैं इसलिए इनका निर्वहन करने में हम स्वयं को संतुलित और सहज अनुभव करते हैं। फिर जब हमारी क्षमता बढ़ती है तब स्व-धर्म भी परिवर्तित हो जाता है और हम अगली उच्च कक्षा में प्रवेश करते हैं। इस प्रकार से हम अपने उत्तरदायित्व का निष्ठापूर्वक निर्वहन कर उन्नति की ओर अग्रसर होते हैं।
उदाहरण के तौर पर वैश्य वर्ण के गुण वाला व्यक्ति यदि क्षत्रिय धर्म को स्वीकार भी करे तो शौर्य, तेज अभाव एवम प्राणों के प्रति मोह के रहते वह उस कार्य में सफल नही होगा। यदि शुद्र व्यक्ति ब्राह्मण का या ब्राह्मण शुद्र का कार्य करे तो सात्विकता एवम तामसी विरोधाभासी के गुण के कारण दोनों ही अपने कार्यो के प्रति न्याय नहीं कर सकते।
श्री कृष्ण कहते हैं कि आप जिस भी पेशे में हों, आपको बिल्कुल भी बदलने की जरूरत नहीं है। आपको केवल उस दृष्टिकोण को बदलना है जिसके साथ आप उन गतिविधियों को करते हैं। वह इस बात पर जोर देते हैं कि अपने पेशे को जारी रखें और अपने पेशे में ही बने रहें। आपके पेशे का चयन हमेशा आपके स्वभाव पर निर्भर करता है। आपने अपनी मेहनत और लगन से एक निश्चित स्वभाव विकसित किया है और स्वभाव का कुछ हिस्सा आपके किसी खास देश यानी स्थान, परिवार और समाज में जन्म लेने के कारण अंतर्निहित है या आप कह सकते हैं, यह आपको अपने पिछले जीवन से कर्म के फल के रूप में मिलता है।
1) इसके अलावा, आपने केवल लंबे अभ्यास से ही किसी भी क्षेत्र में कौशल और उत्कृष्टता विकसित की है। अगर मैं पेशा बदलता रहूँगा, तो मुझे किसी भी क्षेत्र में उत्कृष्टता नहीं मिलेगी। इसलिए, सही पेशा चुनने के लिए अपना समय लें; लेकिन एक बार आपने जो पेशा चुन लिया है, आपको उस पर टिके रहना चाहिए और शिखर को छूने के लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए। ध्यान रहे, अपना पेशा अपने गुण धर्म के अनुसार ही चुना जाना चाहिए, यदि वह आप के गुण धर्म के अनुकूल नहीं है तो सब से पहले गुण धर्म के अनुसार पेशे को चुनो।
2) श्री कृष्ण कहते हैं कि अपने चुने हुए पेशे में, वह हमेशा अभिरत: होता है; अभिरत: शब्द का अर्थ है कि व्यक्ति को पूरी तरह से समर्पित होकर उसमें शामिल होना सीखना चाहिए। आप गुणवत्ता सुधारने और सुविधा सुधारने के लिए अधिक से अधिक शोध करें।
3) इसलिए आपके द्वारा चुने गए किसी भी क्षेत्र में, आप अपना दिल और आत्मा लगाने की कोशिश कर सकते हैं, यानी शब्द का अर्थ; “अभिरत:” ‘रं’ रं का अर्थ है आनंद लेना, आनंद लेना, अभिरम, अंतरंग रूप से आनंद लेना; जिसका अर्थ है कि आप जो भी कर रहे हैं, उसमें अपना दिल और आत्मा लगाना; अभिरत:, इसे अपनाकर और फिर कर्म को कर्म योग में परिवर्तित करके, आपको अपना पेशा बदलने की ज़रूरत नहीं है।
4) दृष्टिकोण बदलकर और इसे ठीक से करने से आप धीरे-धीरे आध्यात्मिक रूप से विकसित हो सकते हैं। यहां तक कि सबसे सांसारिक गतिविधि भी आंतरिक विकास में योगदान दे सकती है; अगर इसे ठीक से संभाला जाए। यह आपको मन की शुद्धता की ओर ले जाता है या तकनीकी भाषा में कहें तो, साधना चतुष्टय संपथि या दूसरी भाषा में कहें तो, ज्ञान योग् या दूसरे शब्दों में कहें तो आध्यात्मिक ज्ञान में अधिक से अधिक रुचि। इसलिए आध्यात्मिक ज्ञान में रुचि बढ़नी चाहिए, यही सफल कर्म योग का संकेत है।
प्रकृति के अनुसार नियत कर्म करने से एकाग्रता एवम उस कार्य मे दक्षता रहती है, अंतर काम करते समय की भावना का है, की वह आसक्ति एवम कर्तृत्त्व भाव के साथ है या उस से मुक्त। जीव प्रकृति से बंधा हुआ भी इन्ही कारणों से है।
अतः वर्णों के वर्गीकरण से अपना नियत कर्म ही तय होता है, कोइ उच्च नीच नही। सामाजिक कुरीति वर्ण व्यवस्था में कुछ ही लोगों द्वारा आसक्ति एवम मोह से उत्पन्न की हुई है।
अपने स्वभाव एवं विकास की स्थिति को पहचान कर प्रत्येक व्यक्ति को अपने स्वाभाविक कर्म का निष्ठापूर्वक पालन करना चाहिए। इसी कर्तव्य पालन से प्रथम चित्तशुद्धि एवं तदुपरान्त परमात्मस्वरूप की अनुभूति की संसिद्धि प्राप्त हो सकती है। केवल सतही दृष्टिकोण से अवलोकन करने पर मनुष्यों का उपर्युक्त चतुर्विध वर्गीकरण स्पष्टत बोधगम्य नहीं हो सकता। परन्तु जीवन में श्रेष्ठ उपलब्धियों को प्राप्त किये महान् पुरुषों के जीवन चरित्र इस वर्गीकरण की सत्यता का बारम्बार उद्घोष करते हैं। वर्ण व्यवस्था जन्म से तय नहीं होती, इस को प्रकृति बार बार अन्तःकरण में कुदेरती रहती है, जिसे प्राप्त कर के नियत कर्म में लगना आवश्यक है।
स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने यादव कुल में जन्म ले कर विभिन्न वर्णों के नियत कर्म निसंकोच करते हुए, एक उदाहरण दिया।
एक छोटे से बालक ने भेड़ पालन के कार्य को अस्वीकार कर दिया और पेरिस जा पहुँचा, जो कालान्तर में विश्व में नेपोलियन के नाम से प्रसिद्ध महानतम सेनापति बना।
गोल्डस्मिथ या कीट्स व्यापारिक कार्य द्वारा आराम एवं सुख सुविधाओं का जीवन जीने की अपेक्षा किसी अटारी में रहते हुए काव्य रचना करना अधिक पसन्द करेगा।
प्रत्येक मनुष्य अपने स्वभाव के अनुरूप कार्यक्षेत्र में कर्म करते हुए ही सुख एवं पूर्णता का अनुभव करता है। मानव के लौकिक व्यवहार, मानसिक स्वभाव एवं बौद्धिक अभिरुचि के आधार पर किया गया यह विवकपूर्ण वर्गीकरण केवल भारत में ही नहीं, वरन् सर्वत्र प्रयोज्य (लागू करने योग्य) है। जीवन में इस की प्रयोज्यता तथा मनुष्य के विकास के लिए इसकी उपादेयता सार्वभौमिक है।
जो माँ-बाप बच्चों को स्वावभिक रूप में बढ़े होने की अपेक्षा अपनी इच्छा के अनुरूप शिक्षित बिना संस्कारो, ज्ञान, तप एवम बुद्धि- धृति के विकास के करना चाहते है, वो उन के मोक्ष में मार्ग में बाधक ही बनते है।
अपने कर्मों में प्रीतिपूर्वक तत्परता से लगा हुआ मनुष्य परमात्मा को किस प्रकार प्राप्त होता है एवम कर्ममात्र परमात्मा प्राप्ति का साधन है, इस बात को आगे पढ़ कर समझते है।
।। हरि ॐ तत सत ।। गीता – 18.45।।
Complied by: CA R K Ganeriwala (+91 9422310075)