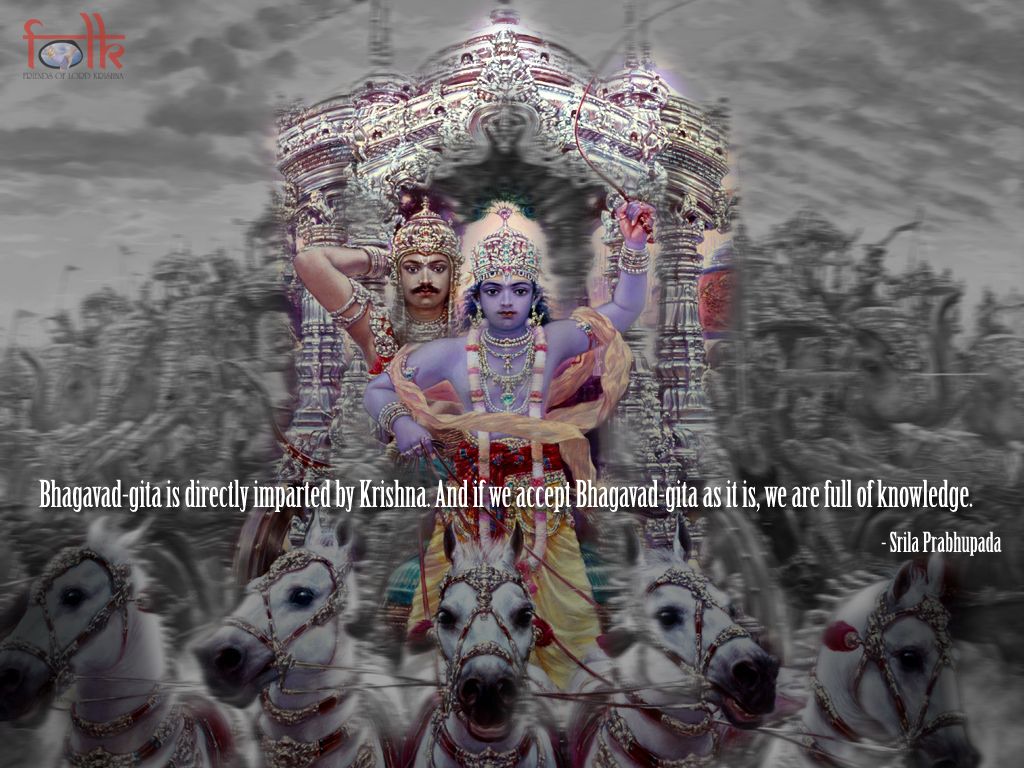।। श्रीमद्भगवत गीता ।। एक व्यवहारिक सोच ।।
।। Chapter 18.24 II
।। अध्याय 18.24 II
॥ श्रीमद्भगवद्गीता ॥ 18.24॥
यत्तु कामेप्सुना कर्म साहङ्कारेण वा पुनः।
क्रियते बहुलायासं तद्राजसमुदाहृतम्॥
‘yat tu kāmepsunā karma,
sāhańkāreṇa vā punaḥ..।
kriyate bahulāyāsaḿ,
tad rājasam udāhṛtam”..।।
भावार्थ:
परन्तु जो कर्म बहुत परिश्रम से युक्त होता है तथा भोगों को चाहने वाले पुरुष द्वारा या अहंकारयुक्त पुरुष द्वारा किया जाता है, वह कर्म राजस कहा गया है ॥२४॥
Meaning:
But that action performed by a person desiring pleasure, or with egoism, with exertion, that is called raajasic.
Explanation:
To understand raajasic action, we need to revisit the notion of raajasic knowledge. As we saw earlier, raajasic knowledge presents a highly fragmented, chopped-up version of the world. It gives reality to the differences created by the senses and the mind. Additionally, it gives different “values” to objects, people and situations perceived by the senses and the mind. Simply put, we either like, dislike, or are indifferent to objects, people and situations. A classic example is the precious stone that is liked by its owner, disliked by the owner’s enemy, and treated with indifference by a monk.
The nature of rajo guṇa is that it creates intense desires for materialistic enhancement and sensual enjoyment. So, action in the mode of passion is motivated by huge ambition and characterized by intense effort. It entails heavy toil and great physical and mental fatigue.
Such raajasic knowledge results in commencement of raajasic action. Shri Krishna says that a raajasic action is begun in pursuit of an object, person or situation that will give pleasure to the doer of the action. It involves exertion of mental or physical effort, and therefore, the mind is good at calculating how much effort is needed for acquiring one object versus the other. Another aspect of the raajasic action is that the I, the ego, is given a lot of prominence. We want the entire world to know that we helped such and such person, or we did someone a favour. Unfortunately, such thinking interferes with the action, causing us to shift our attention from the action to the ego.
Let’s constrast this with saattvic action. Instead of pursuing an object of pleasure, a saattvic action is done with a sense of duty. There is no calculation that weighs the effort needed for object a verse the effort needed for object b. All actions happen spontaneously. Also, there is no sense of egoism. Instead, there is a firm understanding that the action is being performed by me who is an instrument, a nimiitta, of Ishvara. This lack of egoistic thinking makes the actions more efficient. In fact, people with high degrees of sattva are the most productive, simply because they are performing their svadharma with no ulterior motive.
In present world, the life we live under stress and mental fatigue. The reason behind is the social status competition among the people and family of a person always taunt for progress by his friends, brothers and other person in form of big house, high post, cars, jewellaries, parties and bank balances. The person always finds himself in race of competition and this gives him nothing but stress, mental fatigue and various deceases. Where in satvik Guna, the same work has been performed without any desire as duty.
An example of rājasic action is the corporate world. Management executives regularly complain of stress. This is because their actions are usually motivated by pride and an inordinate ambition for power, prestige, and wealth. The efforts of political leaders, over-anxious parents, and businesspersons are also often typical examples of actions in the mode of passion.
।। हिंदी समीक्षा ।।
रजो गुण की प्रकृति ऐसी है कि यह भौतिक सुख-सुविधाओं और कामुक भोगों की तीव्र इच्छाएँ पैदा करता है। इसलिए, रजोगुण में किया गया कार्य अत्यधिक महत्वाकांक्षा से प्रेरित होता है और तीव्र प्रयास की विशेषता रखता है। इसमें भारी परिश्रम और अत्यधिक शारीरिक और मानसिक थकान शामिल है।
सात्विक कर्म को ही यदि कर्ता यदि अधिक परिश्रम, अहंकार एवम फलाशा के साथ करे तो उस कर्म का प्रकार सात्विक न हो कर राजसी हो जाता है। किसी भी कर्म को सात्विक, राजसी या तामसी वर्गीकरण कर्म के आधार पर नही किया जा सकता है, उस का आधार कर्ता की वह मानसिक बुद्धि एवम ज्ञान है, जिस के आधार पर वह कर्म करता है। इसलिए जब तक बुद्धि समभाव की नही होती, कर्म भी सात्विक नही हो सकता।
वेदशास्त्र को जाननेवाले लौकिक निरहंकारी ही आत्मतत्व को जानता है, इसलिये उस से अपेक्षा है क्योंकि जो वास्तविक निरहंकारी आत्मवेत्ता हो, उस में तो फलेच्छुकता और बहुत परिश्रमयुक्त कर्तृत्व की आशंका ही नहीं हो सकती। किंतु सात्त्विक कर्म का भी कर्ता, आत्मतत्त्व को न जाननेवाला अहंकारयुक्त मनुष्य ही होता है, फिर राजस- तामस कर्मों के कर्ता की तो बात ही क्या है संसार में आत्मतत्त्व को न जाननेवाला भी, वेदशास्त्रका ज्ञाता पुरुष निरहंकारी कहा जाता है। जैसे अमुक ब्राह्मण निरहंकारी है ऐसा प्रयोग होता है। ऐसे पुरुष की अपेक्षा से ही इस श्लोक में साहंकारेण वा यह वचन कहा गया है अर्थात जिस मनुष्य का शरीर मे अभिमान है और जो प्रत्येक कर्म को अहंकार पूर्वक करता है तथा मन एवम वाणी से इस तरह के वचन कहता है कि यह काम मैंने मेहनत एवम अथक प्रयासों से किया है, मुझे इस काम के लिये अमुक पद या परिश्रम मिलना चाहिये, वह कर्म राजस कहा गया है। इसलिये मात्र वेदशास्त्र का ज्ञान रखने वाला, अच्छे वचन बोलने वाला और अच्छे आचरण से मनुष्य सात्विक हो सकता है, परंतु कर्तृत्त्व भाव होने से आत्मतत्त्व वेत्ता नहीं हो सकता। उस के सभी कर्म राजस श्रेणी में आते है।
शरीर के सुख आराम की मुख्यता होने से फलेच्छा की अवहेलना हो जाती है और फलेच्छा की मुख्यता होने से शरीर के सुख आराम की अवहेलना हो जाती है। लोगों के सामने कर्म करते समय अहंकारजन्य सुख की खुराक मिलने से और शरीर के सुख आराम की मुख्यता न होने से राजस मनुष्य को कर्म करने में परिश्रम नहीं मालूम देता। परन्तु एकान्त में कर्म करते समय अहंकारजन्य सुख की खुराक न मिलने से और शरीर के सुख आराम की मुख्यता होने से राजस मनुष्य को कर्म करने में ज्यादा परिश्रम मालूम देता है।
लोगों के सामने कर्म करने से लोग देखते हैं और वाहवाह करते हैं तो अभिमान आता है और जहाँ लोग सामने नहीं होते, वहाँ (एकान्त में) कर्म करने से दूसरों की अपेक्षा अपने में विलक्षणता, विशेषता देखकर अभिमान आता है। जैसे दूसरे आदमी हमारी तरह सुचारुरूप से साङ्गोपाङ्ग कार्य नहीं कर सकते हमारे में काम करने की जो योग्यता, विद्या, चतुरता आदि है, वह हरेक आदमी में नहीं मिलेगी हम जो भी काम करते हैं, उसको बहुत ही ईमानदारी से और जल्दी करते हैं, आदिआदि।
क्योंकि राजस कर्म में फलाशा होती है, इसलिए व्यापारी, किसान या व्यवसाय करने वाले शरीर, धन और समय की परवाह किए बेगेर अधिक से अधिक कार्य पर ध्यान देते है। कभी कभी कर्जा भी ले कर कार्य करते है। इसलिए राजस कर्म में अत्यधिक दबाव एवम तनाव, कष्ट, सामाजिक, कानूनी और आर्थिक नीतियों का उल्लघंन भी होता है। शारीरिक स्वास्थ्य भी खराब रहता है। कार्य करने वाला चिंता और क्रोध से घिर जाता है। कर्ता भाव और कर्म से प्राप्त फलों मुझे ही भोगने को मिले, यह आशा बनी रहती है।
वर्तमान दुनिया में हम जिस तरह से तनाव और मानसिक थकान में जी रहे हैं, उसका कारण है सामाजिक प्रतिष्ठा की होड़, परिवार के लोग और व्यक्ति हमेशा अपने दोस्तों, भाइयों और दूसरे लोगों से बड़े घर, उच्च पद, गाड़ी, गहने, पार्टी और बैंक बैलेंस के रूप में आगे बढ़ने का ताना मारते रहते हैं। व्यक्ति हमेशा खुद को प्रतिस्पर्धा की दौड़ में पाता है और इससे उसे तनाव, मानसिक थकान और कई तरह की बीमारियाँ ही मिलती हैं। जबकि सात्विक गुण में वही काम बिना किसी इच्छा के कर्तव्य के रूप में किया जाता है।
इस श्लोक का अर्थ स्पष्ट है। वर्तमान समय मे राजनीतिक नेताओं, सामाजिक कार्यकर्ताओं, बड़े बड़े उद्योगपतियों अत्यधिक चिन्तित पालकों, कट्टर धर्म प्रचारकों, धर्म परिवर्तन कराने वाली मिशनरियों तथा अन्धाधुन्ध धन कमाने वालों के प्राय समस्त कर्म राजस श्रेणी में ही आते हैं। कभी कभी तो वे तमोगुण के स्तर तक भी गिर जाते हैं।
राजसिक क्रिया का एक उदाहरण कॉर्पोरेट जगत है। प्रबंधन अधिकारी नियमित रूप से तनाव की शिकायत करते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि उनके कार्य आमतौर पर गर्व और शक्ति, प्रतिष्ठा और धन की अत्यधिक महत्वाकांक्षा से प्रेरित होते हैं। राजनीतिक नेताओं, अत्यधिक चिंतित माता-पिता और व्यवसायियों के प्रयास भी अक्सर जुनून की स्थिति में किए जाने वाले कार्यों के विशिष्ट उदाहरण हैं।
।। हरि ॐ तत सत ।। गीता – 18.24 ।।
Complied by: CA R K Ganeriwala (+91 9422310075)