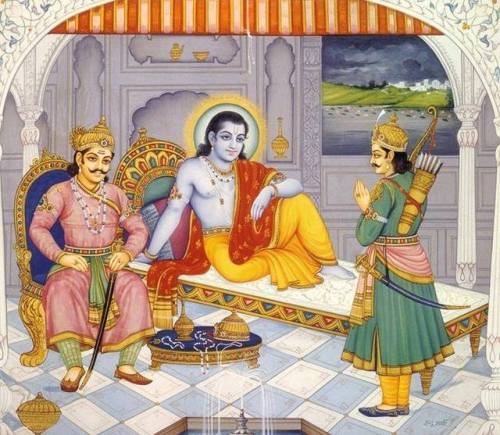।। Shrimadbhagwad Geeta ।। A Practical Approach ।।
।। श्रीमद्भगवत गीता ।। एक व्यवहारिक सोच ।।
।। Chapter 17.17 II
।। अध्याय 17.17 II
॥ श्रीमद्भगवद्गीता ॥ 17.17॥
श्रद्धया परया तप्तं तपस्तत्त्रिविधं नरैः ।
अफलाकाङ्क्षिभिर्युक्तैः सात्त्विकं परिचक्षते॥
“śraddhayā parayā taptaḿ,
tapas tat tri- vidhaḿ naraiḥ..।
aphalākāńkṣibhir yuktaiḥ,
sāttvikaḿ paricakṣate”..।।
भावार्थ:
पूर्ण श्रद्धा से युक्त होकर मनुष्यों द्वारा बिना किसी फल की इच्छा से उपर्युक्त तीनों प्रकार से जो तप किया जाता है उसे सात्विक (सतोगुणी) तप कहा जाता है।(१७)
Meaning:
This threefold penance, performed by balanced people with supreme faith, without expectation of reward, is called sattvic.
Explanation:
So far, we saw that tapas or penance comprises three aspects. Bodily or shaaririka tapas, speech or vaangmaya tapas, and mental or maanasika tapas. Tapas is used to conserve and channel our energy in the pursuit of a goal or objective, whether it be material or spiritual. Shri Krishna now describes three types of tapas, and how they can be used to assess the texture of our faith. He first describes the conditions under which penance is revealed to be sattvic.
The unique nature of sattvic tapas is that it is performed in the pursuit of the highest possible goal, which is self-realization. It is not performed for any material gain, or the pursuit of physical or mental powers. Furthermore, it is performed with the utmost faith in the statements of the scriptures. Shri Krishna uses the word naraha or human in this shloka, and not in the shlokas that described the other two types of penance. He implies that only humans have the ability to perform penance without expectation of material gain.
Who has the ability to perform this highest level of penance, this sattvic penance? It is one who is yukta, one who has integrated his mind with his intellect, one who can remain balanced in success and failure. Only such a person is able to incorporate all the three aspects of penance, physical, mental and speech, referred in the shloka as three-fold. Even if one of these is missing, the tapas lose its sattvic aspects. Mental penance is the toughest of all the three, since it is hardest to conquer the mind.
।। हिंदी समीक्षा ।।
पूर्व में तप के कायिक, वाचिक और मानसी यह तीन स्वरूप बताने के बाद भगवान श्रीकृष्ण कहते है कि तीनो प्रकार के तप से युक्त श्रद्धा ही पराश्रद्धा अर्थात उत्कृष्ट श्रद्धा है, यह जिस किसी की भी हो वह उस से सत्य की प्राप्ति कर सकता है और सत्य ही ब्रह्म है। अतः फलाकांक्षा से रहित यह तप परम पुरुष की आराधना मानते हुए, जो मनुष्य उत्कृष्ट श्रद्धा से युक्त त्रिविध तप शरीर, मन और वाणी के द्वारा तपता है, उसे सात्विक कहते है।
फलाकांक्षा से रहित और श्रद्धा से युक्त में युक्त शब्द को समझना भी आवश्यक है। जिस का मन, बुद्धि और इंद्रियां अनासक्त, निगृहीत तथा शुद्ध होने के कारण, कभी किसी भोग के सबंध से विचलित नहीं हो सकते हो, जिस में आसक्ति का सर्वथा अभाव हो गया हो, उसे ही युक्त कहा जाता है। युक्त होना ही निष्काम होने का प्रथम चरण है। अनासक्त होना और आलसी होना, दोनों में अंतर निष्काम कर्म का होना ही है।
इसे निस्वार्थ भाव से, बिना किसी पुरस्कार की आसक्ति के किया जाना चाहिए। साथ ही, तपस्या के मूल्य पर हमारा विश्वास सफलता और असफलता दोनों में ही दृढ़ रहना चाहिए, तथा आलस्य या असुविधा के कारण इसका अभ्यास स्थगित नहीं करना चाहिए। निस्वार्थ का अर्थ मोक्ष या चित्तशुद्धि की भी कोई अभिलाषा नहीं होना। शुद्ध सात्विक प्रेम की भांति जिस में कोई आकांक्षा नहीं हो।
योगयुक्त पुरुष सात्त्विक होते है, जो भविष्य में प्राप्त होने वाले फलों की कदापि चिन्ता नहीं करते हैं। वे जानते हैं कि प्रकृति में सामञ्जस्य और नियमबद्धता है। अत, वर्तमान काल की दशा से प्रभावित हुआ सम्पूर्ण भूतकाल का परिणामी फल ही भविष्य होता है, वे इस तथ्य से भलीभांति परिचित होते हैं। वर्तमान की कर्म कुशलता पर ही भावी फल निर्भर करता है। इसलिए फल की चिन्ता कर के वर्तमान के सुअवसरों को खोना मूढ़ता का ही लक्षण है। सात्त्विक पुरुष फलासक्ति का त्याग कर त्रिविध तप का आचरण करते हैं जिस का उन्हें स्वत: ही सर्वाधिक फल प्राप्त होता है।
यहाँ केवल सात्त्विक तप में त्रिविध पद दिया है और राजस तथा तामस तप में,त्रिविध पद न देकर यत्तत् पद दे कर ही काम चलाया है। इसका आशय यह है कि शारीरिक, वाचिक और मानसिक, तीनों तप केवल सात्त्विक में ही साङ्गोपाङ्ग आ सकते हैं, राजस तथा तामस में तो आंशिक रूप से ही आ सकते हैं। इस में भी राजस में कुछ अधिक लक्षण आ जायँगे क्योंकि राजस मनुष्य का शास्त्रविधि की तरफ खयाल रहता है। परन्तु तामस में तो उन तपों के बहुत ही कम लक्षण आयँगे क्योंकि तामस मनुष्यों में मूढ़ता, दूसरों को कष्ट देना आदि दोष रहते हैं।
तेरहवें अध्याय में सातवें से ग्यारहवें श्लोक तक जो ज्ञान के बीस साधनों का वर्णन आया है, उन में भी शारीरिक तप के तीन लक्षण – शौच, आर्जव और अहिंसा तथा मानसिक तप के दो लक्षण – मौन और आत्मविनिग्रह आये हैं। ऐसे ही सोलहवें अध्याय में पहले से तीसरे श्लोक तक जो दैवीसम्पत्ति के छब्बीस लक्षण बताये गये हैं, उन में भी शारीरिक तप के तीन लक्षण – शौच, अहिंसा और आर्जव तथा वाचिक तप के दो लक्षण – सत्य और स्वाध्याय आये हैं। अतः ज्ञान के जिन साधनों से तत्त्वबोध हो जाय तथा दैवीसम्पत्ति के, जिन गुणों से जीव को मुक्ति प्राप्त हो जाय, वे लक्षण या गुण राजस-तामस नहीं हो सकते। इसलिये राजस और तामस तप में शारीरिक, वाचिक और मानसिक – यह तीनों प्रकार का तप साङ्गोपाङ्ग नहीं लिया जा सकता।
त्रिविध तप में निष्काम होना और कर्म करना ही प्रमुख है।शरीर, वाणी और मन के द्वारा जो तप किया जाता है, वह तप ही मनुष्यों का सर्वश्रेष्ठ कर्तव्य है और यही मानवजीवन के उद्देश्य की पूर्ति का अचूक उपाय है । तप के शाब्दिक अर्थ में तपना लिया जाता है, आज के युग में श्रद्धा के साथ त्रिविध हो कर रहना, अत्यंत दुष्कर है, इसलिए इसे तप का नाम दिया है। हमे जब यह मालूम हो, कि जाना कहां है, तो हम उस स्थान के लिए कदम बढ़ा सकते है। भौतिकवाद और स्वार्थ के युग में सात्विक त्रिविध पद के अनुसार व्यवहार करते हुए रहना, किसी एकांत में बैठ कर आंखे बंद कर के, ध्यान या मनन करने से अत्यंत कठिन है। अर्जुन युद्ध भूमि में युद्ध के लिए खड़ा है, युद्ध करना कर्तव्य धर्म है, किंतु युद्ध करते हुए शारीरिक, मानसिक और व्यवहारिक स्थिति में श्रद्धा और विश्वास किस प्रकार का हो, जिस से युद्ध के परिणाम में निष्काम भाव बना रहे, तो उस का स्वरूप यही सात्विक गुण का तप है।
युद्ध ही क्यों, जब आप व्यापार , व्यवसाय , राजनीति, वकील, CA, नौकरी आदि करते हुए, किसी को कष्ट पहुंचाने, लोभ, स्वार्थ या अधिक धन कमाने के उद्देश्य से किसी को परेशान नहीं करते, जो व्यवहारिक और उचित है, उसी के अनुसार व्यवहार करते है, तो आप त्रिविध तप ही करते है, क्योंकि व्यवसाय की मर्यादा के अनुसार कार्य करना, कर्तव्य धर्म है। व्यवहार में अपेक्षा रहती ही है, किंतु अपेक्षा की परिणीति असंतोष, प्रेम, विश्वास, द्वैष, क्रोध, ईर्ष्या, में न हो कर निष्काम स्थितप्रज्ञ भाव में रहे, तो यह तप ही है।
कर्म के सत और असत का विवेचन भी इसी अध्याय के अंत मे किया गया है। श्रद्धा से युक्त विविध कर्मो के प्रकार समझने के बाद ही हम इस को समझ पाएंगे। यदि श्रद्धा युक्त तप निष्काम नही है तो यह तप क्या कहलाता है, इसे आगे पढ़ते है।
।। हरि ॐ तत सत ।। गीता – 17.17।।
Complied by: CA R K Ganeriwala (+91 9422310075)