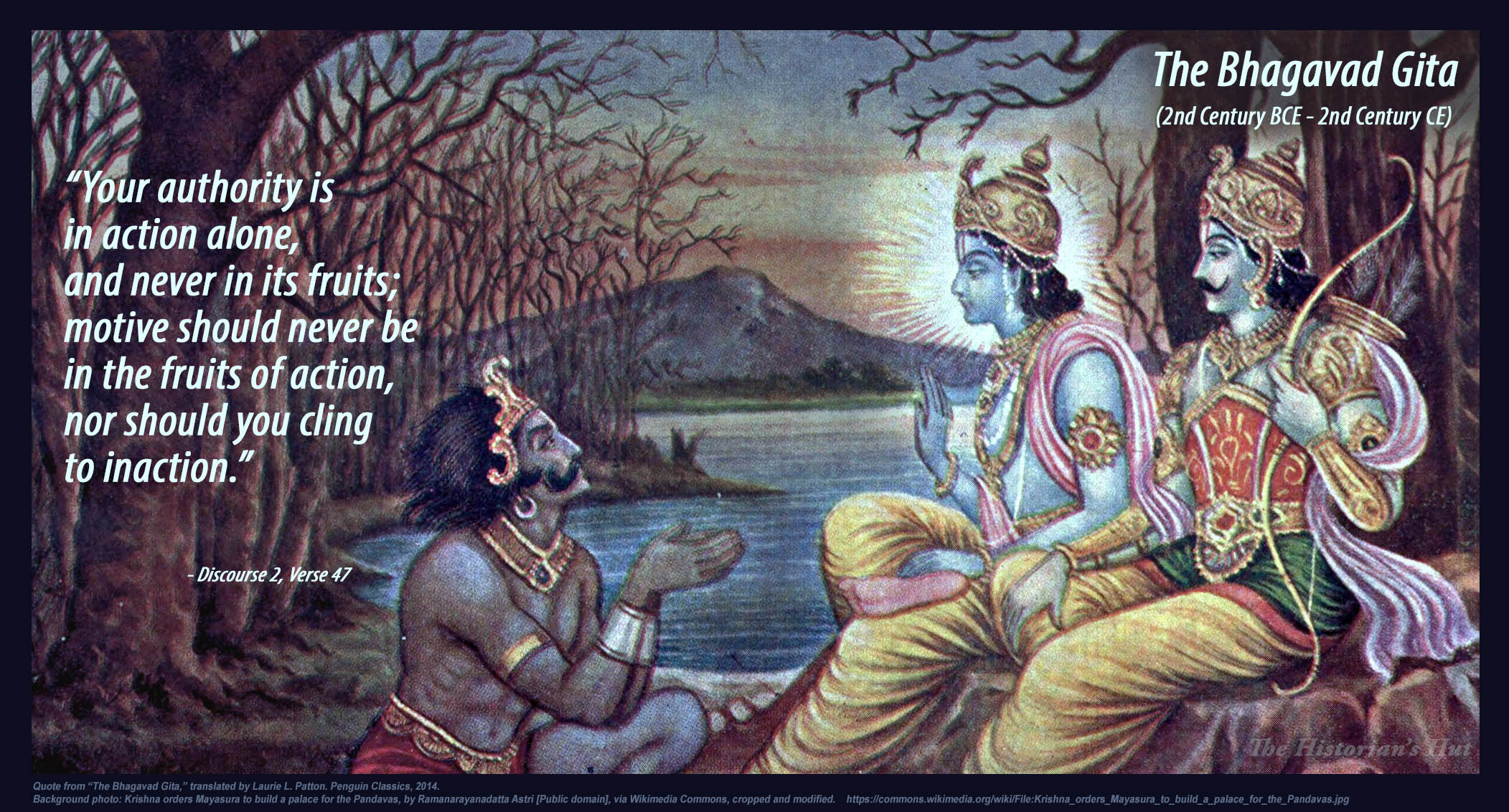।। Shrimadbhagwad Geeta ।। A Practical Approach ।।
।। श्रीमद्भगवत गीता ।। एक व्यवहारिक सोच ।।
।। Chapter 12.13 II
।। अध्याय 12.13 II
॥ श्रीमद्भगवद्गीता ॥ 12.13॥
अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च ।
निर्ममो निरहङ्कारः समदुःखसुखः क्षमी॥
“adveṣṭā sarva- bhūtānāḿ,
maitraḥ karuṇa eva ca..।
nirmamo nirahańkāraḥ,
sama- duḥkha- sukhaḥ kṣamī”..।।
भावार्थ:
जो मनुष्य किसी से द्वेष नही करता है, सभी प्राणीयों के प्रति मित्र-भाव रखता है, सभी जीवों के प्रति दया-भाव रखने वाला है, ममता से मुक्त, मिथ्या अहंकार से मुक्त, सुख और दुःख को समान समझने वाला, और सभी के अपराधों को क्षमा करने वाला है। (१३)
Meaning:
He who is without dislike towards all beings, who is friendly and compassionate, who is also without (the sense of) mineness and egoism, who is the same in sorrow and joy, who is forgiving…
Explanation:
Shri Krishna always elaborates on the practical aspects of his teaching and brings it to the level of the student’s understanding. In the second chapter, he devoted several shlokas to describe the traits towards aspects of one who is established in the eternal essence. Here, he describes the traits of saints and accomplished devotees towards other people, which are easier for us to connect with, and become goals for people like us to strive towards.
An accomplished devotee essentially is convinced of two things: that everything in this world is not different than Ishvara, and that the devotee himself is also not different from Ishvara. When he has this outlook, he loses all sense of “I-ness” and “mine-ness”. He never believes that he exists outside of the existence of Ishvara. There is no sense of “I”-ness because only one “I” – Ishvara – exists. There is no sense of possession because everything belongs to Ishvara. It is somewhat similar to the outlook one has towards a large family.
Now learning the ladder of bhakti i.e. from practice to selfless work, nishkaam karm or reverse to it, the highest level when a person gets the status of adwait or Aham brahmasmi. So, he needs knowledge and dhyaan or meditation. But mere doing the same does make him await gyaani, he must have some inherent characteristics. Now he is explaining the same in for pra bhakt qualities.
Without inherent qualities the steps for Bhakti of God are mechanical process where you get high spiritual status without knowing the parbraham or adwait. If you are in status of dwait, all your devotion is covered under nature but not for complete liberalisation. You cannot free from reincarnation and circle of birth and death. The qualities are as under:
1. Free from malice toward all living beings. The devotees realize that all living beings are tiny parts of God. If they harbor envy toward others, it is tantamount to harboring envy toward God Himself. So the devotees are free from malice even toward those who are inimical toward them.
2. Friendly and compassionate. Devotion engenders the feeling of unity amongst all living beings by virtue of their being children of the one God. The notion of seeing others as alien to oneself is wiped out. This leads to the growth of affability in the devotees and sympathy toward the sufferings of others.
3. Free from attachment to possessions and egotism. The biggest enemy of devotion is pride. One can only progress on the spiritual path if one practices self-effacement. Proficient devotees naturally become humble and eliminate pride and proprietorship from their personality, as well as the false identification of being the body.
4. Equipoised in happiness and distress. Devotees have faith that only efforts are in their hands, while the results are in the hands of God. So whatever results come their way, they see them as the will of God, and accept them with equanimity.
5. Ever forgiving. Devotees never think of punishing wrongdoers for their emotional satisfaction. Harboring such negative thoughts toward others ruins one’s own devotion. So accomplished devotees refuse to harbor unforgiving thoughts in all circumstances and leave the task of punishing wrongdoers upon God.
So when there is such a universal sense of oneness with everything, the devotee becomes extremely friendly towards everyone. There is no sense of dislike or hatred present in him towards those who oppose him. Instead, he instantly forgives everyone. He is compassionate towards those who are in need. When all sense of duality is gone, the mind does not get agitated in sorrowful situations, nor does it get excited in joyful situations. It maintains a sense of equanimity.
This partial shloka continues next.
।। हिंदी समीक्षा ।।
पूर्व के श्लोक में भगवान से मोक्ष के लिए भक्ति की विभिन्न तरीकों को क्रम बद्ध किया जिस में अभ्यास से निष्काम कर्म और निष्काम कर्म से अभ्यास की श्रेष्ठता को हम ने पढ़ा। किंतु भक्ति में यह प्रक्रिया तकनीकी है जो हमे प्रकृति में उच्च पद पर भले ही ले जाए किंतु मुक्ति या मोक्ष नहीं प्राप्त हो सकता। मोक्ष के लिए पराभक्ति तभी हो सकती है, जब भक्त में कुछ आत्मीय गुण हो। यह गुण भक्त की परमात्मा के समीप ले जाते है, जिस से भक्त अहम ब्रह्मास्मी का बोध कर सके और पूर्ण अद्वैत भाव में जन्म – मरण से मुक्त हो सके।
कर्म- ज्ञान योग में मन इंद्रियों बुद्धि को वश में करते योगी ज्ञान द्वारा अपने को ब्रह्म में स्थापित कर देता है। अतः ब्रह्मसंथ के लिये यह प्रक्रिया जटिल तप एवम योग द्वारा प्राप्त की जाती है। इसलिये योगी पुरुष के लक्षणों में परमात्मा ने उसे स्थितप्रज्ञ, समभाव, अद्वेत माना है, जो सीधा अपने प्रकृति से अलग मानते हुए, परमात्मा में ही विलीन होता है। यहाँ परमात्मा ने ऐसे किसी से अपने संबंधों को नही कहा।
अतः यह गुण किताबी गुण है या बौद्धिक, इन से जीव को कोई उच्च स्तर नहीं मिलता। यह गुण अंतकरण के स्वाभाविक गुण होने चाहिए जिस से जीव का आचरण बिना प्रयास से गुणानुसार होना चाहिए। इस को हम गुणों की क्रम से अध्ययन से समझने की चेष्टा भी करेंगे।
भक्ति योग में भक्त और भगवान द्वेत स्वरूप है जिस में भक्त अनन्य भक्ति, स्मरण एवम समर्पण से परमात्मा को प्राप्त होता है। इसलिये भगवान उस से सम्बंध जोड़ते है, उस का योगक्षेम वहन करते है एवम उस का मार्गदर्शन करते है।
ग्याहरवें अध्याय के श्लोक 55 में भक्त के कुछ गुणों का वर्णन है। अब श्लोक 13 से 19 तक हम भक्त के गुणों को और अधिक जानेंगे। यह इसलिये भी महत्वपूर्ण है कि नीति शास्त्र या धर्म शास्त्र में सत्य या असत्य का विवेचन किया जाता है तो व्यक्ति गुण- दोषों के अनुसार ही हम सही निर्णय कर सकते है कि हमारा कर्तव्य धर्म उस व्यक्ति के प्रति क्या होना चाहिये। कुरुक्षेत्र में कौरव एवम पांडव द्वारा युद्ध नियम के विरुद्ध जो भी नीति का सहारा लिया गया था वो उस सामने खड़े प्रतिद्वंदी के लिये धर्म युक्त थी या सत्य थी या मात्र युद्ध जीतने के लिये छल कपट था।
परमात्मा प्रेम का भूखा है, ज्ञानी स्वयं को ब्रह्मसिद्ध करता है, इसलिये अद्वैत भाव मे वह ब्रह्म अर्थात परमात्मा के आत्मस्वरूप में स्थित है। किंतु भक्त सगुण उपासक है, इसलिये भक्त और भगवान दो पृथक पृथक अस्तित्व के साथ जुड़ कर एक रहते है। प्रेम आत्मा से भिन्न वस्तु का विषय है, आत्मास्वरूप हो जाने पर प्रेम करने को कुछ नही है। परमात्मा अपने भक्तों को अत्यंत प्रेम करते है, इसलिये उन का योगक्षेम वहन करते है और उन की रक्षा और जीवन व्यापन का भार उठाते है। किन्तु भक्त होना भी उतना सरल नही है, जितना भजन-कीर्तन को ऊंची आवाज में गाने वाले समझते है। अतः अद्वैत ब्रह्म को प्राप्त करने लिए विभिन्न सीढ़ियों से गुजरना ही नही पड़ता, वरन कुछ गुणों से युक्त भी होना पड़ता है। अब इसमें कितना समय लगेगा? हम नहीं जानते; यह एक जीवन में संभव हो सकता है; या इसे अगले जीवन में आगे बढ़ाया जा सकता है; इसमें कई जन्म भी लग सकते हैं; इससे कोई फर्क नहीं पड़ता; आइए हम कल्पना करें कि एक व्यक्ति सभी पाँच चरणों से गुजरता है; वह क्या बन जाता है? एक ज्ञानी; जिसे परा भक्त: भी कहा जाता है; एक भक्त जो सफलतापूर्वक सभी पाँचों से गुजर चुका है। इसलिए परा भक्त: का अर्थ है सर्वोच्च भक्त और इस परा भक्त के पास अनिवार्य रूप से ज्ञान होना चाहिए; क्योंकि पाँचवें चरण में निर्गुण ईश्वर की जाँच शामिल है।
और इसलिए जैसा कि हम तैत्तिरीय उपनिषद में देख रहे हैं; वह पहले एक रूप ईश्वर को जानेगा; एक रूप वाला भगवान; बाद में वह ईश्वर को विश्व रूप ईश्वर: के रूप में समझेगा; स्वयं ब्रह्मांड के रूप में; और अंततः वह पहचान लेगा कि ईश्वर का न तो एक रूप है और न ही अनेक रूप हैं; ईश्वर इस निर्मित ब्रह्मांड के पीछे का निराकार सत्य है। ईश्वर इस निर्मित ब्रह्मांड के पीछे का निराकार सत्य है और वह और कोई नही, स्वयं ही ब्रह्म स्वरूप है। जैसे लहर और सागर का अस्तित्व कुछ भी नही, दोनो एकाकार स्वरूप में जल ही है। जीव और परमात्मा ऐसी कोई दो स्वतंत्र सत्ता नही है। जीव और परमात्मा एक स्वरूप है।
भक्त कौन है, यही परमात्मा बतला रहे है।
1. अनिष्ट करने वालों के दो भेद हैं (1) इष्ट की प्राप्ति में अर्थात् धन, मानबड़ाई, आदरसत्कार आदि की प्राप्ति में बाधा पैदा करने वाले और (2) अनिष्ट पदार्थ, क्रिया, व्यक्ति, घटना आदि से संयोग कराने वाले। भक्त के शरीर, मन, बुद्धि, इन्द्रियाँ और सिद्धान्त के प्रतिकूल चाहे कोई कितना ही, किसी प्रकार का व्यवहार करे, इष्ट की प्राप्ति में बाधा डाले, किसी प्रकार की आर्थिक और शारीरिक हानि पहुँचाये, पर भक्त के हृदय में उस के प्रति कभी किञ्चिन्मात्र भी द्वेष नहीं होता। कारण कि वह प्राणि मात्र में अपने प्रभु को ही व्याप्त देखता है, ऐसी स्थिति में वह विरोध करे तो किस से करे।
कर्तव्य धर्म के पालन में प्राणि मात्र के प्रति द्वेषभाव से रहित होने पर ही भगवान् में पूर्ण प्रेम हो सकता है। इसलिये भक्त में प्राणिमात्र के प्रति द्वेष का सर्वथा अभाव होता है।
2. भक्त के अन्तःकरण में प्राणि मात्र के प्रति केवल द्वेष का अत्यन्त अभाव ही नहीं होता, प्रत्युत सम्पूर्ण प्राणियों में भगवद्भाव होने के नाते उस का सब से मैत्री और करुणा का व्यवहार भी होता है। दया मन एवम बुद्धि से उपजी अन्य व्यक्ति के प्रति भावना है, जिस में दया करने वाला कही न कही अपने को ऊपर मान लेता है, करुणा ह्रदय से उपजी भावना है जिस में समान भाव रहता है। मैत्रय बराबर या सम भाव है जिस में कोई भी, किसी भी किस्म का भेदभाव नही है।
3. यद्यपि भक्त का प्राणि मात्र के प्रति स्वाभाविक ही मैत्री और करुणा का भाव रहता है, तथापि उस की किसी के प्रति किञ्चिन्मात्र भी ममता नहीं होती। प्राणियों और पदार्थों में ममता (मेरेपन का भाव) ही मनुष्य को संसार में बाँधनेवाली होती है। भक्त इस ममता से सर्वथा रहित होता है। उस की अपने कहलाने वाले शरीर, इन्द्रियाँ, मन और बुद्धि में भी बिलकुल ममता नहीं होती। इंग्लिश में इस के लिये एक शब्द sympathy और दूसरा शब्द ampathy है।
4. शरीर, इन्द्रियाँ आदि जडपदार्थों को अपना स्वरूप मानने से अहंकार उत्पन्न होता है। भक्त की अपने शरीरादि के प्रति किञ्चिन्मात्र भी अहंबुद्धि न होने के कारण तथा केवल भगवान् से अपने नित्य सम्बन्ध का अनुभव हो जाने के कारण उस के अन्तःकरण में स्वतः श्रेष्ठ, दिव्य, अलौकिक गुण प्रकट होने लगते हैं। इन गुणों को भी वह अपने गुण नहीं मानता, प्रत्युत (दैवी सम्पत्ति होनेसे) भगवान् के ही मानता है। सत् (परमात्मा) के होने के कारण ही ये गुण सद्गुण कहलाते हैं। ऐसी दशा में भक्त उन को अपना मान ही कैसे सकता है इसलिये वह अहंकार से सर्वथा रहित होता है।
5. भक्त सुखदुःखों की प्राप्ति में सम रहता है अर्थात् अनुकूलता प्रतिकूलता उस के हृदय में रागद्वेष, हर्ष शोक आदि विकार पैदा नहीं कर सकते। इसलिये सुखदुःख में सम होने का अर्थ है। अनुकूल या प्रतिकूल परिस्थिति आने पर अपने में हर्ष शोकादि विकारों का न होना। भक्त के शरीर, इन्द्रियाँ, मन, सिद्धान्त आदि के अनुकूल या प्रतिकूल प्राणी, पदार्थ, परिस्थिति, घटना आदि का संयोग या वियोग होनेपर उसे अनुकूलता और प्रतिकूलता का ज्ञान तो होता है, पर उस के अन्तःकरण में हर्षशोकादि कोई विकार उत्पन्न नहीं होता। यहाँ यह बात समझ लेनी चाहिये कि किसी परिस्थितिका ज्ञान होना अपने आप में कोई दोष नहीं है, प्रत्युत उस से अन्तःकरण में विकार उत्पन्न होना ही दोष है। भक्त रागद्वेष, हर्षशोक आदि विकारों से सर्वथा रहित होता है। जैसे, प्रारब्धानुसार भक्त के शरीर में कोई रोग होने पर उसे शारीरिक पीड़ा का ज्ञान (अनुभव) तो होगा किन्तु उस के अन्तःकरण में किसी प्रकार का विकार नहीं होगा।
6. अपना किसी तरह का भी अपराध करने वाले को किसी भी प्रकार का दण्ड देने की इच्छा न रख कर उसे क्षमा कर देनेवाले को क्षमी कहते हैं। जब द्वेष नही है, विकार भी नही, अहंकार भी नही है, न ही सुख-दुख का अनुभव है तो किसी के कार्य के प्रति प्रतिकार भी नही है। इसलिये वह हमेशा क्षमा भाव रखता है। यदि कोई अपराधी अपराध करे तो उसे दंड नही दिया जाना चाहिये, ऐसा कोई भी भाव क्षमा में नही है। अपराध को रोकना कर्तव्य है किंतु किये हुये अपराध के प्रति करुणा – दया रखना एवम उसे क्षमा कर देना गुण है।
कोई चोरी करें किन्तु भूल को समझ कर पश्चाताप करे तो क्षमा का पात्र है किंतु कोई चोरी की करता रहे तो उस को दंडित करने कर्तव्य है जिस में उस के पूर्व के अपराधों के लिये क्षमा होनी चाहिये।
किसी भक्त के यह गुण उस के कर्तव्य धर्म के पालन में बाधक होंगे या सहायक, इस पर विचार हम सम्पूर्ण भक्त के गुणों के अध्ययन के बाद करेंगे। हमे यह ध्यान रखना है कि अर्जुन के मन मे युद्धभूमि में स्वजनों को देख कर जो करुणा, मोह, दया और क्षमा का भाव उपजा था, वह इन सब से किस प्रकार मेल खायेगा। यह हमारे जीवन का सब से अधिक द्वंदशील विचार है।
आज के भारत वर्ष में जब वातावरण जातिगत द्वेष और हिंसा से भरा हो अज्ञान, स्वार्थ, लोभ और अहंकार में अपने ही लोग अपनों के विरुद्ध हो तो क्या ऐसा नहीं लगता कि सनातन संस्कृति की रक्षा में जो खड़ा है, उस की स्थिति अर्जुन के समान है। उसे जिन के विरोध का सामना करना है, वे उस के अपने भी लोग है। अतः ऐसे में उस का कर्तव्य धर्म क्या कहता है, इसे भी आगे समझने की चेष्टा करते है।
मोह, ममता, हिंसा, घृणा, क्रोध और लोभ आदि प्रकृति के गुण है, यह संसार प्रकृति के निमित्त हो कर कार्य करता है अतः जो होना है वह नियति तय करती है और जीव निमित्त मात्र है। जल का प्रवाह अंत में समुंद्र में विलीन होता है किंतु कर्तव्य कर्म से उस पर बांध बना कर या नहर बना कर दिशा परिवर्तन किया जा सकता है। यही कर्म के अधिकार में कर्तव्य कर्म निष्काम लोकसंग्रह के हो या प्रकृति के गुणों के अंदर फल दे कर बांधने वाले हो, यह जीव तय करता है। इसलिए भक्त जिसे मुक्ति चाहिए, उस के कर्तव्य कर्म में किन गुणों का होना या अभाव होना हम अभी पढ़ रहे है।
भक्त के और क्या गुण होने चाहिए यह आगे पढ़ते है।
।। हरि ॐ तत सत।। 12.13।।
Complied by: CA R K Ganeriwala (+91 9422310075)