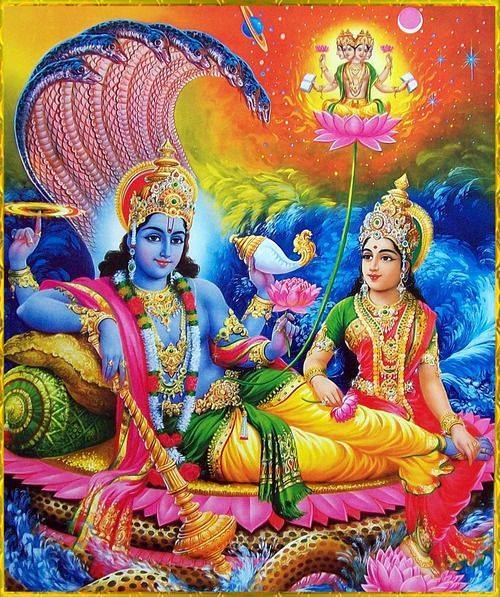।। Shrimadbhagwad Geeta ।। A Practical Approach ।।
।। श्रीमद्भगवत गीता ।। एक व्यवहारिक सोच ।।
।। Chapter 10.28 II Additional -2 II
।। अध्याय 10.28 II विशेष -2 II
।। व्यक्तित्व के विकास के पांच बुद्धि वज्र ।। विशेष 2- गीता 10.28 ।।
आप को यह जरुर समझना चाहिए कि आप की बुद्धि आप की पांचों इंद्रियों के जरिए ही काम करती है। अगर इंद्रियों के जरिये सूचना नहीं मिल रही है, तो आप की बुद्धि काम नहीं करेगी। बुद्धि के पांच बुनियादी रूप होते हैं। आकार, ध्वनि, सुगंध, स्वाद और स्पर्श को समझने के लिए बुद्धि के ये पांच अलग-अलग रूप होते हैं। इन में से आकार को समझने वाली बुद्धि को सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि इसी से सृष्टि की ज्यामिति समझ में आती है। अतः बुद्धि के उन गुणों के समझिए, जिस से बुद्धि कुशाग्र, पैनी, बज्र के समान मजबूत हो।
हमारे जीवन की सबसे बुनियादी क्षमता विचार, भाव और संवेदनाएं हैं और इन्हें ही संभालने का तरीका लोग जीवन भर नहीं सीख पाते। कुत्ते, बिल्ली जैसे सारे जानवर अपनी सभी क्षमताओं को अपनी खुशहाली के लिए इस्तेमाल करने का तरीका अच्छी तरह जानते हैं, लेकिन इंसान यह सब नहीं सीख पाता। किसी भी दूसरे प्राणी की तुलना में इंसान के पास कहीं ज्यादा उच्च स्तरीय क्षमताएं और योग्यताएं हैं। चूंकि वह इन्हें अपनी खुशहाली के लिए इस्तेमाल करने का तरीका नहीं सीखता, इसलिए उसकी ये क्षमताएं एक बड़ा झमेला बन जाती हैं।
इन्हें बोध धर्म मे पांच बुद्धि बुद्ध भी कहते है।
1. बुद्ध- वैरोकाना – अनुकूलता, अनुभव के लिए खुलापन – अज्ञान, भ्रम
2. कर्म – अमोघसिद्धि – मानसिक गठन, रक्षा करना, कर्त्तव्य निष्ठां – ईर्ष्या
3. पद्या – अमिताभः – जिज्ञासा, धारणा, बहिर्मुखता, ध्यान, वश में करना – स्वार्थ, लगाव
4. रत्न- रत्नसंभव – समभाव, समृद्धि, सहमतता- अभिमान, लालच
5. वज्र – अकोभ्य – अद्वैतवादी, विज्ञान, मनोविक्षुब्धता, नम्रता – आक्रमण, घृणा
उच्च स्तर यदि मानसिकता उच्च स्तर की हो तो निम्न गुण होंगे।
आविष्कारशील, जिज्ञासु
कुशल, संगठित
आउटगोइंग, ऊर्जावान
मिलनसार, दयालु
संवेदनशील, नर्वस
निम्न स्तर यदि मानसिकता निम्न स्तर की हो तो निम्न गुण होंगे।
सतर्क, रूढ़िवादी
आराम से, लापरवाह
एकान्त आरक्षित
प्रतिस्पर्धी, मुखर
सुरक्षित, आत्मविश्वासी
व्यक्तित्व के आयाम:
1. अनुभव के लिए खुलापन: (आविष्कारशील/जिज्ञासु बनाम सुसंगत/सतर्क):
अनुभव के लिए खुलापन एक व्यक्ति की बौद्धिक जिज्ञासा, रचनात्मकता, कला के लिए प्रशंसा, भावना, रोमांच, असामान्य विचार, जिज्ञासा और अनुभव की विविधता का वर्णन करता है।
इसे उस सीमा के रूप में भी वर्णित किया जाता है जिस हद तक कोई व्यक्ति कल्पनाशील या स्वतंत्र होता है, और एक सख्त दिनचर्या पर विभिन्न प्रकार की गतिविधियों के लिए व्यक्तिगत वरीयता को दर्शाता है ।
उच्च खुलेपन को अप्रत्याशितता या फोकस की कमी के रूप में माना जा सकता है।
इसके अलावा, उच्च खुलेपन वाले व्यक्तियों के बारे में कहा जाता है, कि वे विशेष रूप से स्काइडाइविंग, विदेश में रहने, जुआ, आदि जैसे गहन, उत्साहपूर्ण अनुभवों की तलाश में आत्म-साक्षात्कार का पीछा करते हैं।
इसके विपरीत, कम खुलेपन वाले लोग दृढ़ता के माध्यम से पूर्णता प्राप्त करना चाहते हैं और उन्हें व्यावहारिक और डेटा-चालित के रूप में चित्रित किया जाता है – कभी-कभी उन्हें हठधर्मी और बंद दिमाग वाला भी माना जाता है।
खुलेपन कारक की व्याख्या और संदर्भ के बारे में कुछ असहमति बनी हुई है।
2. कर्तव्यनिष्ठा (कुशल/संगठित बनाम आसान/लापरवाह):
कर्तव्यनिष्ठा आत्म-अनुशासन दिखाने, कर्तव्यपरायणता से कार्य करने और उपलब्धि का लक्ष्य रखने की प्रवृत्ति है।
कर्तव्यनिष्ठा का तात्पर्य नियोजन, संगठन और निर्भरता से भी है।
उच्च कर्तव्यनिष्ठा को अक्सर हठ और जुनून के रूप में माना जाता है।
कम कर्तव्यनिष्ठा लचीलेपन और सहजता के साथ जुड़ी हुई है, लेकिन यह ढिलाई और विश्वसनीयता की कमी के रूप में भी प्रकट हो सकती है।
3. बहिर्मुखता: (आउटगोइंग/ऊर्जावान बनाम एकान्त/आरक्षित):
बहिर्मुखता ऊर्जा, सकारात्मक भावनाओं, मुखरता, सामाजिकता, बातूनीपन और दूसरों की संगति में उत्तेजना की तलाश करने की प्रवृत्ति का वर्णन करती है।
उच्च अपव्यय को अक्सर ध्यान आकर्षित करने वाले और दबंग के रूप में माना जाता है।
कम बहिर्मुखता एक आरक्षित, चिंतनशील व्यक्तित्व का कारण बनती है, जिसे अलग या आत्म-अवशोषित माना जा सकता है।
4. सहमतता: (मैत्रीपूर्ण/दयालु बनाम विश्लेषणात्मक/अलग):
सहमतता दूसरों के प्रति शंकालु और विरोधी होने के बजाय दयालु और सहयोगी होने की प्रवृत्ति है।
यह किसी के भरोसेमंद और मददगार स्वभाव का भी एक पैमाना है, और क्या कोई व्यक्ति आम तौर पर अच्छे स्वभाव वाला है या नहीं।
उच्च सहमतता को अक्सर अनुभवहीन या विनम्र के रूप में देखा जाता है।
कम सहमत व्यक्तित्व अक्सर प्रतिस्पर्धी या चुनौतीपूर्ण लोग होते हैं, जिन्हें तर्कपूर्ण या अविश्वसनीय के रूप में देखा जा सकता है।
5. विक्षिप्तता:
(संवेदनशील/नर्वस बनाम सुरक्षित/आत्मविश्वास)
विक्षिप्तता आसानी से अप्रिय भावनाओं का अनुभव करने की प्रवृत्ति है, जैसे कि क्रोध, चिंता, अवसाद और भेद्यता।
न्यूरोटिसिज्म भावनात्मक स्थिरता और आवेग नियंत्रण की डिग्री को भी संदर्भित करता है और कभी-कभी इसके निम्न ध्रुव, “भावनात्मक स्थिरता” द्वारा संदर्भित किया जाता है।
स्थिरता की उच्च आवश्यकता एक स्थिर और शांत व्यक्तित्व के रूप में प्रकट होती है, लेकिन इसे उदासीन और असंबद्ध के रूप में देखा जा सकता है।
स्थिरता की कम आवश्यकता एक प्रतिक्रियाशील और उत्साही व्यक्तित्व का कारण बनती है, अक्सर बहुत गतिशील व्यक्ति, लेकिन उन्हें अस्थिर या असुरक्षित माना जा सकता है।
व्यक्तित्व विकास:
व्यक्तित्व विकास में ऐसी गतिविधियाँ शामिल हैं जो जागरूकता और पहचान में सुधार करती हैं, प्रतिभा और क्षमता का विकास करती हैं, मानव पूंजी का निर्माण करती हैं और रोजगार की सुविधा प्रदान करती हैं, जीवन की गुणवत्ता में वृद्धि करती हैं और सपनों और आकांक्षाओं को साकार करने में योगदान करती हैं।
जब व्यक्तिगत विकास संस्थाओं के संदर्भ में होता है, तो यह उन तरीकों, कार्यक्रमों, उपकरणों, तकनीकों और मूल्यांकन प्रणालियों को संदर्भित करता है जो संगठनों में व्यक्तिगत स्तर पर मानव विकास का समर्थन करते हैं।
व्यक्तित्व विकास में ऐसी गतिविधियाँ शामिल हैं जो प्रतिभा विकसित करती हैं, जागरूकता में सुधार करती हैं, क्षमता को बढ़ाती हैं और जीवन की गुणवत्ता में सुधार करती हैं। इसमें औपचारिक और अनौपचारिक गतिविधियाँ शामिल हैं जो लोगों को उनकी पूरी क्षमता का एहसास करने में मदद करने के लिए नेताओं, मार्गदर्शकों, शिक्षकों और प्रबंधकों की भूमिका में डालती हैं।
इसलिए, यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि व्यक्तित्व में सुधार या परिवर्तन की प्रक्रिया को व्यक्तित्व विकास कहा जाता है।
।। हरि ॐ तत सत ।। विशेष 2- 10. 28 ।।
Complied by: CA R K Ganeriwala (+91 9422310075)