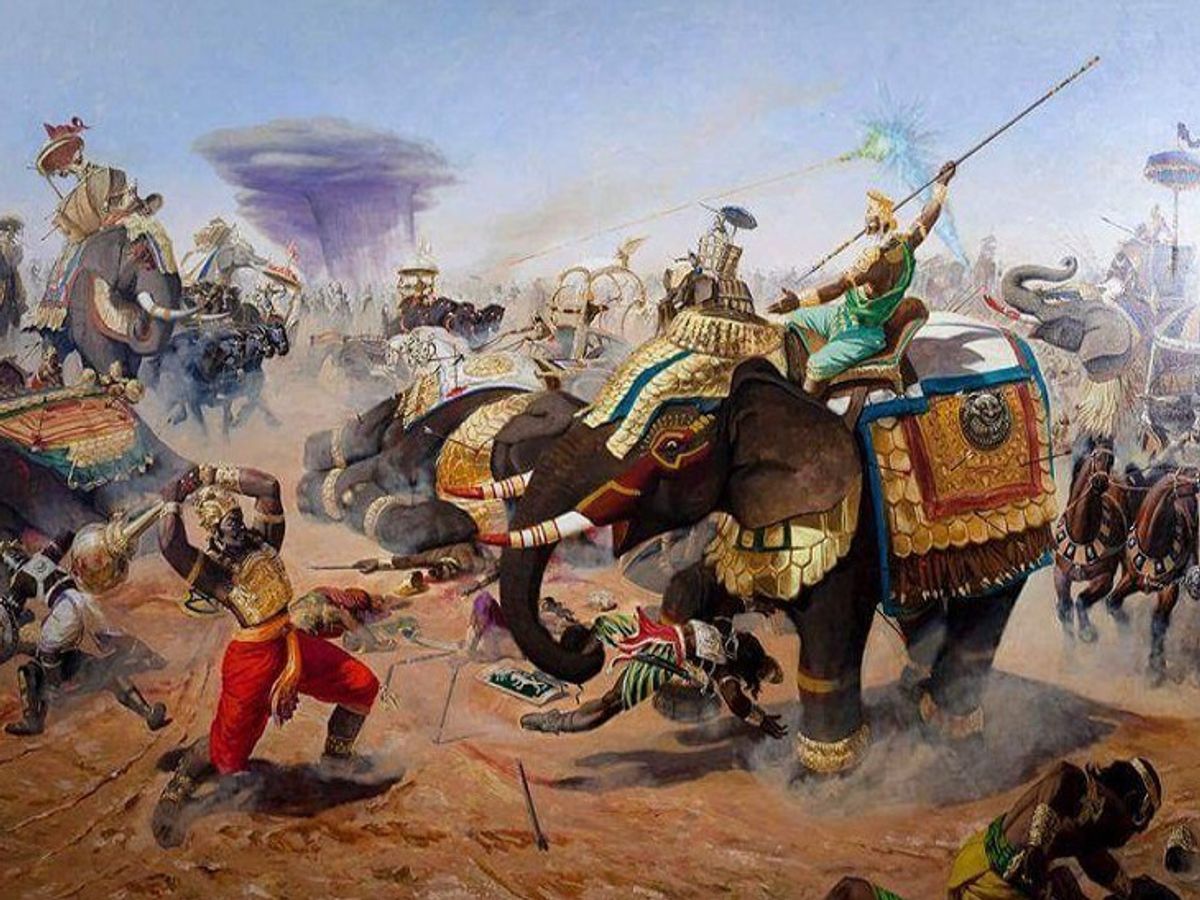।। Shrimadbhagwad Geeta ।। A Practical Approach ।।
।। श्रीमद्भगवत गीता ।। एक व्यवहारिक सोच ।।
।। Chapter 10.18 II
।। अध्याय 10.18 II
॥ श्रीमद्भगवद्गीता ॥ 10.18॥
विस्तरेणात्मनो योगं विभूतिं च जनार्दन ।
भूयः कथय तृप्तिर्हि श्रृण्वतो नास्ति मेऽमृतम् ॥
“vistareṇātmano yogaḿ,
vibhūtiḿ ca janārdana..।
bhūyaḥ kathaya tṛptir hi,
śṛṇvato nāsti me ‘mṛtam”..।।
भावार्थ:
हे जनार्दन! अपनी योग-शक्ति और अपने ऎश्वर्यपूर्ण रूपों को फिर भी विस्तार से कहिए, क्योंकि आपके अमृत स्वरूप वचनों को सुनते हुए भी मेरी तृप्ति नहीं हो रही है। (१८)
Meaning:
Elaborately describe your yoga and expressions again, O Janaardana. I am not satisfied by listening to your nectar-like (words).
Explanation:
So far, Shri Krishna just gave a taste of Ishvara’s expressions. Arjuna clearly was relishing and enjoying hearing these expressions because he compared them to the sweetness of nectar. He wanted to hear them all over again. But this time, he would not be content with hearing so little. He requested Shri Krishna to give a detailed and elaborate description of Ishvara’s expressions as well as yoga, the power of maaya that creates many expressions of the one Ishvara.
Arjuna addressed Shri Krishna as “Janaardana” which has two meanings. “Arda” means one who moves, or makes others move. Jana means people, and therefore Janaardana means one who moves people to heaven or hell, in other words, dispenses justice to evildoers. Another meaning of Janaardana is one whom people ask for prosperity and wellbeing.
Arjuna understood that the true nature of Shri Krishna was Ishvara. So, he says, “hey janārdana! kathayaḥ; may you enumerate, narrate, enlist, what?
ātmanaḥ yōgam”. Atma here is reflective pronoun, your own yōga śakti, potentiality, What potentiality? the potentiality to become the universe.
Arjun says, “… hearing your nectar,” instead of “… hearing your words that are like nectar.” He has omitted “your words that are like.” This is a literary technique called atiśhayokti, or hyperbole (statement of extreme expression), in which the subject of comparison is omitted. He now cheers him, by saying bhūyaḥ kathaya, “Once more! My thirst for hearing your glories is not satiated.”
Now as far as amritam, nectar, is concerned, any narration or statement concerning Krishna is just like nectar. And this nectar can be perceived by practical experience. Modern stories, fiction and histories are different from the transcendental pastimes of the Lord in that one will tire of hearing mundane stories, but one never tires of hearing about Krishna. It is for this reason only that the history of the whole universe is replete with references to the pastimes of the incarnations of Godhead. The Puranas are histories of bygone ages that relate the pastimes of the various incarnations of the Lord. In this way the reading matter remains forever fresh, despite repeated readings.
With this shloka, Shri Krishna concluded his statements and requests. Starting with the next shloka, Shri Krishna will provide a total of 82 vibhootis or expressions of Ishvara. Most of these are drawn from the Indian Vedic and Puraanic tradition since Arjuna would be easily able to identify with and connect with those examples. We can try to look for similarities in the present time so that we are also able to connect with those.
।। हिंदी समीक्षा ।।
अर्जुन यहां श्री कृष्ण से योग एवम विभूतियों को जो पहले भी बताया जा चुका था, उसे विस्तार से सुनना चाहता है। भगवान् ने दसवाँ अध्याय आरम्भ करते हुए कहा कि तू फिर मेरे परम वचन को सुन। ऐसा सुनकर भगवान् की कृपा और महत्त्व की तरफ अर्जुन की दृष्टि विशेषता से जाती है और अर्जुन कहते हैं कि आप अपने योग और विभूतियोंको विस्तारपूर्वक फिर से कहिये क्योंकि आप के अमृतमय वचन सुनते हुए तृप्ति नहीं हो रही है। मन करता है कि सुनता ही चला जाऊँ।
परमात्मा ने अध्याय 7 से 9 के मध्य भी अपनी विभूतियों के अक्षर ॐ, सभी के पिता और मूल बीज के रूप आदि में कहा था। इसलिए किसी शिक्षक, प्रवक्ता या उपदेशक से किसी बात को पुनः दोहराने के अनुरोध को कहना भी अपने आप मे एक कला है। क्योंकि इस से शिक्षक, प्रवक्ता या उपदेशक के अंदर यह भाव भी आ सकता है कि उस का श्रोता उसे ध्यान से नही सुन रहा जिस से उस की रुचि ज्ञान प्रदान करने की कम हो सकती है। इसलिये अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को जनार्दन कह सम्बोधित करते है जिस का अर्थ है सब को साथ ले कर उच्च मार्ग में चलने वाले, और उन के वचनों को अमृतमय कहते है, अर्थात उन्होंने पहले कहे वचनों की ध्यान से सुना है। उन का आग्रह उस की जिज्ञासा को प्रेरित करता है, जिस में भगवान से उन के योग और विभूतियों को अधिक विस्तार से कहने को कहा है।
इस के अतिरिक्त अर्जुन “आप की वाणी अमृत के समान है” यह कहने के स्थान पर “आप की अमृत वाणी सुनकर” जैसे शब्दों का प्रयोग करता है। वह यह नहीं कहता “आप की वाणी उस के समान है।” या “आप की वाणी उस के जैसी है।” यह साहित्यिक विधा है जिसे अतिशयोक्ति कहते हैं जिसमें किसी गुण, स्थिति या वस्तु का बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाता है। अब वह उन्हें ‘भूयः कथय’ जिसका अर्थ ‘एक बार और’ कहकर प्रसन्न करता है।
नौमिषारण्य के ऋषियों ने सुत गोस्वामी से श्रीमद्भागवतम् की कथा सुनते हुए ऐसे ही कथन व्यक्त किए थे।
वयं तु न वितृप्याम उत्तमश्लोकविक्रमे। यच्छृण्वतां रसज्ञानां स्वादु स्वादु पदे पदे।।(श्रीमद्भागवतम्-1.1.19)
“वे जो भगवान श्रीकृष्ण के शरणागत हैं, भगवान की दिव्य लीलाओं का श्रवण करने से कभी तृप्त नहीं होते। इन लीलाओं का अमृतरस ऐसा है कि इनका जितना अधिक आस्वादन किया जाता है ये उतना अधिक आनन्द प्रदान करती हैं।”
दर्शनशास्त्र के तथा अन्य किसी विषय के विद्यार्थी में भी, सर्वप्रथम प्रखर जिज्ञासा का होना अत्यावश्यक है। विषय को जानने और समझने की इस जिज्ञासा के बिना कोई भी ज्ञान दृढ़ नहीं होता है और न विद्यार्थी के लिए वह लाभदायक ही हो सकता है। आत्मविकास के आध्यात्मिक ज्ञान में यह बात विशेष रूप से लागू होती है क्योंकि अन्य ज्ञानों के समान, न केवल इसे ग्रहण करना है बल्कि धारण भी करना है। यह आत्मज्ञान होने पर उसे अपने जीवन में दृढ़ता से जीना भी होता है। इसलिए श्रवण की इच्छा को एक श्रेष्ठ और आदर्श गुण माना गया है, जो वेदान्त के उत्तम अधिकारी के लिए अनिवार्य है। इस गुण के होने से ज्ञानमार्ग में प्रगति तीव्र गति से होती है। पाण्डुपुत्र अर्जुन इस श्रेष्ठ गुण से सम्पन्न था जो कि उसके इस कथन से स्पष्ट होता है कि आप के अमृतमय वचनों को सुन कर मेरी तृप्ति नहीं होती है। इस में कोई सन्देह नहीं कि वेदान्त का शुद्धिकारी प्रभाव रुचिपूर्वक श्रवण करने वाले सभी बुद्धिमान विद्यार्थियों पर पड़ता है। एक सच्चे ज्ञानी गुरु के मुख से आत्मतत्त्व का उपदेश सुनकर प्रारम्भ में शिष्य को होने वाला आनन्द क्षणिक उल्लास ही देता है, जो स्थिर नहीं रह पाता। जब वह शिष्य प्रवचन के बाद अकेला रह जाता है, तब उसका मन पुन अनेक कारणों से अशान्त हो सकता है। इसलिये श्रवण किये हुए प्रत्येक शब्द को मनन करना भी उतना ही आवश्यक है। और फिर भी, कितना ही क्षणिक आनन्द क्यों न हो, उस मे जिज्ञासा, श्रवण एवम मनन के कारण उस की उस विषय के प्रति रुचि एक व्यसन के समान बढ़ती ही जाती है। वेदान्त प्रवचनों के श्रवणार्थ इस अधिकाधिक अभिरुचि को यहाँ स्पष्ट दर्शाया गया है। यद्यपि यह साधना है, साध्य नहीं, तथापि, निसन्देह यह एक शुभ प्रारम्भ है। जिन लोगों को तत्त्वज्ञान के बौद्धिक अध्ययन से ही सन्तोष का अनुभव होता हो, वे भी निश्चय ही उन सहस्रों लोगों से श्रेष्ठतर हैं, जो दिव्य आत्मस्वरूप को दर्शाने वाले एक भी आध्यात्मिक प्रवचन को नहीं सुन सकते या सह नहीं सकते।
यहां भक्ति योग पढ़ रहे है अतः योग का अर्थ चित्त वृति निरोध न करते हुए परमात्मा के दिव्य गुण से लेंगे क्योंकि प्रकरण विभूति योग है। जैसे सेंधवा यदि भोजन करते समय मांगा जाए तो उस का अर्थ नमक होगा न कि घोड़ा। प्रकरण का अर्थ ही निर्णायक होता है। अतः योग का अर्थ परमात्मा की योगमाया से है जो सातवे अध्याय के 25वे श्लोक में परमात्मा के कहे वचन को ध्यान में रख कर कहा गया है, जिस में परमात्मा कहते है “जो मूढ़ मनुष्य मेरे को अज और अविनाशी ठीक तरह से नहीं जानते (मानते), उन सब के सामने योगमाया से अच्छी तरह से आवृत हुआ मैं प्रकट नहीं होता। यह मोहित लोक (मनुष्य) मुझ जन्मरहित, अविनाशी को नहीं जानता है।”
विभूति का अर्थ उस दिव्य स्वरूप, भाव एवम गुणों का है जो परमात्मा के स्वरूप को, गुणों को, उन के भाव को एवम उन के चिंतन को स्मरण एवम समर्पित किया जा सके। मनुष्य जन्म अपूर्ण है अतः इस मे गुण एवम अवगुण दोनो की होते है, विभूति का अर्थ उन के गुणों से उस को जानना और अनुसरण करना। उन के अवगुणों को विस्मृत करना। यदि किसी विभूति के अवगुणों का वर्णन कर के हम उस की आलोचना करते है, तो हम अपनी ही कमजोरियों को उजागर करते है, जो हमे प्रभावित करती है। यह अक्सर हम आलोचकों के लेख में पढ़ते है। जब हम करुणा, भक्ति, दया, धृणा, ईर्ष्या आदि के चित्र, लेख या घटना, वीडियो आदि देखते है तो ह्रदय में जिस को देख कर अधिक भावुकता उत्पन्न हो, वही हमारा स्वावभिक गुण होता है, यह गुण जितना सात्विक होगा, उतना ही हम परमात्मा की विभूतियों को अधिक चिंतन के साथ पढ़ पाएंगे और उच्च स्तर को प्राप्त कर पाएंगे।
किसी भी विभूति के सद्गुण हमेशा उस के अवगुण से अधिक होते है, जिस के कारण वह विभूति परमात्मा के अत्यधिक निकट होती है। विभूतियों को विस्तार से वर्णन सुनने की इच्छा का अर्थ यही है, हम अधिक से अधिक उन भाव, विचारो, कर्म, ज्ञान को प्राप्त कर सके, जिन से हमारा व्यक्तित्व भी उच्चतर स्तर को प्राप्त हो। किसी की बुराई करना सरल है किंतु उस की अच्छाइयों को समझ कर अपनाना कठिन।
जैसे हम जेरोक्स कहते ही फ़ोटो कॉपी या प्रतिलिपि की समस्त कंपनियों के उस उत्पाद को समझ जाते है वैसे ही विभूति से उस विषय एवम पदार्थ संबंधित सभी गुण उस विभूति से समझ जाए। इस में जो श्रेष्ठ है वो दिव्य है।
जीवन मुक्त महामुनि जेऊ।
हरि गुन सुनहि निरन्तर तेऊ।।
मुक्त जीव कभी भी भगवान की कथा से तृप्त नही होते। अतः जब भी मौका मिले हरि कथा में लीन रहते है, अर्जुन भी उपदेशामृत पीने के लिए तृप्त नही है इसलिये वो विस्तार से समस्त योगमाया और विभूतियों को जानना चाहता है, जिस से उस को कोई शंका न रहे।
अर्जुन के चिंतन करने की जिज्ञासा पूर्व श्लोक में प्रकट हो चुकी है, अतः चिन्तन के स्वरूप को जानने की जिज्ञासा वह अब प्रकट करते है। ज्ञान को रुचि एवम जिज्ञासा, श्रवण, मनन एवम शंका रहित हो कर ही प्राप्त करना चाहिए।
व्यवहार में जिज्ञासा और रुचि, श्रवण करने की इच्छा, गुरु के प्रति सम्मान और इसी सम्मान में किसी कही हुई बात को पुनः दोहराने के अनुग्रह को कहने की कला ही शिष्य का ज्ञान मार्ग प्रशस्त करती है। जो शिष्य गुरु या प्रवक्ता के प्रति सम्मान नही करते या जो स्वयं को अत्यधिक ज्ञानी मानते हुए, गुरु से प्रश्न गुरु के ज्ञान की परीक्षा की भांति पूछते है, उन के लिए गुरु भी ज्ञान देते वक्त उदार नहीं होता। इसी प्रकार जब ईश्वर को अपने समक्ष पा कर अर्जुन अपने युद्ध में जीतने या सांसारिक सुखों की मांग नही करते हुए, उन के दिव्य स्वरूप और परमात्मा को जानने की चेष्टा करता है। गीता जैसा अद्वितीय ग्रंथ को पढ़ते हुए, हम में से पता नही, कितने लोग ज्ञान की उपासना करते है और कितने अपने लिए सुख, शांति और समृद्धि को तलाशते है। इसी प्रकार परमात्मा की विभूतियों को कौन कैसे दिखेगा और समझेगा, पता नहीं।
अर्जुन की प्रार्थना स्वीकार कर के भगवान् अब आगे के श्लोक से अपनी 82 विभूतियों और योग को कहना आरम्भ करते हैं, जिसे हम आगे पढ़ते है।
।।हरि ॐ तत सत।। 10.18।।
Complied by: CA R K Ganeriwala (+91 9422310075)