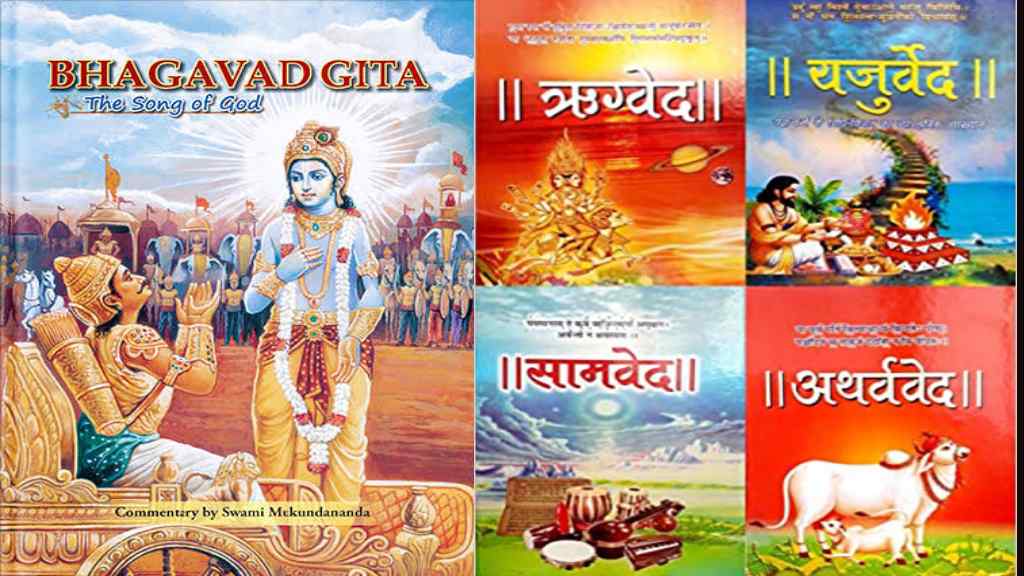।। Shrimadbhagwad Geeta ।। A Practical Approach ।।
।। श्रीमद्भगवत गीता ।। एक व्यवहारिक सोच ।।
।। Chapter 02. 10 ।। Additional II
।। अध्याय 02. 10 ।। विशेष II
।। प्रज्ञावाद एवम अर्जुन का अज्ञान ।। विशेष 2.10 ।।
दूसरे अध्याय का नाम सांख्य योग है। इस में जीवन की दो प्राचीन संमानित परंपराओं का तर्कों द्वारा वर्णन आया है। अर्जुन को उस कृपण स्थिति में रोते देखकर कृष्ण ने उसका ध्यान दिलाया है कि इस प्रकार का क्लैव्य और हृदय की क्षुद्र दुर्बलता अर्जुन जैसे वीर के लिए उचित नहीं।
प्रज्ञा द्वारा जीव अन्तःकरण , वृत्ति / परिणाम के भेद से चार प्रकार — मन , बुद्धि , चित्त और अहंकार — के नाम से जाना जाता है । संकल्प करनेे मन , विषय के निश्चय करने के कारण से बुद्धि , अभिमान करने के कारण अहंकार और विषयों का चिन्तन करने के कारण चित्त कहलाता है ।।
जैसे संकल्प आदि मन के धर्म हैं , वैसे ही चिन्तन भी मन का धर्म है । इसलिए मन में ही चित्त का अन्तर्भाव भले प्रकार से सिद्ध होता है ।।
बुद्धि में शरीर आदि के प्रति अत्यंत दृढ भाव / संस्कार दीखते हैं– ‘मैं दुःखी हूँ , मैं सुखी हूँ इत्यादि ‘ ; जिससे बुद्धि में अन्तर्भाव का मानना युक्त अहंकार प्रतीत होता है ।।
लिंग शरीर के लक्षण की सिद्धि के लिए मन में और बुद्धि में , क्रम से चित्त और अहंकार का अन्तर्भाव जानना चाहिए । इस तरह लिंग शरीर सत्तरह अवयवों वाला न होकर, उन्नीस अवयवों वाला हो जायेगा ।।
उपर्युक्त विवेचना से यह निश्चित रूप से सिद्ध होता है कि अहंभाव अर्थात कर्तापना बुद्धि का अज्ञान है और करणपना मन का अज्ञान है । कर्तापना और करणपना — इन दोनों प्रकारों के अज्ञानों के वश में होने से जीव जन्म – मरणरूप संसार-चक्र में फंसा रहता है ।।
यहाँ यह स्पष्ट भी करना उचित होगा कि इस अध्याय के वर्णित सांख्य योग कपिल या पतंजलि के योग सूक्त का नही है। यहां प्रज्ञा के अध्यास को वर्णित किया गया है कि किस प्रकार मनुष्य यह जानते हुए भी जन्म-जीवन- मरण प्रकृति के निरूपित हिस्से का होते हुए भी, इस अज्ञान की प्रज्ञा के साथ जीता है। अर्जुन का प्राथमिक मोह अपने स्वजनों की ले कर जो उत्पन्न हुआ था, वह इसी अज्ञान का ही एक हिस्सा है।
कृष्ण ने अर्जुन की अब तक दी हुई सब युक्तियों को प्रज्ञावाद का झूठा रूप कहा। उनकी युक्ति यह है कि प्रज्ञा दर्शन काल, कर्म और स्वभाव से होने वाले संसार की सब घटनाओं और स्थितियों को अनिवार्य रूप से स्वीकार करता है। जीना और मरना, जन्म लेना और बढ़ना, विषयों का आना और जाना। सुख और दुख का अनुभव, ये तो संसार में होते ही हैं, इसी को प्राचीन आचार्य पर्यायवाद का नाम भी देते थे। काल की चक्रगति इन सब स्थितियों को लाती है और ले जाती है। जीवन के इस स्वभाव को जान लेने पर फिर शोक नहीं होता। यही भगवान का व्यंग्य है कि प्रज्ञा के दृष्टिकोण को मानते हुए भी अर्जुन इस प्रकार के मोह में क्यों पड़ गया है।
ऊपर के दृष्टिकोण का एक आवश्यक अंग जीवन की नित्यता और शरीर की अनित्यता था। नित्य जीव के लिए शोक करना उतना ही व्यर्थ है जितना अनित्य शरीर को बचाने की चिंता। ये दोनों अपरिहार्य हैं। जन्म और मृत्यु बारी बारी से होते ही हैं, ऐसा समझकर शोक करना उचित नहीं है।
फिर एक दूसरा दृष्टिकोण स्वधर्म का है। जन्म से ही प्रकृति ने सब के लिए एक धर्म नियत कर दिया है। उस में जीवन का मार्ग, इच्छाओं की परिधि, कर्म की शक्ति सभी कुछ आ जाता है। इस से निकल कर नहीं भागा जा सकता। कोई भागे भी तो प्रकृत्ति उसे फिर खींच लाती है।
इस प्रकार काल का परिवर्तन या परिमाण, जीव की नित्यता और अपना स्वधर्म या स्वभाव जिन युक्तियों से भगवान्, ने अर्जुन को समझाया है उसे उन्होंने सांख्य की बुद्धि कहा है। इससे आगे अर्जुन के प्रश्न न करने पर भी उन्होंने योगमार्ग की बुद्धि का भी वर्णन किया। यह बुद्धि कर्म या प्रवृत्ति मार्ग के आग्रह की बुद्धि है इसमें कर्म करते हुए कर्म के फल की आसक्ति से अपने को बचाना आवश्यक है। कर्मयोगी के लिए सबसे बड़ा डर यही है कि वह फल की इच्छा के दल दल में फँस जाता है; उससे उसे बचना चाहिए।
अर्जुन को संदेह हुआ कि क्या इस प्रकार की बुद्धि प्राप्त करना संभव है। व्यक्ति कर्म करे और फल न चाहे तो उसकी क्या स्थिति होगी, यह एक व्यावहारिक शंका थी। उसने पूछा कि इस प्रकार का दृढ़ प्रज्ञावाला व्यक्ति जीवन का व्यवहार कैसे करता है? आना, जाना, खाना, पीना, कर्म करना, उनमें लिप्त होकर भी निर्लेप कैसे रहा जा सकता है? कृष्ण ने कितने ही प्रकार के बाह्य इंद्रियों की अपेक्षा मन के संयम की व्याख्या की है। काम, क्रोध, भय, राग, द्वेष के द्वारा मन का सौम्यभाव बिगड़ जाता है और इंद्रियाँ वश में नहीं रहतीं। इंद्रियजय ही सबसे बड़ी आत्मजय है। बाहर से कोई विषयों को छोड़ भी दे तो भी भीतर का मन नहीं मानता। विषयों का स्वाद जब मन से जाता है, तभी मन प्रफुल्लित, शांत और सुखी होता है। समुद्र में नदियाँ आकर मिलती हैं पर वह अपनी मर्यादा नहीं छोड़ता। ऐसे ही संसार में रहते हुए, उसके व्यवहारों को स्वीकारते हुए, अनेक कामनाओं का प्रवेश मन में होता रहता है। किंतु उनसे जिस का मन अपनी मर्यादा नहीं खोता उसे ही शांति मिलती हैं। इसे प्राचीन अध्यात्म परिभाषा में गीता में ब्राह्मीस्थिति कहा है।
क्योंकि अब हम गीता के योगशास्त्र में प्रवेश ले रहे है, इसलिए विषय को किस प्रकार ग्रहण करते है, महत्वपूर्ण है। प्रकृति भी ज्ञान देती है और जीव का अपना भी अध्यास होता है, जिस से वह प्रकृति से उत्पन्न ज्ञान के अज्ञान को समझ कर भ्रमित न हो। शास्त्र में इसे रस्सी को सर्प न समझने की भूल कहा गया है। अतः अब आगे पढ़ते है।
।। हरि ॐ तत सत ।। विशेष 2.10 ।।
Complied by: CA R K Ganeriwala ( +91 9422310075)