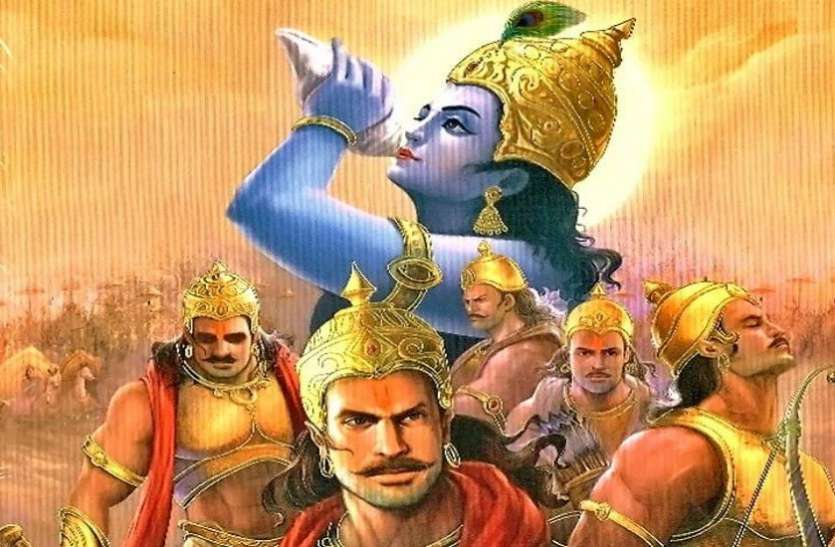।। Shrimadbhagwad Geeta ।। A Practical Approach ।।
।। श्रीमद्भगवत गीता ।। एक व्यवहारिक सोच ।।
।। Chapter 08.11 II
।। अध्याय 08.11 II
॥ श्रीमद्भगवद्गीता ॥ 8.11॥
यदक्षरं वेदविदो वदन्ति विशन्ति यद्यतयो वीतरागाः ।
यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण प्रवक्ष्ये॥
“yad akṣaraḿ veda-vido vadanti
viśanti yad yatayo vīta-rāgāḥ
yad icchanto brahmacaryaḿ caranti
tat te padaḿ sańgraheṇa pravakṣye”
भावार्थ:
वेदों के ज्ञाता जिसे अविनाशी कहते है तथा बडे़-बडे़ मुनि-सन्यासी जिसमें प्रवेश पाते है, उस परम-पद को पाने की इच्छा से जो मनुष्य ब्रह्मचर्य-व्रत का पालन करते हैं, उस विधि को तुझे संक्षेप में बतलाता हूँ। (११)
Meaning:
That which is declared imperishable by the knowers of the Vedas, that which dispassionate sages enter, that whose desire leads them to engage in the study of brahman; for you, I shall speak of that goal, in summary.
Explanation:
Having spoken of the technique of meditating upon Ishvara’s form, Shri Krishna now begins the topic of meditating upon Ishvara’s name. This shloka is written in the style of the Upanishads, and just like the previous shloka, is in a different meter.
Before the actual technique of meditation is described, Shri Krishna highlights the qualifications of the seeker who is about to perform this meditation. He should be free of selfish desires, likes and dislikes, indicated by the word “veetaraagaahaa”. We have already encountered this word under the topic of karma yoga. Strong passions or dislikes become obstacles in meditation as they push the mind to jump from one thought to the other. Only one who has managed to control the mind can perform such meditation.
The seeker should also possess a strong desire to inquire into the knowledge of the eternal essence, indicated by the word “brahmachaari”. The typical meaning of this word, celibacy, is not used here. It is used to indicate one who “moves around” or is preoccupied with the study of brahman or the eternal essence. Most of us, however, are preoccupied with actions. We are “karmachaaris”. Preoccupation with action will also become an obstacle in meditation, as we have already seen in the sixth chapter.
Shree Krishna mentions in this verse the word sangraheṇa, which means “in brief.” He says that this path is very difficult to follow and not suitable for everyone. Therefore, He will not elaborate much and briefly describe this path of yog-miśhrā bhakti; that leads to attaining the formless aspect of God. It demands living a life of rigid continence and perform severe austerities. Renouncing worldly desires and practicing brahmacharya, a vow of celibacy. As was previously detailed in verse 6.14, the practice of celibacy conserves a person’s physical energy. This energy, when channelized through sadhana, gets transformed into spiritual energy. It also enhances the intellect and memory power of the sādhaks (spiritual aspirants) and helps them comprehend the spiritual subjects better.
Endowed with these qualifications, the seeker is ready to meditate upon that which is considered as the ultimate goal: the imperishable Ishvara or “aksharam”. What is the process by which one can perform this meditation? This is taken up in the next two shlokas.
।। हिंदी समीक्षा ।।
भगवान द्वारा अर्जुन के सातवें प्रश्न का उत्तर देते हुए पूर्ण ब्रह्म के ज्ञान देने के अपने वचन को आगे बढ़ाते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते है।
अब मैं उस पद अक्षर अर्थात ॐकार के विषय मे संक्षेप में बताता हूँ। यह पद समस्त वेदों को जानने वाले, अविरत साधना करने वाले और अंत मे उसे प्राप्त करने वाले ज्ञानी महात्मा वेदविद लोग जिस को अक्षर निर्गुणनिराकार कहते हैं जिस का कभी नाश नहीं होता जो सदासर्वदा एकरूप एकरस अविनाशी रहता है और जिस को इसी अध्याय के तीसरे श्लोक में अक्षरं ब्रह्म परमम् कहा गया है उसी निर्गुणनिराकार तत्त्व का यहाँ अक्षर नाम से वर्णन हुआ है। यह ध्यान देने योग्य बात है कि गीता में प्रणव अक्षर के लिये ॐ शब्द का प्रयोग नही किया किन्तु वेद एवं उपनिषद में प्रणव अक्षर ॐ को ही माना गया है। हो सकता है प्रणव अक्षर भी वर्णमाला का अक्षर होने से परमात्मा ने अविनाशी नही भी माना हो, और उन के मन मे कुछ और अर्थ हो, किन्तु उपनिषद एवम वेदों को आधार मानते हुए हम इसे ॐ ही मानते हुए आगे बढ़ते है।
वीतरागी योगी पुरुष अभेद भाव से जिस में प्रवेश कर के पूर्णब्रह्म को प्राप्त होते है और जिस को प्राप्त करने के लिये योगी पुरुष ब्रह्मचर्य का पालन करता है।
पहले भी बताया गया था कि ब्रह्मचर्य का वास्तविक अर्थ ब्रह्म में या ब्रह्म के मार्ग में संचरण करना है। ब्रह्मचर्य का प्रधान तत्व बिंदु का सरंक्षण एवम संशोधन। अपने वीर्य को उर्धगामी रखना ऊर्ध्वरेता नैष्ठिक ब्रह्मचर्य है एवम मन, वचन एवम कर्म से मैथुन का त्याग निम्न स्तर का ब्रह्मचर्य है।
ध्यान साधना में पूर्ण सफलता प्राप्त करने के लिए मन की योग्यता अत्यावश्यक होती है। इस योग्यता के सम्पादन के लिए प्रायः सभी उपनिषदों में प्रणवोपासना(ओंकारोपासना) का अनेक स्थानों पर उपदेश दिया गया है। पौराणिक युग से इस उपासना का स्थान श्रद्धा भक्ति पूर्वक किये जाने वाले ईश्वर के साकार रूप या अवतारों के ध्यान पूजा आदि ने ले लिया है। इस प्रकार के ध्यान का प्रयोजन और उपयोगिता वही है जो वैदिक उपासनाओं की है।
अचल चित्त और ह्रदय से भक्ति भाव होने पर जो निर्विचार की निर्मलता में अध्यात्म की निर्मलता आने लगती है। यही अध्यात्म (प्रज्ञा) की निर्मलता में उसे प्रकृति पर्यंत समस्त पदार्थ शीशे की तरह साफ दिखने लगते है, इस प्रज्ञा को ऋतम्भरा प्रज्ञा भी कहते है, क्योंकि यह सत्य को धारण करती है। इस मे कोई भी भ्रांति नही रहती।
जो प्रज्ञा आगम और अनुमान पर आधारित होती है, वह सत्य प्रज्ञा नही कही जा सकती क्योंकि यह किसी अन्य के अनुभव और ज्ञान पर आधारित होती है। अतः ऋतम्भरा प्रज्ञा की स्थिति अचल मन और ह्रदय से परमात्मा के स्मरण से प्राप्त होगी। इस के जिस ब्रह्मचर्य का पालन करना है, वह निष्काम भाव और रागद्वेष से मुक्त हो कर कर्तव्य धर्म के पालन करने से ही प्राप्त होगा।
यहाँ साधक को अनेक प्रकार के प्रतिबन्धों की सूचनाओं और आवश्यक सावधानियों का निर्देश दिया गया है जिससे उसकी आध्यात्मिक तीर्थयात्रा अधिक सरल और आनन्दप्रद हो सके। साधारणतः जिन विघ्नों की शिकायत साधक करते हैं वे सब विघ्न अनात्म उपाधियों से हुए तादात्म्य के कारण ही आते हैं। इन उपाधियों के तादात्म्य से मन को परावृत्त करने में वह स्वयं को असमर्थ पाता है।
आत्मोन्नति के शास्त्र के रूप में वेदान्त के लिए आवश्यक है कि यह साधक को ध्यान की विधि बताने के साथ साथ सम्भावित विघ्नों का भी संकेत देकर उनसे सुरक्षित रहने के उपायों का भी वर्णन करे। यदि साधक को इनका सम्पूर्ण ज्ञान हो तो शीघ्र ही वह अपनी सुरक्षा कर सकता है। यह श्लोक यह इंगित करता है कि आत्मसंयम और वैराग्य के द्वारा किस प्रकार इस मार्ग पर सुखपूर्वक अग्रसर हुआ जा सकता है।
संसार मे रहने वाले हम जैसे लोगो के लिये यह कुछ अव्यवहारिक एवम सन्यासी धर्म के जैसा ज्ञान हो सकता है किंतु वास्तव में जीव को स्वयं का पूर्ण ज्ञान होने से इस संसार मे कर्मयोगी बन कर अपने जीने का मकसद मिल सकता है। स्वेच्छा से असहाय, गरीब एवम कष्ट में पड़े लोगो की सेवा में अपना सम्पूर्ण जीवन व्यतीत करदेने वाला भले ही परिवार, धन, पद या सम्मान को प्राप्त न करता हो किन्तु उस का आत्मबल वीतरागी की भांति सांसारिक कार्यो में दिनरात जुटे लोगो से अधिक होता है। बिना इस ज्ञान के अंत समय मोक्ष प्राप्त करना दुष्कर ही है।
हर व्यक्ति अपने अंदर कुछ न कुछ कमी महसूस करता ही रहता है किंतु जिस के पा लेने से कुछ भी कमी न रहे एवम जीवन की ढलान की अवस्था मे उसे यह कमी कुछ ज्यादा महसूस होती है। कभी कभी अपने होने का उद्देश्य या कारण भी जानने की इच्छा प्रबल होती है। कभी कभी तो यह भी लगता है कि पता नही क्या करने आये थे और क्या कर रहे है। इसलिये यह ज्ञान पूर्ण ब्रह्मतत्व आत्मबल को पूर्णता के साथ कर्मयोग में सही दिशा में जीने के आज भी सांसारिक जीवन के लिये आवश्यक है।
अतः जिस परब्रह्म के ज्ञान विषय में हम आगे पढ़ने जा रहे, वह समस्त कामना और आसक्ति को त्यागने वाला वीतरागी एवम ब्रह्मचर्य के तप से तपा हुआ सन्यासी अक्षर ब्रह्म के नाम से जानते है, अर्थात सन्यास मार्ग में परब्रह्म के ज्ञान को कर्मयोगी द्वारा किस प्रकार से जाना जा सकता है, जिस से युद्ध भूमि में खड़े अर्जुन को सन्यास मार्ग ही श्रेष्ठ है, इस भ्रम का भी निवारण हो जाए।
उस निर्गुणनिराकार तत्त्व की प्राप्ति की फल सहित विधि हम आगे पढ़ते हैं।
।।हरि ॐ तत सत।।08.11।।
Complied by: CA R K Ganeriwala ( +91 9422310075)