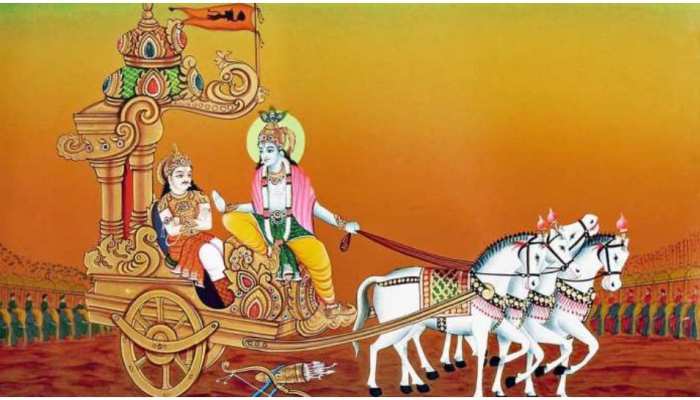।। Shrimadbhagwad Geeta ।। A Practical Approach ।।
।। श्रीमद्भगवत गीता ।। एक व्यवहारिक सोच ।।
।। Chapter 07. 02 ।I Additional II
।। अध्याय 07. 02 ।। विशेष II
।। ज्ञान -विज्ञान उपासना और जीव एवम प्रकृति।। विशेष 07.02 ।।
1 – ज्ञान – विज्ञान उपासना
ईश्वर का कथन है कि ज्ञान- विज्ञान से तृप्त हुआ योगयुक्त पुरुष समस्त प्राणियों में परमेश्वर को एवम परमेश्वर में समस्त प्राणियों को देखता है। अतः मन एवम इंद्रियाओ के निग्रह की विधि के पश्चात ज्ञान एवम विज्ञान किसे कहते है, जानना भी जरूरी है।
सृष्टि में अनेक प्रकार के अनेक विनाशवान पदार्थो में एक ही अविनाशी परमेश्वर समा रहा है- यह समझ लेना ही ज्ञान है एवम एक ही नित्य परमेश्वर से विविध नाशवान पदार्थो की उत्पत्ति को समझ लेना ही विज्ञान है।
ज्ञान-विज्ञान के इसी ज्ञान को क्षर-अक्षर का ज्ञान भी कहा गया है तथा अपने शरीर मे जिसे क्षेत्र माना गया है उस मे आत्मा का कहा है, उस के सच्चे स्वरूप को जानना भी परमेश्वर के स्वरूप का बोध करवाता है जिस को क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ एवम विचार भी कहते है।
परमेश्वर का पूर्ण ज्ञान हो कर कर्मो को न छोड़ते हुए भी कर्मयोग मार्ग की किन विधियों से अंत मे निःसंदिग्ध मोक्ष मिलता है, परमेश्वर के उस स्वरूप के ज्ञान को इस सातवे अध्याय से सत्तरवें अध्याय के अंत पर्यंत ग्यारह अध्यायों में हम इस विषय को पढेंगे।
परमेश्वर एक ही है, तथापि उपासना की दृष्टि से उस मे दो भेद होते है, उस का अव्यक्त स्वरूप केवल बुद्धि से ग्रहण करने योग्य है और व्यक्त स्वरूप प्रत्यक्ष अवगम्य है। अतः इन दोनों मार्गो या विधियों को इसी निरूपण में परमेश्वर ने अर्जुन को बताया कि बुद्धि से परमेश्वर को कैसे पहचाने और श्रद्धा या भक्ति से व्यक्त स्वरूप की उपासना करने से उन के द्वारा अव्यक्त का ज्ञान कैसे होता है, इस के विवेचन में ग्यारह अध्याय लग गए तो भी आश्चर्य नही होना चाहिए।
परमेश्वर के ज्ञान से ही इंद्रियाओ एवम मन का निग्रह भी हो जाता है। कुछ विद्वान मीमांसक गीता के इन ग्यारह अध्याय में भक्ति योग को देखते है क्योंकि यह भक्ति भाव से ही ज्ञान मार्ग का विवेचन है। किन्तु गीता की पृष्ठ भूमि एवम अर्जुन जैसे कर्मयोगी को भगवान ने सन्यास धारण करने को कभी नही कहते हुए समय एवम स्थान के अनुसार कर्तव्य धर्म का पालन करने को कहा। युद्ध भूमि में उसे युद्ध करने को कहना वो भी योगयुक्त कर्म योगी की भांति यह ही बताता है, भक्ति योग परमात्मा को पूर्ण रूप से जानना भी कर्मयोगी के परम आवश्यक है जिस से वो मन एवम इंद्रियाओ का निग्रह कर के निष्काम भाव से कर्म करता रहे।
विपर्यय का अर्थ हम मिथ्या ज्ञान से लेते है, अर्थात जिस ज्ञान को हम जो पंच इन्द्रियों से देखते, सुनते, सूंघते, रस लेते है या स्पर्श करते है उस से वस्तु का वास्तविक ज्ञान का न होना विपर्यय है। जैसे रस्सी को सर्प समझना। पांच इन्द्रियों द्वारा जो भी अनुमान, प्रत्यक्ष या आगम किया जाता है, आत्मा उसी के अनुसार देखती या समझती है। यह ही वृति कहलाती है। वृतियां राग-द्वेष उत्पन्न करने वाली क्लिष्ट या राग-द्वेष नाश करने वाली अक्लिष्ट होती है। अक्लिष्ट वृतियां संस्कारो एवम वैराग्य से उत्पन्न होती है। वृति प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निंद्रा एवम स्मृति पांच प्रकार की होती है।
जो हम पांच इन्द्रियों से देखते, सुनते, सूंघते, स्पर्श करते या रस लेते है उस से जो प्रमाण होता है, वह बोध कहलाता है। बोध सही हो तो प्रमा और सही अर्थात यथार्थ से भिन्न हो तो अप्रमा कहलाता है।
प्रत्यक्ष प्रमा वह है जो पंच इन्द्रियों से प्राप्त होता है। जब किसी चिन्ह या वस्तु से अनुमान लगा कर कोई बोध लिया जाए तो वह अनुमिति कहलाता है।
जब कोई पुस्तक पढ़ कर, प्रवचन या चित्र देख कर वृति प्राप्त की जाए उसे आगम प्रमाण कहते है।
वेद, शास्त्र, पुराण हमारे आगम प्रमाण है क्योंकि इन्हें उन व्यक्तियों द्वारा दिया गया है जिन्होंने प्रत्यक्ष प्रमाण प्राप्त किया है। आगम प्रमाण रखने और कहने का अधिकार उसे ही है जो प्रत्यक्ष प्रमाण का अधिकारी हो। अर्थात जिस ने ज्ञान को प्राप्त किया है वही ज्ञान देने का अधिकारी है।
आज कल व्हाट्सएप्प या किसी सूचना माध्यम से जो ज्ञान कोई भी प्रसारित कर देता है वह भ्रमित ज्ञान है क्योंकि जब तक भेजने वाला उस का प्रत्यक्ष प्रमाण नही प्राप्त करता, वह भ्रमित ज्ञान के प्रसारण का अपराध ही करता है।
वृतियां जब क्लिष्ट हो तो व्यक्ति में अहंकार, लोभ, ईर्ष्या आदि दुर्गुण होते है। साथ मे उस समय जो भी ज्ञान-विज्ञान वह पढ़ता, समझता, देखता है वह उस की क्लिष्ट वृत्तियों के अनुसार ही होगा। इसलिये पूजा पाठ, यज्ञ, दान आदि सांसारिक सुखों एवम स्वर्ग के ज्यादा किये जाते और मुक्ति और मोक्ष के नगण्य। अतृप्त वासना, कामना एवम रज-तम वृति होने से ध्यान का उद्देश्य सिद्धियां प्राप्त करना या सत्ता हासिल करना रहता है। पुराणों में क्लिष्ट वृति के राक्षस लोग ध्यान आदि कर के अपनी तमोवृति की शक्तियां ही प्राप्त करते थे।
वृत्तियों को अक्लिष्ट बनाने के लिये संस्कार, वैराग्य का उत्पन्न होना आवश्यक है। इस ले लिए सतत अभ्यास, यम- नियम – श्रद्धा, स्मृति, ध्यान, प्रज्ञा आदि अंतरंग एवम बहिरंग शुद्धिकरण सतत अभ्यास से प्राप्त करते है। यही मन, इन्द्रिय एवम बुद्धि का आत्मा के साथ एकत्व एवम समतत्व भाव है। इसलिए कुछ विद्वान इन अध्यायों को भक्ति मार्ग में रख कर विवेचना करते है। जब मार्ग योग का हो तो श्रद्धा, प्रेम, विश्वास और संशयहीन हो कर ही ज्ञान प्राप्त हो सकता है। इसलिए सन्यास, कर्म, ध्यान या बुद्धि और भक्ति सभी मार्ग आगे चल कर ज्ञान मार्ग में मिल जाते है। जब हम अध्याय 7 से 12 पढ़ रहे है तो हमे यह भी ध्यान रखना होगा कि इस से पूर्व के 6 अध्याय के अनुसार हम अपनी वृत्तियों को उत्तम करे, जिस से वास्तविक ज्ञान की प्राप्ति हो।
चित्त की वृतियां सात्विक ही होती है, जिस से करुणा, दया, परोपकार आदि की ओर मन कर्म करने को अग्रसर होता है, किन्तु रज गुण का प्रभाव उस को कर्म करने से कामना, मोह, लोभ और आसक्ति से रोकता है और यदि तमो गुण का प्रभाव हो जाये तो आलस्य और निंद्रा हमे घेर लेती है। इसलिये जब भी यह गुण हमे कर्म करते महसूस हो तो हमे तुरंत समझ जाना चाहिये कि हमारे अंदर रज या तम गुण का प्रभाव बढ़ रहा है।
2 जीव और प्रकृति
चिदानंद स्वरूप ब्रह्म के प्रतिबिंब से युक्त तम, रज तथा सत्व गुण एक वस्तु “प्रकृति” कहलाती है। यह दो प्रकार की होती है।
सत्व गुण की शुद्धि से उस प्रकृति को “माया” और सत्व गुण की अशुद्धि (मलिनता) से उस प्रकृति को अविद्या मान लिया गया है। माया में पड़ा हुआ बिम्ब उस माया को वश में कर रहा है और इस कारण से वह सर्वज्ञ ईश्वर बना बैठा है।
प्रकाशात्मक सत्व गुण की शुद्धि से जब कि सत्व गुण दूसरे गुणों से कलुषित नही हो जाता – तब वह प्रकृति “माया” कहीं जाती है। जब तो वह सत्व गुण दूसरे गुणों से कलुपित हो कर अशुद्ध हो जाता है, तब वही प्रकृति अविद्या कहाने लगती है। संक्षेप यह है कि विशुद्ध सत्व प्रधान प्रकृति को माया तथा मलिन सत्व प्रधान प्रकृति को अविद्या कहते है। माया में प्रतिफलित उस आत्मा ने माया को अपने स्वाधीन कर रखा है और वही सर्वज्ञता आदि गुणों वाला ईश्वर हो गया है।
दूसरा तो अविद्या के वश में फस जाता है। अविद्या की विचित्रता के कारण वह अनेक हो जाता है। उस अविद्या को “कारण शरीर” कहते है। इस कारण शरीर कहानेवाली अविद्या में अभिमान करने वाले को “प्राज्ञ” मानते है।
अविद्या में प्रतिबिंबित हो कर उस के पराधीन हो जाने वाला आत्मा तो जीव कहाने लगता है। वह जीव तो उस अविद्या रूपी उपाधि की विचित्रता (किंवा अशुद्धि की न्यूनाधिकता) के कारण अनेक प्रकार का हो जाता है। उस के देवता, मनुष्य, पशु, पक्षी आदि अनेक भेद हो जाते है। वह अविद्या ही कारण शरीर कहाती हैं, क्योंकि स्थूल, सूक्ष्म शरीर तथा स्थूल सूक्ष्म भूतों का वही कारण मानी गई है। उस कारण शरीर में अभिमान करने अथवा उसी में “मैं” भावना करने वाले जीव को प्राज्ञ नाम से कहा जाता है।
उन प्राज्ञों के भोग के लिए ईश्वर की आज्ञा से तम प्रधान प्रकृति में से आकाश, वायु, अग्नि, जल तथा भूमि नाम के पांच महाभूत उत्पन्न हुए।
उन प्राज्ञ नामक जीवों के सुख – दुख – साक्षात्कार रूपी भोग के लिए उस प्रकृति में से ( जिस में तमों गुण की प्रधानता है) ईशान आदि शक्ति वाले जगत के अधिष्ठाता की से ( जिस को उस का ईक्षण भी कहा जाता है) आकाश आदि पांच भूत उत्पन्न हो गए।
उन आकाश आदि पांच भूतों के पृथक पृथक पांच सत्व भागों से क्रमानुसार श्रोत्र, त्वचा, चक्षु, रसना तथा घ्राण नाम की पांच ज्ञानेद्रिया उत्पन्न हो जाती है। अर्थात एक एक भूत के पृथक पृथक सत्वांश से एक एक इंद्रिय की उत्पत्ति होती है।
उन पांचों भूतों के पांचों सत्वांशों से मिल कर एक अन्त: करण नाम का द्रव्य उत्पन्न हो जाता है। वह अन्त:करण अपने वृतिभेद के कारण दो प्रकार का होता है। जब वह विमर्श किंवा संश्यात्मिका वृति करता है अथवा यों कहो कि जब वह विमर्श रूप हो जाता है तब उस को मन कहा जाता है। निश्चय स्वरूप हो जाने पर उसी को बुद्धि नाम से कहने लगते है।
उन आकाश आदि पांचों भूतों के पृथक पृथक पांच रजो भागों से क्रमानुसार वाक, पाणि, पाद, पायु तथा उपस्थ नाम की पांच कर्मेंद्रियां उत्पन्न हो जाती है।
उन पांचों भूतों के पांचों रजो भागों से मिल कर एक प्राण का जन्म हो जाता है। वह प्राण वृति भेद किंवा प्राणनादि व्यापारों के भेद से, पांच प्रकार का होता है। ये पांच प्रकार ये है – प्राण, अपान, समान, उदान तथा व्यान।
पांच ज्ञानेद्रियां, पांच कर्मेंद्रियां, पांच प्राण, मन तथा बुद्धि इन सत्रह पदार्थों से मिल कर सूक्ष्म शरीर बनता है। उसी को वेदांतो में लिंग शरीर भी कहते है।
वह प्राज्ञ नाम का जीव उस लिंग शरीर में अभिमान करने से तैजस हो जाता है तथा जब वह ईश्वर उस लिंग देह में अभिमान करता है तब वह “हिरण्यगर्भ” हो जाता है। उन दोनों में भेद केवल इतना ही है कि तैजस “व्यष्टि” है और हिरण्यगर्भ “समष्टि” है। इस के अतिरिक्त और कोई भेद नहीं है।
मलिनसत्व प्रधान अविद्या रूपी उपाधि वाला जीव जब लिंग शरीर में अभिमान करता है, जब वह उसी को अपना आत्मा मान लेता है, तब उसे तैजस कहने लगते है। विशुद्ध सत्व प्रधान माया रूपी उपाधिवाला परमेश्वर उसी लिंग शरीर में जब “मैपने” का अभिमान करता है तब उस का नाम हिरण्यगर्भ हो जाता है। तैजस और हिरण्यगर्भ दोनो ही यद्यपि लिंग शरीर पर अभिमान करने वाले है परंतु उन में से एक व्यष्टी और दूसरा समष्टि है। इसी से दोनो में भेद हो गया है।
वह ईश्वर – हिरण्यगर्भ कहा गया है – लिंग शरीर उपाधि वाले सभी तैजसो के साथ अपने आत्मा की एकता को समझता रहता है। वह समझता है कि ये सब मिल कर मैं हूं। इसी से वह समष्टि होता है। उस ईश्वर से अन्य जो जीव है वे तो उस तादात्म्य वेदन के अभाव से ( उन सब के साथ एकत्व ज्ञान के न होने से ) व्यष्टि नाम से कहे जाते है।
भगवान परमेश्वर उस के बाद उन जीवों के भोग के लिए ही भोग्य ( अन्नपान आदि) तथा भोग मंदिरों ( जरायुज आदि चार प्रकार के शरीरों की उत्पत्ति करने के लिए, आकाश आदि पांच महाभूतों में से प्रत्येक भूत को ( जो कि अभी तक अपंचात्मक ही थे) पंचात्मक कर देता है। ( जिस से कि उन से जीवो के भोग के लिए भोग्य अन्नपान आदि तथा भोग्य मंदिर शरीर का निर्माण हो सके।
आकाशादि प्रत्येक भूत के पहले दो दो भाग किए जाए। फिर उन में के पहले एक भाग ले तो चार चार भाग किए जाए (तथा दूसरे आधे भागों को पूरा रखा आए) उस के पश्चात अपने अपने से भिन्न दूसरे दूसरे भागों के साथ योग करने से ये पांचों भूत पंचीकृत हो जाते है।
उस पंचीकृतं भूतों से ब्रह्मांड की उत्पत्ति होती है। ब्रह्मांड में भुवन, प्राणियों के भोगने योग्य भोग्य पदार्थ तथा उन उन लोकों के अनुकूल शरीर (ईश्वर की आज्ञा से) उत्पन्न हो जाते है। इस सम्पूर्ण स्थूल (विराट) शरीर में अहम भाव से बैठने वाला हिरण्यगर्भ वैश्वानर कहाने लगता है।
इस स्थूल शरीर में आते ही तैजस विश्व हो जाते है। जिनको देव, तिर्यंग तथा मनुष्य आदि कहा जाने लगता है। वे सभी बहिर्मुख हैं। इन किसी को भी आत्मतत्व का बोध नहीं है।
इस स्थूल शरीर में अहंभाव से निवास करने वाले तैजस ही विश्व कहाने लगते है। देवता, पशु, पक्षी तथा मनुष्यादि भेद इन विश्व के ही होते है। तैजसो में इस तरह का कोई भेद नहीं होता। कारण शरीर और लिंग शरीर तो सब प्राणियों का एक समान ही होता है। इन के केवल स्थूल शरीर ही भिन्न भिन्न प्रकार के होते है। वे देवादि सभी परागदर्शी (बाह्यदर्शी) है। ये बाह्य शब्द आदि विषयों को ही देख पाते है। अपने दुर्भाग्य के कारण ये प्रत्यागात्मा को नही देख पाते है। इन सभी को आत्मतत्व का यथार्थ ज्ञान नही होता। यद्यपि तार्किक आदि लोग देह से भिन्न आत्मा को पहचानते है परंतु श्रुति प्रतिपादित असंग आत्मरूप का यथार्थ ज्ञान उन को भी नही है।
इसी प्रकार जब किन्ही के पूर्व उपार्जित कोटि पुण्य कर्मों का परिपाक होता है तब वे प्राणी किसी तत्वदर्शी आचार्य से उपदेश (श्रवण) को पा कर ( आगे बतायी विधि से) पांच कोशों का विवेक कर लेने पर, परानिर्वृति (मोक्ष सुख) को पा लेते है।
अन्न, प्राण, मन, बुद्धि (विज्ञान) तथा आनंद ये पांच कोश कहाते है। ( इन को कोश कहने का कारण यह है कि) इन कोशो से आच्छादित हुआ अपना आत्मा, अपने स्वरूप को भूल जाने से कारण , जन्म मरण रूपी संसार में फंस जाता है। कोश (बंदा) जैसे कोश बनाने वाले कीड़े के क्लेश का कारण होता है अथवा जैसे कोश (म्यान) के अंदर रखी हुई तलवार का रूप छिप जाता है, इसीप्रकार इन अन्नादि कोशो ने, अद्वयानंद आत्म तत्व को ढक दिया है और आत्मा को क्लेश पहुंचा रखा है इसी से इस को कोश कहा जाता है।
पंचीकृत भूतों से उत्पन्न हुआ यह स्थूल देह अन्नमय कोश कहाता है। लिंग शरीर में के राजस ( रजोगुण से बने हुए) पांच प्राणों से तथा वागादी कर्मेद्रियो से मिलकर प्राणमय कोश हो जाता है
विमर्श आत्मा मन तथा सात्विक ज्ञानेद्रियां मिल कर मनोमय कोश कहाते है। उन्ही ज्ञानेद्रियों के साथ मिली हुई निश्चयात्मिका बुद्धि विज्ञानमय कोश कही जाती है।
कारण शरीर में मोदादि वृत्तियों के साथ रहने वाले (मालिन) सत्व को आनंदमय कोश कहते है। यह हमारा आत्मा उन उन कोशो के साथ तादात्म्य कर लेने से तत्तन्मय ( उन उन के रूप का) सा हो जाता है।
कारण शरीर कहानेवाली अविद्या में जो कि मालिन सत्व रहता है, वह जब उन उन प्रिय मोद तथा प्रमोद नाम की वृत्तियों से युक्त हो जाता है।( जो कि वृत्तियें क्रम से इष्ट पदार्थ के मिलने की आशा से, इष्ट पदार्थ के मिलने से तथा इष्ट पदार्थ भोगने से पैदा हुआ करती है) तब आनंदमय कोश कहाने लगता है।
वह आत्मा उस उस कोश के साथ जब तादात्म्याभिमान कर लेता है, तब उस उस कोशमय सा हो जाता है। परंतु असल में तो वह उन उन कोशो से अत्यंत विलक्षण ही रहता है।
अन्वयव्यतिरेक नाम की युक्ति से, या तो पांच कोशो को आत्मा से पृथक पहचान कर या आत्मा को उन पांच कोशो में से पृथक पहचान कर अपने आत्मा को उन में से बाहर कर के परब्रह्म ही हो जाता है।
अन्वय व्यतिरेक नाम की विभिन्न युक्तियों से पांच कोशो का विवेक कर लेने पर ( उन को आत्मा से पृथक कर लेने पर) अथवा आत्मा को ही उन में से पृथक कर लेने पर, बुद्धि की सहायता से अपने आत्मा को उन कोशो में से बाहर निकाल कर, अपने चिदानंद स्वरूप का निश्चय कर के अधिकारी पुरुष परब्रह्म को प्राप्त हो जाता है, किंवा स्वयं परब्रह्म ही हो जाता है।
उपरोक्त शब्दावली का उद्देश्य भगवान श्री कृष्ण द्वारा ज्ञान को समझने के लिये स्वयं को कितना परिपक्क होना होगा, यही जानने हेतु बताया गया है। जिसे हम विस्तार से आगे के अध्याय में पढ़ेंगे।
इन उपरोक्त बातों को मनन करते हुए हम सातवे अध्याय का पठन जारी करते है।
।। हरि ॐ तत सत।। विशेष 07.02 ।।
Complied by: CA R K Ganeriwala ( +91 9422310075)