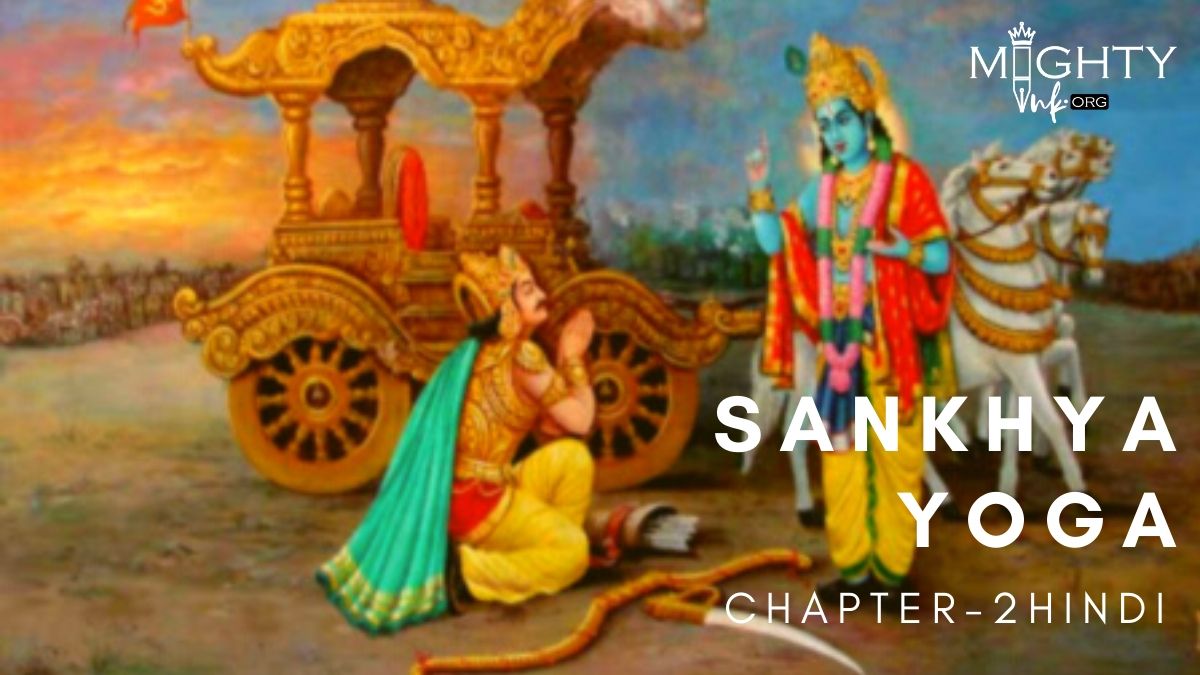।। Shrimadbhagwad Geeta ।। A Practical Approach ।।
।। श्रीमद्भगवत गीता ।। एक व्यवहारिक सोच ।।
।। Chapter 02. Preamble ।।
।। अध्याय 02. प्रस्तावना।।
।। PEAMBLE – Chapter Two –“ Contents of the Geeta Summerised “ “ Sankhay Yog”।।
In this chapter, Arjun reiterates to Shree Krishna that he is unable to cope with his current situation, where he has to kill his elders and teachers. He refuses to take part in such a battle and requests Shree Krishna to be his spiritual teacher and guide him on the proper path of action.
Then the Supreme Lord starts imparting divine knowledge to Arjun. He begins with the immortal-nature of the soul, which is eternal and imperishable. Death only destroys the physical body, but the soul continues its journey. Just as a person discards his old clothes and adorns new ones, the soul keeps changing bodies from one lifetime to another.
The first stage is discovery of the problem of Samsara. That I have the Samsara-disease consisting of ragaḥ, sokah and mohaḥ – and this has to be experienced and recognised. And even after recognising the problem, a person tries to solve the problem by himself or herself and generally what we do is: we do not understand the problem is with us and therefore we tend to blame the external factors for our problem And since we consider the external world is the cause of our problem, we try to adjust or change the external condition. A poor man thinks, that it is the poverty which is the cause. An unmarried person thinks that it is the ‘unmarried’ness that is the making him unhappy. A married person thinks that it is the childless state that is the cause of the problem. Thus each one places the problem outside and goes on tampering and adjusting and after long struggle some rare intelligent ones discover the problem to be within themselves, not outside. From wrong decision coming to a doubt, is a great progress. Doubt is better or wrong decision is better, if you ask, I would say that doubt is better than wrong decision because, when a person has a doubt at least he will try to take the help of someone. Always our progress is like this; from wrong decision, to doubt, to knowledge, wrong decision to doubt to right decision.
The Lord then reminds Arjun that his social responsibility as a warrior is to fight for upholding righteousness. He explains that performing one’s social duty is a virtuous act that can take him to the celestial abodes, while dereliction only leads to infamy and humiliation.
At first, Shree Krishna tries to motivate Arjun at a mundane level. Then he moves deeper and starts explaining to Arjun the Science of Work. He asks Arjun to perform his deeds without any attachment to their fruits. This science of working without desire for rewards is called the yog of the intellect or buddhi-yog. He further advises that the intellect should be used to control the desire for rewards from work. By working with such intent, the bondage-creating karmas get transformed into bondage-breaking karmas and a state beyond sorrows can be attained.
Arjun is curious to know more about those who are situated in divine consciousness. Shree Krishna, therefore, describes how persons who have attained transcendence are free from attachment, fear, and anger. They are undisturbed and equipoised in every situation. With their senses subdued, they keep their minds always absorbed in God. He also explains the progression of afflictions of the mind—such as greed, anger, lust, etc. and advises how these can be overcome.
(Preamble – Courtesy – “The songs of GOD – Swami Mukundanandan”)
II प्रस्तावना – अध्याय– द्वितीय “ सांख्य योग” II
दूसरे अध्याय का नाम सांख्ययोग है। इस मे शोकयुक्त शरणागत अर्जुन द्वारा अपने शोक की निवृत्ति का एकांतिक उपाय पूछे जाने पर आत्म तत्व का वर्णन किया है। इस में जीवन की दो प्राचीन संमानित परंपराओं का तर्कों द्वारा वर्णन आया है। अर्जुन को उस कृपण स्थिति में रोते देखकर कृष्ण ने उस का ध्यान दिलाया है कि इस प्रकार का क्लैव्य और हृदय की क्षुद्र दुर्बलता अर्जुन जैसे वीर के लिए उचित नहीं। व्यक्ति को अपने कर्तव्य धर्म का पालन करना चाहिये। इस के लिये निष्काम कर्मयोग की व्याख्या सांख्य योग के साथ की गई है।
वैदिक दर्शनों में षड्दर्शन (छः दर्शन) अधिक प्रसिद्ध और प्राचीन हैं। ये सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा और वेदान्त के नाम से विदित है। इस की स्थापना करने वाले मूल व्यक्ति कपिल कहे जाते हैं। ‘सांख्य’ का शाब्दिक अर्थ है – ‘संख्या सम्बंधी’ या विश्लेषण। इस की सबसे प्रमुख धारणा सृष्टि के प्रकृति-पुरुष से बनी होने की है, यहाँ प्रकृति (यानि पंचमहाभूतों से बनी) जड़ है और पुरुष (यानि जीवात्मा) चेतन। योग शास्त्रों के ऊर्जा स्रोत (ईडा-पिंगला), शाक्तों के शिव-शक्ति के सिद्धांत इसके समानान्तर दीखते हैं। सांख्य योग को निष्काम कर्म योग के साथ सामंजस्य करते हुए भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उस के कर्तव्य धर्म का पालन क्यों करना चाहिए, बताते है।
कृष्ण ने अर्जुन की अब तक दी हुई सब युक्तियों को प्रज्ञावाद का झूठा रूप कहा। उन की युक्ति यह है कि प्रज्ञा दर्शन काल, कर्म और स्वभाव से होने वाले संसार की सब घटनाओं और स्थितियों को अनिवार्य रूप से स्वीकार करता है। जीना और मरना, जन्म लेना और बढ़ना, विषयों का आना और जाना। सुख और दुख का अनुभव, ये तो संसार में होते ही हैं, इसी को प्राचीन आचार्य पर्यायवाद का नाम भी देते थे। काल की चक्रगति इन सब स्थितियों को लाती है और ले जाती है। जीवन के इस स्वभाव को जान लेने पर फिर शोक नहीं होता। यही भगवान का व्यंग्य है कि प्रज्ञा के दृष्टिकोण को मानते हुए भी अर्जुन इस प्रकार के मोह में क्यों पड़ गया है।
ग्याहरवें श्लोक से भगवान श्री कृष्ण का उपदेश मुस्करा कर शुरू करते है, ऊपर के दृष्टिकोण का एक आवश्यक अंग जीवन की नित्यता और शरीर की अनित्यता था। नित्य जीव के लिए शोक करना उतना ही व्यर्थ है जितना अनित्य शरीर को बचाने की चिंता। ये दोनों अपरिहार्य हैं। जन्म और मृत्यु बारी बारी से होते ही हैं, ऐसा समझकर शोक करना उचित नहीं है।
फिर एक दूसरा दृष्टिकोण स्वधर्म का है। जन्म से ही प्रकृति ने सबके लिए एक धर्म नियत कर दिया है। उसमें जीवन का मार्ग, इच्छाओं की परिधि, कर्म की शक्ति सभी कुछ आ जाता है। इससे निकल कर नहीं भागा जा सकता। कोई भागे भी तो प्रकृत्ति उसे फिर खींच लाती है।
इस प्रकार काल का परिवर्तन या परिमाण, जीव की नित्यता और अपना स्वधर्म या स्वभाव जिन युक्तियों से भगवान्, ने अर्जुन को समझाया है उसे उन्होंने सांख्य की बुद्धि कहा है। इस से आगे अर्जुन के प्रश्न न करने पर भी उन्होंने योगमार्ग की बुद्धि का भी वर्णन किया। यह बुद्धि कर्म या प्रवृत्ति मार्ग के आग्रह की बुद्धि है इस में कर्म करते हुए कर्म के फल की आसक्ति से अपने को बचाना आवश्यक है। कर्मयोगी के लिए सब से बड़ा डर यही है कि वह फल की इच्छा के दल दल में फँस जाता है; उस से उसे बचना चाहिए। अर्जुन को समभाव का फल अनामय पद की प्राप्ति बतलाते हुए, उसे समबुद्धि युक्त कर्मयोगी होने को कहा है।
अर्जुन को संदेह हुआ कि क्या इस प्रकार की बुद्धि प्राप्त करना संभव है। व्यक्ति कर्म करे और फल न चाहे तो उस की क्या स्थिति होगी, यह एक व्यावहारिक शंका थी। उसने पूछा कि इस प्रकार का दृढ़ प्रज्ञावाला व्यक्ति जीवन का व्यवहार कैसे करता है? आना, जाना, खाना, पीना, कर्म करना, उनमें लिप्त होकर भी निर्लेप कैसे रहा जा सकता है? कृष्ण ने कितने ही प्रकार के बाह्य इंद्रियों की अपेक्षा मन के संयम की व्याख्या की है। काम, क्रोध, भय, राग, द्वेष के द्वारा मन का सौम्यभाव बिगड़ जाता है और इंद्रियाँ वश में नहीं रहतीं। इंद्रियजय ही सबसे बड़ी आत्मजय है। बाहर से कोई विषयों को छोड़ भी दे तो भी भीतर का मन नहीं मानता। विषयों का स्वाद जब मन से जाता है, तभी मन प्रफुल्लित, शांत और सुखी होता है। समुद्र में नदियाँ आकर मिलती हैं पर वह अपनी मर्यादा नहीं छोड़ता। ऐसे ही संसार में रहते हुए, उसके व्यवहारों को स्वीकारते हुए, अनेक कामनाओं का प्रवेश मन में होता रहता है। किंतु उन से जिस का मन अपनी मर्यादा नहीं खोता उसे ही शांति मिलती हैं। इसे प्राचीन अध्यात्म परिभाषा में गीता में ब्राह्मीस्थिति कहा है। यह जड़ प्रश्न कि जब तक फल की इच्छा न हो, व्यक्ति कर्म क्यों और किस लिये करे, गीता में विस्तृत रूप से बताया है, जिस का प्रथम उपदेश अध्याय दो से शुरू होता है।
हमे यह भी ध्यान रखना चाहिये कि गीता में युद्ध भूमि महाभारत के विभिन्न पात्रों में गीता केवल अर्जुन ने सुनी, संजय ने सुन कर धृतराष्ट्र को सुनाई और बबरीक ने सुनी। इन सब के अतिरिक्त सभी अभिज्ञ दर्शक मात्र थे। समय, स्थान एवम विभिन्न पात्रों में यह ही पात्र गीता को क्यों जान सके, इस का विश्लेषण भी हम आगे पढ़ते है।
यह अध्याय वस्तुतः गीता है समस्त अध्यायों का सार भी है, जिस के प्रत्येक वचन और शब्दों को अर्जुन की शंका के माध्यम से आगे विस्तार से समझाया गया है।
गीता को त्रयषष्ठी अर्थात गीता के 18 अध्यायों को छह – छह अध्याय के तीन भागों में बांटा गया है जिस का आधार “तत् त्वम् असि” है। इस को विस्तार में आगे हम पढ़ेंगे। प्रथम छह अध्याय “त्वम” अर्थात जीव को भ्रम से मुक्त हो कर स्वयं को जानने के है। गीता वेदांत के सिद्धांतो का प्रतिपालन करते हुए, सांख्य के नियम को वेदांत के विरुद्ध नही है, स्वीकार करती है एवम वेदांत को भी परिकृषत करती है।
अतः अब आगे अध्ययन शुरू करते है।
।। हरि ॐ तत सत – प्रस्तावना।। अध्याय 2 ।।
Complied by: CA R K Ganeriwala ( +91 9422310075)