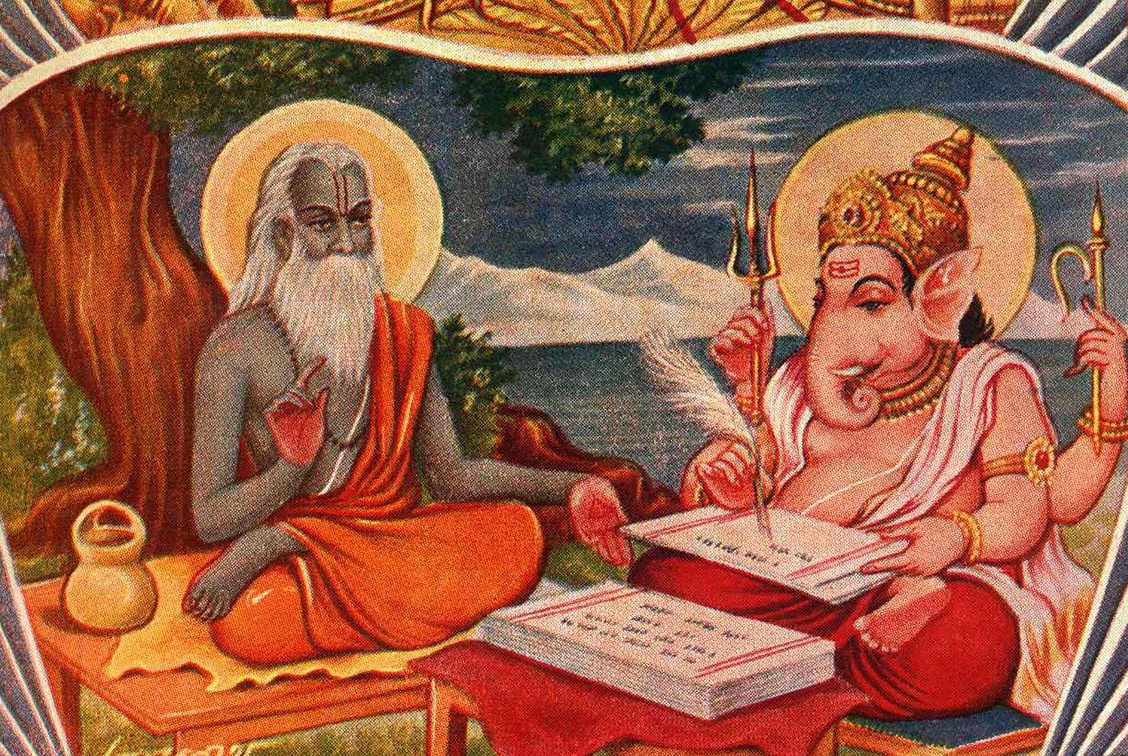।। Shrimadbhagwad Geeta ।। A Practical Approach ।।
।। श्रीमद्भगवत गीता ।। एक व्यवहारिक सोच ।।
।। Chapter 04.30।।
।। अध्याय 04.30 ।।
॥ श्रीमद्भगवद्गीता ॥ 4.30॥
अपरे नियताहाराः प्राणान्प्राणेषु जुह्वति ।
सर्वेऽप्येते यज्ञविदो यज्ञक्षपितकल्मषाः॥
“apare niyatāhārāḥ,
prāṇān prāṇeṣu juhvati..।
sarve ‘py ete yajña-vido,
yajña-kṣapita-kalmaṣāḥ”..।।
भावार्थ :
कुछ मनुष्य भोजन को कम करके प्राण-वायु को प्राण-वायु में ही हवन किया करते हैं, ये सभी यज्ञ करने वाले यज्ञों का अर्थ जानने के कारण सभी पाप-कर्मों से मुक्त हो जाते हैं। (३०)
Meaning:
Others regulate their diet, offering the life force into the life force. All these (seekers) destroy sin through sacrifice, who are the knowers of sacrifice.
Explanation:
In an earlier shloka, Shri Krishna spoke about the yajnya of regulating the quality of sensory intake. In this shloka, he describes a yajnya where one not only controls the quality of sensory intake but also the quantity. Although this is applicable to all senses such as smell, taste, sight and so on, let us consider one which is the simplest to understand: taste. Dieting becomes a form of yajnya.
By controlling or regulating the intake of food, we can control our mind. Our body and mind is ultimately made up of the food we consume.
The digestive systems gets healthy and once the digestive system is mastered, then praṇa, apana, vyana, udana, all these five praṇas are disciplined by ahara niyama. Ahara niyama comes in two stages; the first is quantity control; then comes quality control. Gradually getting rid of tamasic food; gradually cutting rajasic food and thereafterwards making satvika ahara. More we read in chapter 16 and 17.
Shri Krishna describes different types of food. For now, let us consider three main types. Saatvic food is that which is conducive to mind, which creates harmony in our system. Raajasic food makes us more active. It is usually spicy to taste. Taamasic food makes us dull, sleepy and sometimes intoxicated as well. It is food that has lost all its nutritional value, and is usually stale. It is also known as junk food.
On a subtler level, food also acquires the characteristics of how it has been prepared. At some level, we can always tell whether the food we eat has been mass produced, or has been made with care and attention. That is why many serious students of meditation will usually prepare their own food.
So therefore, Shri Krishna says here that we can perform yajnya by restricting our sensory intake. Now, let’s look at the deeper meaning of this shloka. By regulating the intake of our senses, we reduce our dependence on the senses and in doing so, offer them senses back to the universe. In parallel, our life forces also do not need to work hard in order to digest and process all this sensory “food” that we consume. Therefore, we also offer our life force back to the universal or cosmic life force. In other words, we say “Here, please take these senses and life force back. It is your property to begin with. It is not mine.”
Mental discipline; praṇayama; like this, he gave 12 spiritual disciplines, of which self-knowledge is also one of the sadanas. Krishna indicates that they all must involve Iśvara; even regular eating can become yajnah, if you are going to offer the food to the Lord and eat. That is condition No.1. And the second condition is all of them can be called spiritual sadanas, only when the motive is spiritual growth. upavasaḥ is day in which I reduce all my all other sensory transactions, so that the time saved by avoiding those sensory transactions I can use for the religious practice, like parayaṇam, japa or anything. In other case all are exercises for routine work of daily life in nature.
।। हिंदी समीक्षा।।
कुछ ऐसे साधक होते हैं जो आहार संयम के द्वारा कामक्रोधादि से उत्पन्न मन की उत्तेजनाओं को संयमित करने का अभ्यास करते हैं। भारत में आहार संयम की विधि अपरिचित और नई नहीं है। प्राचीन ऋषियों को अन्न के पोषक तत्त्वों के विषय में पूर्ण ज्ञान था। इतना ही नहीं बल्कि उन्होंने समाज के विभिन्न स्तर के व्यक्तियों के स्वभाव एवं कार्यों के लिए उपयुक्त शाकसब्जियों तथा धान्यों का भी वैज्ञानिक पद्धति से वर्गीकरण किया था। केवल विचार ही नहीं वरन् उन्होंने प्रयोग करके यह दर्शाया भी था कि आहार संयम के द्वारा किस प्रकार मनुष्य अपने गुणों तथा व्यवहार को परिष्कृत करके सांस्कृतिक उन्नति कर सकता है तथा अन्य कितने ही नियताहारी अर्थात् जिनका आहार नियमित किया हुआ है ऐसे परिमित भोजन करने वाले प्राणों को यानी वायु के भिन्न भिन्न भेदों को प्राणों में ही हवन किया करते हैं। भाव यह है कि वे जिस जिस वायु को जीत लेते हैं उसी में वायु के दूसरे भेदों को हवन कर देते हैं यानी वे सब वायु भेद उस में विलीन से हो जाते हैं। ये सभी पुरुष यज्ञों को जाननेवाले और यज्ञों द्वारा निष्पाप हो गये होते हैं अर्थात् उपर्युक्त यज्ञों द्वारा जिन के सब पाप नष्ट हो गये हैं वे यज्ञक्षपितकल्मष कहलाते हैं।
प्राण का स्थान हृदय तथा अपान का स्थान गूदा है। श्वांस को बाहर निकलते समय वायु की गति ऊपर की ओर तथा श्वास को भीतर ले जाते समय वायु की गति नीचे की ओर होती है इसलिए श्वास को बाहर निकालना प्राण का कार्य और श्वास को भीतर ले जाना अपान का कार्य। अपान वायु में प्राण वायु का हवन (पूरक प्राणायाम) इस में बाहर की वायु को भीतर रोका जाता है। प्राणवायु का अपान वायु में हवन (रेचक प्राणायाम) इस में भीतर की वायु को बाहर निकाल कर रोका जाता है तथा बाहर भीतर को भेद कर नही कर के, समस्त वायु भेदों को, प्राण – अपान सहित अपने अपने स्थानों में ही रोक देना अर्थात प्राण अपान की गति को रोक कर, प्राणों का प्राणों में हवन कुंभक या स्तंभ वृति प्राणायाम करना है।
प्राणायाम अर्थात प्राणों का आयाम, प्राण गति का नियमन है। मन का नियमन करने के लिए, प्राणायाम बहुत लाभदायक है, इस से मन – बुद्धि के संकल्प – विकल्प खत्म हो कर, मन स्थिर होने लगता है और अंत: करण में शुद्धि होने लगती है।
योगी का आहार, आसन एवम निंद्रा दृढ़ होना चाहिए। आहार की प्रकृति के तीन गुणों की भांति सात्विक, राजसी एवम तामसी बांट सकते है। सात्विक आहार से आप के विचार एवम क्रियाए नियंत्रित रहेंगी।
यज्ञविद शब्द से तात्पर्य उन साधकों से है जो उपर्युक्त साधनों को समझ कर उनमें से सभी अथवा कुछ साधनों का ही अभ्यास निस्वार्थ भावना से करते हैं। ऐसे ही लोग इनसे लाभान्वित होंगे। यहां ध्यान देने योग्य बात यह है कि इस श्लोक में स्पष्ट कहा गया है कि यज्ञ के द्वारा मनुष्य पापमुक्त होगा और न कि इनसे सीधे ही परमात्मा की प्राप्ति होगी। देहादि अनात्म पदार्थों के साथ तादात्म्य से उत्पन्न अहम का देह तथा बाह्य विषयों में आसक्त हुआ अनेक प्रकार के संकल्प करता रहता है। इन संकल्पों के अनुरूप ही कर्म और फलोपभोग से वासनायें उत्पन्न होती हैं जो सदैव मनुष्य को विषयों में प्रवृत्त करती हैं। यही पाप है जो मनुष्य को पशु के स्तर तक गिरा देता है। उपर्युक्त यज्ञों के अनुष्ठान से न केवल विद्यमान वासनायें नष्ट होती हैं वरन् नवीन विनाशकारी वासनायें भी नहीं उत्पन्न होती।संक्षेप में निष्कर्ष निकलता है कि ये समस्त यज्ञ साध्य न होकर अन्तकरण की शुद्धि के साधनमात्र हैं। चित्त शुद्ध होने पर निदिध्यासन के अभ्यास से ही परमात्मा की प्राप्ति होती है। अनेक साधक लोग अज्ञानवश किसी एक विशेष साधना में ही इतना आसक्त हो जाते हैं कि उनकी आगे की प्रगति अवरुद्ध हो जाती है।इन सभी यज्ञों में पुरुषार्थ अर्थात् स्वयं का प्रयत्न अत्यन्त आवश्यक है।
आहार के विषय में अध्याय 16 और 17 में भी बताया गया है। अभी हम इतना याद रखे कि शारीरिक विज्ञान की दृष्टि में भी आहार हमारे शरीर, मन और बुद्धि के विकास पर पूरा पड़ता है। अध्यात्म में जीव और प्रकृति के स्वरूप को अन्नमय कोश भी माना गया है। यज्ञ के विभिन्न स्वरूपों का वर्णन ज्ञान, तप, अग्नि, प्राण आदि का वर्णन करने के बाद, यज्ञ से क्या प्रभाव होता है, यह हम आगे पढ़ते है।
।। हरि ॐ तत सत।।4.30।।
Complied by: CA R K Ganeriwala ( +91 9422310075)