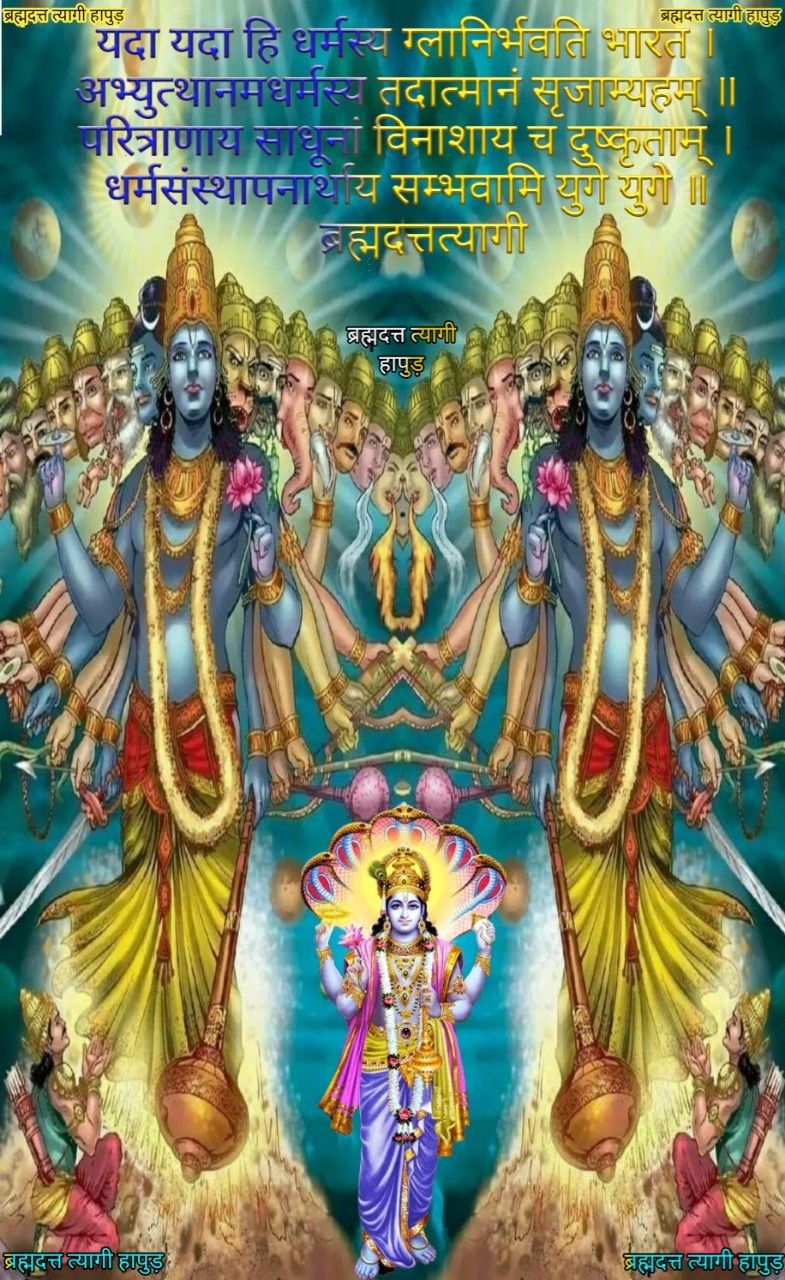।। Shrimadbhagwad Geeta ।। A Practical Approach ।।
।। श्रीमद्भगवत गीता ।। एक व्यवहारिक सोच ।।
।। Chapter 04.24।।
।। अध्याय 04.24 ।।
॥ श्रीमद्भगवद्गीता ॥ 4.24॥
ब्रह्मार्पणं ब्रह्म हविर्ब्रह्माग्रौ ब्रह्मणा हुतम् ।
ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्मकर्मसमाधिना॥
“brahmārpaṇaḿ brahma havir,
brahmāgnau brahmaṇā hutam..।
brahmaiva tena gantavyaḿ,
brahma-karma-samādhin”..।।
भावार्थ :
ब्रह्म-ज्ञान में स्थित उस मुक्त पुरूष का समर्पण ब्रह्म होता है, हवन की सामग्री भी ब्रह्म होती है, अग्नि भी ब्रह्म होती है, तथा ब्रह्म-रूपी अग्नि में ब्रह्म-रूपी कर्ता द्वारा जो हवन किया जाता है वह ब्रह्म ही होता है, जिसके कर्म ब्रह्म का स्पर्श करके ब्रह्म में विलीन हो चुके हैं ऎसे महापुरूष को प्राप्त होने योग्य फल भी ब्रह्म ही होता हैं। (२४)
Meaning:
Brahman is the oblation, brahman is the offering, brahman is the fire, brahman is the one who offers. One whose actions happen while absorbed in brahman, he only attains brahman.
Explanation:
Having given us a series of practical tips, Shri Krishna delivers yet another milestone shloka. If we truly perform all actions in this world with a an attitude of yajnya, not just some actions, our vision of the world changes. In this shloka, Shri Krishna uses the ritual of a yajnya to paint a picture of what this ultimate vision looks like. We begin to see brahman, the eternal essence, in everything.
Six components of a yajyna ritual are pointed out here. One who sees God everywhere and in all beings is the highest spiritualist.” For such advanced spiritualists whose minds are completely absorbed in God- consciousness, the person making the sacrifice, the object of the sacrifice, the instruments of the sacrifice, the sacrificial fire, and the act of sacrifice, are all perceived as non- different from God.
This example can be interpreted from several perspectives. Let’s first examine it from a purely physical perspective. The ladle is made of wood, which has come from the earth, and so has the offering. The person who performs the yajnya is created out of food, which also has come out of the earth. The flame and the act of yajnya are both manifestations of cosmic forces. Their ultimate cause can be traced back to the cosmic big bang. The goal has as a thought in the mind of the person, a mind that also has come from nature.
Now, how can we make it more concrete? Consider a computer programmer writing a software application. What should his vision become? The act of programming, the code he writes, the computer he uses to write the code, the software application that his code becomes a part of, his goal of writing good code, and the programmer himself – everything is the eternal essence. This is “brahma- drishti” or the vision of brahman that is achieved while interacting in this world.
Krishna had talked about jnanam as differentiating atma and anatma; Atma anatma vivekaḥ; dehi-deha vivekaḥ; and there we saw that every individual is a mixture of two principles, one is the consciousness principle and the other is the body principle. And we clearly differentiated the body and conscious, through those five points;
1. consciousness is not part, product or property of the body.
2. consciousness is an independent entity which pervades and enlivens the body;
3. consciousness is not limited by the boundaries of the body.
4. Consciousness survives even after the fall the body; and
5. that surviving consciousness cannot interact with the world because the body medium is not available.
Thus we have differentiated consciousness and body. And after claiming that I am consciousness, you have to use all these five points; replacing the word ‘consciousness’ by the word I. vedanta says this knowledge is incomplete; because in this knowledge, I say I- am- consciousness, everything else is matter; I am atma; everything else is anatma; and why do we say this knowledge is incomplete; you must be knowing the answer, the answer is still we are in dvaitam only.
I- am- consciousness is a big progress; but still there is a duality in the form of spirit and matter; cetana- acetanam; and therefore the next stage of vedanta is, knowing that there is no- matter- other- than- consciousness; matter is a myth; matter is non- substantial; even though it appears as tangible solid substance; matter does not have a substantiality of its own; the substance is what; consciousness, atma alone is the substance; matter does not exist separate from consciousness and what is that consciousness?; I- am- that- consciousness; and therefore what should be conclusion?; there is no material world separate from me, the observer.
Therefore, uttiṣṭataḥ jāgrataḥ prāpyavarān nibodhataḥ; Wake up, arise and awake. The Upaniṣads tells and addresses us: Wake Up, what does it mean; you think you are awake; but you are a somnambulist. You know what is somnambulism; walking in dream or walking in sleep; according to Upaniṣad, we are all somnambulist walking in dream only. Therefore Krishna wants to say that everything is nothing but atma; there is no anatma separate from ātma.
Krishna concludes the jnanam topic and this is a very important verse; a significant verse; a deep philosophical verse; important not because that you will get food only if you chant that; in some houses, brahmarpaṇaṁ you have to say before food. it is incidentally used
before food in some places; but it has got a deep philosophical sense.
।। हिंदी समीक्षा ।।
कोई आप को आप का परिचय देने लगे तो आप उसे यही कहेंगे कि मैं आप से ज्यादा अपने आप को जानता हूँ। किन्तु जब ब्रह्मसन्ध गुरु आप को आप से परिचय करवायेगा, कि तुम अपने को जिस स्वरूप में जानते हो, वह मिथ्या भ्रम है, तुम स्वयं परब्रह्म के अंश, इस समस्त प्रकृति से परे सत- चित्त- आनन्दस्वरूप हो, तो आप विश्वास नही कर पाएंगे। यही अज्ञान प्रकृति के साथ जीव के संबंध का है कि उसे अपने वास्तविक स्वरूप का ज्ञान नही है।
मान लीजिये आप समुन्द्र के किनारे खड़े है। एक लहर उठती है। एक आगे बढ़ती है। एक पीछे हटती है और एक नीचे गिरती है। किंतु आप इसे अलग अलग न जानते हुए सभी समुन्द्र ही है, जानते है। वैसे ही यह जीव है।
जीवन मे जिस दिन अहम समाप्त हो जाये तो शेष जो बचेगा वो ब्रह्म होगा। यज्ञ की समस्त क्रियाओं एवम कर्म प्रवृति में 6 कारक होते है। वे इस प्रकार है।
1- क्रिया का कर्ता
2- जिस पर क्रियारूप व्यवहार हो, वह कर्म
3- जिस साधन द्वारा क्रिया हो वो करण
4- जिस के लिए क्रिया की जाए वह सम्प्रदान
5- जहां से क्रिया की जाए वह अपादान
6-जिस में क्रिया की जाए वह अधिकरण
कर्म योगी की समस्त ब्रह्म स्वरूप कर्म की क्रिया एकत्व दृष्टि से ब्रह्मरूप ही होती है। इसलिये उस को ब्रह्मकर्म समाधि पुरुष कहा जाता है।
जिस पुरुष को इस का ज्ञान है, वह जानता है कि अव्यक्त (प्रकृति ) से लेकर स्थूलपर्यन्त, यह समस्त विश्व- ब्रह्माण्ड आभासमात्र प्रतीत होता है तथा जो आकाश के समान सूक्ष्म और अनादि- अनन्त है, वह अद्वय ब्रह्म मैं ही हूँ ।।
जो सब का आधार , सब वस्तुओं का प्रकाशक, सर्वरूप, सर्वव्यापी ,सबसे रहित नित्य, शुद्ध, निश्चल और निर्विकल्प अद्वैत ब्रह्म है, वही मैं हूँ ।।
जो माया के समस्त विकारों- भेदों से रहित है , जो अन्तरात्मा के रूप में अधिष्ठित है,जो बुद्धि -वृत्तियों के परे है; वह सत्य, ज्ञान, अनन्त आनन्दरूप अद्वितीयब्रह्म ही मेरा स्वरूप है।।
मैं निष्क्रिय हूँ , मैं निर्विकार- अपरिवर्तनीय हूँ, मैं पूर्ण-अंशरहित हूँ, मैं निराकार हूँ, मैं निर्विकल्प- नित्य- निरालम्ब अद्वितीय ब्रह्म हूँ ।।
मैं सब का आत्मस्वरूप हूँ, मैं सबकुछ हूँ मैं सब से परे हूँ, मैं, अद्वय हूँ, मैं शुद्ध अखण्ड चैतन्य-स्वरूप हूँ, मैं निरन्तर- आनन्दस्वरूप हूँ ।।
अतः चौबीसवे श्लोक का यह वर्णन ही तत्वदृष्टि से ठीक है, कि सृष्टि के सब पदार्थ में सदैव ही ब्रह्म भरा हुआ है। इस कारण इच्छा रहित बुद्धि से सब व्यवहार करते करते ब्रह्म से ही ब्रह्म का यजन यानि अर्पण होता रहता है। किये जानेवाले कर्म अपना कार्य आरम्भ किये बिना ही ( कुछ फल दिये बिना ही ) किस कारण से फलसहित विलीन हो जाते हैं इस पर कहते हैं ब्रह्मवेत्ता पुरुष जिस साधनद्वारा अग्नि में हवि अर्पण करता है उस साधन को ब्रह्मरूप ही देखा करता है अर्थात् आत्मा के सिवा उस का अभाव देखता है। जैसे ( सीप को जाननेवाला ) सीप में चाँदी का अभाव देखता है ब्रह्म ही अर्पण है इस पद से भी वही बात कही जाती है। अर्थात् जैसे यह समझता है कि जो चाँदी के रूप में दीख रही है वह सीप ही है। ( वैसे ही ब्रह्मवेत्ता भी समझता है कि जो अर्पण दिखता है वह ब्रह्म ही है ) ब्रह्म और अर्पण यह दोनों पद अलग अलग हैं। अभिप्राय यह कि संसार में जो अर्पण माने जाते हैं वे स्रुक् स्रुव आदि सब पदार्थ उस ब्रह्मवेत्ता की दृष्टि में ब्रह्म ही हैं। वैसे ही जो वस्तु हविरूप से मानी जाती है वह भी उस की दृष्टि में ब्रह्म ही होता है। ब्रह्माग्नौ यह पद समासयुक्त है। इसलिये यह अर्थ हुआ कि ब्रह्मरूप कर्ताद्वारा जिस में हवन किया जाता है वह अग्नि भी ब्रह्म ही है और वह कर्ता भी ब्रह्म ही है और जो उस के द्वारा हवनरूप क्रिया की जाती है वह भी ब्रह्म ही है। उस ब्रह्मकर्म में स्थित हुए पुरुष द्वारा प्राप्त करने योग्य जो फल है वह भी ब्रह्म ही है। अर्थात् ब्रह्मरूप कर्म में जिस के चित्त का समाधान हो चुका है उस पुरुष द्वारा प्राप्त किये जाने योग्य जो फल है वह भी ब्रह्म ही है। इस प्रकार लोकसंग्रह करना चाहनेवाले पुरुष द्वारा किये हुए कर्म भी ब्रह्मबुद्धि से बाधित होने के कारण अर्थात् फल उत्पन्न करने की शक्ति से रहित कर दिये जाने के कारण वास्तव में अकर्म ही हैं।
साक्षीभाव में रहनेवाला वह ब्रह्मज्ञ पुरुष, न तो इन्द्रियों को भोग्य विषयों में लगाता है और न ही दूर करता है ।आत्मानन्दरस में सदा आल्हादित रहनेवाला, वह कर्मफलों की अल्पमात्र भी अपेक्षा नहीं रखता ।।
मोक्ष न देह की मृत्यु का नाम है और न दण्ड-कमण्डलु के त्याग का, बल्कि हृदय (अन्तःकरण) की अविद्यारूपी ग्रन्थि के नाश को मोक्ष कहते हैं ।।
अतः ज्ञान से प्रकाशित आत्म स्वरूप ब्रह्म के अंश में जो अज्ञान भ्रमित कर के उस के अंदर फैल गया है, वह ही अज्ञान है। हमे ब्रह्मज्ञान की आवश्यकता नहीं क्योंकि हम तो स्वयं प्रकाशवान और परमब्रह्म के अंश है। हमे आवश्यकता अपने अज्ञान को हटाने की है। उपनिषदों में भी कहा है “उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान्निबोधत । क्षुरस्य धारा निशिता दुरत्यया दुर्गं पथस्तत्कवयो वदन्ति ।।” अर्थात जिसका अर्थ कुछ यूं हैः उठो, जागो, और जानकार श्रेष्ठ पुरुषों के सान्निध्य में ज्ञान प्राप्त करो । विद्वान् मनीषी जनों का कहना है कि ज्ञान प्राप्ति का मार्ग उसी प्रकार दुर्गम है जिस प्रकार छुरे के पैना किये गये धार पर चलना ।
(कठोपनिषद्, अध्याय १, वल्ली ३, मंत्र १४)
मैं ब्रह्म स्वरूप हूं, यह जानलेना या मान लेना ही प्रर्याप्त नही है क्योंकि मैं और ब्रह्म स्वरूप को जानकर भी जीव द्वैत के भाव में है, जहां ब्रह्म है वहां मैं भी नही, जो कुछ है वह ब्रह्म ही है, ब्रह्म के अतिरिक्त कुछ नही। द्वैत से अद्वैत को हम आगे पढ़ेंगे।
यज्ञ की दृष्टिकोण से अन्न ग्रहण करने से पूर्व भी इस श्लोक द्वारा ब्रह्म के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने इस श्लोक का पठन किया जाता रहा है। यह एक प्रसिद्ध श्लोक है जिस को भारत में भोजन प्रारम्भ करने के पूर्व पढ़ा जाता है किन्तु अधिकांश लोग न तो इस का अर्थ जानते हैं और न जानने का प्रयत्न ही करते हैं। तथापि इस का अर्थ गंभीर है और इस में सम्पूर्ण वेदान्त के सार को बता दिया गया है।वह अनन्त पारमार्थिक सत्य जो इस दृश्यमान नित्य परिवर्तनशील जगत् का अधिष्ठान है वेदान्त में ब्रह्म शब्द के द्वारा निर्देशित किया जाता है। यही ब्रह्म एक शरीर से परिच्छिन्नसा हुआ आत्मा कहलाता है। एक ही तत्त्व इन दो शब्दों से लक्षित किया है और वेदान्त केसरी की यह गर्जना है कि आत्मा ही ब्रह्म है।यज्ञ भावना से कर्म करते हुए ज्ञानी पुरुष की मन की स्थिति एवं अनुभूति का वर्णन इस श्लोक में किया गया है। उसके अनुभव की दृष्टि से एक पारमार्थिक सत्य ही विद्यमान है न कि अविद्या से उत्पन्न नामरूपमय यह जगत्। अत वह जानता है कि सभी यज्ञों की उत्पत्ति ब्रह्म से ही होती है जिन में देवता अग्नि हवि और यज्ञकर्ता सभी ब्रह्म हैं। यदि कोई व्यक्ति जगत् के असंख्य नामरूपों कर्मों और व्यवहारों में अंतर्बाह्य व्याप्त अधिष्ठान स्वरूप परमार्थ तत्त्व को देख सकता है तो फिर उसे सर्वत्र सभी परिस्थितियों में वस्तुओं और प्राणियों का दर्शन अनन्त आनन्द स्वरूप सत्य का ही स्मरण कराता है। संत पुरुष ब्रह्म का ही आह्वान करके प्रत्येक कर्म करता है इसलिये उसके सब कर्म लीन हो जाते हैं।भोजन के पूर्व इस श्लोक के पाठ का प्रयोजन अब स्वत स्पष्ट हो जाता है। शरीर धारण के लिये भोजन आवश्यक है और तीव्र क्षुधा लगने पर किसी भी प्रकार का अन्न स्वादिष्ट लगता है। इस प्रार्थना का भाव यह है कि भोजन के समय भी हमें सत्य का विस्मरण नहीं होना चाहिए। यह ध्यान रहे कि भोक्तारूप ब्रह्म ब्रह्म का आह्वान करके अन्नरूप ब्रह्म की आहुति उदर में स्थित अग्निरूप ब्रह्म को ही दे रहा है। इस ज्ञान का निरन्तर स्मरण रहने पर मनुष्य भोगों से ऊपर उठकर अपने अनन्त स्वरूप को प्राप्त कर लेता है।
यज्ञ की सर्वोच्च भावना को स्पष्ट करने के पश्चात् भगवान् अर्जुन को आगे समझाते हैं कि सम्यक् भावना के होने से किस प्रकार प्रत्येक कर्म यज्ञ बन जाता है।
।।हरि ॐ तत सत।। 4.24।।
Complied by: CA R K Ganeriwala ( +91 9422310075)